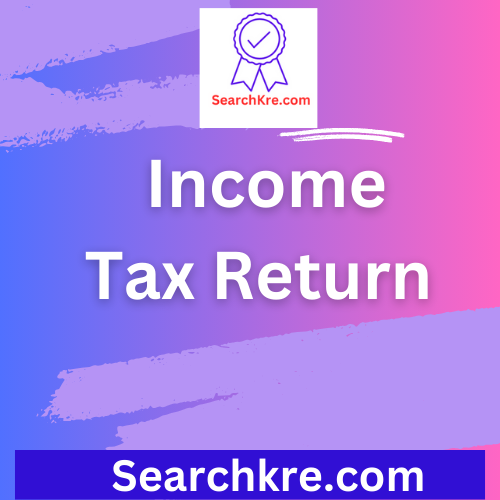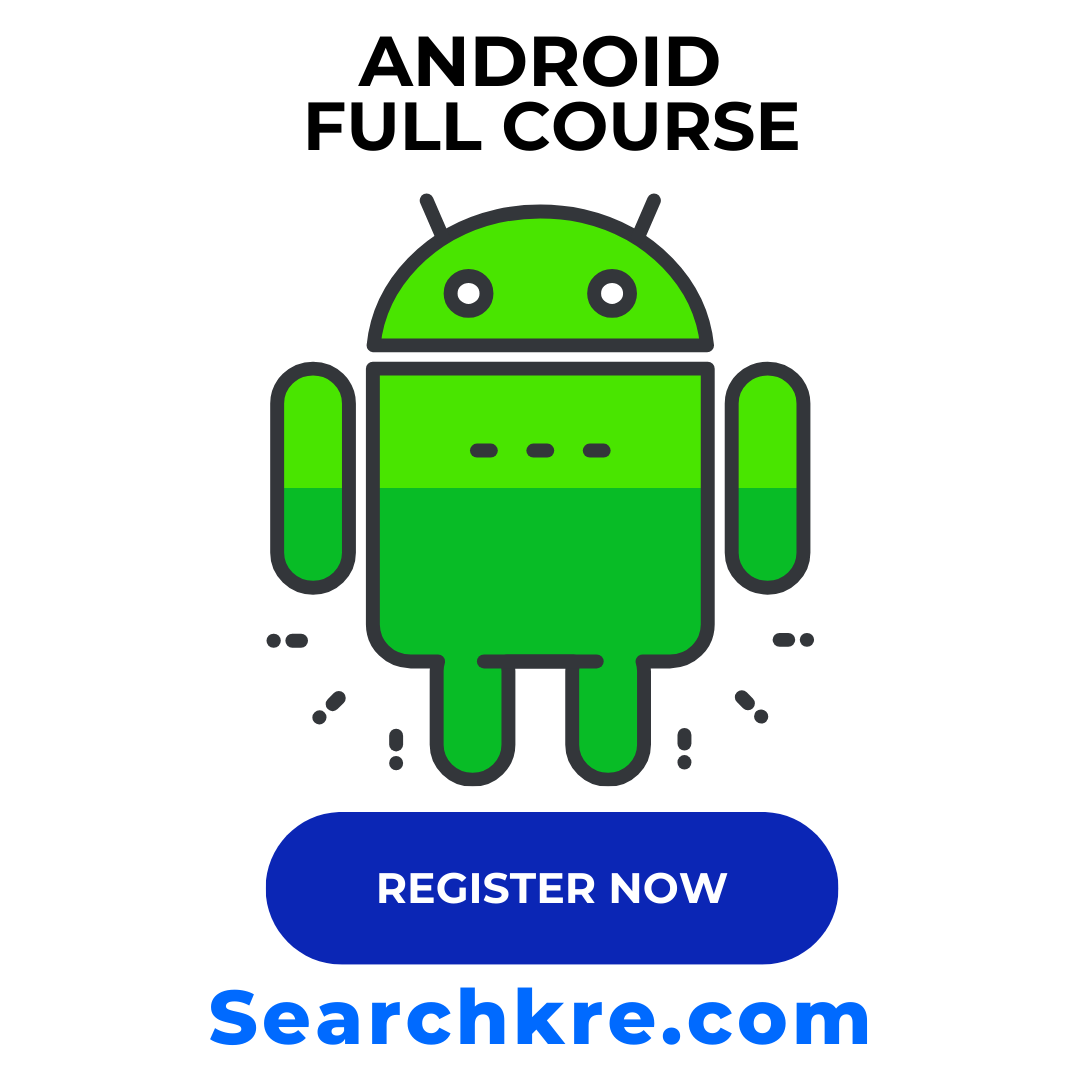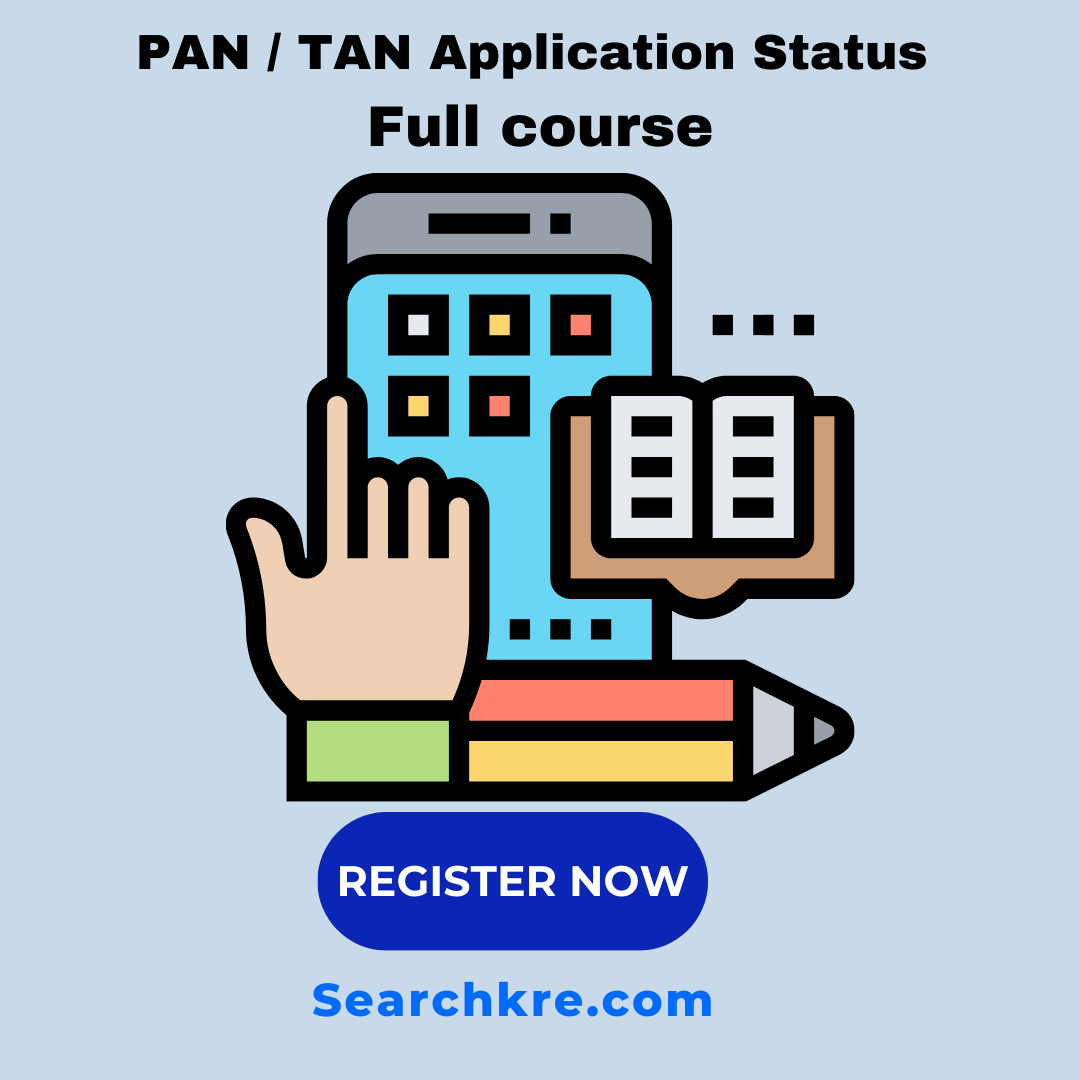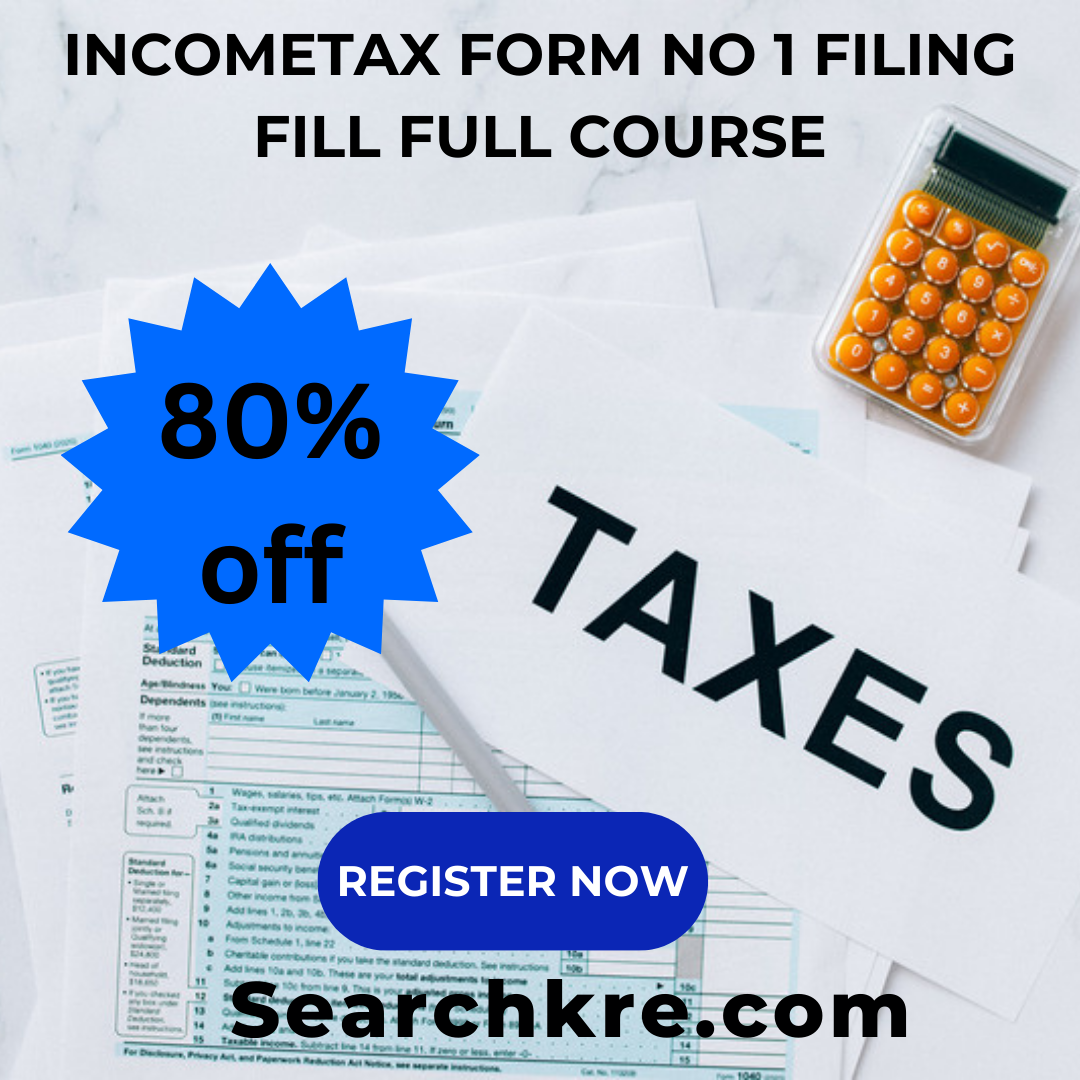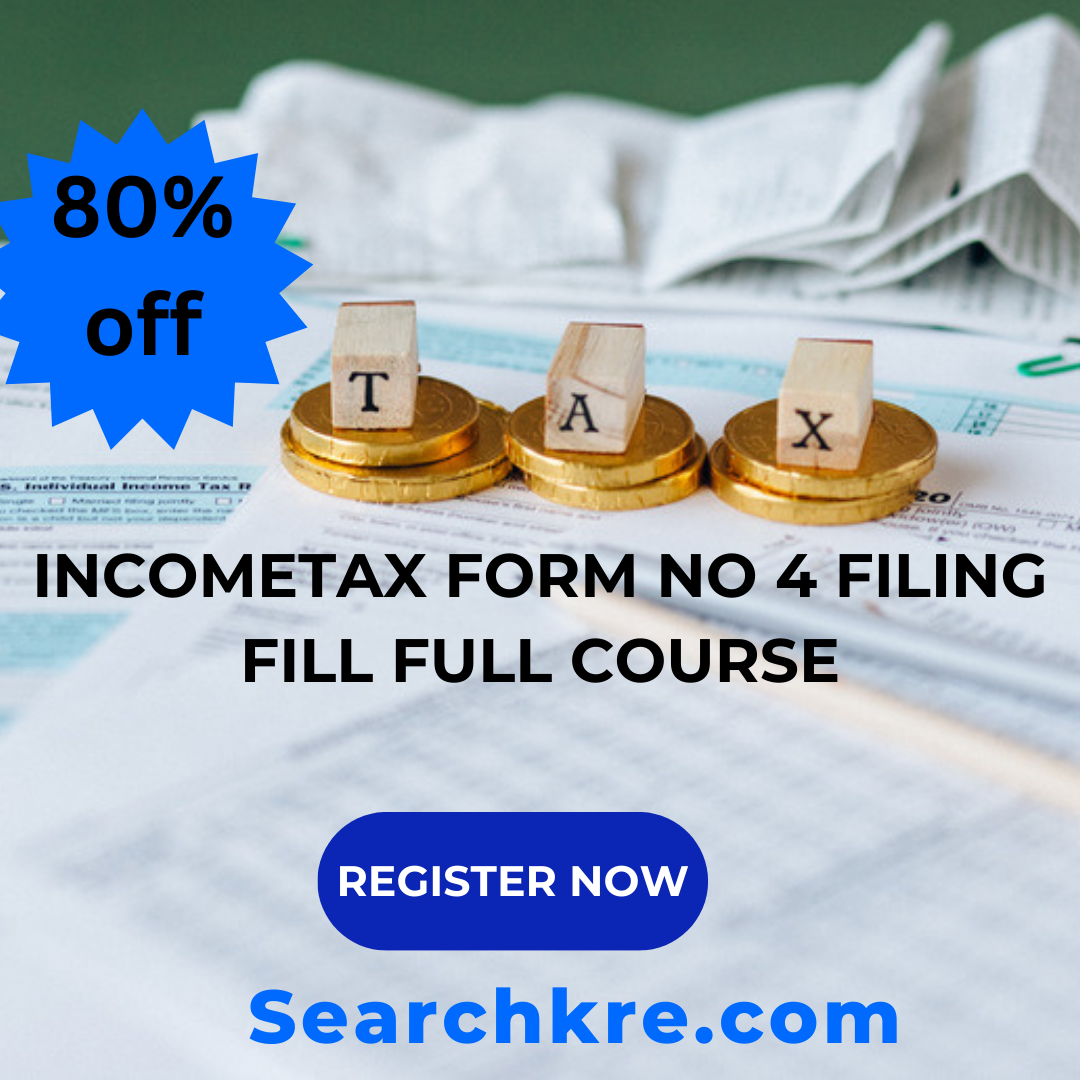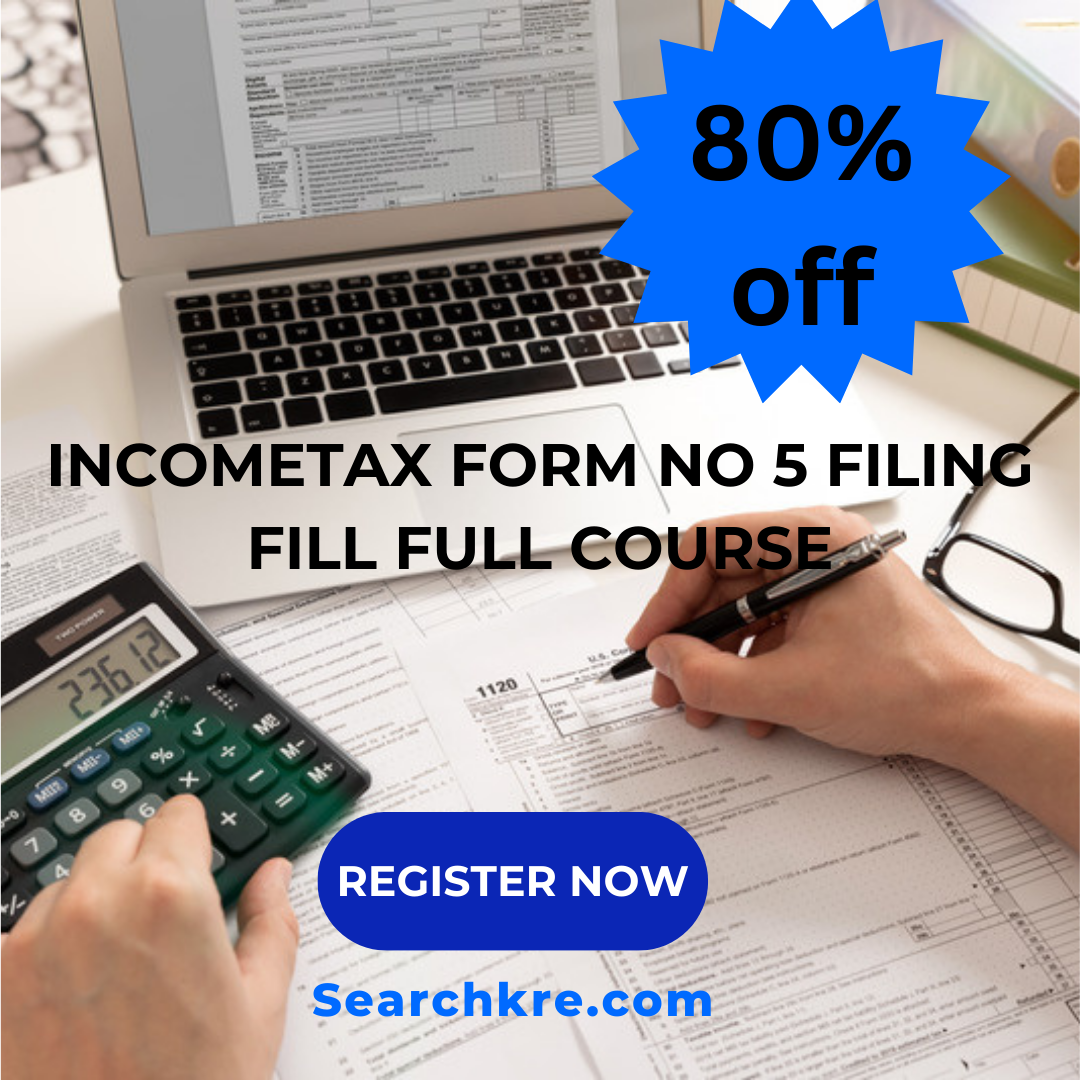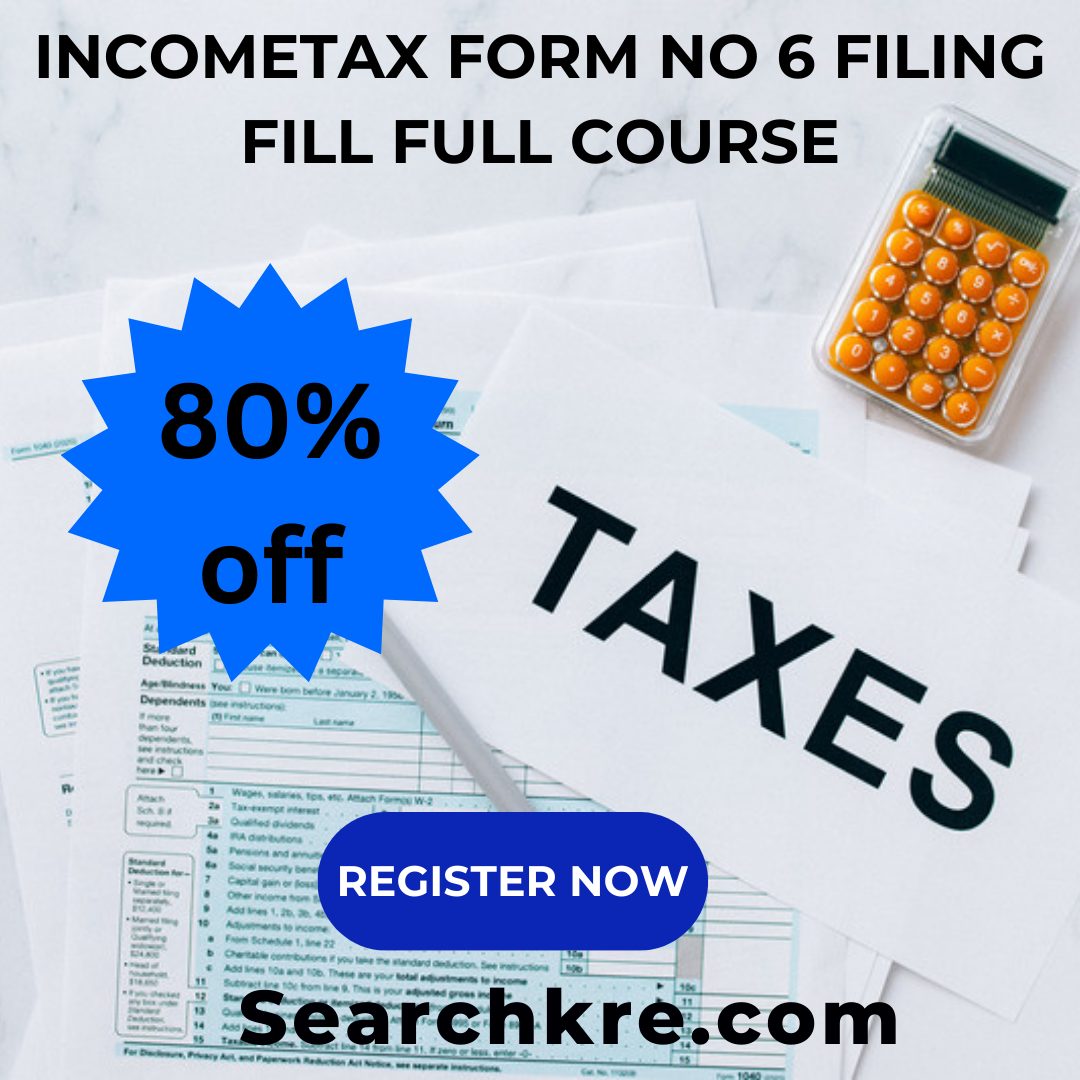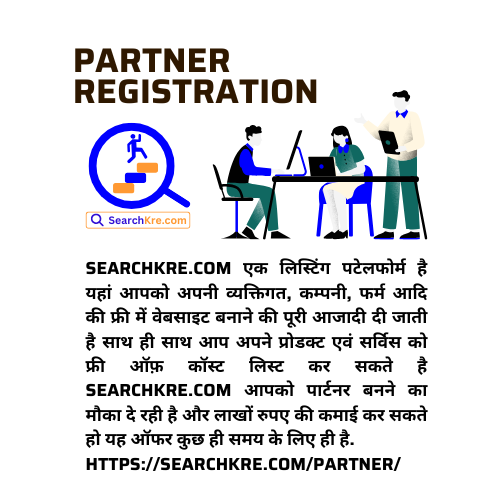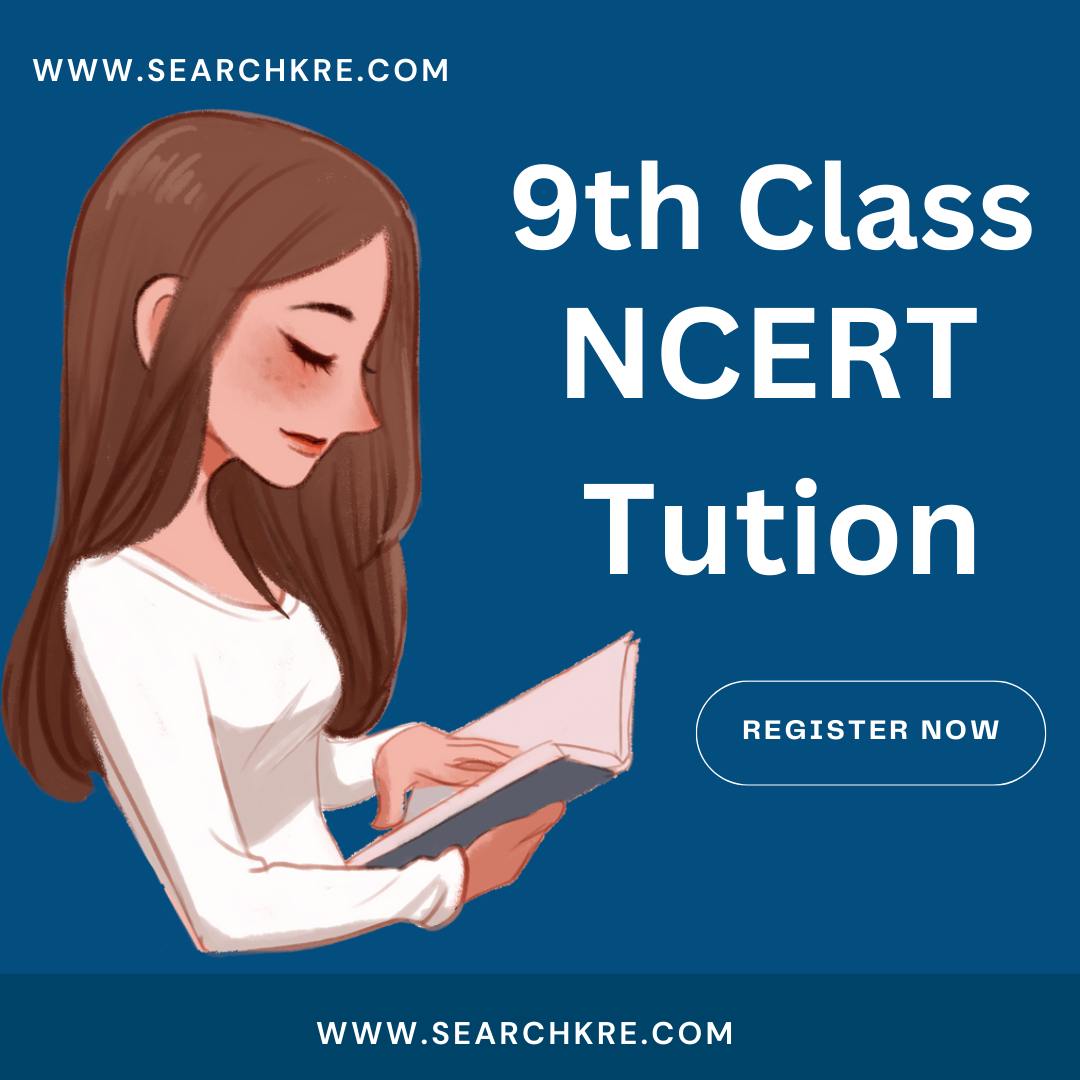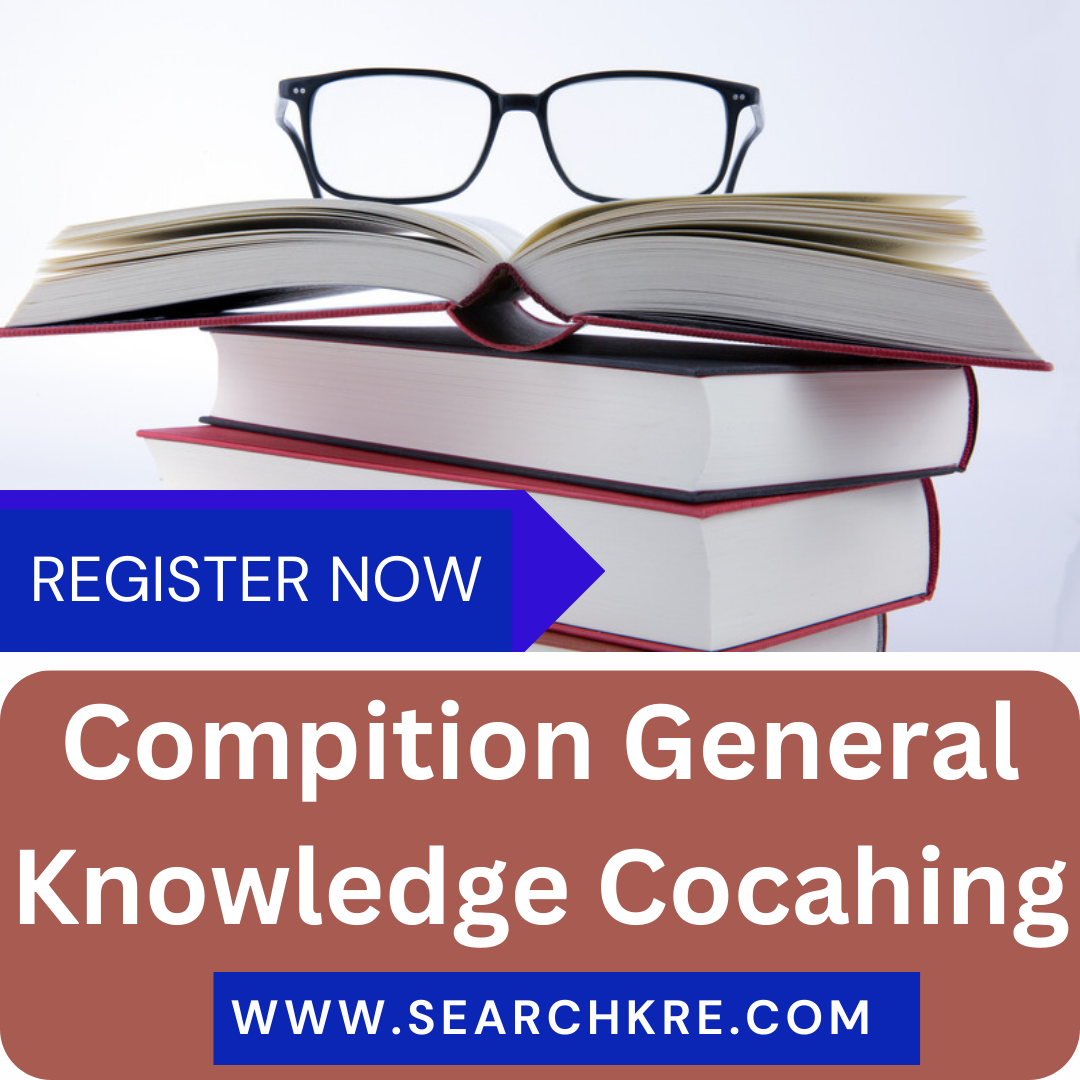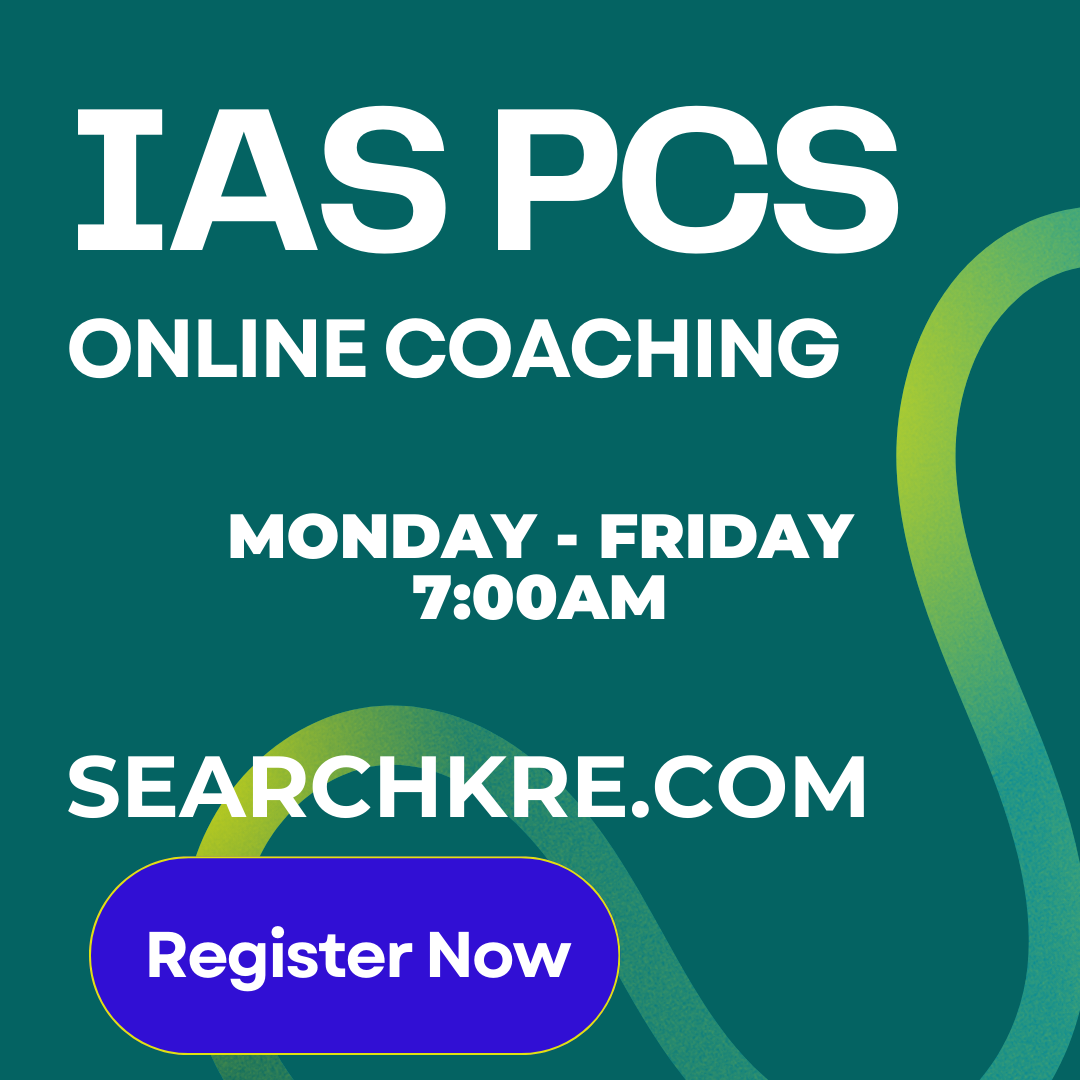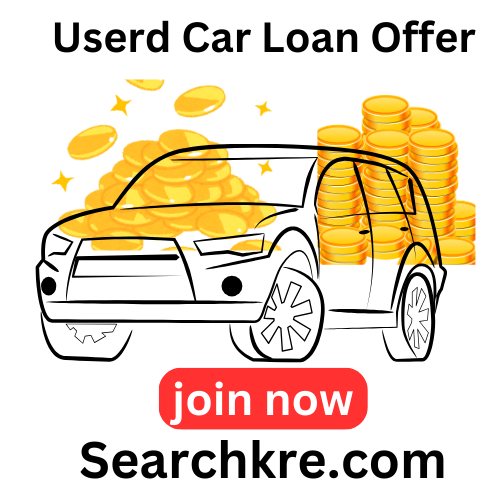Kho-Kho game
jp Singh
2025-06-02 12:55:34
searchkre.com@gmail.com /
8392828781
खो-खो खेल/Kho-Kho game
खो-खो खेल/Kho-Kho game
इतिहास
खो-खो भारत का एक पारंपरिक टैग खेल है, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई और इसे महाराष्ट्र में विशेष रूप से विकसित किया गया। कुछ स्रोतों के अनुसार, इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है, जहां "चक्रव्यूह" रणनीति खो-खो की रक्षात्मक रणनीति "रिंग प्ले" से मिलती-जुलती है। प्राचीन समय में इसे "रथेरा" के नाम से रथों पर खेला जाता था। आधुनिक खो-खो के नियम 1914 में पुणे के डेक्कन जिमखाना क्लब द्वारा मानकीकृत किए गए। यह 1936 के बर्लिन ओलंपिक में प्रदर्शन खेल के रूप में दिखाया गया। भारत में खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया (KKFI) 1950 के दशक में स्थापित हुआ, और 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में इसे अंतरराष्ट्रीय मंच मिला। 2022 में शुरू हुए अल्टीमेट खो-खो (UKK) लीग ने खेल को पेशेवर रूप दिया। 2025 में दिल्ली में पहला खो-खो विश्व कप आयोजित हुआ, जिसमें भारत की पुरुष और महिला टीमों ने स्वर्ण जीता।
स्वरूप
खो-खो एक तेज गति वाला, गैर-संपर्क टैग खेल है, जो दो टीमों के बीच खेला जाता है। यह गति, चपलता, और रणनीति पर केंद्रित है, जिसमें एक टीम (चेज़र) दूसरी टीम (रनर) को टैग करने की कोशिश करती है। यह मुख्य रूप से आउटडोर खेला जाता है, लेकिन इंडोर संस्करण भी मौजूद हैं। भारत में यह कबड्डी के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय पारंपरिक खेल है। स्वरूप:
प्रतिस्पर्धी: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट, जैसे नेशनल गेम्स, UKK लीग।
मनोरंजक: स्कूल, कॉलेज, और स्थानीय स्तर। पेशेवर: UKK लीग में संशोधित नियम, जैसे कम समय और टाई-ब्रेकर।
प्रारूप
मैच संरचना: दो टीमें, प्रत्येक में 12 खिलाड़ी, जिनमें से 9 मैदान पर उतरते हैं। एक मैच में दो पारी (इनिंग्स), प्रत्येक में 9 मिनट चेज़िंग और 9 मिनट रनिंग। रनर: 3 खिलाड़ी एक साथ मैदान पर, बाकी बेंच पर। प्रत्येक टर्न में नए 3 रनर। चेज़र: 8 खिलाड़ी सेंट्रल लेन में बैठते हैं, एक सक्रिय चेज़र रनर को टैग करता है। अल्टीमेट खो-खो: 7 मिनट प्रति टर्न, अतिरिक्त पावरप्ले और सुपर ओवर। यouth: छोटा मैदान (22x12 मीटर), कम समय (5-7 मिनट)।
नियम
उद्देश्य: चेज़र टीम रनर को टैग करके अंक (1 प्रति टैग) अर्जित करती है। टैग किए गए रनर मैदान छोड़ते हैं। खेल क्षेत्र: आयताकार, 27 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा (पुरुष), 25x14 मीटर (महिला)। सेंट्रल लेन (23.5 मीटर) में 8 वर्ग (30x30 सेमी), जहां चेज़र बैठते हैं। खो देना: सक्रिय चेज़र बैठे खिलाड़ी को "खो" कहकर गेंद देता है, जो नया चेज़र बनता है। खो केवल पीछे बैठे खिलाड़ी को दिया जा सकता है।
चेज़र नियम
चेज़र सेंट्रल लेन पार नहीं कर सकता, केवल एक दिशा में दौड़ सकता है। वैकल्पिक दिशाओं में बैठे चेज़र विपरीत दिशा का सामना करते हैं। रनर नियम: रनर फ्री ज़ोन और क्रॉस लेन में दौड़ते हैं, टैग से बचते हैं। फाउल: गलत खो, सेंट्रल लेन पार करना, गलत दिशा में दौड़ना, रनर का शारीरिक संपर्क। स्कोरिंग: प्रत्येक टैग = 1 अंक। UKK में बोनस अंक (पावरप्ले में डबल अंक)। विजेता: अधिक अंक वाली टीम, या टाई होने पर रनर का बचा समय।
ग्राउंड
मैदान: आयताकार, 27x16 मीटर (पुरुष), 25x14 मीटर (महिला), मिट्टी, घास, या मैट सतह। सेंट्रल लेन: 23.5 मीटर लंबी, 30 सेमी चौड़ी, 8 वर्गों में विभाजित। पोल: दोनों सिरों पर 120-125 सेमी ऊंचे लकड़ी/धातु के खंभे। फ्री ज़ोन: पोल के पास 2.5 मीटर क्षेत्र, जहां रनर स्वतंत्र रूप से दौड़ सकते हैं। क्रॉस लेन: सेंट्रल लेन को पार करने वाली रेखाएं। भारत में: पुणे का डेक्कन जिमखाना, दिल्ली का IG स्टेडियम, भुवनेश्वर।
खिलाड़ियों की संख्या
टीम: प्रत्येक में 12 खिलाड़ी, 9 मैदान पर (8 चेज़र + 1 सक्रिय चेज़र, या 3 रनर)। सब्स्टीट्यूट: 3 खिलाड़ी, पारी के बीच परिवर्तन। यouth: 9-12 खिलाड़ी, छोटे मैदान पर।
रणनीतियां
चेज़िंग: पोल डाइव: पोल के पास तेज डाइविंग से रनर को टैग करना। रिंग प्ले: चेज़र का रनर को घेरने के लिए समन्वित दौड़। फेक खो: रनर को भ्रमित करने के लिए नकली खो देना।
रनिंग: ज़िग-ज़ैग: क्रॉस लेन में अनियमित दौड़। फ्री ज़ोन उपयोग: पोल के पास समय बिताना। समय प्रबंधन: अधिक समय तक टैग से बचना। टीमवर्क: चेज़र के बीच खो का त्वरित आदान-प्रदान, रनर का समन्वय।
तकनीकी पहलू और तकनीक का उपयोग
वीडियो रिव्यू: UKK और विश्व कप में टैग और फाउल की समीक्षा। डेटा एनालिटिक्स: गति (20-25 किमी/घंटा), टैग सटीकता, और स्टैमिना विश्लेषण। सेंसर: जूतों में गति ट्रैकिंग। प्रकाश: रात के मैचों के लिए LED लाइट्स (UKK में)। सतह: मैट सतह चोट कम करती है, गति बढ़ाती है।
शब्दावली
खो: चेज़र का नया चेज़र को सक्रिय करने का आदेश। पोल डाइव: पोल के पास डाइविंग टैग। रिंग प्ले: रनर को घेरने की रणनीति। क्रॉस लेन: सेंट्रल लेन को पार करने वाली रेखाएं। फ्री ज़ोन: पोल के पास खुला क्षेत्र। फेक खो: भ्रामक खो देना। माइनस खो: गलत खो, जिससे रनर को अंक मिलता है।
उपकरण
पोल: 120-125 सेमी, लकड़ी/धातु, दोनों सिरों पर। जूते: हल्के, गैर-चिह्नित, अच्छी पकड़ (100-200 ग्राम)। वर्दी: हल्की जर्सी, शॉर्ट्स, रंगीन (100-150 ग्राम)। सुरक्षा: घुटने/कोहनी पैड (वैकल्पिक), माउथगार्ड (UKK में)। मैदान चिह्न: चूना या टेप से रेखाएं।
प्रशिक्षण और फिटनेस
शारीरिक फिटनेस: गति: 30-50 मीटर स्प्रिंट, इंटरवल ट्रेनिंग। चपलता: ज़िग-ज़ैग ड्रिल्स, लैडर ड्रिल्स। सहनशक्ति: 9 मिनट निरंतर दौड़, कार्डियो। ताकत: कोर और लेग वर्कआउट।
तकनीकी प्रशिक्षण: चेज़िंग: पोल डाइव, टैगिंग तकनीक, खो देना। रनिंग: ज़िग-ज़ैग, फ्री ज़ोन उपयोग। रणनीतिक प्रशिक्षण: रिंग प्ले, फेक खो, समय प्रबंधन।
मानसिक प्रशिक्षण: त्वरित निर्णय, दबाव प्रबंधन। पोषण: 60% कार्बोहाइड्रेट, 20% प्रोटीन, 2-3 लीटर हाइड्रेशन।
खिलाड़ियों की भूमिका
चेज़र: सक्रिय चेज़र (टैगिंग), बैठे चेज़र (खो प्राप्ति)। रनर: टैग से बचने वाला, समय प्रबंधन। कप्तान: रणनीति और समन्वय। पोल डाइवर: पोल के पास विशेषज्ञ।
प्रमुख टूर्नामेंट
अंतरराष्ट्रीय: दक्षिण एशियाई खेल (2016 से), खो-खो विश्व कप (2025)। राष्ट्रीय: नेशनल गेम्स, नेशनल खो-खो चैंपियनशिप, खेलो इंडिया। पेशेवर: अल्टीमेट खो-खो लीग (2022 से)। स्थानीय: पुणे, महाराष्ट्र, और बिहार में टूर्नामेंट।
आंकड़े और रिकॉर्ड
विश्व कप 2025: भारत (पुरुष और महिला) ने स्वर्ण जीता। राष्ट्रीय: महाराष्ट्र और बिहार का वर्चस्व। खिलाड़ी: मीनू धतरवाल (हरियाणा, 2025 विश्व कप में बेस्ट डिफेंडर)। गति: शीर्ष चेज़र 25 किमी/घंटा तक।
रोचक तथ्य
खो-खो का चक्रव्यूह से संबंध महाभारत के अभिमन्यु की रणनीति से प्रेरित। 1936 बर्लिन ओलंपिक में प्रदर्शन खेल। UKK लीग में 6 फ्रेंचाइजी टीमें। बिहार और हरियाणा उभरते खो-खो केंद्र।
लोकप्रियता
खो-खो भारत में कबड्डी के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय पारंपरिक खेल है, विशेष रूप से महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, और हरियाणा में। स्कूल और कॉलेज स्तर पर व्यापक। UKK और विश्व कप 2025 ने इसे वैश्विक मंच दिया। दक्षिण एशिया (नेपाल, बांग्लादेश) में भी लोकप्रिय।
सामाजिक प्रभाव
एकता: स्थानीय टूर्नामेंट समुदायों को जोड़ते हैं। प्रेरणा: युवाओं में फिटनेस, चपलता, और टीमवर्क को बढ़ावा। आर्थिक प्रभाव: UKK और टूर्नामेंट्स से प्रायोजन और रोजगार।
सांस्कृतिक प्रभाव
भारत में: महाराष्ट्र और बिहार में उत्सवों का हिस्सा।
महाभारत: चक्रव्यूह से प्रेरित रणनीति।
मीडिया: नसरीन शेख की बायोपिक (2023, UKK उद्घाटन)।
खेल का भविष्य :
प्रौद्योगिकी: वीडियो रिव्यू, डेटा एनालिटिक्स, और स्मार्ट जूते।
वैश्विक विस्तार: दक्षिण एशिया और यूरोप (KKFE, इंग्लैंड) में प्रचार।
महिला खो-खो: बढ़ता निवेश, जैसे मीनू धतरवाल की सफलता।
पेशेवरता: UKK और विश्व कप से वैश्विक पहचान।
भारत का योगदान :
ऐतिहासिक: 1914 में नियम मानकीकरण, 1936 ओलंपिक प्रदर्शन।
आधुनिक: 2025 विश्व कप में पुरुष और महिला स्वर्ण।
खिलाड़ी: मीनू धतरवाल (हरियाणा), आकाश बालियान (उत्तर प्रदेश)।
विकास: KKFI, SAI, और खेलो इंडिया द्वारा ग्रासरूट प्रोग्राम।
पुरस्कार: अर्जुन और एकलव्य पुरस्कार।
महिलाओं का खेल में योगदान
ऐतिहासिक: 1950 के दशक से राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी।
आधुनिक सफलता:
मीनू धतरवाल: 2025 विश्व कप में बेस्ट डिफेंडर।
नसरीन शेख: UKK में प्रेरक खिलाड़ी।
प्रभाव: ग्रामीण क्षेत्रों (हरियाणा, बिहार) में लड़कियों की भागीदारी।
चुनौतियां: सीमित प्रायोजन, लेकिन UKK और KKFI से सुधार।
विकास: SAI और KKFI द्वारा महिला अकादमियां, जैसे पुणे और बिहार में।
Conclusion
Thanks For Read
jp Singh
searchkre.com@gmail.com
8392828781
 Gst Registration
Gst Registration
 DSC Registration
DSC Registration
 Pancard Registration
Pancard Registration
 Company Registration
Company Registration
 Fssai Registration
Fssai Registration
 TradeMark Registration
TradeMark Registration
 MSME Registration
MSME Registration
 Passport Registration
Passport Registration
 Income Tax Return
Income Tax Return
 LLP Company Registration
LLP Company Registration
 Marriage And Court Marriage Registration
Marriage And Court Marriage Registration
 PVT LTD Company Registration
PVT LTD Company Registration
 GST Filing Services
GST Filing Services
 Coaching Insititute Registration
Coaching Insititute Registration
 GYM Registration
GYM Registration
 NGO Registration
NGO Registration
 Political Party Registration
Political Party Registration
 Society Registration
Society Registration
 Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
 Make Website on EMI
Make Website on EMI



























































































 9th Class Scholarship Competition Test
9th Class Scholarship Competition Test
 10th Class Scholarship Competition Test
10th Class Scholarship Competition Test
 11th Class Scholarship Competition Test
11th Class Scholarship Competition Test
 12th Class Scholarship Competition Test
12th Class Scholarship Competition Test
 Graduation Scholarship Competition Test
Graduation Scholarship Competition Test
 Post Graduation Scholarship Competition Test
Post Graduation Scholarship Competition Test
 Diploma Scholarship Competition Test
Diploma Scholarship Competition Test
 Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 JEE Coaching Scholarship Competition Test
JEE Coaching Scholarship Competition Test
 NEET Coaching Scholarship Competition Test
NEET Coaching Scholarship Competition Test
 Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test