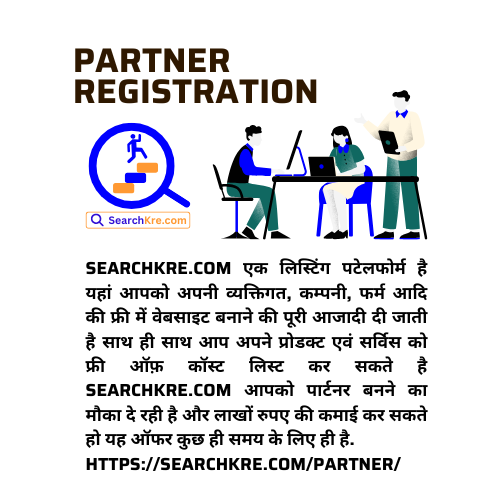Ryotwari System
jp Singh
2025-05-28 13:43:35
searchkre.com@gmail.com /
8392828781
रैय्यतवाड़ी व्यवस्था
रैय्यतवाड़ी व्यवस्था
रैयतवारी व्यवस्था (Ryotwari System) ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा भारत में लागू की गई एक भू-राजस्व व्यवस्था थी, जो मुख्य रूप से दक्षिण और पश्चिमी भारत, विशेष रूप से मद्रास प्रेसीडेंसी (वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक के कुछ हिस्से), बॉम्बे प्रेसीडेंसी (वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्से), और असम में लागू थी। इसे थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने 19वीं सदी की शुरुआत में विकसित किया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य जमींदारों की मध्यस्थता को हटाकर किसानों (रैयतों) को सीधे सरकार से जोड़ना और स्थिर राजस्व सुनिश्चित करना था।
रैयतवारी व्यवस्था की पृष्ठभूमि
औपनिवेशिक संदर्भ: 18वीं और 19वीं सदी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी राजस्व नीतियों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त (1793) की कमियों, जैसे जमींदारों का शोषण और राजस्व की स्थिरता में कमी, के कारण दक्षिण भारत में एक वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई। थॉमस मुनरो, जो मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नर बने, ने रैयतवारी व्यवस्था को 1820 में औपचारिक रूप दिया, जो पहले से मौजूद मुगल और मराठा भू-राजस्व प्रथाओं से प्रेरित थी। उद्देश्य: जमींदारों की मध्यस्थता को समाप्त करना और किसानों को सीधे सरकार से जोड़ना। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना और ब्रिटिश सरकार के लिए नियमित राजस्व सुनिश्चित करना। किसानों को जमीन का मालिकाना हक देकर उनकी स्थिति को मजबूत करना।
रैयतवारी व्यवस्था की विशेषताएँ रैयतों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी: रैयत (किसान) को जमीन का मालिक माना जाता था, और वह सीधे ब्रिटिश सरकार को लगान देता था, बिना किसी जमींदार या मध्यस्थ के। लगान की राशि प्रत्येक किसान की जमीन की उर्वरता और उत्पादन क्षमता के आधार पर तय की जाती थी। लगान का संशोधन: लगान की राशि समय-समय पर (आमतौर पर हर 20-30 साल में) संशोधित की जा सकती थी, जो इसे स्थायी बंदोबस्त से अधिक लचीली बनाता था। लगान आमतौर पर उपज का 50% तक हो सकता था, जो अक्सर बहुत भारी था।
जमीन का सर्वेक्षण: जमीन की माप और मूल्यांकन (Land Survey) के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किए गए, जिसमें मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की पैदावार का आकलन शामिल था। यह कार्य ब्रिटिश अधिकारियों और स्थानीय कर्मचारियों (जैसे पटवारी) द्वारा किया जाता था। किसानों का मालिकाना हक: रैयतों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक दिया गया, जिसे वे बेच, हस्तांतरित, या गिरवी रख सकते थे। हालांकि, भारी लगान और साहूकारों के कर्ज के कारण कई किसानों ने अपनी जमीन खो दी।
प्रशासनिक ढांचा: स्थानीय स्तर पर राजस्व संग्रह के लिए तहसीलदार और पटवारी नियुक्त किए गए। यह व्यवस्था मद्रास रेगुलेशन 1820 और बॉम्बे रेगुलेशन 1827 के तहत औपचारिक रूप से लागू की गई।
रैयतवारी व्यवस्था के प्रभाव
1. किसानों पर प्रभाव: प्रारंभिक लाभ: किसानों को जमींदारों के शोषण से कुछ राहत मिली, क्योंकि वे सीधे सरकार से जुड़े थे। मालिकाना हक ने उन्हें कुछ सुरक्षा दी। भारी लगान: लगान की राशि अक्सर बहुत अधिक होती थी (उपज का 50% तक), जिसे चुकाना किसानों के लिए मुश्किल था, खासकर अकाल या खराब फसल के समय। कर्ज और साहूकारी: साहूकारों ने उच्च ब्याज पर कर्ज देकर किसानों को कर्ज के जाल में फँसाया। कई किसानों ने अपनी जमीन साहूकारों या धनाढ्य वर्ग को खो दी। बेदखली का खतरा: लगान न चुका पाने पर जमीन नीलाम हो सकती थी, जिससे किसानों की स्थिति अनिश्चित थी। आंदोलनों का उदय: भारी लगान और साहूकारी ने कई विद्रोहों को जन्म दिया, जैसे दक्कन दंगे (1875) और रामोसी विद्रोह (1822-29)।
2. साहूकारों और धनाढ्य वर्ग पर प्रभाव: नए भूस्वामियों का उदय: साहूकारों और व्यापारियों ने नीलाम हुई जमीनें खरीदकर एक नया भूस्वामी वर्ग बनाया। आर्थिक शक्ति: साहूकारों की शक्ति बढ़ी, क्योंकि किसान कर्ज पर निर्भर थे।
3. ब्रिटिश सरकार पर प्रभाव: राजस्व में लचीलापन: समय-समय पर लगान संशोधन के कारण यह व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त से अधिक लचीली थी। प्रशासनिक जटिलता: प्रत्येक रैयत के साथ अलग-अलग समझौता करने और जमीन का सर्वेक्षण करने में समय और संसाधन लगते थे। सामाजिक अशांति: भारी लगान और साहूकारी ने किसानों में असंतोष पैदा किया, जिससे विद्रोह हुए।
4. सामाजिक और आर्थिक प्रभाव: कृषि में ठहराव: भारी लगान और कर्ज के कारण किसानों के पास कृषि सुधारों के लिए संसाधन नहीं थे, जिससे उत्पादकता घटी। सामाजिक असमानता: साहूकारों और नए भूस्वामियों का उदय हुआ, जिसने सामाजिक असमानता को बढ़ाया। आदिवासी और ग्रामीण असंतोष: रैयतवारी क्षेत्रों में आदिवासियों और किसानों ने जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए विद्रोह किए, जैसे रंपा विद्रोह (1879, 1922-24)। रैयतवारी व्यवस्था की कमियाँ भारी लगान: लगान की राशि अक्सर किसानों की वहन क्षमता से अधिक थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई। साहूकारी और कर्ज: साहूकारों ने उच्च ब्याज पर कर्ज देकर किसानों की जमीनें हड़प लीं।
प्रशासनिक जटिलता: प्रत्येक रैयत के साथ अलग-अलग समझौता और जमीन का सर्वेक्षण समय-गहन और महँगा था। बेदखली का डर: लगान न चुका पाने पर जमीन नीलाम होने का खतरा बना रहता था। कृषि विकास में कमी: भारी लगान और कर्ज ने कृषि में निवेश और नवाचार को हतोत्साहित किया।
रैयतवारी व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं से तुलना
स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement): स्थायी बंदोबस्त में जमींदार मध्यस्थ थे, और राजस्व स्थायी रूप से निश्चित था, जबकि रैयतवारी में रैयत सीधे सरकार को लगान देते थे, और लगान समय-समय पर संशोधित हो सकता था। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, और उड़ीसा में लागू था, जबकि रैयतवारी दक्षिण और पश्चिमी भारत में। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का शोषण अधिक था, जबकि रैयतवारी में साहूकारों का शोषण प्रमुख था। महालवारी व्यवस्था: महालवारी में गाँव या समूह (महाल) सामूहिक रूप से राजस्व के लिए जिम्मेदार थे, जबकि रैयतवारी में प्रत्येक रैयत व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार था। महालवारी उत्तर-पश्चिमी प्रांतों और पंजाब में लागू थी, जबकि रैयतवारी मद्रास और बॉम्बे में। दोनों में भारी लगान और शोषण आम था, लेकिन रैयतवारी में जमींदारों की भूमिका कम थी।
निज़ाम की जागीरदारी (तेलंगाना में): तेलंगाना में जागीरदारी प्रथा स्थायी बंदोबस्त से मिलती-जुलती थी, लेकिन रैयतवारी में जमींदारों की मध्यस्थता नहीं थी। तेलंगाना विद्रोह (1946-51) में जागीरदारी का शोषण प्रमुख था, जबकि रैयतवारी क्षेत्रों में दक्कन दंगे (1875) जैसे आंदोलन हुए। रैयतवारी व्यवस्था और आपके द्वारा पूछे गए आंदोलनों से संबंध आपके द्वारा पूछे गए आंदोलनों में से कई रैयतवारी व्यवस्था के क्षेत्रों से संबंधित थे, विशेष रूप से दक्कन दंगे (1875) और रामोसी विद्रोह (1822-29), जो बॉम्बे प्रेसीडेंसी में हुए। अन्य आंदोलनों के साथ इसका संबंध निम्नलिखित है:
दक्कन दंगे (1875): रैयतवारी व्यवस्था के तहत भारी लगान और साहूकारों के शोषण ने पुणे और अहमदनगर में किसानों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। यह रैयतवारी की कमियों का प्रत्यक्ष परिणाम था।
रामोसी विद्रोह (1822-29): रैयतवारी क्षेत्रों में भारी कर और अकाल ने रामोसी जनजाति को ब्रिटिश शासन और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया।
रंपा विद्रोह (1879, 1922-24): रैयतवारी क्षेत्रों में वन नीतियों और भारी करों ने आदिवासियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया।
नील आंदोलन (1859-60), पाबना विद्रोह (1873-76), मोपला विद्रोह (1921), और तेभागा आंदोलन (1946-47): ये मुख्य रूप से स्थायी बंदोबस्त क्षेत्रों में हुए, लेकिन रैयतवारी क्षेत्रों में भी समान आर्थिक शोषण था।
अवध किसान सभा (1918-22): यह महालवारी क्षेत्र में हुआ, लेकिन रैयतवारी की तरह भारी लगान और बेदखली का मुद्दा इसमें भी था।
मुंडा विद्रोह (1899-1900) और ताना भगत आंदोलन (1914-20): ये आदिवासी आंदोलन थे, जो जंगल और जमीन के अधिकारों से संबंधित थे। रैयतवारी क्षेत्रों में भी वन नीतियों ने असंतोष पैदा किया।
कूका आंदोलन (1871-72): पंजाब में महालवारी लागू थी, लेकिन रैयतवारी क्षेत्रों में भी भारी करों का असंतोष था।
तेलंगाना सशस्त्र विद्रोह (1946-51): यह निज़ाम की जागीरदारी के खिलाफ था, लेकिन रैयतवारी की तरह भारी कर और साहूकारी इसमें भी थी।
रैयतवारी व्यवस्था का ऐतिहासिक महत्व
किसान आंदोलनों का आधार: रैयतवारी व्यवस्था ने भारी लगान और साहूकारी के कारण कई विद्रोहों को जन्म दिया, जैसे दक्कन दंगे और रामोसी विद्रोह।
स्वतंत्रता संग्राम में योगदान: रैयतवारी क्षेत्रों में किसानों और आदिवासियों का असंतोष स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बना, खासकर खेड़ा सत्याग्रह (1918) में, जो गुजरात में रैयतवारी क्षेत्र में हुआ। स्वतंत्र भारत में सुधार: स्वतंत्रता के बाद, रैयतवारी और जमींदारी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए भूमि सुधार अधिनियम लागू किए गए।
Conclusion
Thanks For Read
jp Singh
searchkre.com@gmail.com
8392828781
 Gst Registration
Gst Registration
 DSC Registration
DSC Registration
 Pancard Registration
Pancard Registration
 Company Registration
Company Registration
 Fssai Registration
Fssai Registration
 TradeMark Registration
TradeMark Registration
 MSME Registration
MSME Registration
 Passport Registration
Passport Registration
 Income Tax Return
Income Tax Return
 LLP Company Registration
LLP Company Registration
 Marriage And Court Marriage Registration
Marriage And Court Marriage Registration
 PVT LTD Company Registration
PVT LTD Company Registration
 GST Filing Services
GST Filing Services
 Coaching Insititute Registration
Coaching Insititute Registration
 GYM Registration
GYM Registration
 NGO Registration
NGO Registration
 Political Party Registration
Political Party Registration
 Society Registration
Society Registration
 Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
 Make Website on EMI
Make Website on EMI


























































































 9th Class Scholarship Competition Test
9th Class Scholarship Competition Test
 10th Class Scholarship Competition Test
10th Class Scholarship Competition Test
 11th Class Scholarship Competition Test
11th Class Scholarship Competition Test
 12th Class Scholarship Competition Test
12th Class Scholarship Competition Test
 Graduation Scholarship Competition Test
Graduation Scholarship Competition Test
 Post Graduation Scholarship Competition Test
Post Graduation Scholarship Competition Test
 Diploma Scholarship Competition Test
Diploma Scholarship Competition Test
 Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 JEE Coaching Scholarship Competition Test
JEE Coaching Scholarship Competition Test
 NEET Coaching Scholarship Competition Test
NEET Coaching Scholarship Competition Test
 Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test