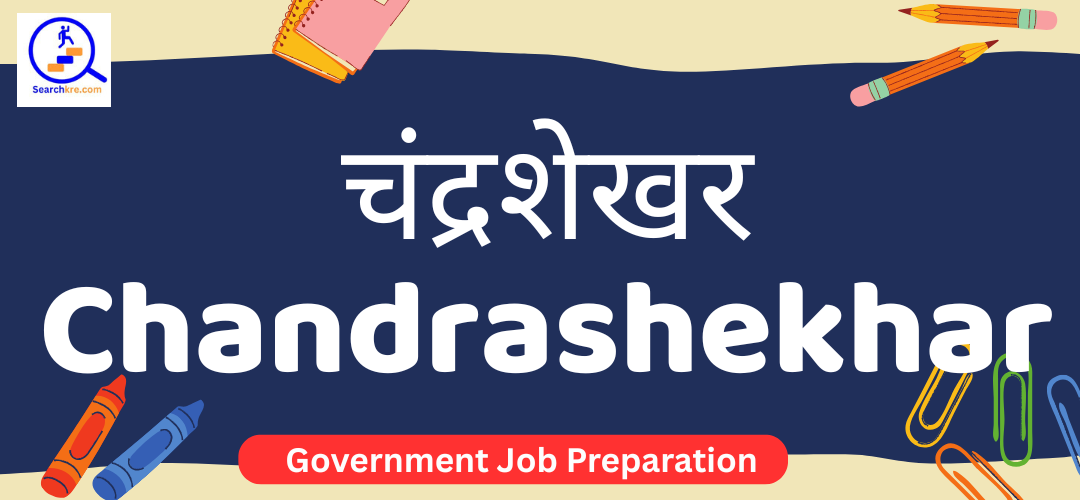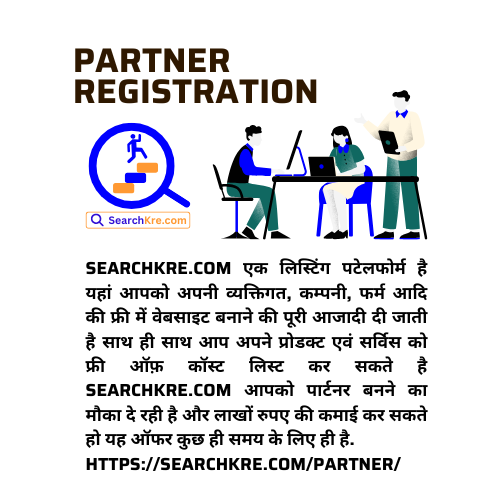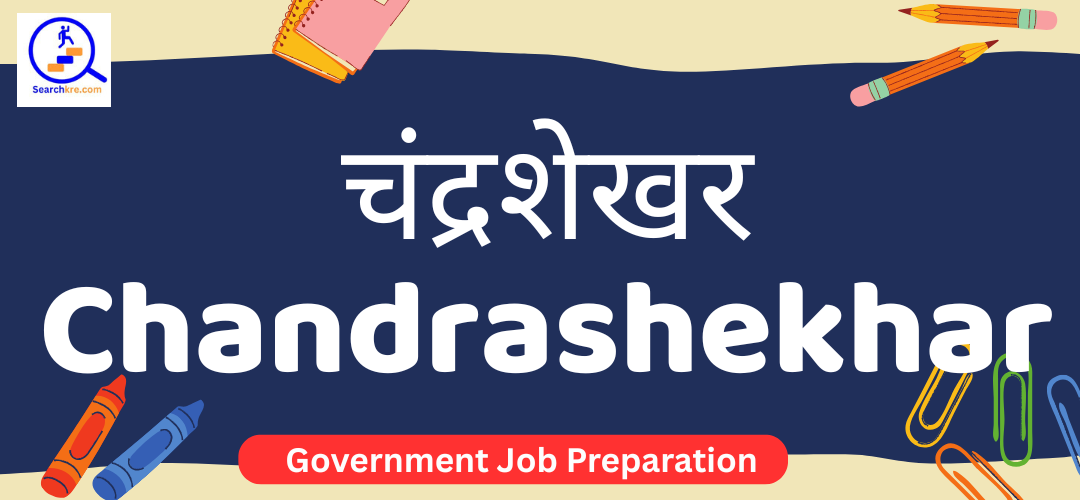
Chandrashekhar
jp Singh
2025-05-28 11:31:33
searchkre.com@gmail.com /
8392828781
चंद्रशेखर
चंद्रशेखर
चंद्रशेखर भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। चंद्रशेखर एक समाजवादी नेता थे, जो अपनी सादगी, सिद्धांतनिष्ठा और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उनका कार्यकाल केवल सात महीने का रहा, जो भारत के सबसे छोटे प्रधानमंत्री कार्यकालों में से एक है।
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा
जन्म: चंद्रशेखर का जन्म 1 जुलाई 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिमपट्टी गाँव में एक राजपूत किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता, साधु शरण सिंह, एक मध्यमवर्गीय किसान थे। शिक्षा: चंद्रशेखर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर (M.A.) की डिग्री प्राप्त की। उनकी शिक्षा ने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर गहरी समझ दी, जो उनकी समाजवादी विचारधारा का आधार बनी। प्रारंभिक जीवन: युवावस्था से ही चंद्रशेखर समाजवादी आंदोलन से प्रभावित थे। वे जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं से प्रेरित थे और सामाजिक न्याय, समानता और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित थे। स्वतंत्रता संग्राम और प्रारंभिक राजनीति स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान: चंद्रशेखर ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग नहीं लिया, क्योंकि वे उस समय बहुत युवा थे। हालांकि, 1940 के दशक में वे समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए और छात्र राजनीति में सक्रिय रहे।
समाजवादी आंदोलन: 1950 के दशक में, वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (PSP) से जुड़े और उत्तर प्रदेश में समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी वक्तृत्व कला और जनता से जुड़ने की क्षमता ने उन्हें जल्द ही एक प्रमुख नेता बना दिया। राजनीतिक करियर चंद्रशेखर का राजनीतिक सफर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू हुआ, लेकिन बाद में वे समाजवादी और गैर-कांग्रेसी राजनीति के प्रमुख चेहरों में से एक बन गए।
कांग्रेस में शुरुआत लोकसभा में प्रवेश: 1962 में, चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश के बलिया से लोकसभा के लिए चुने गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद बने। वे जल्द ही कांग्रेस के भीतर समाजवादी धड़े के एक प्रभावशाली नेता बन गए। यंग तुर्क के रूप में: 1960 के दशक में, चंद्रशेखर को “यंग तुर्क” के रूप में जाना गया, जो कांग्रेस के उन युवा नेताओं का समूह था, जो समाजवादी नीतियों और सुधारों की वकालत करते थे। वे बैंकों के राष्ट्रीयकरण और जमींदारी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर जोर देते थे। कांग्रेस से अलगाव: 1975 में, इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा के बाद, चंद्रशेखर ने इसका कड़ा विरोध किया। आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और लगभग दो साल तक जेल में रखा गया। इस अनुभव ने उन्हें कांग्रेस के खिलाफ और अधिक मुखर बना दिया। जनता पार्टी और बाद में
जनता पार्टी में भूमिका: आपातकाल के बाद, 1977 में, चंद्रशेखर जनता पार्टी में शामिल हो गए, जो विभिन्न गैर-कांग्रेसी दलों का गठबंधन था। जनता पार्टी की सरकार में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी गई, और वे पार्टी के अध्यक्ष बने। समाजवादी नेतृत्व: 1980 के दशक में, जनता पार्टी के विघटन के बाद, चंद्रशेखर ने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जनता पार्टी (समाजवादी) का गठन किया। वे सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित रहे।
प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल (10 नवंबर 1990 - 21 जून 1991) 1989 के आम चुनाव के बाद, वी.पी. सिंह की जनता दल सरकार को बीजेपी और वामपंथी दलों का समर्थन प्राप्त था। लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशों और राम मंदिर आंदोलन के कारण बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, जिससे वी.पी. सिंह की सरकार गिर गई। इसके बाद, चंद्रशेखर ने जनता दल के एक गुट (जनता दल (समाजवादी)) का नेतृत्व किया और कांग्रेस (इंदिरा) के बाहरी समर्थन से 10 नवंबर 1990 को भारत के आठवें प्रधानमंत्री बने।
प्रमुख नीतियाँ और उपलब्धियाँ चंद्रशेखर का कार्यकाल केवल सात महीने का था, और उनकी सरकार अल्पमत में थी। इस कारण उनकी नीतियाँ और उपलब्धियाँ सीमित रहीं। फिर भी, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए
आर्थिक संकट से निपटने की कोशिश: 1990-91 में, भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुके थे। चंद्रशेखर की सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए कुछ शुरुआती कदम उठाए। सोना गिरवी रखना: उनकी सरकार ने भारत के स्वर्ण भंडार को गिरवी रखकर विदेशी मुद्रा जुटाई। यह एक विवादास्पद लेकिन आवश्यक कदम था, जिसने भारत को डिफॉल्ट (ऋण चूक) से बचाया। उनकी सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कुछ कदम उठाए, जो बाद में 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा लागू उदारीकरण का आधार बने।
पंजाब और कश्मीर में शांति प्रयास: चंद्रशेखर ने पंजाब में सिख आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए बातचीत और शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने की कोशिश की। उन्होंने विभिन्न पक्षों के साथ संवाद की पहल की, लेकिन समय की कमी के कारण ज्यादा सफलता नहीं मिली। कश्मीर में बढ़ते अलगाववाद को संबोधित करने के लिए भी प्रयास किए गए, लेकिन गठबंधन की अस्थिरता ने इन प्रयासों को सीमित कर दिया। सामाजिक न्याय: चंद्रशेखर ने वी.पी. सिंह की मंडल आयोग नीति को समर्थन दिया और सामाजिक न्याय के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। हालांकि, उनके छोटे कार्यकाल में इस दिशा में कोई नई नीति लागू नहीं हो सकी।
विदेश नीति: चंद्रशेखर ने भारत की गुट-निरपेक्ष नीति को बनाए रखा और पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की। हालांकि, आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण विदेश नीति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका। सादगी और नैतिकता: चंद्रशेखर अपनी सादगी और नैतिकता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सत्ता के दुरुपयोग से बचने और पारदर्शी शासन पर जोर दिया। चुनौतियाँ अल्पमत सरकार: चंद्रशेखर की सरकार कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर निर्भर थी। यह समर्थन सशर्त था, और कांग्रेस ने अपनी शर्तों के आधार पर सरकार पर दबाव बनाए रखा। आर्थिक संकट: 1991 का आर्थिक संकट भारत के इतिहास में सबसे गंभीर संकटों में से एक था। चंद्रशेखर की सरकार के पास इसे पूरी तरह हल करने का समय या संसाधन नहीं थे।
राजनीतिक अस्थिरता: जनता दल के भीतर विभाजन और गठबंधन की कमजोर स्थिति ने उनकी सरकार को अस्थिर बनाया। वी.पी. सिंह और अन्य नेताओं के साथ मतभेद भी उनकी सरकार के लिए चुनौती थे। कांग्रेस के साथ तनाव: 1991 में, कांग्रेस ने चंद्रशेखर पर जासूसी का आरोप लगाया, जिसमें दावा किया गया कि उनकी सरकार ने राजीव गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं की जासूसी करवाई। इस विवाद ने कांग्रेस को समर्थन वापस लेने के लिए प्रेरित किया। सरकार का पतन: मार्च 1991 में, कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद चंद्रशेखर की सरकार अल्पमत में आ गई। 6 मार्च 1991 को, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन राष्ट्रपति ने उन्हें 21 जून 1991 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने को कहा।
बाद का जीवन राजनीति से दूरी: 1991 के बाद, चंद्रशेखर ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन वे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते रहे। वे बलिया से सांसद बने रहे और समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देते रहे। सामाजिक कार्य: चंद्रशेखर ने गरीबों और वंचितों के लिए काम किया और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई। वे अपनी सादगी और जनता से जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। निधन: 8 जुलाई 2007 को दिल्ली में कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी।
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा जन्म: पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को तत्कालीन हैदराबाद रियासत (वर्तमान तेलंगाना) के करीमनगर जिले के लकनेपल्ली गाँव में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शिक्षा: राव एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से स्नातक (B.A.) और नागपुर विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री (LL.B.) प्राप्त की। बाद में, उन्होंने हिस्लॉप कॉलेज, नागपुर से विज्ञान में मास्टर डिग्री (M.Sc.) भी हासिल की। बौद्धिक रुचियाँ: राव एक बहुभाषी विद्वान थे, जो हिंदी, तेलुगु, मराठी, संस्कृत, उर्दू, कन्नड़, और अंग्रेजी सहित 17 भाषाएँ जानते थे। वे साहित्य, कविता और लेखन में रुचि रखते थे। उनकी आत्मकथा द इनसाइडर (1998) उनकी बौद्धिक गहराई को दर्शाती है।
स्वतंत्रता संग्राम: राव ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल करने के आंदोलन में सक्रिय थे। वे निज़ाम शासन के खिलाफ आंदोलनों में शामिल हुए और कई बार जेल गए। राजनीतिक करियर पी.वी. नरसिम्हा राव का राजनीतिक सफर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ शुरू हुआ, और वे अपने करियर में राज्य और केंद्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे।
प्रारंभिक भूमिका आंध्र प्रदेश में शुरुआत: 1957 में, राव आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और विभिन्न मंत्रालयों में कार्य किया। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने भूमि सुधार और शिक्षा पर ध्यान दिया। मुख्यमंत्री के रूप में: राव ने आंध्र प्रदेश में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने और भूमिहीन किसानों को जमीन वितरण की नीतियाँ लागू कीं। उनकी सरकार ने तेलुगु भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया, और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए। केंद्र में भूमिका केंद्रीय मंत्रिमंडल: 1970 के दशक में, राव इंदिरा गांधी की सरकार में शामिल हुए और विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कार्य किया
गृह मंत्री (1984): राजीव गांधी की सरकार में वे गृह मंत्री रहे और पंजाब संकट से निपटने में भूमिका निभाई। विदेश मंत्री (1980-1984, 1988-1989): राव ने भारत की विदेश नीति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने गुट-निरपेक्ष आंदोलन (NAM) को बढ़ावा दिया और पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारे। रक्षा और शिक्षा जैसे मंत्रालय: राव ने कई अन्य मंत्रालयों में भी काम किया, जिसने उनकी प्रशासनिक क्षमता को प्रदर्शित किया। कांग्रेस में स्थिति: राव को कांग्रेस का एक वफादार और बौद्धिक नेता माना जाता था। हालांकि, वे कभी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में नहीं रहे और नेहरू-गांधी परिवार के छायांकन में रहे।
प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल (21 जून 1991 - 16 मई 1996) 1991 के आम चुनाव के दौरान, राजीव गांधी की हत्या ने कांग्रेस को एक सहानुभूति लहर दी, जिसके परिणामस्वरूप पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला। चंद्रशेखर की अल्पमत सरकार के पतन के बाद, कांग्रेस ने राव को अपना नेता चुना, और वे 21 जून 1991 को भारत के नौवें प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल भारत के आर्थिक और राजनीतिक इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में जाना जाता है।
प्रमुख नीतियाँ और उपलब्धियाँ आर्थिक उदारीकरण (1991): पृष्ठभूमि: 1991 में, भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार केवल 1 बिलियन डॉलर के बराबर रह गया था, जो दो सप्ताह के आयात के लिए भी पर्याप्त नहीं था। भारत डिफॉल्ट (ऋण चूक) के कगार पर था। आर्थिक सुधार: राव ने अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। प्रमुख सुधारों में शामिल थे: लाइसेंस राज का अंत: औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त किया गया, जिसने निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया। निजीकरण और वैश्वीकरण: सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को कम किया गया, और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया।
विनिमय दर सुधार: भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया, जिसने निर्यात को बढ़ावा दिया। कर सुधार: कर प्रणाली को सरल बनाया गया और आयात शुल्क को कम किया गया। प्रभाव: इन सुधारों ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया और मध्यम वर्ग के विकास को बढ़ावा दिया। भारत का IT और सेवा क्षेत्र इन सुधारों का सबसे बड़ा लाभार्थी बना।
विदेश नीति: लुक ईस्ट नीति: राव ने लुक ईस्ट नीति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों (जैसे ASEAN) के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करना था। यह नीति बाद में भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। सोवियत संघ का पतन: 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, राव ने भारत की गुट-निरपेक्ष नीति को नए वैश्विक परिदृश्य में ढाला। उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारे, लेकिन रूस के साथ भी मजबूत रिश्ते बनाए रखे। इज़राइल के साथ संबंध: राव की सरकार ने 1992 में इज़राइल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, जो एक ऐतिहासिक कदम था।
सामाजिक और संवैधानिक सुधार: पंचायती राज और नगरपालिका: राव की सरकार ने 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों (1992) को लागू किया, जिसने पंचायती राज संस्थानों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने स्थानीय शासन को मजबूत किया और ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया। महिलाओं के लिए आरक्षण: इन संशोधनों ने पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित कीं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था। रक्षा और परमाणु नीति: राव ने भारत के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को मजबूत किया। हालांकि, 1995 में प्रस्तावित परमाणु परीक्षण को अमेरिकी दबाव के कारण स्थगित करना पड़ा, जो बाद में 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ। उनकी सरकार ने रक्षा आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया और भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत किया।
शिक्षा और प्रौद्योगिकी: राव ने शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया। उनकी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में योगदान दिया और IITs जैसे संस्थानों को मजबूत किया।
चुनौतियाँ बाबरी मस्जिद विध्वंस (1992): 6 दिसंबर 1992 को, अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कारसेवकों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, जिसके कारण देशभर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। राव पर इस घटना को रोकने में विफलता का आरोप लगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया। इस घटना ने उनकी सरकार की छवि को नुकसान पहुँचाया और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ाया। आर्थिक सुधारों का विरोध: उदारीकरण की नीतियों का कुछ वर्गों, जैसे समाजवादी और वामपंथी दलों, ने विरोध किया। उन्हें पूंजीवादी नीतियों को बढ़ावा देने का आरोप लगा। ग्रामीण और छोटे उद्योगों पर उदारीकरण के प्रभाव को लेकर भी चिंताएँ थीं।
भ्रष्टाचार के आरोप: राव की सरकार पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जैसे हर्षद मेहता शेयर बाजार घोटाला (1992) और झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड (1993)। इनमें राव पर व्यक्तिगत रूप से रिश्वत लेने का आरोप लगा, हालांकि ये आरोप पूरी तरह सिद्ध नहीं हुए। कांग्रेस के भीतर मतभेद: राव को कांग्रेस के भीतर नेहरू-गांधी परिवार के वफादार नेताओं का विरोध झेलना पड़ा। सोनिया गांधी और अन्य नेताओं ने उनकी नीतियों और नेतृत्व पर सवाल उठाए।
996 का चुनाव: 1996 के आम चुनाव में, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। बाबरी मस्जिद विध्वंस, भ्रष्टाचार के आरोप और आर्थिक सुधारों के मिश्रित परिणामों ने कांग्रेस की लोकप्रियता को प्रभावित किया। बाद का जीवन राजनीति से दूरी: 1996 के बाद, राव ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। कांग्रेस नेतृत्व, विशेषकर सोनिया गांधी, ने उन्हें हाशिए पर रखा, क्योंकि उनकी स्वतंत्र नेतृत्व शैली को परिवार के प्रभुत्व के लिए खतरा माना गया। साहित्य और लेखन: राव ने अपने बाद के वर्षों में लेखन और साहित्य पर ध्यान दिया। उनकी आत्मकथा द इनसाइडर एक महत्वपूर्ण रचना है, जो भारतीय राजनीति और उनके अनुभवों पर प्रकाश डालती है।
निधन: 23 दिसंबर 2004 को दिल्ली में हृदय रोग के कारण उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र 83 वर्ष थी। उनकी मृत्यु के बाद, कांग्रेस ने उनकी विरासत को ज्यादा महत्व नहीं दिया, जिसे कई लोग अन्याय मानते हैं। व्यक्तिगत विशेषताएँ और विचारधारा विद्वान और रणनीतिक: राव एक बौद्धिक और रणनीतिक नेता थे। उनकी बहुभाषी क्षमता और गहरी नीतिगत समझ ने उन्हें एक अनूठा नेता बनाया। प्रगतिशील दृष्टिकोण: राव ने समाजवादी नीतियों से हटकर आर्थिक उदारीकरण को अपनाया, जो उस समय एक साहसिक कदम था। सादगी: अपनी विद्वता और उच्च पद के बावजूद, राव सादगी और संयमित जीवनशैली के लिए जाने जाते थे। विवाद: बाबरी मस्जिद विध्वंस और भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी छवि को प्रभावित किया। कुछ लोग उन्हें अवसरवादी मानते थे, जबकि अन्य उनकी दूरदर्शिता की प्रशंसा करते हैं। विरासत पी.वी. नरसिम्हा राव की विरासत भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है
आर्थिक उदारीकरण: 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नई पहचान दी। इन सुधारों ने भारत के मध्यम वर्ग, IT उद्योग और वैश्विक निवेश को बढ़ावा दिया। लुक ईस्ट नीति: उनकी विदेश नीति ने भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ जोड़ा, जो आज भी भारत की विदेश नीति का आधार है।
पंचायती राज: स्थानीय शासन को मजबूत करने के उनके प्रयासों ने ग्रामीण भारत में लोकतंत्र को गहरा किया। विवाद और पुनर्मूल्यांकन: बाबरी मस्जिद विध्वंस और भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी छवि को प्रभावित किया, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी विरासत को पुनर्मूल्यांकन किया गया है। कई लोग उन्हें भारत के आर्थिक परिवर्तन का असली नायक मानते हैं। पुरस्कार: 2015 में, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो उनकी उपलब्धियों को मान्यता देता है।
Conclusion
Thanks For Read
jp Singh
searchkre.com@gmail.com
8392828781
 Gst Registration
Gst Registration
 DSC Registration
DSC Registration
 Pancard Registration
Pancard Registration
 Company Registration
Company Registration
 Fssai Registration
Fssai Registration
 TradeMark Registration
TradeMark Registration
 MSME Registration
MSME Registration
 Passport Registration
Passport Registration
 Income Tax Return
Income Tax Return
 LLP Company Registration
LLP Company Registration
 Marriage And Court Marriage Registration
Marriage And Court Marriage Registration
 PVT LTD Company Registration
PVT LTD Company Registration
 GST Filing Services
GST Filing Services
 Coaching Insititute Registration
Coaching Insititute Registration
 GYM Registration
GYM Registration
 NGO Registration
NGO Registration
 Political Party Registration
Political Party Registration
 Society Registration
Society Registration
 Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
 Make Website on EMI
Make Website on EMI


























































































 9th Class Scholarship Competition Test
9th Class Scholarship Competition Test
 10th Class Scholarship Competition Test
10th Class Scholarship Competition Test
 11th Class Scholarship Competition Test
11th Class Scholarship Competition Test
 12th Class Scholarship Competition Test
12th Class Scholarship Competition Test
 Graduation Scholarship Competition Test
Graduation Scholarship Competition Test
 Post Graduation Scholarship Competition Test
Post Graduation Scholarship Competition Test
 Diploma Scholarship Competition Test
Diploma Scholarship Competition Test
 Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 JEE Coaching Scholarship Competition Test
JEE Coaching Scholarship Competition Test
 NEET Coaching Scholarship Competition Test
NEET Coaching Scholarship Competition Test
 Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test