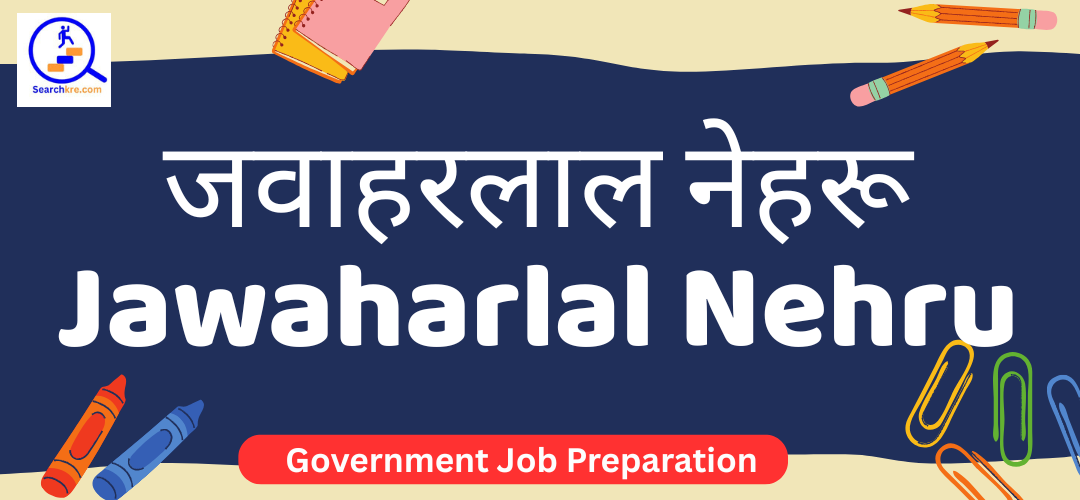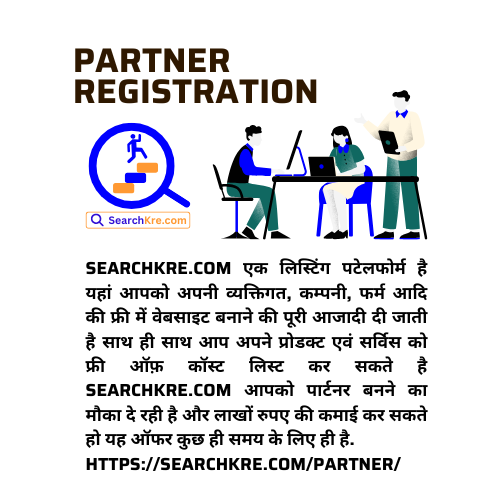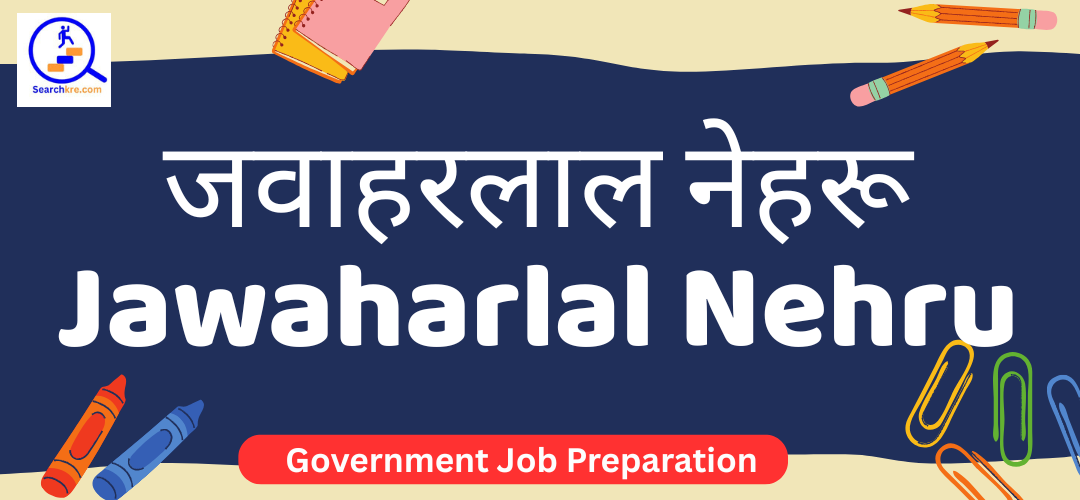
Jawaharlal Nehru
jp Singh
2025-05-28 10:31:10
searchkre.com@gmail.com /
8392828781
जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें प्यार से पंडित नेहरू या चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इस पद पर कार्य किया। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिग्गज, और आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। नेहरू की नीतियों, दृष्टिकोण, और नेतृत्व ने स्वतंत्र भारत के आर्थिक, सामाजिक, और विदेश नीति के ढाँचे को आकार दिया। उनकी गुटनिरपेक्षता की नीति, औद्योगीकरण पर जोर, और लोकतांत्रिक-समाजवादी दृष्टिकोण भारत को वैश्विक मंच पर एक नेमहत्वपूर्ण स्थान दिलाया।
1. प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि
जन्म और शिक्षा: जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद (अब प्रयागराज), उत्तर प्रदेश में एक समृद्ध कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर निजी शिक्षकों द्वारा हुई। इसके बाद, वे इंग्लैंड गए और हैरो स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। उन्होंने इनर टेम्पल, लंदन से बैरिस्टरी की डिग्री प्राप्त की और 1912 में भारत लौटे। स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश: 1916 में, नेहरू की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जिनके अहिंसक और सत्याग्रही दर्शन ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही इसके युवा और प्रगतिशील नेताओं में से एक बन गए। 1917 में, वे एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से जुड़े और इलाहाबाद में सक्रिय रहे।
2. स्वतंत्रता संग्राम में योगदान
प्रमुख आंदोलन: असहयोग आंदोलन (1920-22): नेहरू ने गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और पहली बार 1921 में जेल गए। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को बढ़ावा दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-34): नेहरू ने नमक सत्याग्रह का समर्थन किया और कई बार गिरफ्तार हुए। उनकी राष्ट्रीय चेतना और संगठनात्मक क्षमता ने कांग्रेस को मजबूत किया। भारत छोड़ो आंदोलन (1942): नेहरू इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में थे। 1942 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और अहमदनगर जेल में रखा गया, जहाँ उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक
उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी और प्रगतिशील धड़े का नेतृत्व किया, जो आर्थिक समानता और औद्योगीकरण पर जोर देता था।
साम्प्रदायिकता और एकता: नेहरू धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक माँगों का विरोध किया और एक अखंड भारत की वकालत की। हालांकि, विभाजन की अपरिहार्यता को स्वीकार करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी।
3.1 संवैधानिक और प्रशासनिक स्थिरता
संविधान का कार्यान्वयन: नेहरू ने संविधान सभा (1946-1950) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू हुआ, नेहरू ने इसे एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की नींव के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने डॉ. राजेंद्र प्रसाद (प्रथम राष्ट्रपति) और डॉ. बी. आर. आंबेडकर (संविधान के प्रमुख निर्माता) के साथ मिलकर संवैधानिक ढाँचे को लागू किया। प्रशासनिक ढाँचा: नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक ढाँचे को मजबूत करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और अन्य संस्थानों को बढ़ावा दिया। उन्होंने रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ काम किया, जिसके परिणामस्वरूप हैदराबाद (1948) और जूनागढ़ जैसी रियासतें भारत में शामिल हुईं। लोकतांत्रिक मूल्य: नेहरू ने लोकतंत्र को भारत की नींव बनाया। 1952, 1957, और 1962 के आम चुनावों में कांग्रेस ने उनकी अगुवाई में भारी जीत हासिल की।
3.2 आर्थिक नीतियाँ और नियोजित विकास
पंचवर्षीय योजनाएँ: नेहरू ने नियोजित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई, जो समाजवादी मॉडल पर आधारित थी। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की: प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956): कृषि, सिंचाई, और सामुदायिक विकास पर केंद्रित। द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-1961): भारी उद्योगों और औद्योगीकरण पर जोर, जिसे महलनोबिस मॉडल के नाम से जाना गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-1966): आत्मनिर्भरता और रक्षा पर ध्यान। नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत किया और स्टील, बिजली, और भारी मशीनरी जैसे उद्योगों की स्थापना की। भाखड़ा-नंगल बाँध और अन्य परियोजनाएँ: नेहरू ने बुनियादी ढाँचे के विकास को प्राथमिकता दी। भाखड़ा-नंगल बाँध, जिसे उन्होंने
3.3 सामाजिक सुधार
धर्मनिरपेक्षता: नेहरू धर्मनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति समानता की नीति को लागू किया और साम्प्रदायिकता का विरोध किया। हिंदू कोड बिल: नेहरू ने डॉ. बी. आर. आंबेडकर के साथ मिलकर हिंदू कोड बिल (1955-56) को लागू किया, जिसने हिंदू विवाह, उत्तराधिकार, और संपत्ति के अधिकारों में सुधार किया। यह महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम था। शिक्षा और विज्ञान: नेहरू ने शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता दी। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। उनकी नीतियों ने भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की।
3.4 विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता
3.4 विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता: गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM): नेहरू ने शीत युद्ध के दौरान भारत को गुटनिरपेक्ष बनाए रखा, जिसमें न तो अमेरिका और न ही सोवियत संघ का पक्ष लिया गया। यह नीति 1955 के बांडुंग सम्मेलन और 1961 में NAM की स्थापना के साथ औपचारिक रूप से लागू हुई। नेहरू ने यूगोस्लाविया के जोसिप ब्रोज टीटो और मिस्र के गमाल अब्देल नासर जैसे नेताओं के साथ मिलकर गुटनिरपेक्षता को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। पंचशील सिद्धांत: 1954 में, नेहरू ने चीन के साथ पंचशील (पाँच सिद्धांतों) का समझौता किया, जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित था। हालांकि, यह नीति बाद में 1962 के भारत-चीन युद्ध में विफल साबित हुई। कश्मीर मुद्दा: नेहरू ने जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थिति का बचाव किया। हालांकि, उनकी कश्मीर नीति पर बाद में आलोचना हुई।
3.5 भारत-चीन युद्ध (1962)
पृष्ठभूमि: 1950 के दशक में, भारत और चीन के बीच अक्साई चिन और मैकमोहन रेखा को लेकर सीमा विवाद बढ़ा। नेहरू की
3.6 साम्प्रदायिकता और राष्ट्रीय एकता
नेहरू ने विभाजन के बाद साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। उनकी धर्मनिरपेक्ष नीतियों ने भारत को एक समावेशी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया।
महात्मा गांधी की हत्या (1948) के बाद, नेहरू ने कट्टरवादी संगठनों पर सख्ती बरती और साम्प्रदायिक सद्भाव की अपील की।
4. व्यक्तिगत विशेषताएँ और योगदान
सादगी और लोकप्रियता: नेहरू अपनी सादगी और जनता के साथ जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध थे। बच्चों के प्रति उनके प्रेम के कारण उन्हें
उत्तराधिकार: उनकी मृत्यु के बाद, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने।
लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड चार्ल्स जॉन कैनिंग (Charles John Canning, 1812-1862), जिन्हें लॉर्ड कैनिंग के नाम से जाना जाता है, 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर-जनरल और 1858 से 1862 तक भारत के पहले वायसराय (Viceroy) थे। उनका शासनकाल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इस दौरान 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, मुगल साम्राज्य का अंत हुआ, और ब्रिटिश क्राउन ने भारत में प्रत्यक्ष शासन शुरू किया। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नींव को मजबूत करने और विद्रोह के बाद भारत में स्थिरता लाने के लिए जाना जाता है। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल (1856-1862) नियुक्ति: लॉर्ड कैनिंग को 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का गवर्नर-जनरल नियुक्त किया। वह लॉर्ड डलहौजी के उत्तराधिकारी थे, जिनके शासनकाल में आक्रामक विस्तारवादी नीतियां (जैसे हड़प नीति) अपनाई गई थीं, जिसने 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। पृष्ठभूमि: लॉर्ड कैनिंग एक अनुभवी ब्रिटिश राजनेता थे और उनके पिता जॉर्ज क
सादगी और लोकप्रियता: नेहरू अपनी सादगी और जनता के साथ जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध थे। बच्चों के प्रति उनके प्रेम के कारण उन्हें
उत्तराधिकार: उनकी मृत्यु के बाद, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने।
5. महत्व और प्रभाव
आधुनिक भारत का निर्माण: नेहरू ने स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उनकी पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत को औद्योगीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में ले गया। गुटनिरपेक्षता: नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति ने भारत को शीत युद्ध में एक स्वतंत्र और प्रभावशाली आवाज बनाया। धर्मनिरपेक्षता और एकता: उनकी धर्मनिरपेक्ष नीतियों ने भारत को एक समावेशी राष्ट्र बनाया, जिसमें सभी धर्मों और समुदायों को समान अधिकार दिए गए। आलोचनाएँ: नेहरू की कुछ नीतियों, जैसे भारत-चीन युद्ध में विफलता, कश्मीर मुद्दे पर अनिर्णय, और समाजवादी अर्थव्यवस्था की सीमाओं, की आलोचना हुई। उनकी कश्मीर नीति और संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को ले जाने के निर्णय पर सवाल उठे।
6. विरासत
जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। उनकी नीतियों ने भारत को एक लोकतांत्रिक, औद्योगिक, और वैज्ञानिक रूप से प्रगतिशील राष्ट्र बनाया। उनकी गुटनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता की नीतियाँ आज भी भारत की विदेश और आंतरिक नीतियों को प्रभावित करती हैं। 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी पुस्तकें और विचारधारा आज भी प्रासंगिक हैं और भारत के बौद्धिक इतिहास का हिस्सा हैं।
जवाहरलाल नेहरू
1. व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तित्व
परिवार और प्रारंभिक प्रभाव: जवाहरलाल नेहरू का जन्म एक धनाढ्य और शिक्षित कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक सफल वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने जवाहरलाल को पश्चिमी और भारतीय संस्कृति का मिश्रण दिया। उनकी माँ स्वरूपरानी नेहरू ने उन्हें भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित कराया। जवाहरलाल की पश्चिमी शिक्षा और भारतीय मूल्यों के इस संयोजन ने उनकी विचारधारा को आकार दिया। 1916 में, जवाहरलाल का विवाह कमला कौल से हुआ, जो एक कश्मीरी परिवार से थीं। उनकी एकमात्र संतान इंदिरा गांधी थीं, जो बाद में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। व्यक्तित्व: नेहरू एक करिश्माई, बौद्धिक, और प्रगतिशील नेता थे। उनकी सादगी, बच्चों के प्रति प्रेम, और जनता के साथ सीधा संवाद उन्हें लोकप्रिय बनाता था।
वे एक उत्साही लेखक और विचारक थे। उनकी पुस्तकें, जैसे
2. स्वतंत्रता संग्राम में अतिरिक्त योगदान
युवा नेतृत्व: नेहरू कांग्रेस के युवा और प्रगतिशील धड़े के नेता थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के साथ मिलकर समाजवादी विचारों को कांग्रेस में स्थान दिलाया। 1928 में, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट (मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में) का समर्थन किया, जो भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की माँग करती थी। हालांकि, जब गांधी और अन्य नेताओं ने पूर्ण स्वराज की माँग उठाई, नेहरू ने इसे स्वीकार किया। किसानों और मजदूरों के लिए काम: नेहरू ने किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। 1920 के दशक में, उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलनों का समर्थन किया और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई।
जेल जीवन: नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुल मिलाकर 9 वर्ष जेल में बिताए। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी बौद्धिकता का उपयोग लेखन के लिए किया। उनकी पुस्तक
3. प्रधानमंत्री के रूप में अतिरिक्त पहलू
3.1 रियासतों का एकीकरण
नेहरू ने सरदार वल्लभभाई पटेल और वी.पी. मेनन के साथ मिलकर 562 रियासतों के एकीकरण को सुनिश्चित किया। हैदराबाद (1948), जूनागढ़ (1947), और जम्मू-कश्मीर (1947) के विलय में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। जम्मू-कश्मीर: नेहरू ने जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना। 1947 में, जब महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का संलग्नता पत्र पर हस्ताक्षर किया, नेहरू ने सैन्य और कूटनीतिक समर्थन प्रदान किया। हालांकि, कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का उनका निर्णय विवादास्पद रहा, क्योंकि इसने कश्मीर को एक अंतरराष्ट्रीय विवाद बना दिया।
3.2 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन
950 के दशक में, भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग बढ़ी। पोट्टि श्रीरामुलु के अनशन और मृत्यु (1952) के बाद, नेहरू ने आंध्र प्रदेश (1953) के गठन को मंजूरी दी। 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसने भाषाई आधार पर भारत के राज्यों को पुनर्गठित किया। यह नेहरू की सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को सम्मान दिया। 3.3 शिक्षा और विज्ञान में योगदान: नेहरू ने शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को भारत की प्रगति का आधार माना। उन्होंने निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT): खड़गपुर (1951) में पहला IIT स्थापित हुआ, जो तकनीकी शिक्षा का केंद्र बना। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS): 1956 में दिल्ली में स्थापित, जो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में अग्रणी है।
परमाणु ऊर्जा आयोग: होमी भाभा के साथ मिलकर नेहरू ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण: नेहरू ने
3.4 सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण
हिंदू कोड बिल: नेहरू ने हिंदू कोड बिल को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बिल ने महिलाओं को संपत्ति, विवाह, और तलाक में समान अधिकार दिए, जो सामाजिक सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। अस्पृश्यता उन्मूलन: नेहरू ने संविधान के माध्यम से अस्पृश्यता को गैर-कानूनी घोषित किया और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य: उनकी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया, जिसने ग्रामीण भारत में सुधार लाया।
3.5 विदेश नीति के अतिरिक्त पहलू
चीन के साथ संबंध: नेहरू ने शुरू में चीन के साथ मित्रता की नीति अपनाई (
3.6 भारत-चीन युद्ध के दीर्घकालिक प्रभाव
1962 के युद्ध ने नेहरू की छवि को प्रभावित किया। भारत की हार ने उनकी सैन्य और कूटनीतिक नीतियों पर सवाल उठाए। इस युद्ध के बाद, भारत ने अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत किया, और नेहरू ने अमेरिका और सोवियत संघ से सैन्य सहायता माँगी। युद्ध ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को भी प्रभावित किया, क्योंकि भारत को पश्चिमी देशों के करीब आना पड़ा।
4. नेहरू की नीतियों के दीर्घकालिक प्रभाव
लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता: नेहरू ने भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया। उनकी नीतियों ने भारत को एक समावेशी समाज के रूप में स्थापित किया, जो आज भी भारत की पहचान है। औद्योगीकरण और आत्मनिर्भरता: उनकी पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत को औद्योगिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। भिलाई, राउरकेला, और दुर्गापुर जैसे इस्पात संयंत्र उनकी दूरदर्शिता का परिणाम थे। शिक्षा और विज्ञान: IIT, AIIMS, और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जैसे संस्थानों ने भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया। विदेश नीति: गुटनिरपेक्षता ने भारत को शीत युद्ध के दौरान एक स्वतंत्र आवाज दी। यह नीति आज भी भारत की विदेश नीति का आधार है।
सामाजिक सुधार: हिंदू कोड बिल और अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कदमों ने भारत के सामाजिक ढाँचे को आधुनिक बनाया।5. आलोचनाएँ और विवाद: भारत-चीन युद्ध: 1962 के युद्ध में भारत की हार को नेहरू की सबसे बड़ी विफलता माना जाता है। उनकी
6. व्यक्तिगत जीवन के कुछ अनछुए पहलू
दिरा गांधी के साथ संबंध: नेहरू अपनी बेटी इंदिरा के बहुत करीब थे। उन्होंने इंदिरा को राजनीति और कूटनीति में प्रशिक्षित किया, जो बाद में उनकी उत्तराधिकारी बनीं। महिलाओं के साथ दोस्ती: नेहरू की लेडी माउंटबेटन (एडविना माउंटबेटन) के साथ दोस्ती को लेकर कई चर्चाएँ रही हैं। हालांकि, यह दोस्ती मुख्य रूप से कूटनीतिक और बौद्धिक थी, और इसका कोई ठोस विवाद नहीं उभरा। स्वास्थ्य और अंतिम वर्ष: 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद नेहरू का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 1963 में उन्हें हल्का दिल का दौरा पड़ा, और 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हो गई।
7. विरासत और सांस्कृतिक प्रभाव
नेहरूवियन मॉडल: नेहरू की नीतियों को नेहरूवियन मॉडल के रूप में जाना जाता है, जो लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, और गुटनिरपेक्षता पर आधारित था। यह मॉडल भारत की नीतियों को दशकों तक प्रभावित करता रहा। सांस्कृतिक योगदान: नेहरू ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया। उन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय, साहित्य अकादमी, और ललित कला अकादमी जैसे संस्थानों को समर्थन दिया। बाल दिवस: बच्चों के प्रति उनके प्रेम ने 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में स्थापित किया, जो आज भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। स्मारक और संस्थान: नेहरू के नाम पर कई संस्थान और स्मारक स्थापित किए गए, जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। आलोचनात्मक मूल्यांकन: नेहरू की विरासत को लेकर आज भी बहस होती है। कुछ लोग उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता मानते हैं, जबकि कुछ उनकी आर्थिक और विदेश नीतियों की आलोचना करते हैं।
8. साहित्यिक योगदान
प्रमुख रचनाएँ:
Conclusion
Thanks For Read
jp Singh
searchkre.com@gmail.com
8392828781
 Gst Registration
Gst Registration
 DSC Registration
DSC Registration
 Pancard Registration
Pancard Registration
 Company Registration
Company Registration
 Fssai Registration
Fssai Registration
 TradeMark Registration
TradeMark Registration
 MSME Registration
MSME Registration
 Passport Registration
Passport Registration
 Income Tax Return
Income Tax Return
 LLP Company Registration
LLP Company Registration
 Marriage And Court Marriage Registration
Marriage And Court Marriage Registration
 PVT LTD Company Registration
PVT LTD Company Registration
 GST Filing Services
GST Filing Services
 Coaching Insititute Registration
Coaching Insititute Registration
 GYM Registration
GYM Registration
 NGO Registration
NGO Registration
 Political Party Registration
Political Party Registration
 Society Registration
Society Registration
 Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
 Make Website on EMI
Make Website on EMI


























































































 9th Class Scholarship Competition Test
9th Class Scholarship Competition Test
 10th Class Scholarship Competition Test
10th Class Scholarship Competition Test
 11th Class Scholarship Competition Test
11th Class Scholarship Competition Test
 12th Class Scholarship Competition Test
12th Class Scholarship Competition Test
 Graduation Scholarship Competition Test
Graduation Scholarship Competition Test
 Post Graduation Scholarship Competition Test
Post Graduation Scholarship Competition Test
 Diploma Scholarship Competition Test
Diploma Scholarship Competition Test
 Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 JEE Coaching Scholarship Competition Test
JEE Coaching Scholarship Competition Test
 NEET Coaching Scholarship Competition Test
NEET Coaching Scholarship Competition Test
 Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test