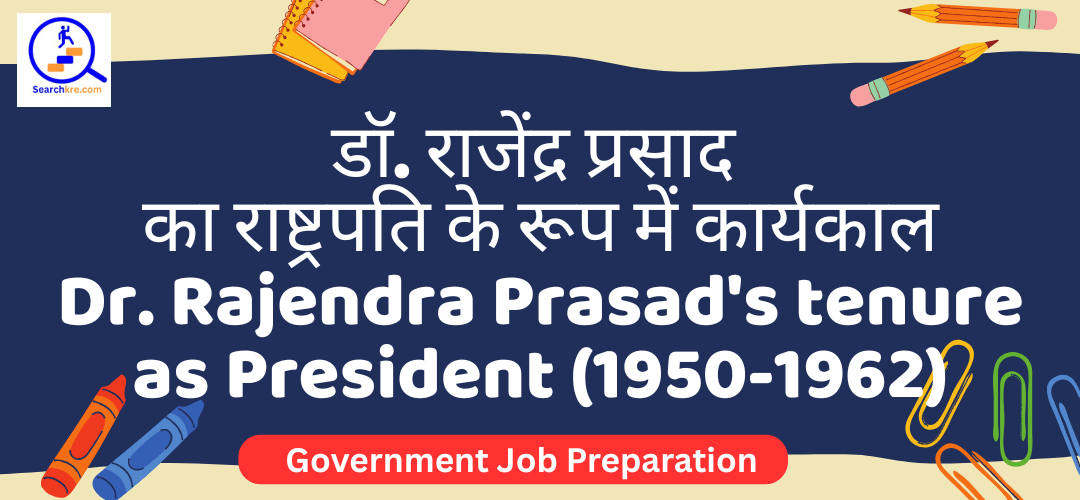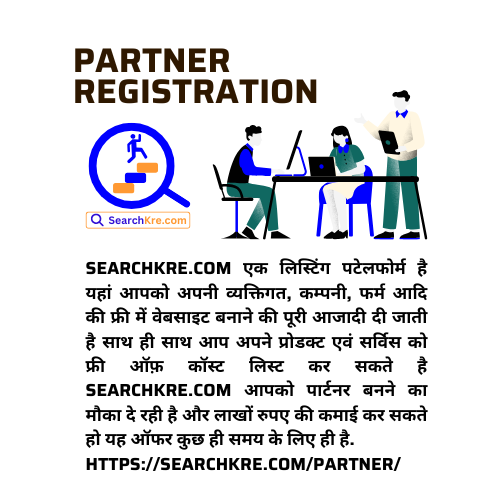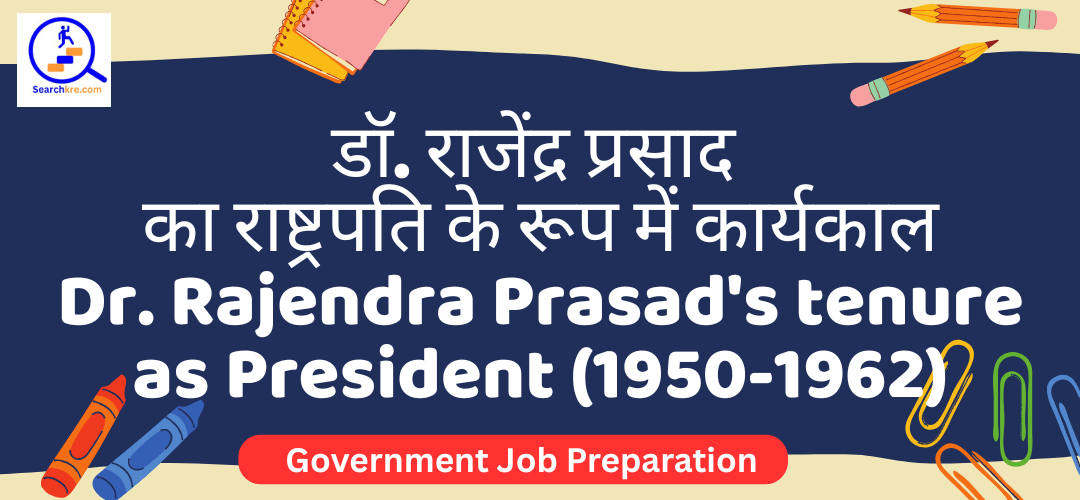
Dr. Rajendra Prasad's tenure as President (1950-1962)
jp Singh
2025-05-28 10:20:15
searchkre.com@gmail.com /
8392828781
डॉ. राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल (1950-1962)
डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक यह पद संभाला। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता, विद्वान, वकील, और गांधीवादी सिद्धांतों के अनुयायी थे। उनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल भारत के नवजात गणतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दौर था, जिसमें संवैधानिक ढाँचे की स्थापना, राष्ट्रीय एकीकरण, और सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य शामिल थे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद अपनी सादगी, निष्ठा, और देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, और उन्हें भारत के इतिहास में एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है।
डॉ. राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल (1950-1962)
डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक यह पद संभाला। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता, विद्वान, वकील, और गांधीवादी सिद्धांतों के अनुयायी थे। उनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल भारत के नवजात गणतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दौर था, जिसमें संवैधानिक ढाँचे की स्थापना, राष्ट्रीय एकीकरण, और सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य शामिल थे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद अपनी सादगी, निष्ठा, और देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, और उन्हें भारत के इतिहास में एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है।
1. पृष्ठभूमि
प्रारंभिक जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान: जन्म: डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गाँव में हुआ था। वे एक कायस्थ परिवार से थे और उनकी शिक्षा-दीक्षा कोलकाता और पटना में हुई। स्वतंत्रता संग्राम: राजेंद्र प्रसाद 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी बने। वे चंपारण सत्याग्रह (1917), असहयोग आंदोलन (1920), नमक सत्याग्रह (1930), और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में सक्रिय रहे। उन्होंने कई बार जेल यात्राएँ कीं और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1934 और 1939 में सेवा की। संविधान सभा: राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे (1946-1950), और उन्होंने भारत के संविधान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति: 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना, डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। वे सी. राजगोपालाचारी के बाद इस भूमिका में आए, जो गवर्नर-जनरल थे। उनकी नियुक्ति उनकी सादगी, अनुभव, और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के कारण स्वाभाविक थी।
2. प्रमुख भूमिकाएँ और घटनाएँ
2.1 संवैधानिक और प्रतीकात्मक भूमिका
संवैधानिक जिम्मेदारियाँ: भारत के संविधान के तहत, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस भूमिका को गरिमा और निष्ठा के साथ निभाया। उन्होंने संसद द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी दी, मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य किया, और संवैधानिक प्रक्रियाओं को सुचारु रूप से चलाने में मदद की। हालांकि संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियाँ सीमित थीं, राजेंद्र प्रसाद ने कुछ अवसरों पर अपनी राय व्यक्त की, विशेष रूप से हिंदू कोड बिल और भूमि सुधार जैसे मुद्दों पर। प्रतीकात्मक भूमिका: भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक बनकर देश को प्रेरित किया। उनकी सादगी और गांधीवादी जीवनशैली ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोला और इसे एक प्रतीकात्मक जन-भवन बनाया।
2.2 राष्ट्रीय एकीकरण और रियासतों का विलय
रियासतों का एकीकरण: स्वतंत्रता के बाद, भारत में 562 रियासतों का एकीकरण एक बड़ी चुनौती थी। लॉर्ड माउंटबेटन और सी. राजगोपालाचारी के समय में अधिकांश रियासतों का विलय हो चुका था, लेकिन कुछ मुद्दे बाकी थे। राजेंद्र प्रसाद ने सरदार वल्लभभाई पटेल और वी.पी. मेनन के नेतृत्व में एकीकरण प्रक्रिया का समर्थन किया। उनके कार्यकाल में, भारत एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा। जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उनके कार्यकाल में भी महत्वपूर्ण रहा। 1950 में, शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में कश्मीर में एक संवैधानिक ढाँचा तैयार किया गया, और राजेंद्र प्रसाद ने भारत सरकार को इस मुद्दे पर समर्थन प्रदान किया। कश्मीर को भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया, जिसे राजेंद्र प्रसाद ने संवैधानिक रूप से स्वीकार किया।
2.3 सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण
सामाजिक सुधार: राजेंद्र प्रसाद गांधीवादी सिद्धांतों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन, ग्रामीण विकास, और शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया। उन्होंने हिंदू कोड बिल (1955-56) पर अपनी राय व्यक्त की, जिसमें हिंदू विवाह, उत्तराधिकार, और संपत्ति के अधिकारों में सुधार प्रस्तावित थे। हालांकि, उन्होंने इस बिल को पारंपरिक हिंदू मूल्यों के दृष्टिकोण से देखा और कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई, लेकिन अंततः इसे मंजूरी दी। आर्थिक नीतियाँ: जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956) शुरू की, जिसमें कृषि, सिंचाई, और औद्योगीकरण पर जोर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद ने इन नीतियों का समर्थन किया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने भूदान आंदोलन (विनोबा भावे द्वारा शुरू) का समर्थन किया, जिसमें जमींदारों से भूमिहीनों के लिए जमीन दान करने की अपील की गई थी।
2.4 साम्प्रदायिक सद्भाव और गांधीवादी सिद्धांत
गांधी की विरासत: महात्मा गांधी की हत्या (30 जनवरी 1948) के बाद, राजेंद्र प्रसाद ने उनके सिद्धांतों को जीवित रखने की कोशिश की। उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और साम्प्रदायिक दंगों के प्रभाव को कम करने में मदद की। उनकी सादगी और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें
2.5 भारत-पाकिस्तान संबंध और कश्मीर मुद्दा
कश्मीर युद्ध का समापन: राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल की शुरुआत में, प्रथम भारत-पाक युद्ध (1947-1948) का समापन हो चुका था। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से 1 जनवरी 1949 को युद्धविराम लागू हुआ। राजेंद्र प्रसाद ने भारत सरकार की नीतियों का समर्थन किया, जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानती थीं। कूटनीतिक भूमिका: उन्होंने भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत स्थिति प्रदान करने में मदद की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर अपनी स्थिति को स्पष्ट किया।
2.6 राष्ट्रमंडल और अंतरराष्ट्रीय संबंध
राष्ट्रमंडल में भारत: 1949 में, भारत ने यह निर्णय लिया कि वह गणतंत्र बनने के बाद भी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहेगा। राजेंद्र प्रसाद ने इस नीति का समर्थन किया और भारत को वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में मदद की। गुटनिरपेक्षता: जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति की शुरुआत राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में हुई। उन्होंने भारत की इस नीति का समर्थन किया, जिसने भारत को शीत युद्ध के दौरान तटस्थ और स्वतंत्र स्थिति प्रदान की।
2.7 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध
जवाहरलाल नेहरू के साथ संबंध: राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच सामान्यतः सौहार्दपूर्ण संबंध थे, लेकिन कुछ मुद्दों पर मतभेद उभरे, जैसे हिंदू कोड बिल और भूमि सुधार। राजेंद्र प्रसाद ने संवैधानिक सीमाओं का सम्मान किया और मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य किया, लेकिन उन्होंने अपनी राय को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में संकोच नहीं किया। संवैधानिक सीमाएँ: भारत के संविधान के तहत, राष्ट्रपति की शक्तियाँ सीमित थीं, और वे मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य थे। राजेंद्र प्रसाद ने इस संवैधानिक ढाँचे का पालन किया, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति की भूमिका को गरिमामय और प्रभावशाली बनाया।
2.8 दोबारा निर्वाचन और लंबा कार्यकाल
दोबारा निर्वाचन: 1952 और 1957 में, राजेंद्र प्रसाद को दोबारा राष्ट्रपति चुना गया। वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने दो पूर्ण कार्यकाल (और तीसरा आंशिक कार्यकाल) पूरा किया। उनकी लोकप्रियता और सादगी ने उन्हें जनता और नेताओं के बीच सम्मानित बनाया। लंबा कार्यकाल: 12 वर्षों (1950-1962) तक राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने के कारण, वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति बने।
3. महत्व और प्रभाव
संवैधानिक स्थिरता: राजेंद्र प्रसाद ने भारत के नवजात गणतंत्र में संवैधानिक ढाँचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी उपस्थिति ने देश को स्थिरता और एकता प्रदान की। राष्ट्रीय एकीकरण: रियासतों का विलय, विशेष रूप से हैदराबाद, और कश्मीर मुद्दे पर उनकी भूमिका ने भारत को एक एकीकृत राष्ट्र बनाने में योगदान दिया। सामाजिक सुधार: उनकी गांधीवादी विचारधारा ने अस्पृश्यता उन्मूलन, ग्रामीण विकास, और साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। अंतरराष्ट्रीय स्थिति: राजेंद्र प्रसाद ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति और राष्ट्रमंडल में भूमिका को समर्थन देकर देश को वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति प्रदान की। सादगी और लोकप्रियता: उनकी सादगी और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें
4. कार्यकाल का अंत
डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 13 मई 1962 को राष्ट्रपति का पद छोड़ा। उनके बाद डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद, राजेंद्र प्रसाद पटना लौट गए और सादा जीवन जिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा और अन्य लेखन कार्यों में समय बिताया। उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को पटना में हुई।
5. विरासत
प्रथम राष्ट्रपति: डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में हमेशा याद किए जाएँगे। उनकी नियुक्ति स्वतंत्र भारत के आत्मविश्वास और संवैधानिक परिपक्वता का प्रतीक थी। गांधीवादी सिद्धांत: उनकी सादगी, निष्ठा, और गांधीवादी विचारधारा ने भारत के सामाजिक और नैतिक ढाँचे को मजबूत किया। संवैधानिक योगदान: संविधान सभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति के रूप में, उन्होंने भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रीय एकता: रियासतों का एकीकरण और साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए उनके प्रयासों ने भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। पुरस्कार: 1962 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
6. व्यक्तिगत विशेषताएँ
सादगी: राजेंद्र प्रसाद अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। वे राष्ट्रपति भवन में सादा भोजन करते थे और गांधीवादी जीवनशैली का पालन करते थे। विद्वता: वे एक विद्वान थे और उन्होंने
Conclusion
Thanks For Read
jp Singh
searchkre.com@gmail.com
8392828781
 Gst Registration
Gst Registration
 DSC Registration
DSC Registration
 Pancard Registration
Pancard Registration
 Company Registration
Company Registration
 Fssai Registration
Fssai Registration
 TradeMark Registration
TradeMark Registration
 MSME Registration
MSME Registration
 Passport Registration
Passport Registration
 Income Tax Return
Income Tax Return
 LLP Company Registration
LLP Company Registration
 Marriage And Court Marriage Registration
Marriage And Court Marriage Registration
 PVT LTD Company Registration
PVT LTD Company Registration
 GST Filing Services
GST Filing Services
 Coaching Insititute Registration
Coaching Insititute Registration
 GYM Registration
GYM Registration
 NGO Registration
NGO Registration
 Political Party Registration
Political Party Registration
 Society Registration
Society Registration
 Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
 Make Website on EMI
Make Website on EMI


























































































 9th Class Scholarship Competition Test
9th Class Scholarship Competition Test
 10th Class Scholarship Competition Test
10th Class Scholarship Competition Test
 11th Class Scholarship Competition Test
11th Class Scholarship Competition Test
 12th Class Scholarship Competition Test
12th Class Scholarship Competition Test
 Graduation Scholarship Competition Test
Graduation Scholarship Competition Test
 Post Graduation Scholarship Competition Test
Post Graduation Scholarship Competition Test
 Diploma Scholarship Competition Test
Diploma Scholarship Competition Test
 Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 JEE Coaching Scholarship Competition Test
JEE Coaching Scholarship Competition Test
 NEET Coaching Scholarship Competition Test
NEET Coaching Scholarship Competition Test
 Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test