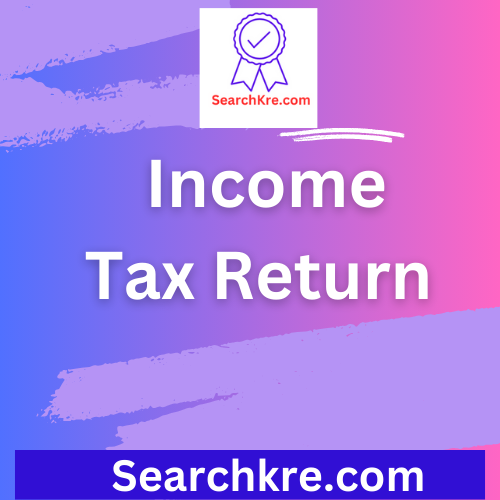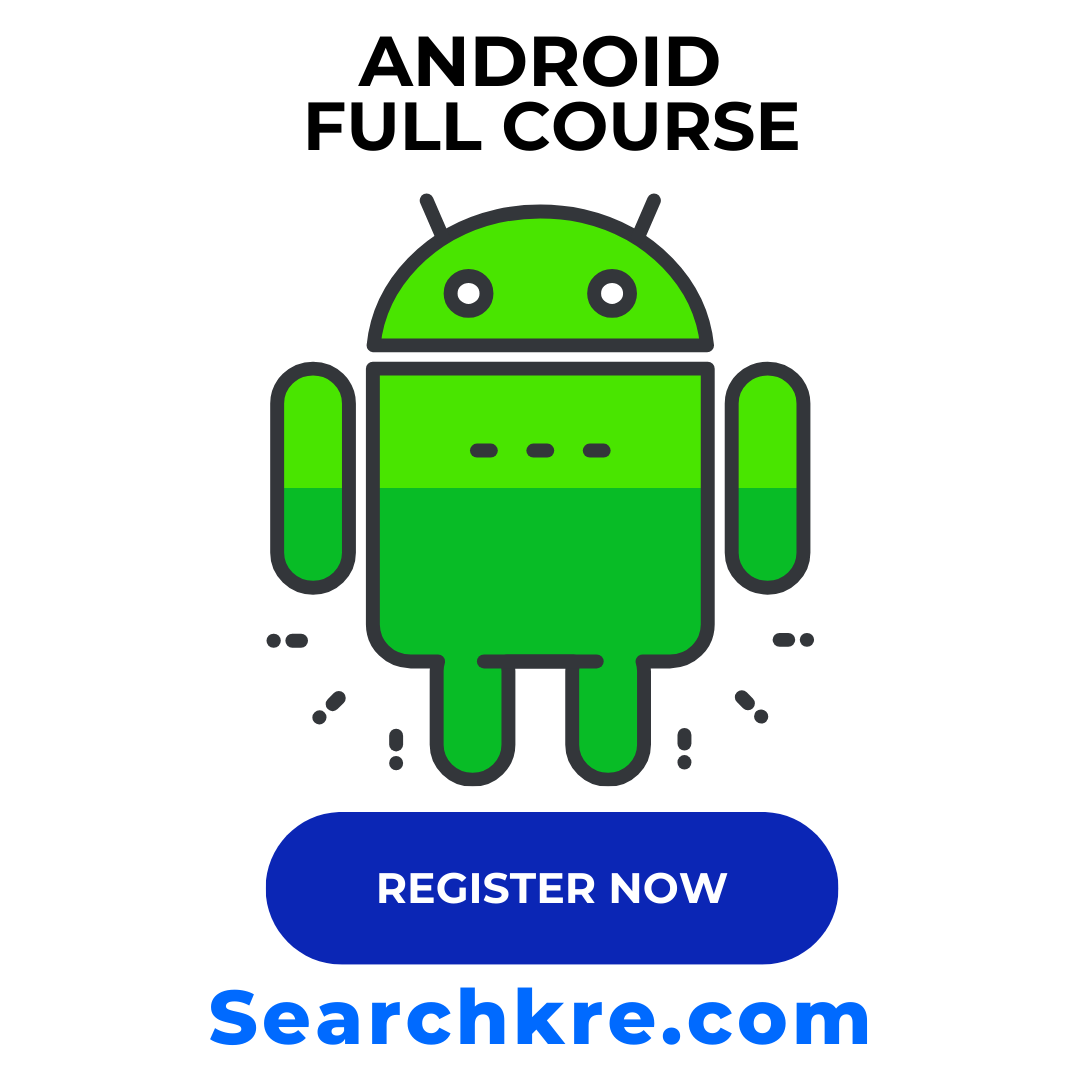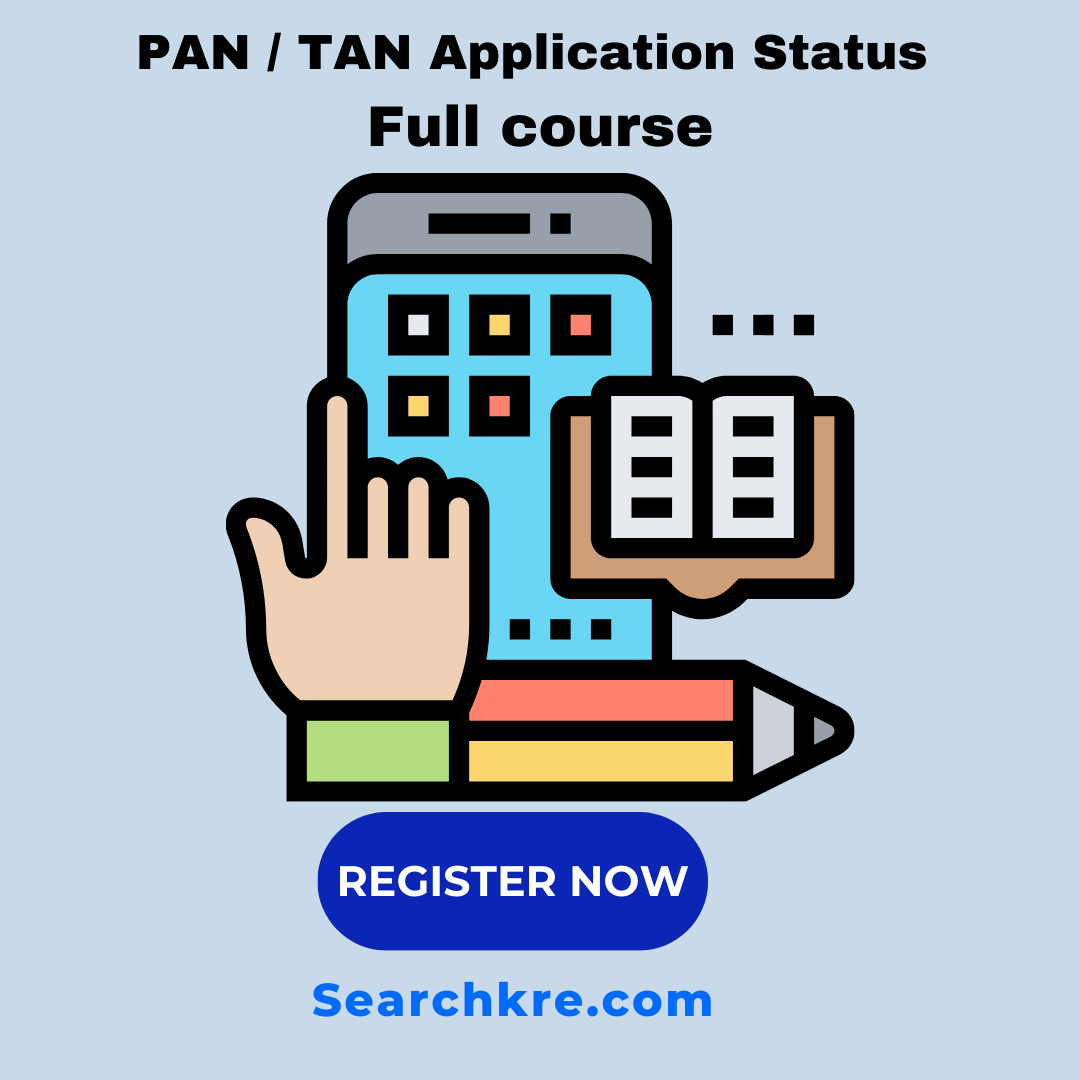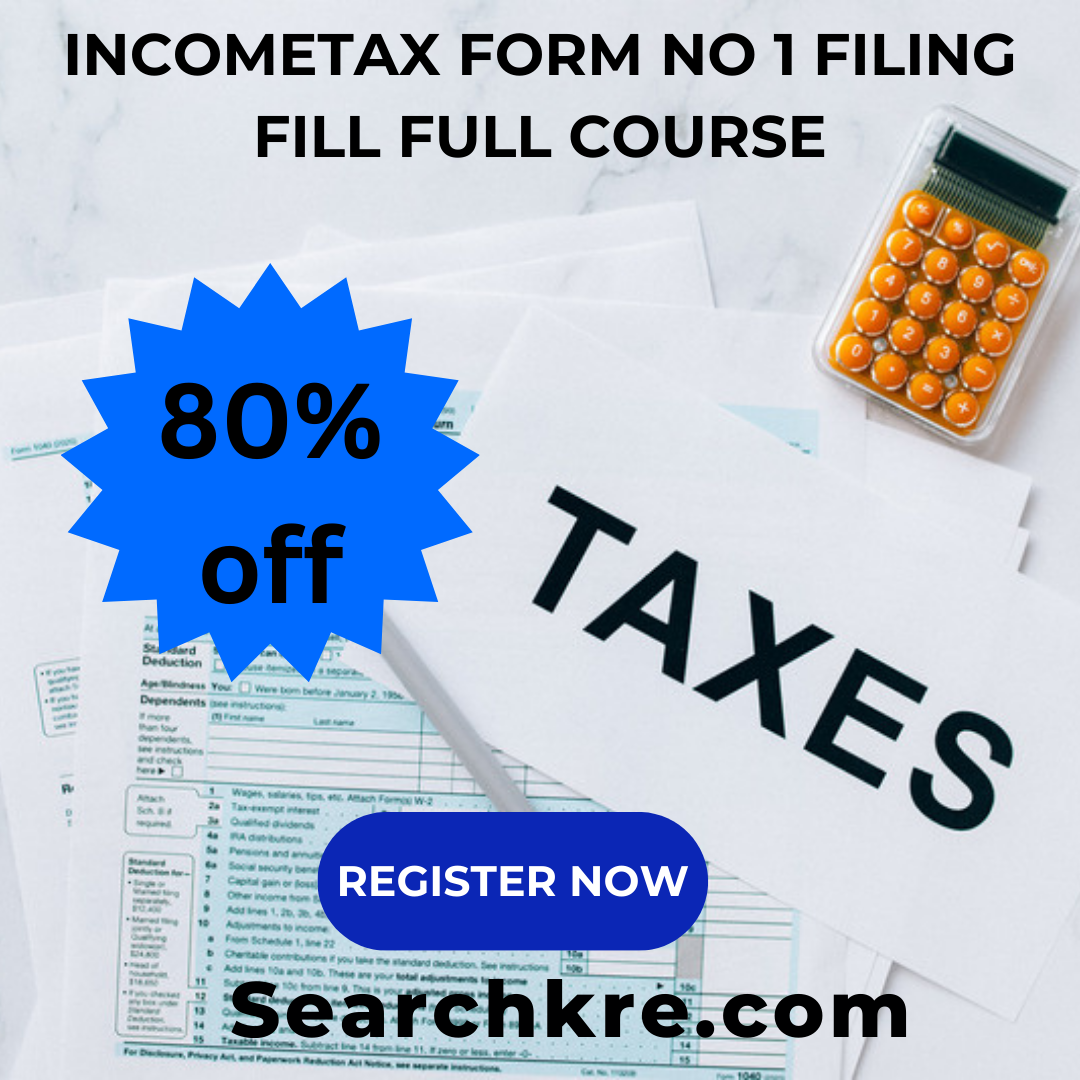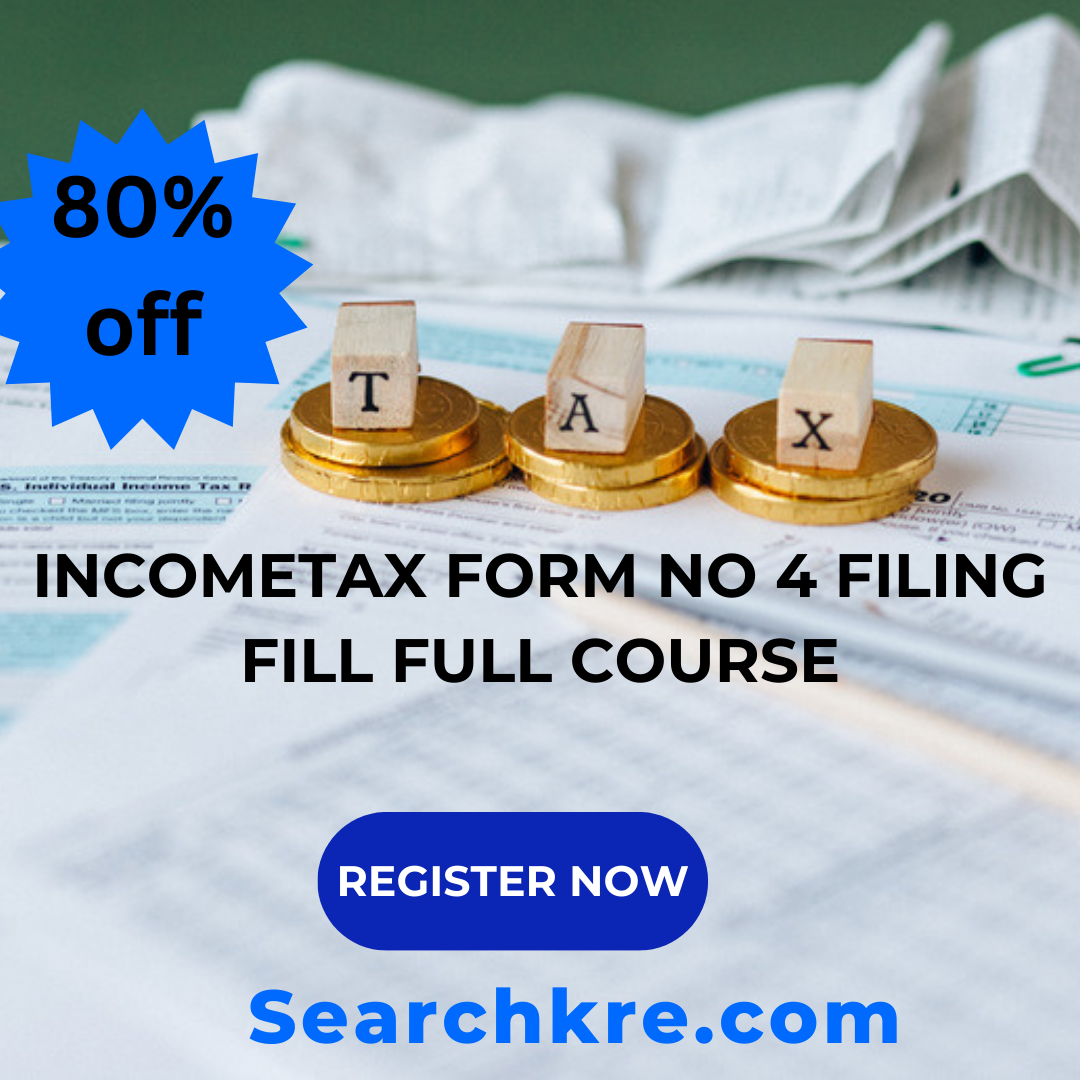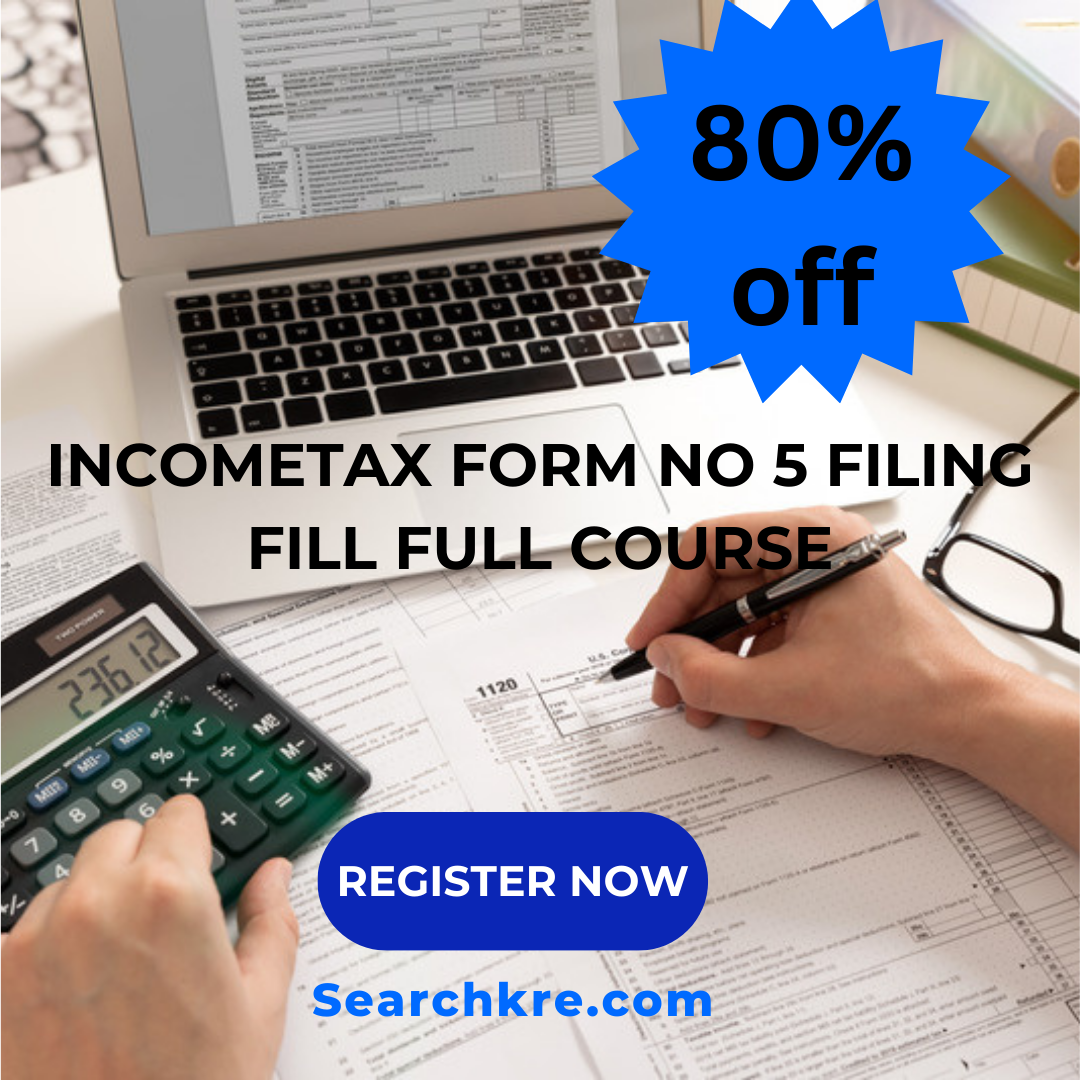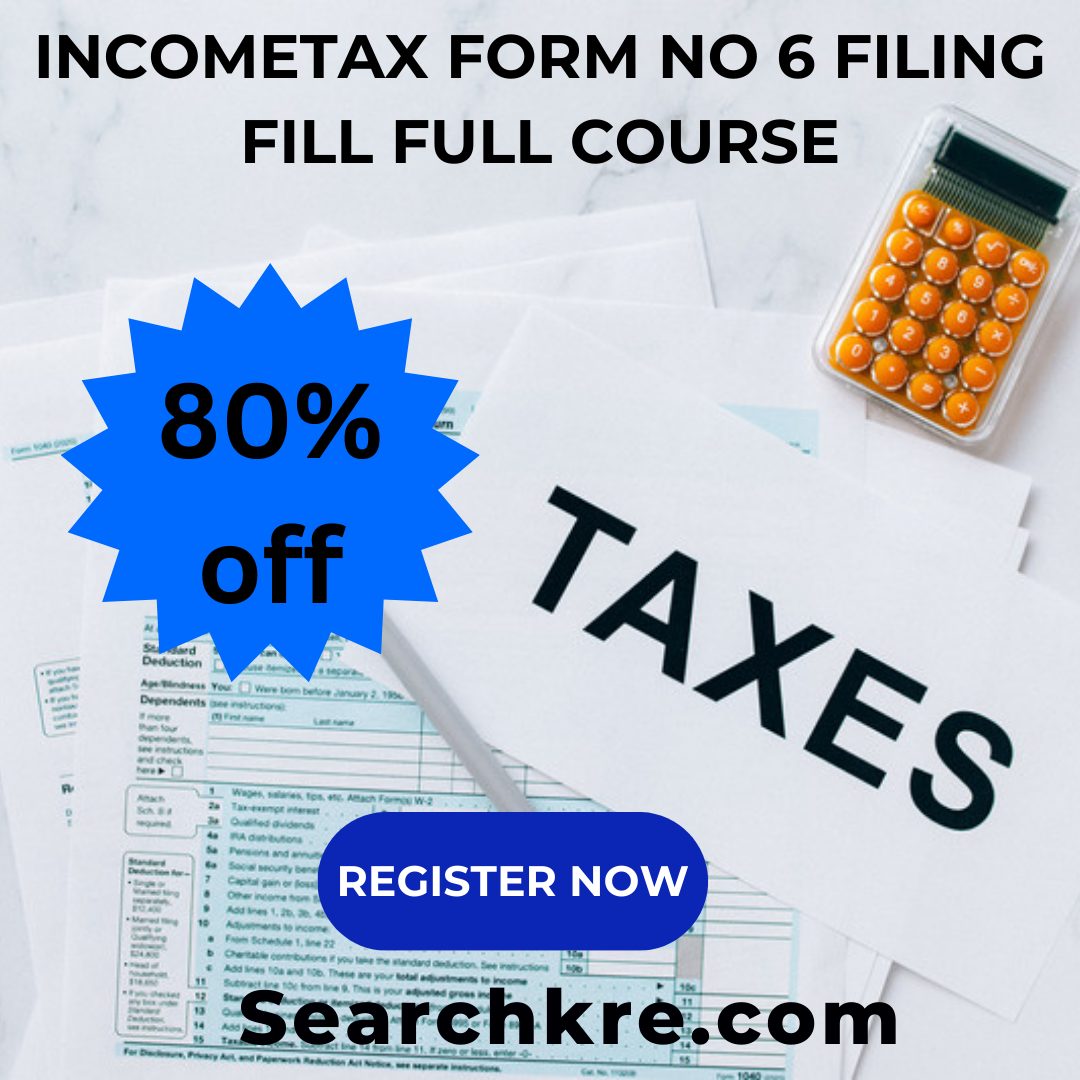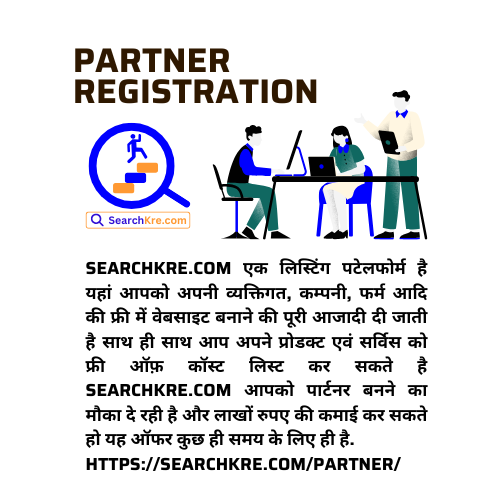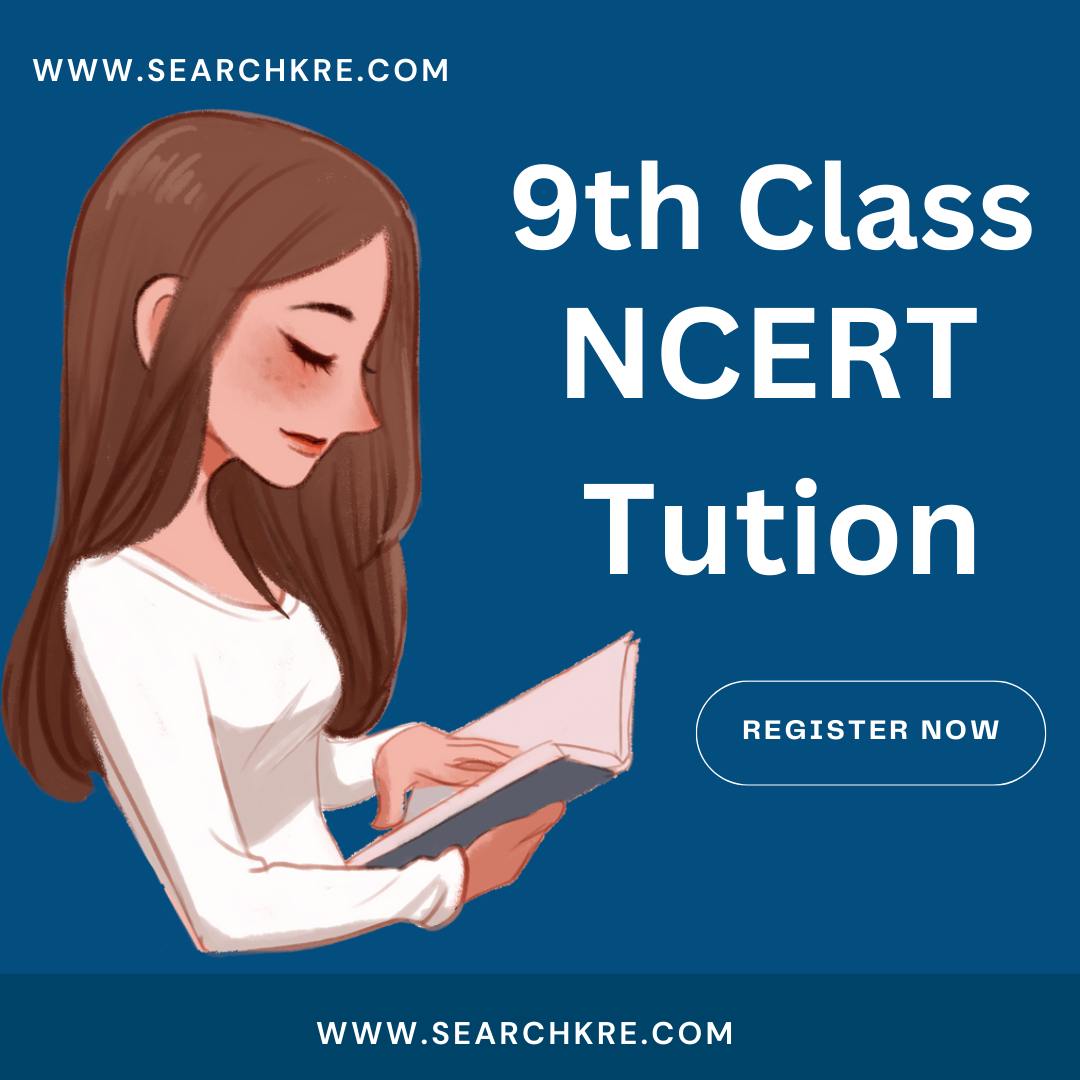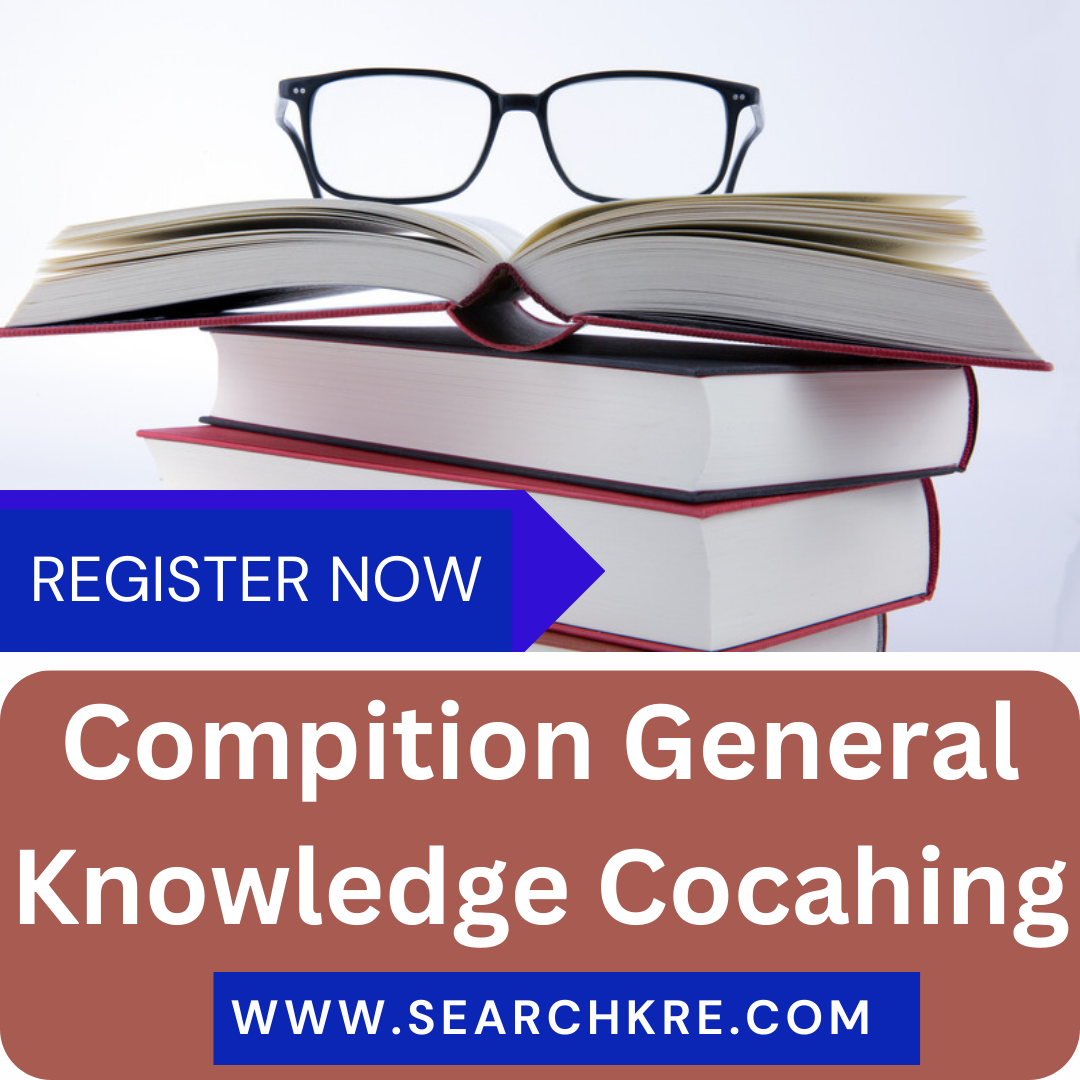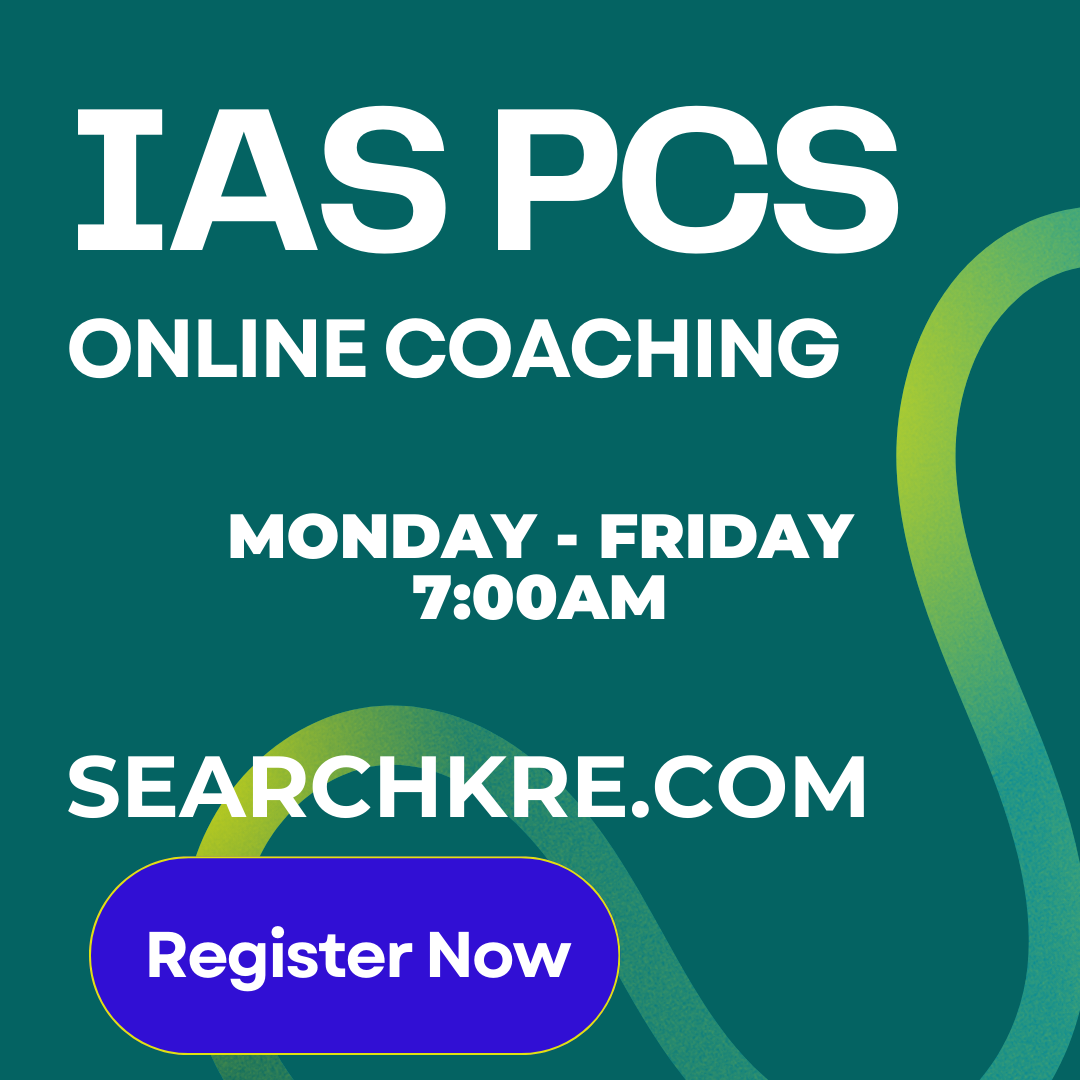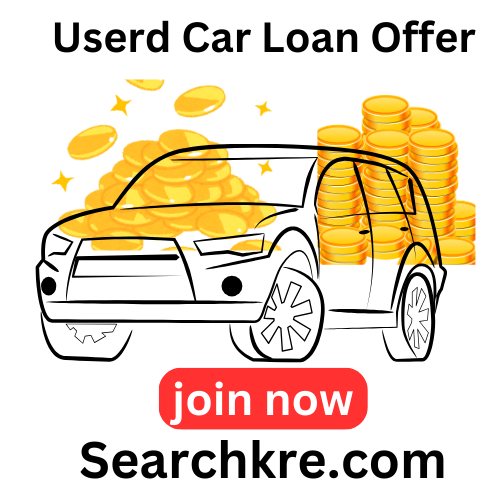.png)
Aalamgir II (1699-1759)
jp Singh
2025-05-27 14:17:14
searchkre.com@gmail.com /
8392828781
आलमगीर द्वितीय (1699-1759)
आलमगीर द्वितीय (1699-1759)
आलमगीर द्वितीय (1699-1759), जिनका मूल नाम अज़ीज़-उद-दीन था, मुगल साम्राज्य के पंद्रहवें सम्राट थे। उनका शासनकाल (1754-1759) लगभग पाँच वर्षों तक चला और मुगल साम्राज्य के पतन के दौर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वह औरंगजेब के पुत्र मुहम्मद आज़म शाह के पुत्र थे और इस तरह औरंगजेब के पौत्र थे। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल अस्थिरता, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों, मराठा प्रभाव, और दरबारी षड्यंत्रों के लिए जाना जाता है। वह अपने वज़ीर इमाद-उल-मुल्क के नियंत्रण में एक कठपुतली शासक थे। उनके शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध (1761) होने वाला था, जिसने मराठा शक्ति को कमजोर किया और मुगल सत्ता को और अधिक नाममात्र का बना दिया।
1. प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि
जन्म: आलमगीर द्वितीय का जन्म 6 जून 1699 को मुल्तान (वर्तमान पाकिस्तान) में हुआ था। वह औरंगजेब के पुत्र मुहम्मद आज़म शाह और उनकी पत्नी जानी बेगम के पुत्र थे। उनका मूल नाम अज़ीज़-उद-दीन था। शिक्षा: मुगल शाही परंपराओं के अनुसार, अज़ीज़-उद-दीन को फारसी, अरबी, इस्लामी धर्मशास्त्र, और प्रशासनिक शिक्षा दी गई। हालाँकि, उनके पास सैन्य या प्रशासनिक अनुभव की कमी थी, जो उनके शासनकाल में उनकी कमजोरी का कारण बनी। पारिवारिक पृष्ठभूमि: आलमगीर द्वितीय का जन्म औरंगजेब के शासनकाल (1658-1707) के अंतिम दौर में हुआ। उनके पिता मुहम्मद आज़म शाह ने औरंगजेब की मृत्यु (1707) के बाद संक्षिप्त रूप से सत्ता संभाली, लेकिन जजाऊ के युद्ध (1707) में बहादुर शाह प्रथम से हार गए और मारे गए। इस हार के बाद अज़ीज़-उद-दीन का परिवार दरबार से अलग-थलग हो गया।
प्रारंभिक जीवन: औरंगजेब की मृत्यु के बाद अज़ीज़-उद-दीन को दिल्ली में नज़रबंदी में रखा गया। वह 1754 तक नज़रबंदी में रहे, जिसके कारण उन्हें कोई प्रशासनिक या सैन्य अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। उनकी नज़रबंदी के दौरान वह धार्मिक अध्ययन और सादगी से जीवन जीते थे।
2. शासनकाल (1754-1759)
आलमगीर द्वितीय का शासनकाल अत्यंत अस्थिर और कमजोर था। वह अपने वज़ीर इमाद-उल-मुल्क (घुलाम कादिर) के नियंत्रण में रहे, और उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य नाममात्र का हो चुका था। सिंहासनारोहण पृष्ठभूमि: 2 जून 1754 को अहमद शाह बहादुर को उनके वज़ीर इमाद-उल-मुल्क ने अपदस्थ कर दिया और नज़रबंद कर लिया। इमाद-उल-मुल्क ने नज़रबंद अज़ीज़-उद-दीन को रिहा किया और उन्हें सम्राट बनाया। उनकी ताजपोशी दिल्ली में हुई, और उन्होंने आलमगीर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की, जो औरंगजेब (आलमगीर प्रथम) की याद में थी। उस समय वह 55 वर्ष के थे। इमाद-उल-मुल्क का नियंत्रण: आलमगीर द्वितीय पूरी तरह इमाद-उल-मुल्क के नियंत्रण में थे। इमाद-उल-मुल्क एक महत्वाकांक्षी और षड्यंत्रकारी वज़ीर था, जिसने अपने हितों के लिए दरबार को नियंत्रित किया।
प्रमुख घटनाएँ अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण: चौथा आक्रमण (1756-1757): अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1756 में पंजाब पर फिर से आक्रमण किया और 1757 में दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। दिल्ली में लूटपाट और नरसंहार हुआ। अब्दाली ने मथुरा और वृंदावन में भी भारी तबाही मचाई। आलमगीर द्वितीय असहाय रहे, और इमाद-उल-मुल्क ने अब्दाली के साथ संधि की, जिसमें पंजाब, कश्मीर, और सिंध को अब्दाली को सौंप दिया गया। पाँचवाँ आक्रमण (1759): अब्दाली ने फिर से उत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसने मराठा और मुगल सत्ता को और कमजोर किया। यह आक्रमण पानीपत के तीसरे युद्ध (1761) की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था। मराठा प्रभाव: मराठा शक्ति (पेशवा बालाजी बाजीराव और रघुनाथराव के नेतृत्व में) उत्तर भारत में बढ़ रही थी। मराठों ने 1758 में पंजाब पर कब्ज़ा किया और अब्दाली के गवर्नर को हटा दिया। मराठों ने आलमगीर द्वितीय को संरक्षण देने का प्रयास किया, लेकिन इमाद-उल-मुल्क ने मराठों के खिलाफ अब्दाली का समर्थन किया। यह पानीपत के तीसरे युद्ध का कारण
सिख विद्रोह: सिखों ने पंजाब में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई और अब्दाली के आक्रमणों का प्रतिरोध किया। सिखों ने मुगल सत्ता को पूरी तरह नकार दिया और पंजाब में स्वायत्तता स्थापित की। जाट और रोहिल्ला: भरतपुर के जाट (सूरजमल के नेतृत्व में) और रोहिल्ला (नजीब-उद-दौला के नेतृत्व में) दिल्ली के आसपास सक्रिय थे। नजीब-उद-दौला ने अब्दाली का समर्थन किया, जबकि जाट मराठों के साथ थे। दरबारी षड्यंत्र: इमाद-उल-मुल्क और नजीब-उद-दौला जैसे दरबारियों ने आलमगीर द्वितीय को कमजोर रखा। आलमगीर द्वितीय ने स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। ह त्या: 29 नवंबर 1759 को इमाद-उल-मुल्क के इशारे पर आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या का कारण उनकी बढ़ती स्वतंत्रता और मराठों के साथ संभावित गठजोड़ था, जो इमाद-उल-मुल्क के हितों के खिलाफ था।
मृत्यु आलमगीर द्वितीय की हत्या 29 नवंबर 1759 को दिल्ली में हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अली गौहर (जो बाद में शाह आलम द्वितीय बने) को सम्राट घोषित किया गया, लेकिन वह उस समय बिहार में थे और दिल्ली पर तुरंत नियंत्रण नहीं कर सके। इमाद-उल-मुल्क ने शाहजहाँ तृतीय को संक्षिप्त रूप से सम्राट बनाया।
3. प्रशासन
आलमगीर द्वितीय का प्रशासन पूरी तरह अस्थिर और नाममात्र का था। इमाद-उल-मुल्क और अन्य दरबारी सत्ता के केंद्र थे।
केंद्रीय शासन सम्राट की भूमिका: आलमगीर द्वितीय एक कठपुतली शासक थे, जिनके पास कोई वास्तविक सत्ता नहीं थी। वह धार्मिक और सादगी से जीवन जीते थे, लेकिन इमाद-उल-मुल्क के नियंत्रण में रहे। मंत्रिपरिषद: इमाद-उल-मुल्क (वज़ीर), नजीब-उद-दौला (रोहिल्ला नेता), और मराठा प्रतिनिधियों ने शासन को नियंत्रित किया। गुटबाजी और षड्यंत्रों ने प्रशासन को अक्षम बना दिया। न्याय व्यवस्था: शरिया के आधार पर नाममात्र की न्याय व्यवस्था थी, लेकिन क्षेत्रीय शासकों ने स्वतंत्र रूप से न्याय प्रदान किया।
प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन सूबे: मुगल साम्राज्य के सूबे (दिल्ली, आगरा, बंगाल, पंजाब) पूरी तरह स्वायत्त हो चुके थे। अवध, बंगाल, और हैदराबाद के नवाब केंद्र को कोई कर नहीं भेजते थे। मनसबदारी प्रणाली: मनसबदारी प्रणाली पूरी तरह ढह चुकी थी। जागीरें क्षेत्रीय शक्तियों (मराठा, रोहिल्ला, जाट) के नियंत्रण में थीं। ज़ब्त प्रणाली: कर संग्रह की व्यवस्था अस्त-व्यस्त थी। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी कर वसूली असंभव हो गई थी।
सैन्य संगठन आलमगीर द्वितीय की सेना नाममात्र की थी और अब्दाली, मराठा, या सिखों का मुकाबला करने में असमर्थ थी। मराठों और रोहिल्लाओं की सेनाओं पर निर्भरता थी, लेकिन यह भी अस्थिर थी। नौसेना का कोई अस्तित्व नहीं था, और तटीय क्षेत्रों में अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारी प्रभावी थे।
4. अर्थव्यवस्था
आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी थी। नादिर शाह (1739) और अब्दाली के आक्रमणों ने खजाने को खाली कर दिया था।
कृषि प्रमुख फसलें: गेहूँ, चावल, जौ, और नील प्रमुख फसलें थीं, लेकिन विद्रोहों और लूटपाट ने कृषि को प्रभावित किया। सिंचाई: कोई नई सिंचाई परियोजना शुरू नहीं हुई। मौजूदा नहरें और कुएँ उपेक्षित थे। कर प्रणाली: कर संग्रह की व्यवस्था पूरी तरह ढह चुकी थी। मराठा, सिख, और जाट ने कर वसूली पर नियंत्रण कर लिया था। व्यापार आंतरिक व्यापार: दिल्ली और आगरा जैसे व्यापारिक केंद्र कमजोर हो गए। अब्दाली के आक्रमणों और मराठा-सिख विद्रोहों ने व्यापार मार्गों को असुरक्षित किया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार: बंगाल और सूरत के बंदरगाहों से व्यापार होता था, लेकिन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण बढ़ाया। 1757 में प्लासी का युद्ध (आलमगीर द्वितीय के समय) अंग्रेजों की शक्ति का प्रतीक था।
यूरोपीय व्यापारी: अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारियों ने भारत के तटीय क्षेत्रों में अपनी स्थिति मज़बूत की। मुद्रा सोने (मुहर), चांदी (रुपया), और तांबे (दाम) के सिक्के प्रचलित थे, लेकिन खजाने की कमी ने सिक्कों की गुणवत्ता को प्रभावित किया। क्षेत्रीय शासकों ने स्वतंत्र सिक्के जारी किए, जिसने मुगल मुद्रा की साख को कम किया। उद्योग कपटा उद्योग: बंगाल की मलमल और गुजरात के सूती वस्त्र विश्व प्रसिद्ध थे, लेकिन यूरोपीय व्यापारियों ने इस पर नियंत्रण बढ़ाया। हस्तशिल्प: आभूषण और कालीन जैसे हस्तशिल्प कमजोर हो रहे थे।
5. समाज और संस्कृति
आलमगीर द्वितीय का समाज अस्थिर और विभाजित था। उनकी धार्मिक प्रवृत्ति ने कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, लेकिन साम्राज्य की कमजोरी ने सांस्कृतिक विकास को सीमित किया।
सामाजिक संरचना अभिजात वर्ग: मनसबदार, जागीरदार, और क्षेत्रीय शासक (मराठा, रोहिल्ला, जाट) समाज के शीर्ष पर थे। इमाद-उल-मुल्क और नजीब-उद-दौला जैसे दरबारी सत्ता के केंद्र थे। मध्यम और निम्न वर्ग: व्यापारी, कारीगर, और किसान समाज का बड़ा हिस्सा थे। लूटपाट और विद्रोहों ने उनकी स्थिति को खराब किया। जाति व्यवस्था: हिंदू समाज में वर्ण और जाति व्यवस्था प्रचलित थी। आलमगीर द्वितीय ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया।
धर्म धार्मिक नीति: आलमगीर द्वितीय धार्मिक प्रवृत्ति के थे और इस्लामी शरिया का पालन करते थे। उन्होंने जज़िया लागू नहीं किया और हिंदुओं के साथ सहिष्णुता बरती। हालाँकि, सिखों और मराठों के साथ तनाव बना रहा। सूफी और भक्ति आंदोलन: सूफी संतों और भक्ति संतों का प्रभाव बना रहा। आलमगीर द्वितीय ने सूफी दरगाहों को संरक्षण दिया। सिख विद्रोह: सिखों ने पंजाब में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई और अब्दाली के साथ-साथ मुगल सत्ता को चुनौती दी। महिलाओं की स्थिति उच्च वर्ग: आलमगीर द्वितीय की पत्नियाँ और हरम की महिलाएँ दरबार में प्रभावशाली थीं, लेकिन उनकी कोई विशेष भूमिका दर्ज नहीं है। सामान्य वर्ग: पर्दा प्रथा, बाल-विवाह, और सती प्रथा प्रचलित थीं। कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। शिक्षा: उच्च वर्ग की महिलाएँ शिक्षित थीं और साहित्य में सक्रिय थीं।
शिक्षा और संस्कृति शिक्षा: मस्जिदों और मदरसों में इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। उर्दू और फारसी साहित्य का सीमित विकास हुआ। साहित्य: आलमगीर द्वितीय के दरबार में उर्दू कविता का कुछ विकास हुआ। मीर तकी मीर जैसे कवियों ने इस युग में योगदान दिया। वास्तुकला: उनके शासन में कोई उल्लेखनीय वास्तुशिल्पीय योगदान नहीं हुआ। आर्थिक कमजोरी ने निर्माण परियोजनाओं को रोक दिया। चित्रकला: मुगल लघुचित्र कला लगभग समाप्त हो चुकी थी। संगीत: आलमगीर द्वितीय ने संगीत को सीमित संरक्षण दिया। ख्याल गायकी का विकास मुहम्मद शाह के समय की तरह जारी रहा।
6. व्यक्तित्व और योगदान
विशेषताएँ: आलमगीर द्वितीय एक धार्मिक, सादगी पसंद, और कमजोर शासक थे। उनकी नज़रबंदी के लंबे वर्षों ने उन्हें सैन्य और प्रशासनिक अनुभव से वंचित रखा, जिसके कारण वह इमाद-उल-मुल्क के नियंत्रण में रहे। सांस्कृतिक योगदान: उनके शासन में उर्दू साहित्य और सूफी परंपराओं को सीमित संरक्षण मिला, लेकिन कोई बड़ा सांस्कृतिक योगदान नहीं हुआ। प्रशासनिक योगदान: उनका कोई उल्लेखनीय प्रशासनिक योगदान नहीं था। इमाद-उल-मुल्क और अन्य दरबारियों ने शासन को नियंत्रित किया। सैन्य योगदान: उनके शासन में कोई सैन्य उपलब्धि नहीं थी। अब्दाली के आक्रमणों और मराठा-सिख विद्रोहों ने मुगल सत्ता को और कमजोर किया। विरासत: आलमगीर द्वितीय का शासन मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण दौर था। उनकी हत्या और पानीपत का तीसरा युद्ध (1761) मुगल सत्ता के अंतिम अवशेषों को समाप्त करने की दिशा में कदम थे।
7. मृत्यु और उत्तराधिकार
हत्या: 29 नवंबर 1759 को इमाद-उल-मुल्क के इशारे पर आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या का कारण उनकी स्वतंत्रता की कोशिश और मराठों के साथ संभावित गठजोड़ था। उत्तराधिकार: उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अली गौहर (शाह आलम द्वितीय) को सम्राट घोषित किया गया, लेकिन वह उस समय बिहार में थे। इमाद-उल-मुल्क ने संक्षिप्त रूप से शाहजहाँ तृतीय को सम्राट बनाया। शाह आलम द्वितीय ने 1760 में औपचारिक रूप से दिल्ली में सत्ता संभाली, लेकिन वह भी नाममात्र के शासक रहे। पानीपत का तीसरा युद्ध (1761): आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। मराठों की हार ने उनकी उत्तर भारत में विस्तार की आकांक्षाओं को रोक दिया और मुगल सत्ता को और कमजोर किया।
8. ऐतिहासिक संदर्भ और पतन का दौर
आलमगीर द्वितीय का शासन मुगल साम्राज्य के पतन के चरम दौर का प्रतीक है। औरंगजेब की मृत्यु (1707) के बाद उत्तराधिकार युद्ध, नादिर शाह का आक्रमण (1739), और क्षेत्रीय शक्तियों (मराठा, सिख, जाट) का उदय साम्राज्य को पहले ही कमजोर कर चुका था। अहमद शाह अब्दाली: अब्दाली के आक्रमणों ने पंजाब और दिल्ली को लूटा और मुगल सत्ता को नाममात्र का बना दिया। पानीपत का तीसरा युद्ध (1761) अब्दाली की शक्ति का प्रतीक था। मराठा और सिख: मराठों ने उत्तर भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पानीपत की हार ने उन्हें कमजोर किया। सिखों ने पंजाब में अपनी स्वायत्तता स्थापित की। यूरोपीय प्रभाव: अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध (आलमगीर द्वितीय के बाद) के माध्यम से बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। यह औपनिवेशिक शासन की शुरुआत थी।
Conclusion
Thanks For Read
jp Singh
searchkre.com@gmail.com
8392828781
 Gst Registration
Gst Registration
 DSC Registration
DSC Registration
 Pancard Registration
Pancard Registration
 Company Registration
Company Registration
 Fssai Registration
Fssai Registration
 TradeMark Registration
TradeMark Registration
 MSME Registration
MSME Registration
 Passport Registration
Passport Registration
 Income Tax Return
Income Tax Return
 LLP Company Registration
LLP Company Registration
 Marriage And Court Marriage Registration
Marriage And Court Marriage Registration
 PVT LTD Company Registration
PVT LTD Company Registration
 GST Filing Services
GST Filing Services
 Coaching Insititute Registration
Coaching Insititute Registration
 GYM Registration
GYM Registration
 NGO Registration
NGO Registration
 Political Party Registration
Political Party Registration
 Society Registration
Society Registration
 Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
 Make Website on EMI
Make Website on EMI



























































































 9th Class Scholarship Competition Test
9th Class Scholarship Competition Test
 10th Class Scholarship Competition Test
10th Class Scholarship Competition Test
 11th Class Scholarship Competition Test
11th Class Scholarship Competition Test
 12th Class Scholarship Competition Test
12th Class Scholarship Competition Test
 Graduation Scholarship Competition Test
Graduation Scholarship Competition Test
 Post Graduation Scholarship Competition Test
Post Graduation Scholarship Competition Test
 Diploma Scholarship Competition Test
Diploma Scholarship Competition Test
 Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 JEE Coaching Scholarship Competition Test
JEE Coaching Scholarship Competition Test
 NEET Coaching Scholarship Competition Test
NEET Coaching Scholarship Competition Test
 Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test















































.png)