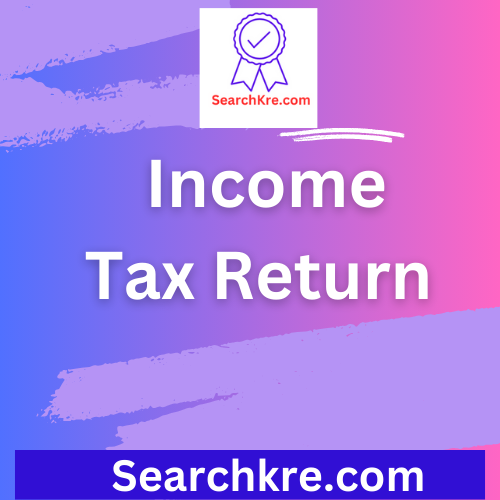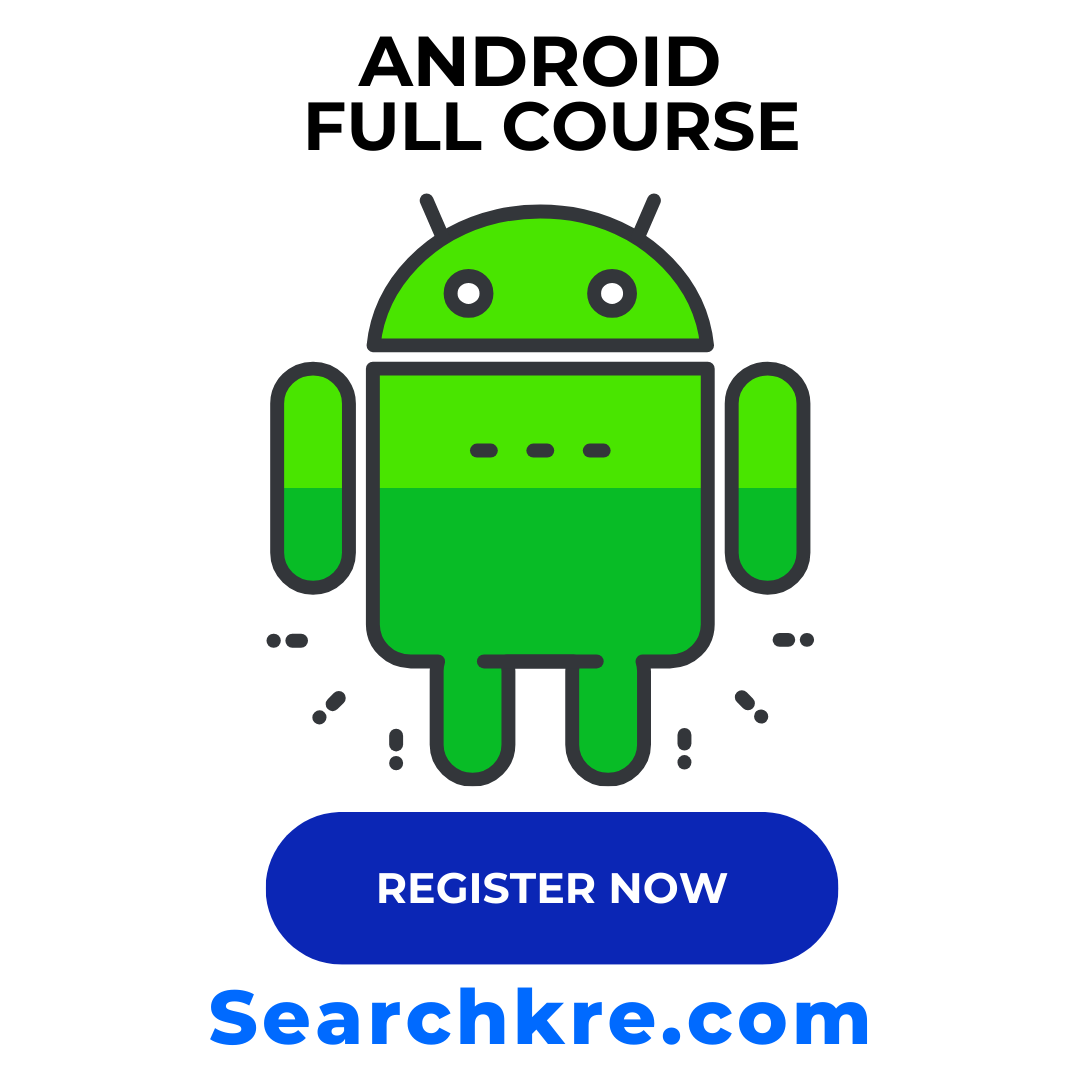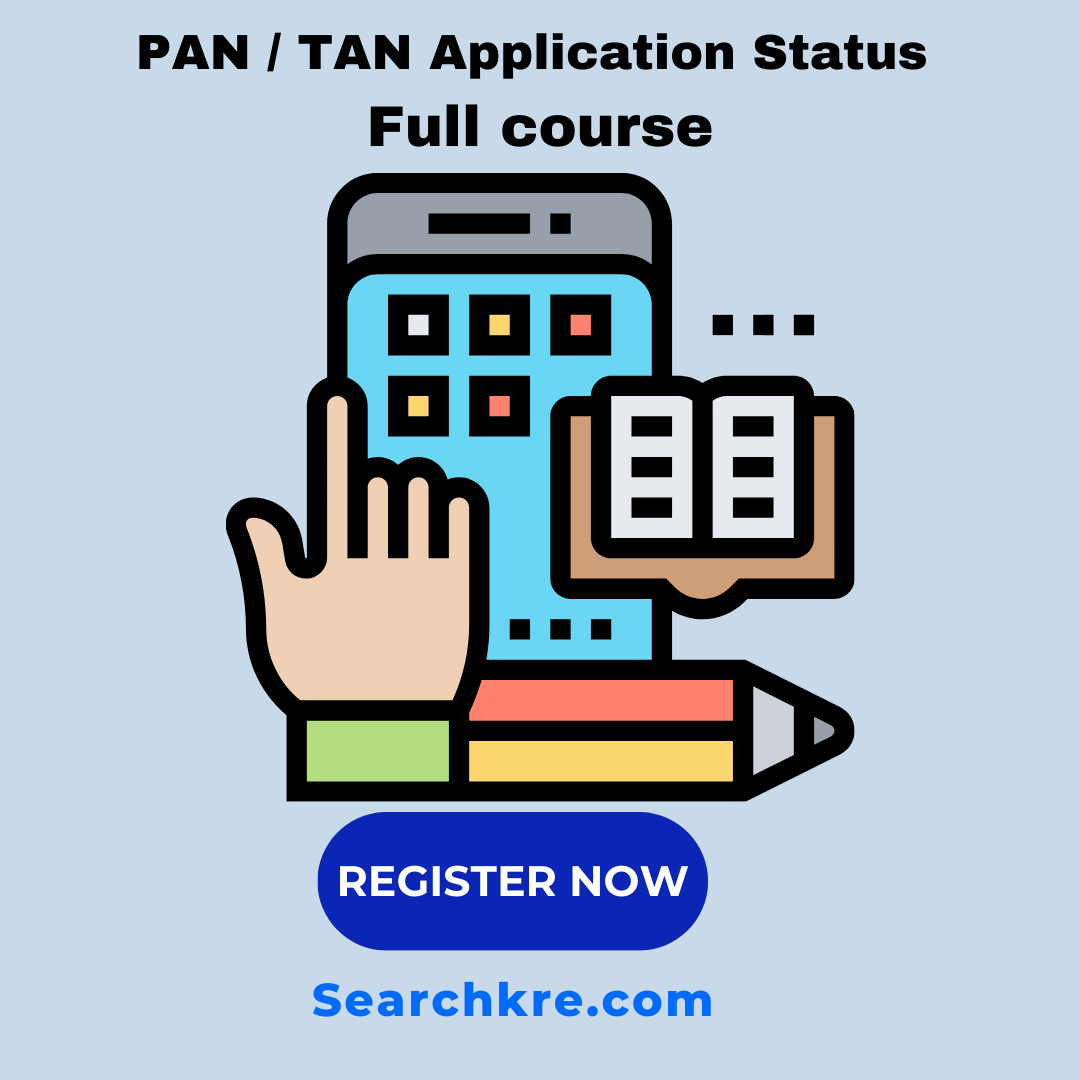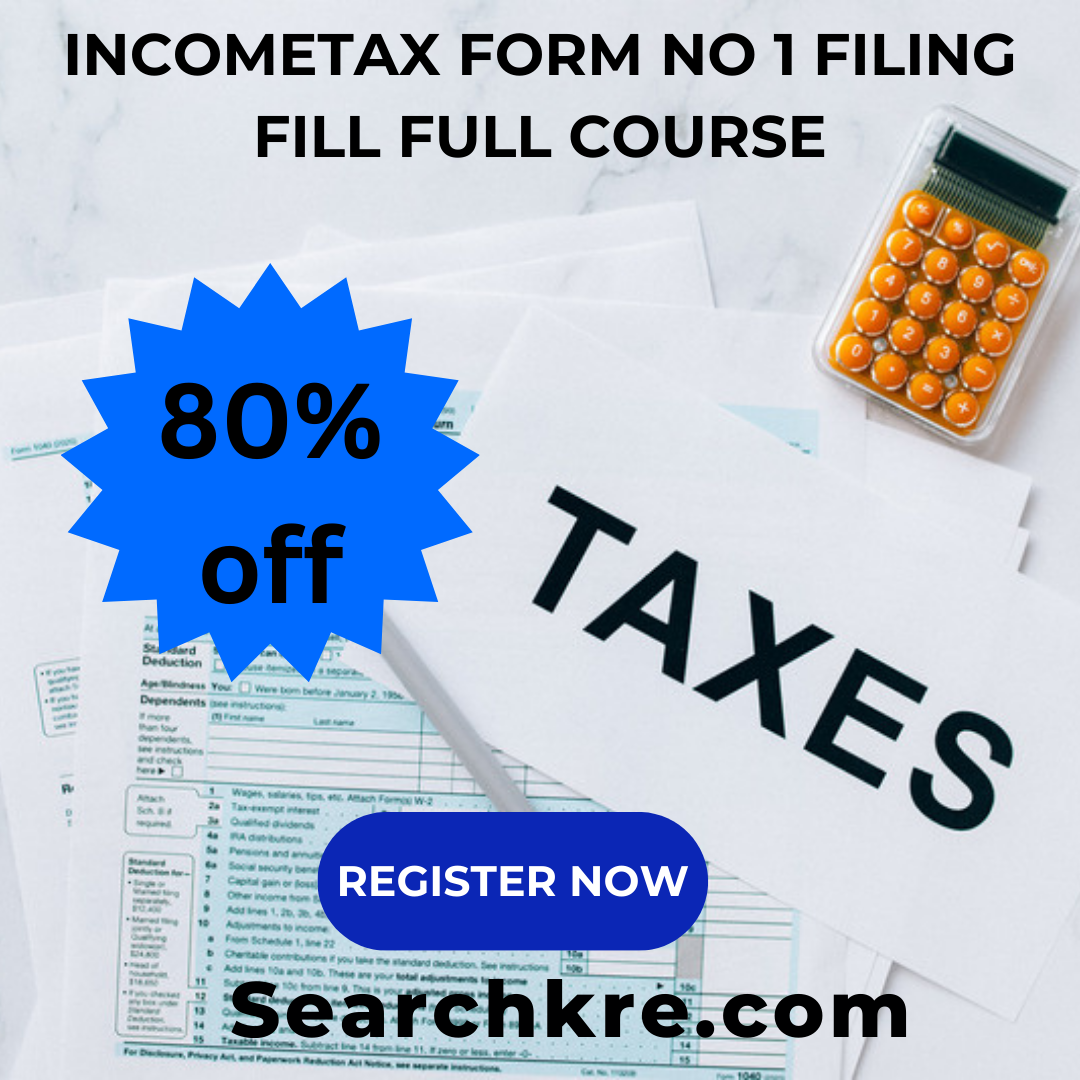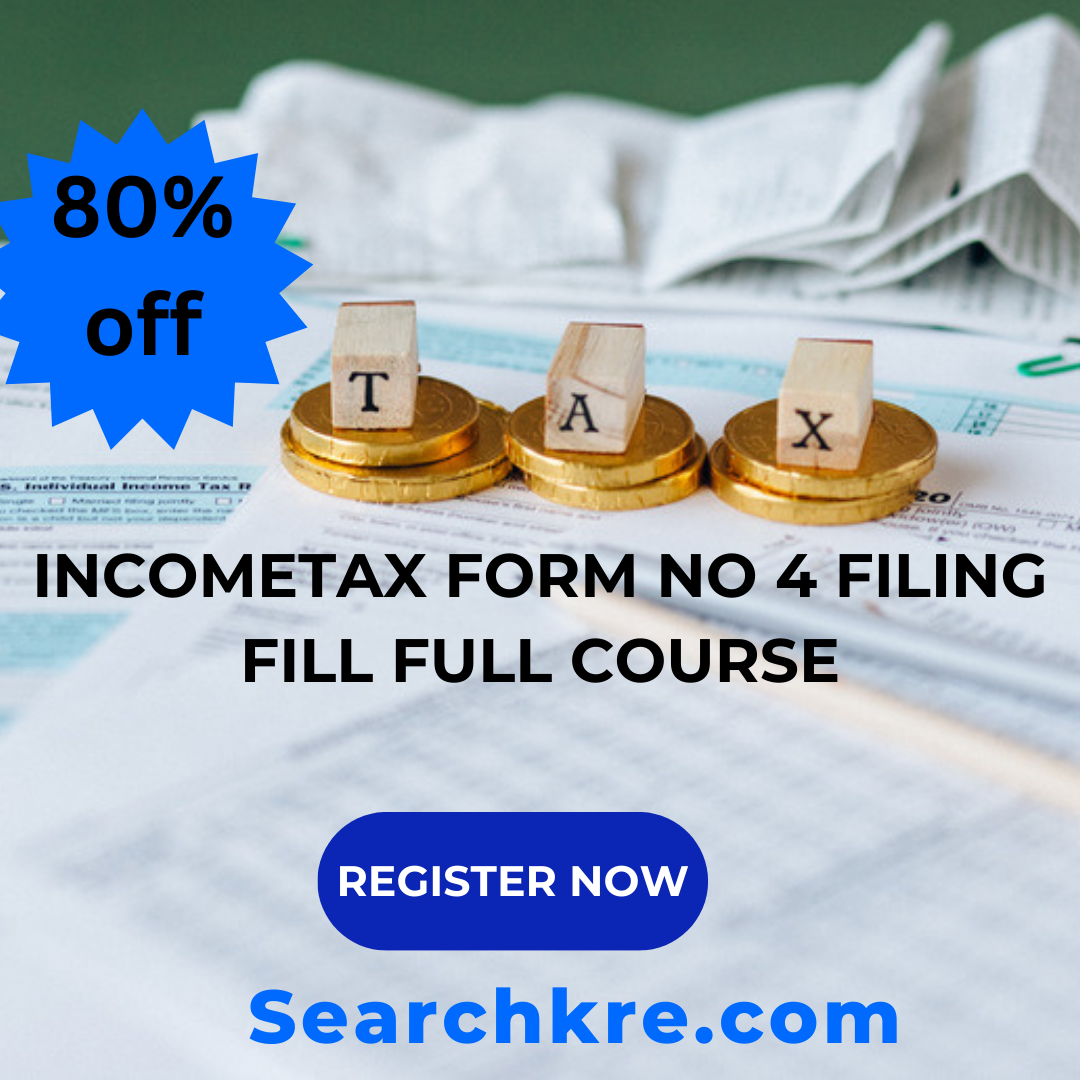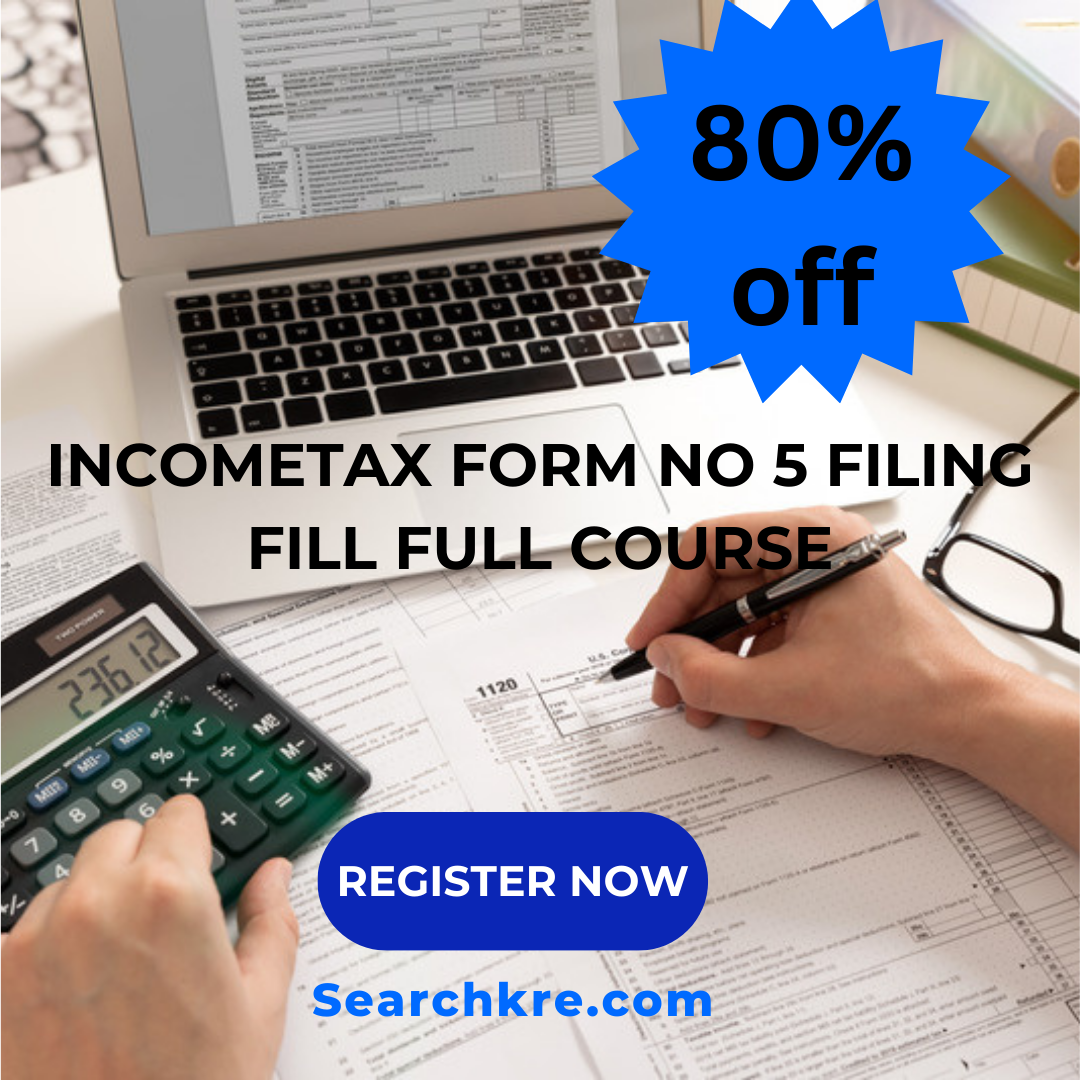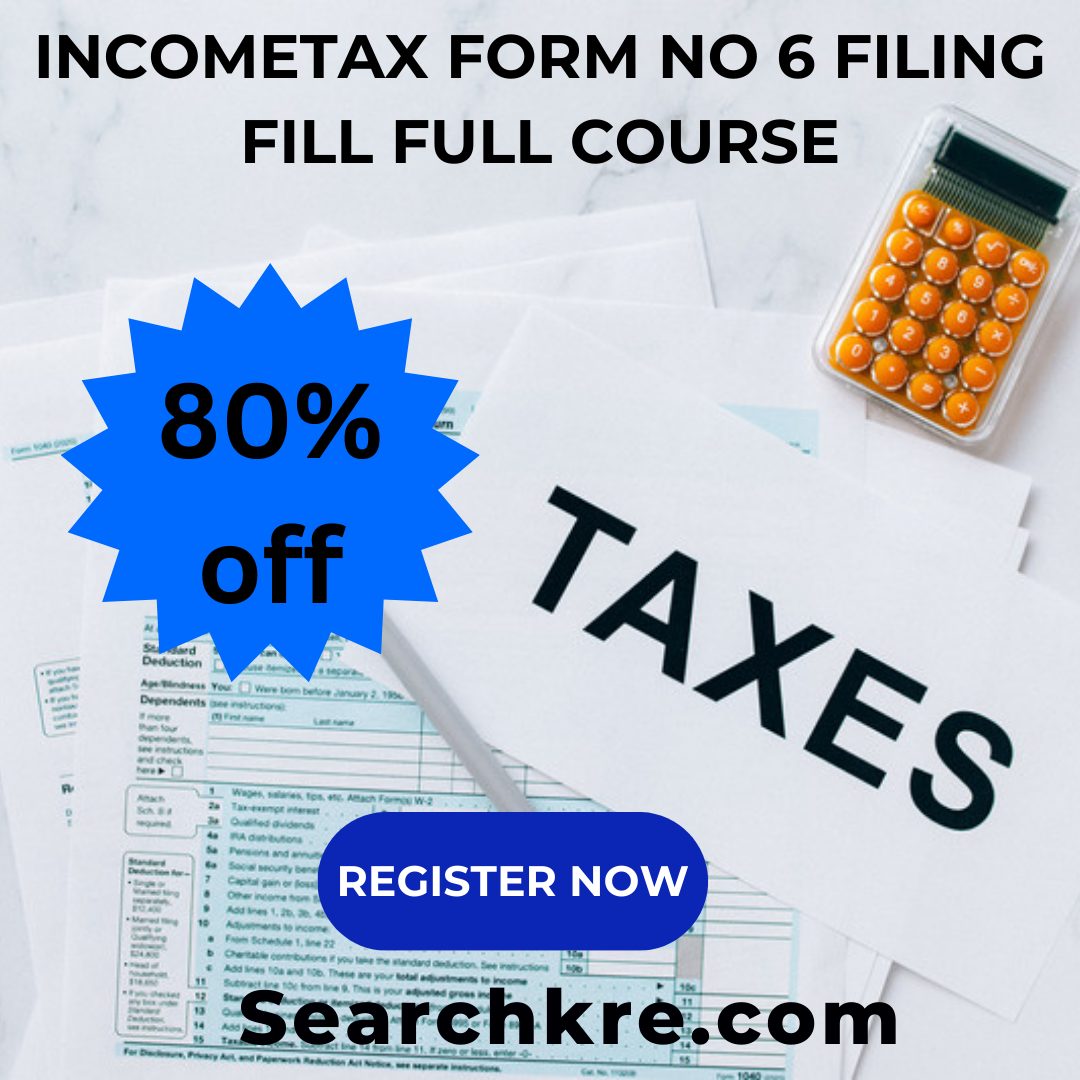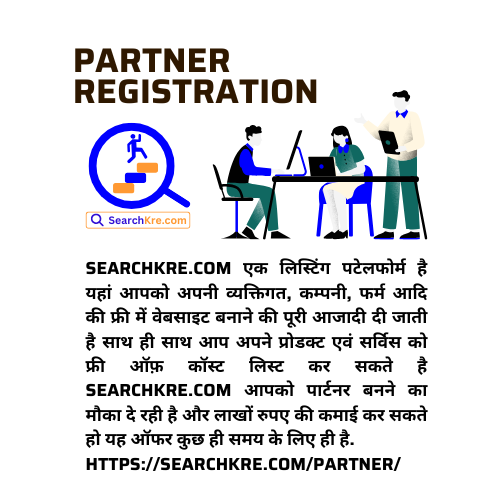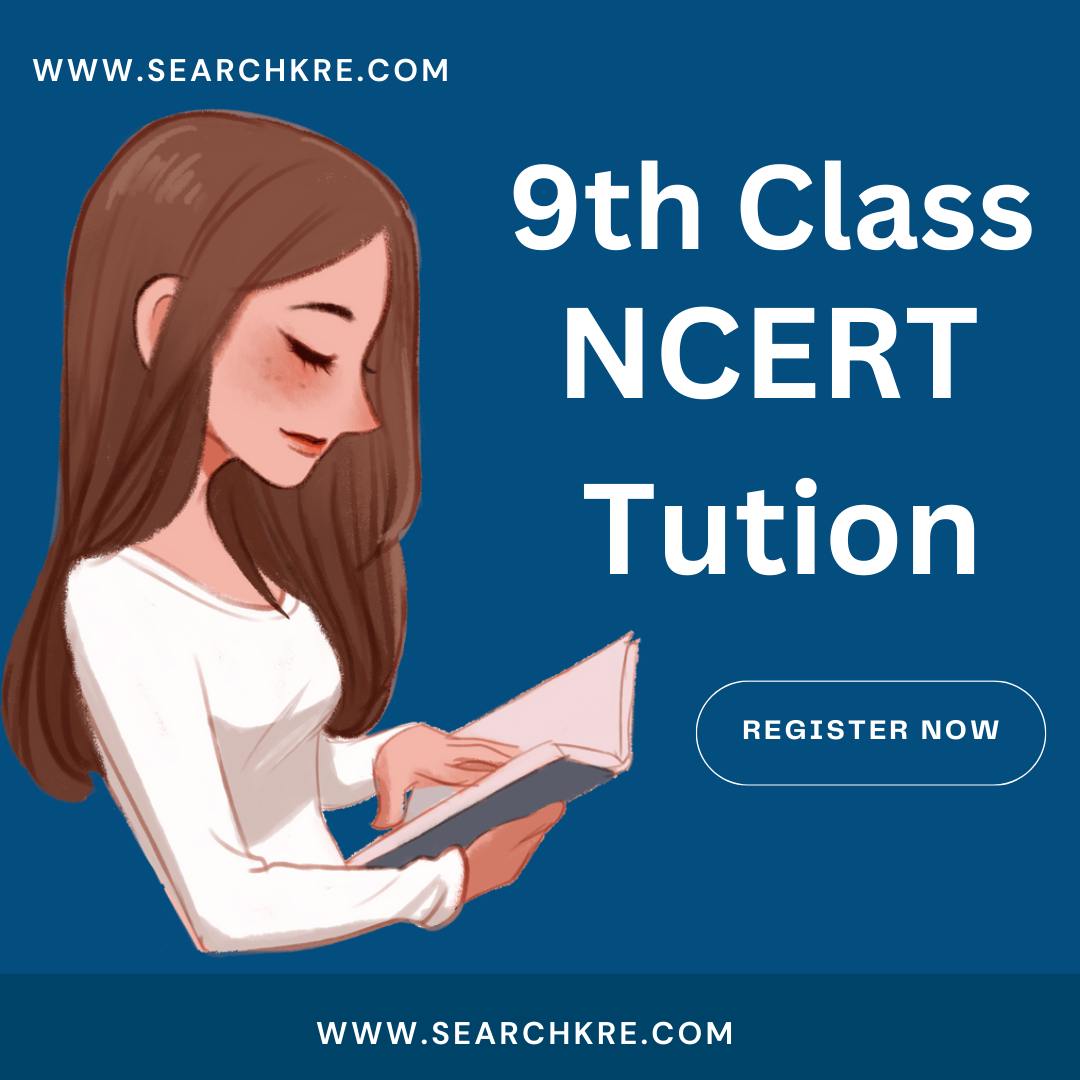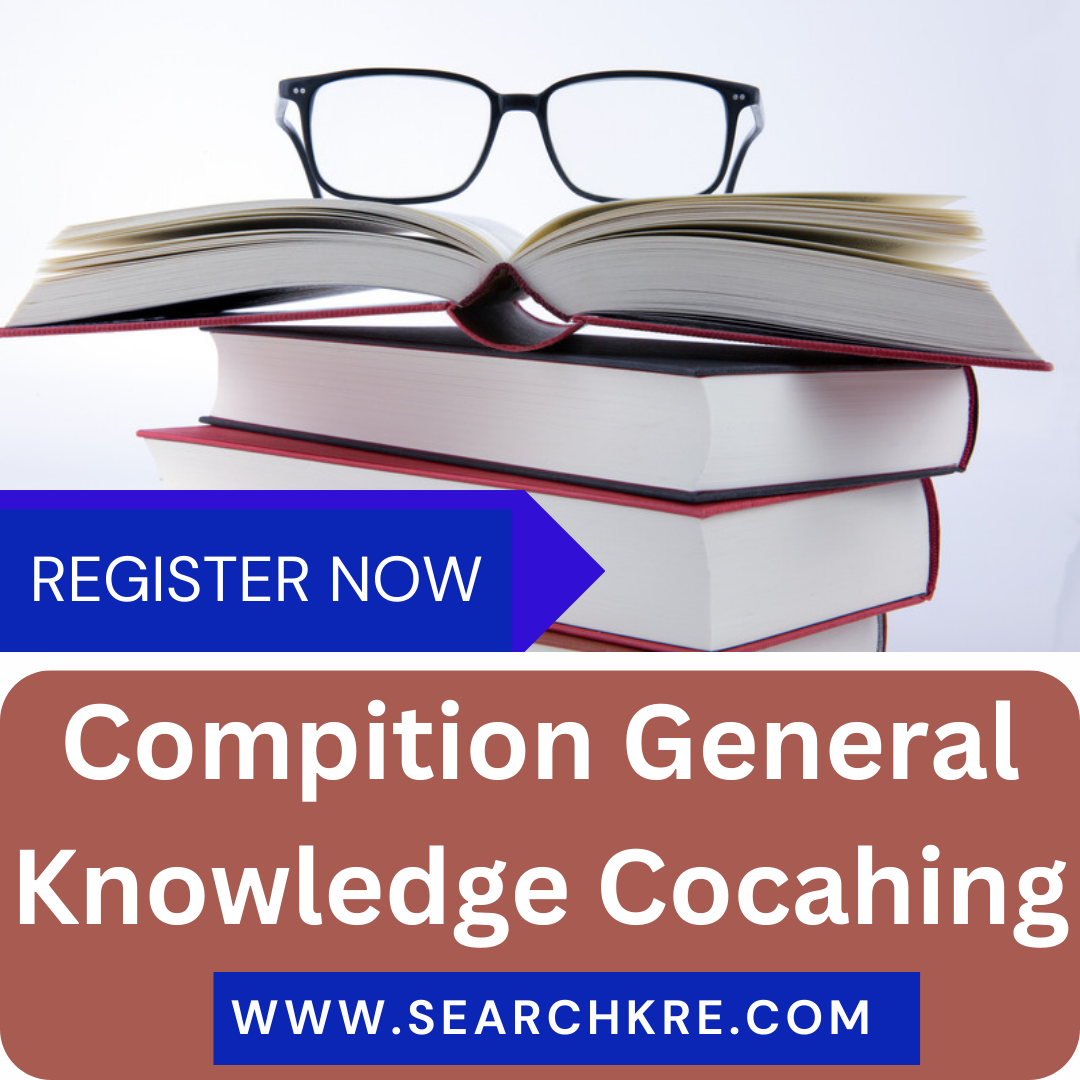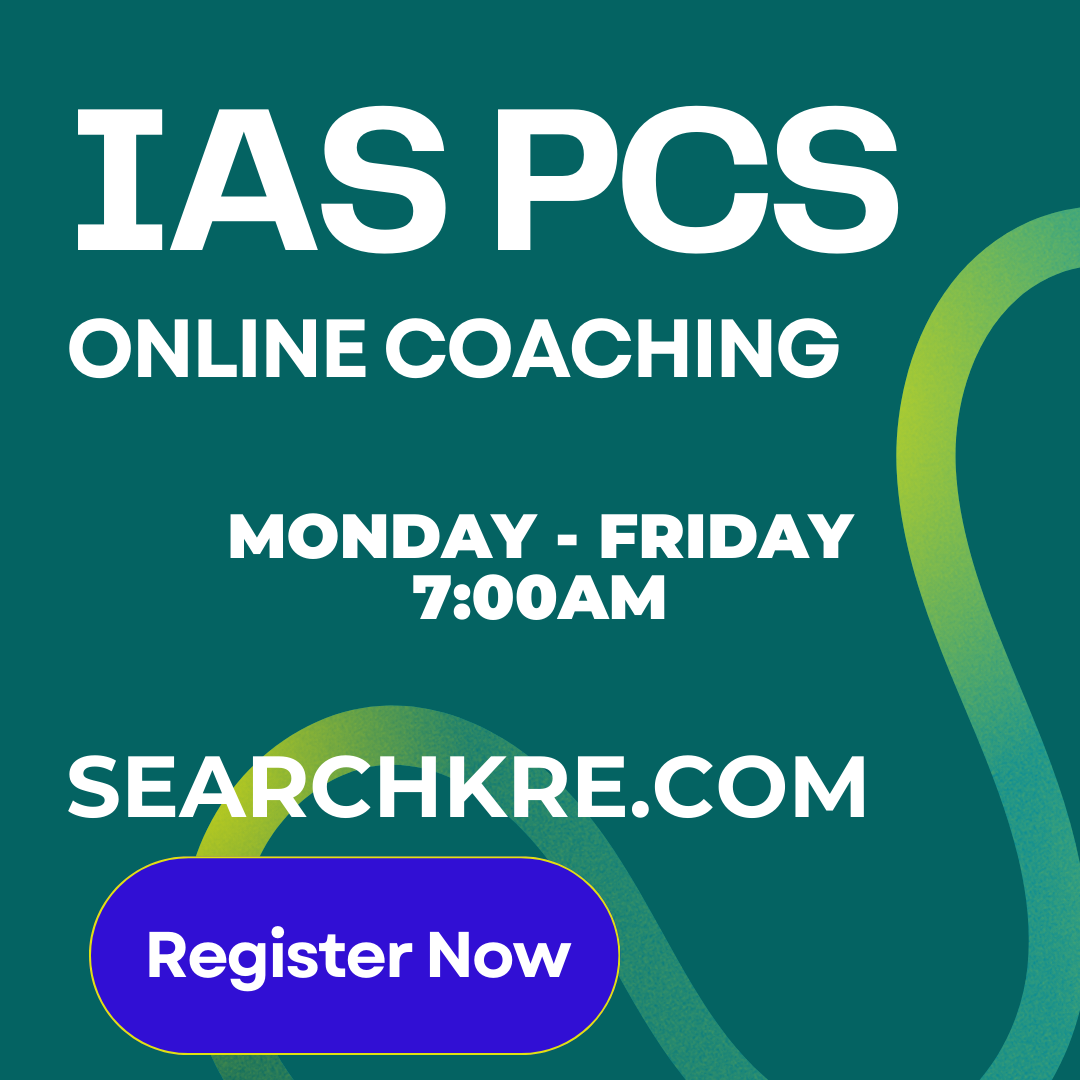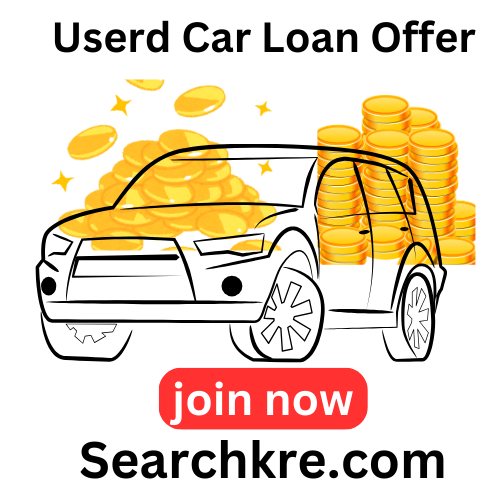.png)
Akbar (1542-1605)
jp Singh
2025-05-27 10:18:50
searchkre.com@gmail.com /
8392828781
अकबर (1542-1605 ई.)
अकबर (1542-1605 ई.)
अकबर (1542-1605 ई.), जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था, मुगल साम्राज्य के तीसरे और सबसे महान शासक थे। उनका शासनकाल (1556-1605) मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, और संस्कृति में अभूतपूर्व प्रगति हुई। अकबर ने अपनी दूरदर्शिता, धार्मिक सहिष्णुता, और संगठनात्मक क्षमता के माध्यम से एक विशाल और स्थिर साम्राज्य स्थापित किया। नीचे उनके जीवन, शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, और योगदान का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है:
1. प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि
जन्म: अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट (सिंध, वर्तमान पाकिस्तान) में हुआ था। वह हुमायूँ और उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के पुत्र थे। उस समय हुमायूँ निर्वासन में थे, और अकबर का जन्म एक कठिन परिस्थिति में हुआ।
शिक्षा: अकबर को औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, और वह पढ़ना-लिखना नहीं सीख पाया। फिर भी, वह अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु था। उसे मौखिक रूप से इतिहास, साहित्य, और दर्शन की शिक्षा दी गई। वह फारसी, तुर्की, और हिंदुस्तानी भाषाएँ समझता था।
प्रारंभिक जिम्मेदारियाँ: हुमायूँ ने उसे कम उम्र में ही प्रशासनिक और सैन्य अनुभव के लिए तैयार किया। 1555 में हुमायूँ की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का था।
2. शासनकाल और सैन्य अभियान
अकबर का शासनकाल दो चरणों में बाँटा जा सकता है: प्रारंभिक चरण (1556-1570), जब वह बैरम खान के संरक्षण में था, और स्वतंत्र शासन (1570-1605), जब उसने स्वयं साम्राज्य का विस्तार और संगठन किया।
प्रारंभिक शासन और बैरम खान का संरक्षण (1556-1560) सिंहासनारोहण: 1556 में हुमायूँ की मृत्यु के बाद अकबर ने 14 वर्ष की आयु में दिल्ली में सिंहासन ग्रहण किया। उस समय बैरम खान उसका संरक्षक और रीजेंट था। पानीपत का द्वितीय युद्ध (1556): बैरम खान ने हेमू (सूरी शासक आदिल शाह का सेनापति) को हराकर दिल्ली पर मुगल नियंत्रण को पुनर्स्थापित किया। इस युद्ध में अकबर ने नाममात्र की भूमिका निभाई। प्रारंभिक चुनौतियाँ: सूरी शासकों, अफ़गानों, और आंतरिक विद्रोहों (जैसे उज़्बेक सरदारों) ने अकबर के प्रारंभिक शासन को अस्थिर करने की कोशिश की। स्वतंत्र शासन और साम्राज्य विस्तार (1560-1605) बैरम खान का अंत: 1560 में अकबर ने बैरम खान को हटाकर स्वतंत्र शासन शुरू किया। बैरम खान की विद्रोही गतिविधियों के कारण 1561 में उसकी हत्या हो गई।
प्रमुख सैन्य अभियान: मालवा (1561): अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर को हराया और क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में मिलाया। राजपूत नीति: अकबर ने राजपूतों को युद्ध और कूटनीति दोनों से अपने साथ जोड़ा। उसने आमेर के राजा भगवान दास और मानसिंह को अपने प्रशासन में शामिल किया। 1562 में आमेर की राजकुमारी जोधा बाई से विवाह ने राजपूत-मुगल गठबंधन को मज़बूत किया। चित्तौड़ (1568): अकबर ने मेवाड़ के राणा उदय सिंह को हराया, जिससे राजपूतों पर मुगल प्रभाव बढ़ा। हालाँकि, राणा प्रताप ने मेवाड़ में प्रतिरोध जारी रखा। हल्दीघाटी का युद्ध (1576): अकबर के सेनापति मानसिंह ने राणा प्रताप को हराया, लेकिन प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध जारी रखा।
गुजरात (1572-1573): अकबर ने गुजरात पर कब्ज़ा किया, जो व्यापार और समृद्धि का केंद्र था। बंगाल और बिहार (1574-1576): दाउद खान कर्रानी को हराकर पूर्वी भारत को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। कश्मीर, सिंध, और बलूचिस्तान (1586-1595): इन क्षेत्रों को जीतकर अकबर ने उत्तर-पश्चिमी भारत में अपनी सत्ता मज़बूत की। दक्कन अभियान: अकबर ने दक्कन में खानदेश (1601) पर कब्ज़ा किया, लेकिन पूर्ण दक्कन विजय अधूरी रही। साम्राज्य का विस्तार: अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य कश्मीर से बंगाल और दक्कन तक फैल गया, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था।
3. प्रशासन
अकबर का प्रशासन अत्यधिक संगठित और केंद्रीकृत था। उसने तुर्की-मंगोल परंपराओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाला और कई सुधार किए।
केंद्रीय शासन सम्राट की भूमिका: अकबर को 'ज़िल्ले-इलाही' (ईश्वर की छाया) माना जाता था। वह प्रशासन, सेना, और न्याय का केंद्र था। उसकी नीति 'सुलह-ए-कुल' (सार्वभौमिक सहिष्णुता) ने सभी धर्मों और समुदायों को एकजुट किया। मंत्रिपरिषद: अकबर को वज़ीर (प्रधानमंत्री), दीवान-ए-आला (वित्त मंत्री), मीर बख्शी (सेना प्रमुख), और सadr-us-sudur (धार्मिक मामलों का प्रमुख) सहायता करते थे। अबुल फज़ल, फैज़ी, और राजा टोडरमल जैसे विद्वान और प्रशासक उसके दरबार में थे। न्याय व्यवस्था: अकबर ने इस्लामी कानून (शरिया) के साथ-साथ गैर-मुस्लिमों के लिए उनकी परंपरागत व्यवस्थाओं को मान्यता दी। उसने जज़िया (गैर-मुस्लिमों पर कर) समाप्त किया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। क़ाज़ी और स्थानीय पंचायतें छोटे-मोटे विवादों का निपटारा करती थीं।
प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन सूबे: साम्राज्य को 15 सूबों (प्रांतों) में बाँटा गया था, जैसे दिल्ली, आगरा, लाहौर, बंगाल, और गुजरात। प्रत्येक सूबे का प्रशासन सूबेदार (गवर्नर) के अधीन था। मनसबदारी प्रणाली: अकबर ने इस प्रणाली को औपचारिक रूप दिया। मनसबदारों को 'ज़ात' (पद) और 'सवार' (घुड़सवारों की संख्या) के आधार पर रैंक दी जाती थी। उन्हें जागीरें दी जाती थीं, जिनसे वे अपनी सेना और प्रशासन का खर्च उठाते थे। ज़ब्त प्रणाली: राजा टोडरमल ने भूमि की पैमाइश और कर निर्धारण के लिए ज़ब्त प्रणाली लागू की। इसमें उपज का एक-तिहाई हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। यह प्रणाली निष्पक्ष और प्रभावी थी। स्थानीय प्रशासन: परगना (तहसील) स्तर पर आमिल और चौधरी कर संग्रह करते थे। गाँवों में पंचायतें और मुखिया स्थानीय शासन संभालते थे।
सैन्य संगठन सेना: अकबर की सेना में घुड़सवार, पैदल सैनिक, तोपखाना, और हाथी शामिल थे। उसने तोपखाने को मज़बूत किया और नियमित सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया। नौसेना: अकबर ने बंगाल और गुजरात में नौसेना को विकसित किया, जो व्यापार और तटीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी। किलों की रक्षा: आगरा, दिल्ली, लाहौर, और इलाहाबाद जैसे किलों को मज़बूत किया गया। 4. अर्थव्यवस्था अकबर के शासनकाल में अर्थव्यवस्था समृद्ध और संगठित थी। कृषि, व्यापार, और उद्योगों ने भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया।
कृषि प्रमुख फसलें: गेहूँ, चावल, जौ, कपास, नील, तंबाकू, और गन्ना प्रमुख फसलें थीं। नकदी फसलों ने अर्थव्यवस्था को और समृद्ध किया। सिंचाई: नहरों, कुओं, और तालाबों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया। यमुना नहर (बाद में शाहनाहर) इसका उदाहरण है। ज़ब्त प्रणाली: राजा टोडरमल ने भूमि की पैमाइश और कर निर्धारण के लिए इस प्रणाली को लागू किया। इसमें दस साल की औसत उपज (दहसाला) के आधार पर कर तय किया जाता था। कर नकद या उपज के रूप में लिया जाता था।
जागीर प्रणाली: मनसबदारों को जागीरें दी जाती थीं, लेकिन अकबर ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए जागीरों का नियमित हस्तांतरण शुरू किया। व्यापार आंतरिक व्यापार: दिल्ली, आगरा, लाहौर, और सूरत जैसे शहर व्यापारिक केंद्र थे। शेरशाह द्वारा बनाई गई ग्रांड ट्रंक रोड और सरायों ने व्यापार को सुगम बनाया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार: सूरत, खंभात, और बंगाल के बंदरगाहों से यूरोप, फारस, मध्य एशिया, और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार होता था। मसाले, कपास, रेशम, और नील निर्यात किए जाते थे, जबकि सोना, चांदी, और घोड़े आयात होते थे। यूरोपीय व्यापारी: पुर्तगाली, डच, और अंग्रेज व्यापारी सक्रिय थे। 1600 में अकबर ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति दी।
मुद्रा अकबर ने सोने (मुहर), चांदी (रुपया), और तांबे (दाम) के सिक्के प्रचलित किए। ये सिक्के उच्च गुणवत्ता वाले और मानकीकृत थे, जिसने व्यापार को विश्वसनीय बनाया। टकसालों (जैसे दिल्ली, आगरा, और सूरत) में सिक्कों का उत्पादन केंद्रीकृत था। उद्योग कपड़ा उद्योग: बंगाल और गुजरात में सूती और रेशमी वस्त्रों का उत्पादन विश्व प्रसिद्ध था। ढाका की मलमल और बनारस की साड़ियाँ विशेष थीं। हस्तशिल्प: आभूषण, कालीन, और धातु कार्य (जैसे बीदरी कला) में उन्नति हुई। निर्माण उद्योग: मस्जिदों, किलों, और शहरों (जैसे फतेहपुर सीकरी) के निर्माण ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया।
5. समाज
अकबर का समाज बहु-धार्मिक और बहु-सांस्कृतिक था। उसकी सहिष्णु नीतियों ने हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, जिसे 'गंगा-जमुनी तहज़ीब' कहा जाता है।
सामाजिक संरचना अभिजात वर्ग: मनसबदार, जागीरदार, और राजपूत सरदार समाज के शीर्ष पर थे। अकबर ने हिंदुओं (जैसे मानसिंह, टोडरमल) को उच्च पदों पर नियुक्त किया। मध्यम और निम्न वर्ग: व्यापारी, कारीगर, और किसान समाज का बड़ा हिस्सा थे। ज़ब्त प्रणाली ने किसानों पर कर का बोझ कम किया। जाति व्यवस्था: हिंदू समाज में वर्ण और जाति व्यवस्था प्रचलित थी, लेकिन अकबर ने इसे हस्तक्षेप किए बिना स्वीकार किया।
धर्म सुलह-ए-कुल: अकबर की यह नीति सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और समानता पर आधारित थी। उसने जज़िया (1579) और तीर्थयात्रा कर समाप्त किया। दीन-ए-इलाही (1582): अकबर ने एक नए धार्मिक दर्शन की शुरुआत की, जो हिंदू, इस्लाम, जैन, पारसी, और ईसाई धर्मों के तत्वों का मिश्रण था। यह धार्मिक सुधार से अधिक एक राजनैतिक और नैतिक दर्शन था। इसे बहुत कम लोग (जैसे बीरबल और अबुल फज़ल) अपनाया। धार्मिक सहिष्णुता: अकबर ने हिंदू मंदिरों, जैन तीर्थस्थलों, और सिख गुरुओं को संरक्षण दिया। उसने गुरु अमरदास और गुरु रामदास से मुलाकात की। इबादतखाना: 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादतखाना (प्रार्थना गृह) स्थापित किया, जहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वान बहस करते थे।
महिलाओं की स्थिति उच्च वर्ग: मुगल हरम में महिलाएँ प्रभावशाली थीं। अकबर की माता हमीदा बानो और पत्नी जोधा बाई ने सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। सामान्य वर्ग: पर्दा प्रथा, बाल-विवाह, और सती प्रथा प्रचलित थीं। अकबर ने सती प्रथा और बाल-विवाह पर अंकुश लगाने की कोशिश की। शिक्षा: उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त थी। गुलबदन बेगम (अकबर की चाची) ने 'हुमायूँनामा' लिखा। शिक्षा और संस्कृति शिक्षा: अकबर ने मस्जिदों, मकतबों, और मदरसों में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। उसने संस्कृत ग्रंथों (जैसे महाभारत और रामायण) का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसे 'रज़्मनामा' कहा गया। साहित्य: अबुल फज़ल की 'आइन-ए-अकबरी' और 'अकबरनामा', फैज़ी की कविताएँ, और बदायूंनी की रचनाएँ इस युग की प्रमुख कृतियाँ थीं। अकबर ने तुलसीदास और सूरदास जैसे भक्ति कवियों को भी संरक्षण दिया।
वास्तुकला: अकबर ने फतेहपुर सीकरी (1571-1585) को अपनी राजधानी बनाया, जहाँ बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, और पंचमहल जैसे स्मारक बनाए गए। आगरा किला और लाहौर किला भी उसकी वास्तुकला की देन हैं। उसकी वास्तुकला में हिंदू, फारसी, और इस्लामी शैलियों का मिश्रण था। चित्रकला: अकबर ने मुगल लघुचित्र (मिनिएचर पेंटिंग) को प्रोत्साहन दिया। उसके दरबार में दासवंत और बसावन जैसे चित्रकार थे। 'रज़्मनामा' और 'तुतीनामा' में चित्रण उल्लेखनीय है। संगीत: तानसेन, बैजू बावरा, और अन्य संगीतकारों को अकबर का संरक्षण प्राप्त था। ध्रुपद और ख्याल गायकी का विकास हुआ।
6. व्यक्तित्व और योगदान
विशेषताएँ: अकबर एक दूरदर्शी, सहिष्णु, और बुद्धिमान शासक था। वह जिज्ञासु था और विभिन्न धर्मों, दर्शनों, और संस्कृतियों को समझने में रुचि रखता था। उसकी सैन्य रणनीति, प्रशासनिक सुधार, और धार्मिक नीतियाँ अद्वितीय थीं। सांस्कृतिक योगदान: अकबर ने हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, जिसे 'गंगा-जमुनी तहज़ीब' कहा जाता है। उसकी कला, वास्तुकला, और साहित्य ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। प्रशासनिक सुधार: मनसबदारी और ज़ब्त प्रणाली ने मुगल शासन को संगठित और स्थिर बनाया। ये सुधार बाद के शासकों के लिए आधार बने। धार्मिक सहिष्णुता: सुलह-ए-कुल और दीन-ए-इलाही ने धार्मिक एकता को बढ़ावा दिया, जो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। सैन्य संगठन: अकबर ने सेना को पुनर्गठित किया और तोपखाने को मज़बूत किया, जिसने साम्राज्य के विस्तार को संभव बनाया।
7. मृत्यु और विरासत
मृत्यु: अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को आगरा में पेचिश (डायसेंट्री) के कारण हुई। उसने अपने पुत्र जहाँगीर को उत्तराधिकारी बनाया। विरासत: अकबर ने एक विशाल, संगठित, और समृद्ध साम्राज्य छोड़ा, जो भारत के इतिहास में स्वर्ण युग का प्रतीक है। उसकी नीतियों ने मुगल साम्राज्य को 200 वर्षों तक स्थिर रखा। फतेहपुर सीकरी, आइन-ए-अकबरी, और उसकी धार्मिक सहिष्णुता आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। स्मारक: फतेहपुर सीकरी और अकबर का मकबरा (सिकंदरा, आगरा) उसकी स्थायी विरासत के प्रतीक हैं।
Conclusion
Thanks For Read
jp Singh
searchkre.com@gmail.com
8392828781
 Gst Registration
Gst Registration
 DSC Registration
DSC Registration
 Pancard Registration
Pancard Registration
 Company Registration
Company Registration
 Fssai Registration
Fssai Registration
 TradeMark Registration
TradeMark Registration
 MSME Registration
MSME Registration
 Passport Registration
Passport Registration
 Income Tax Return
Income Tax Return
 LLP Company Registration
LLP Company Registration
 Marriage And Court Marriage Registration
Marriage And Court Marriage Registration
 PVT LTD Company Registration
PVT LTD Company Registration
 GST Filing Services
GST Filing Services
 Coaching Insititute Registration
Coaching Insititute Registration
 GYM Registration
GYM Registration
 NGO Registration
NGO Registration
 Political Party Registration
Political Party Registration
 Society Registration
Society Registration
 Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
 Make Website on EMI
Make Website on EMI



























































































 9th Class Scholarship Competition Test
9th Class Scholarship Competition Test
 10th Class Scholarship Competition Test
10th Class Scholarship Competition Test
 11th Class Scholarship Competition Test
11th Class Scholarship Competition Test
 12th Class Scholarship Competition Test
12th Class Scholarship Competition Test
 Graduation Scholarship Competition Test
Graduation Scholarship Competition Test
 Post Graduation Scholarship Competition Test
Post Graduation Scholarship Competition Test
 Diploma Scholarship Competition Test
Diploma Scholarship Competition Test
 Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 JEE Coaching Scholarship Competition Test
JEE Coaching Scholarship Competition Test
 NEET Coaching Scholarship Competition Test
NEET Coaching Scholarship Competition Test
 Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test















































.png)