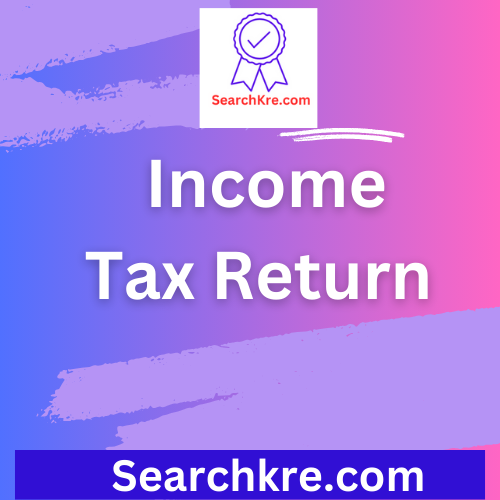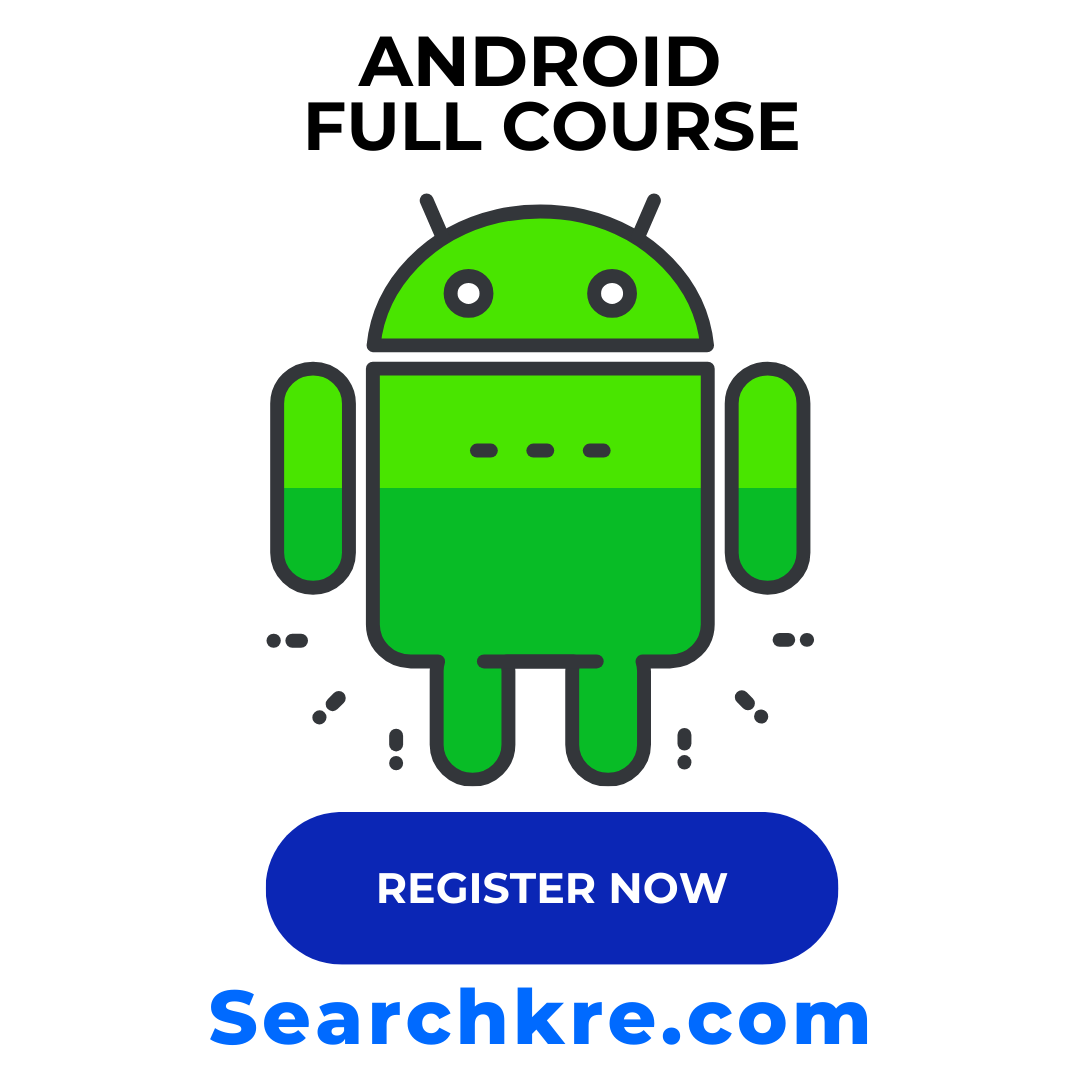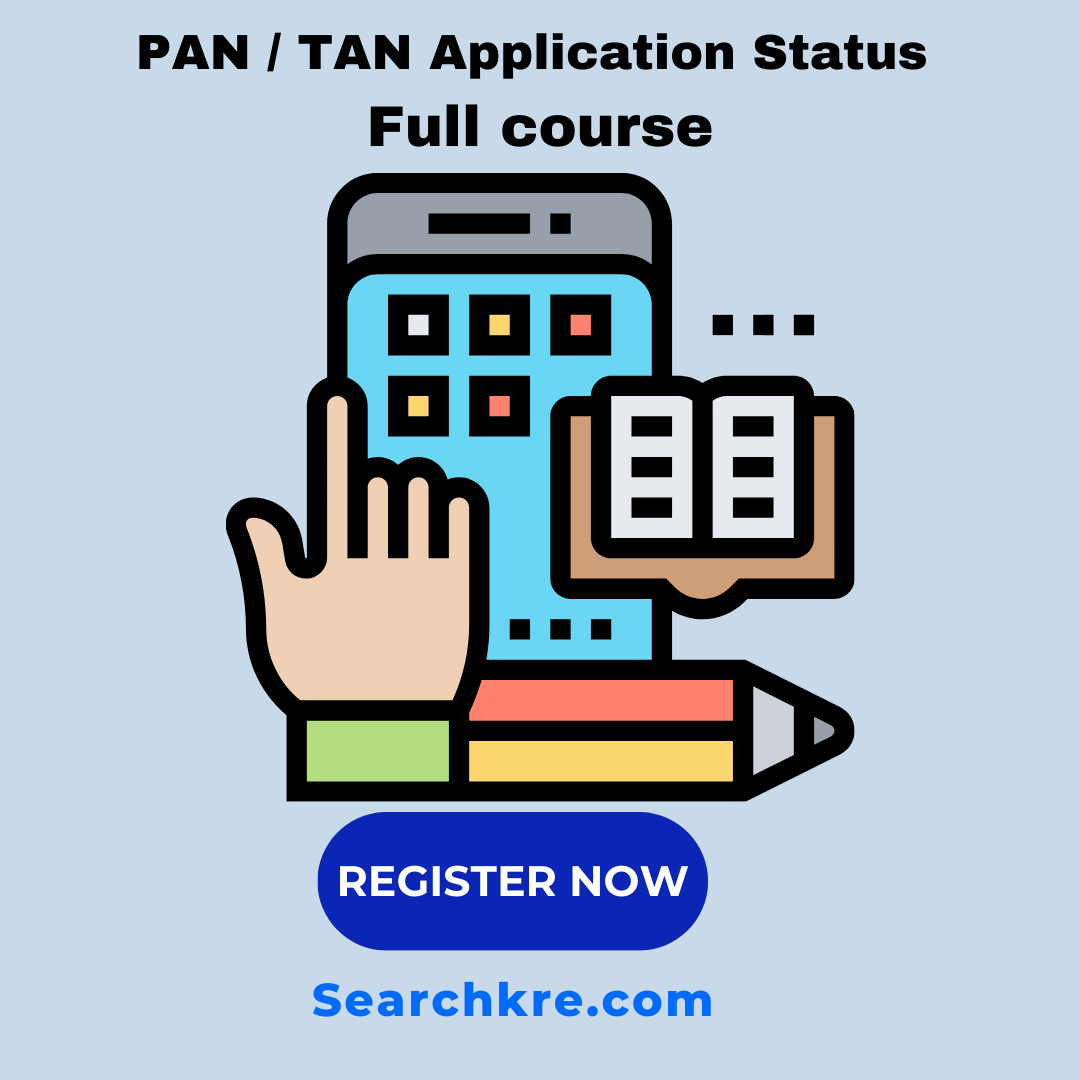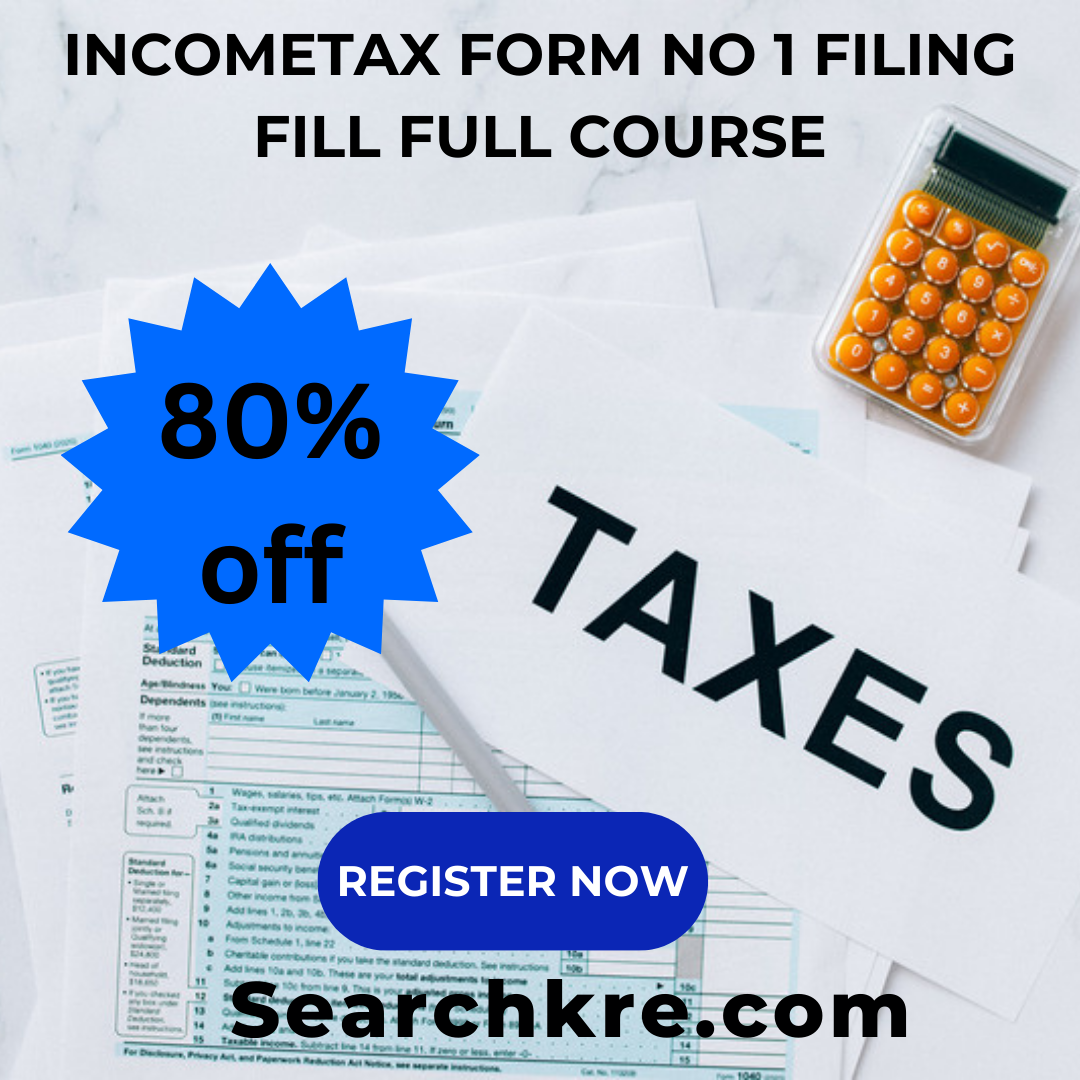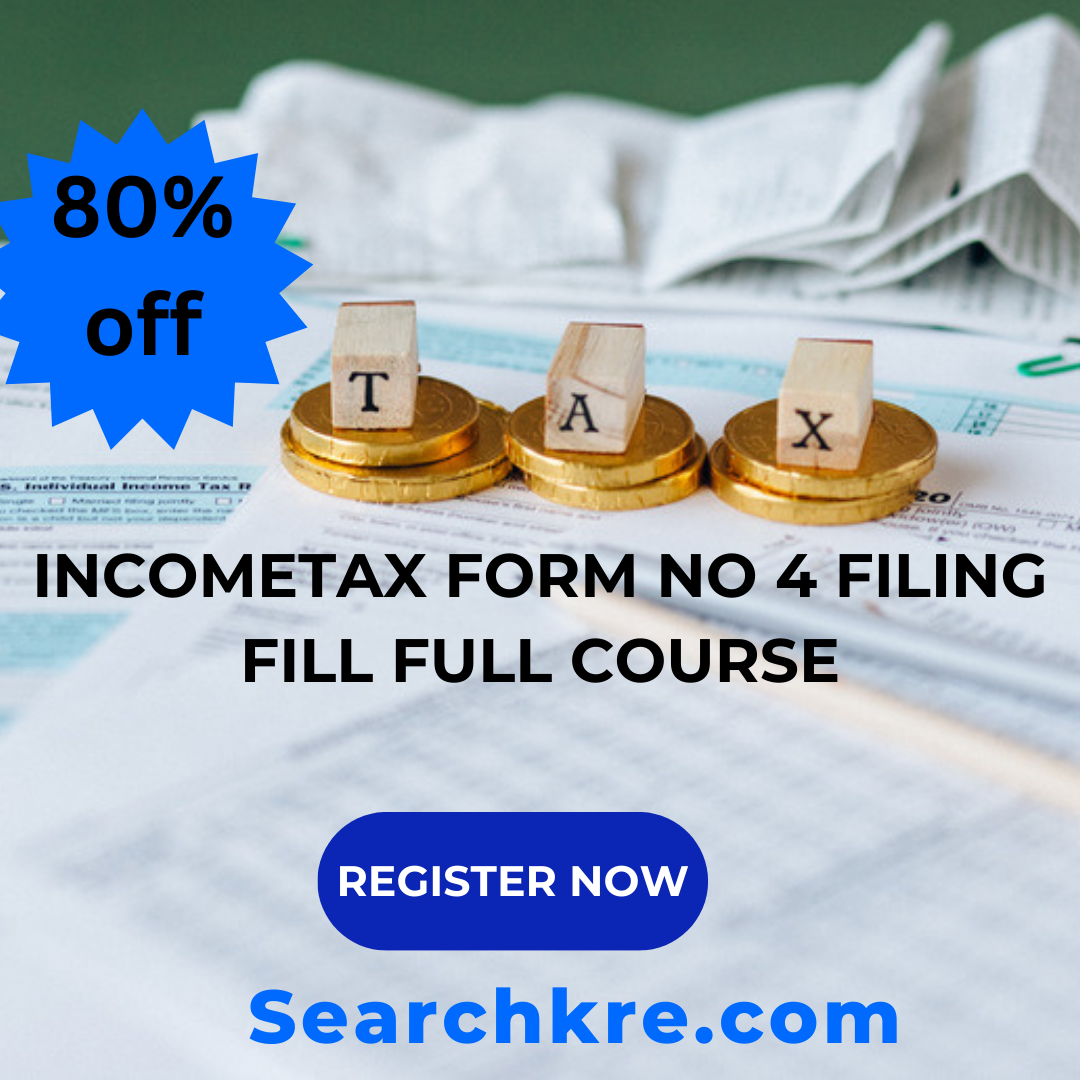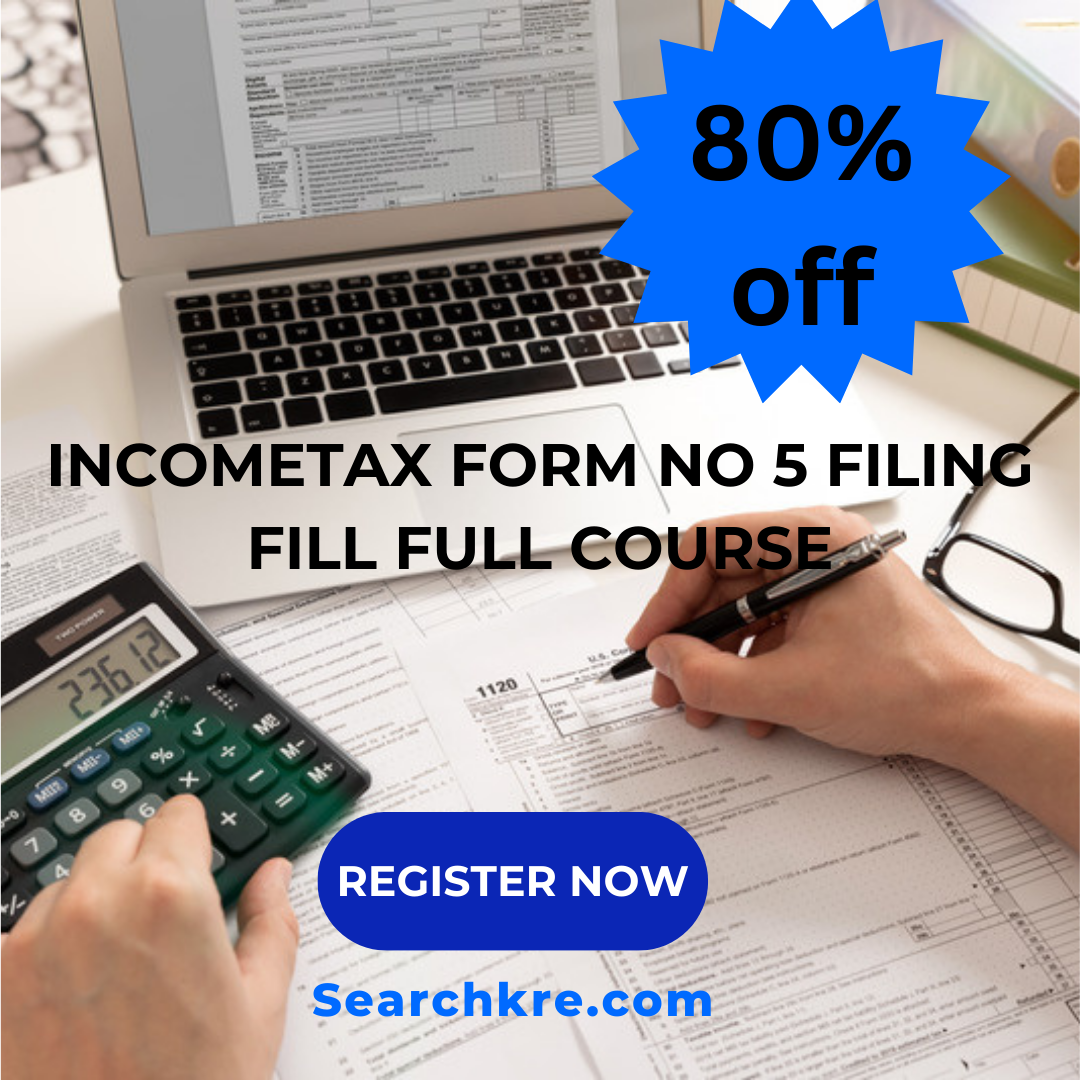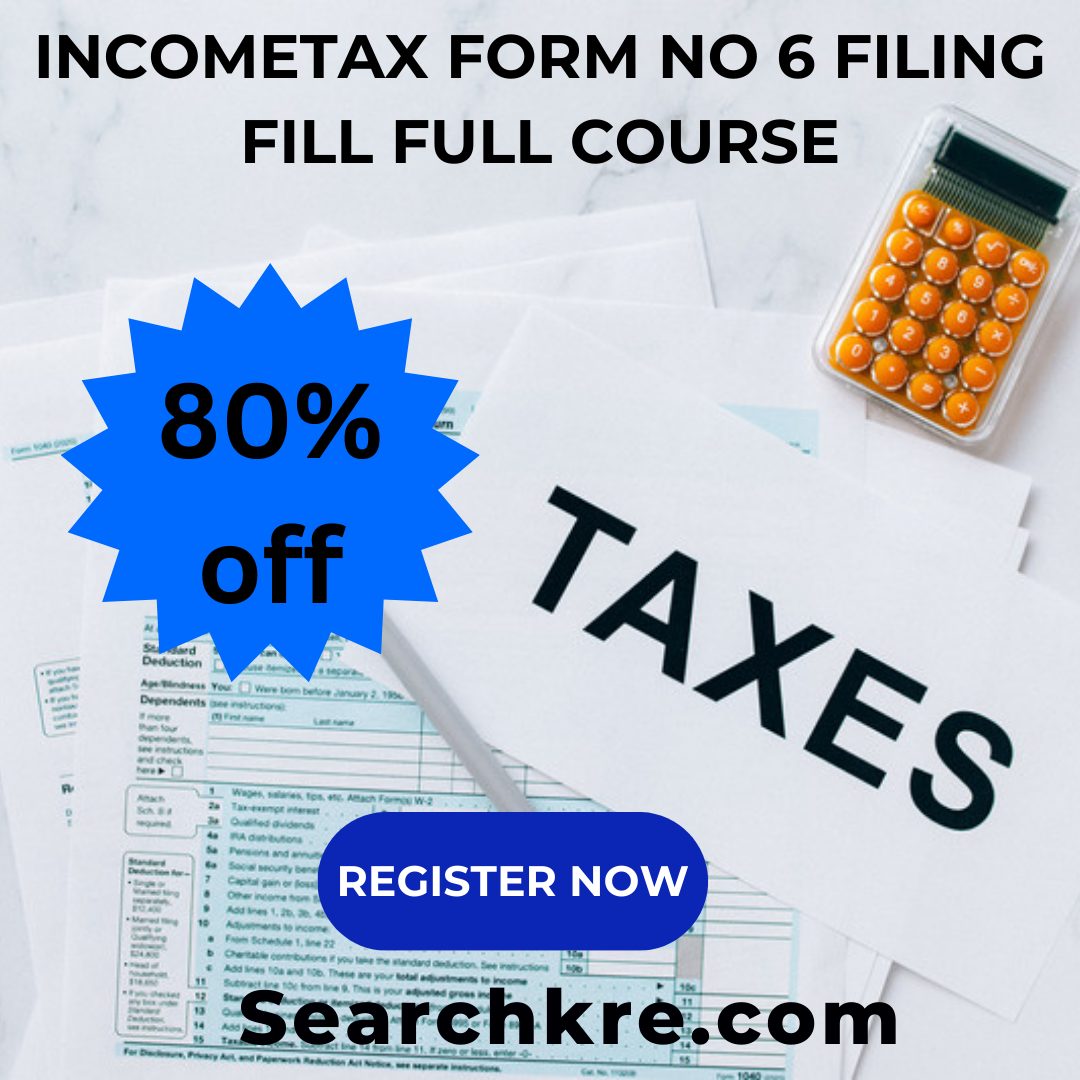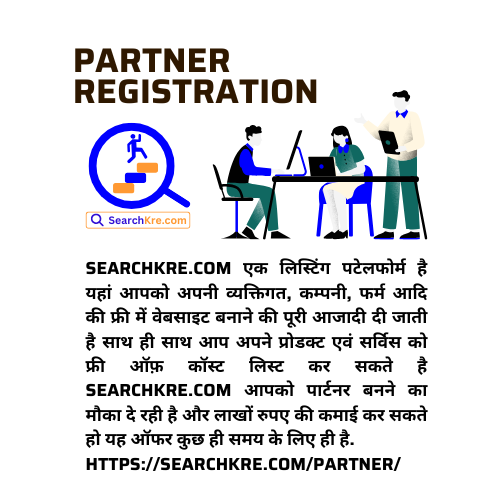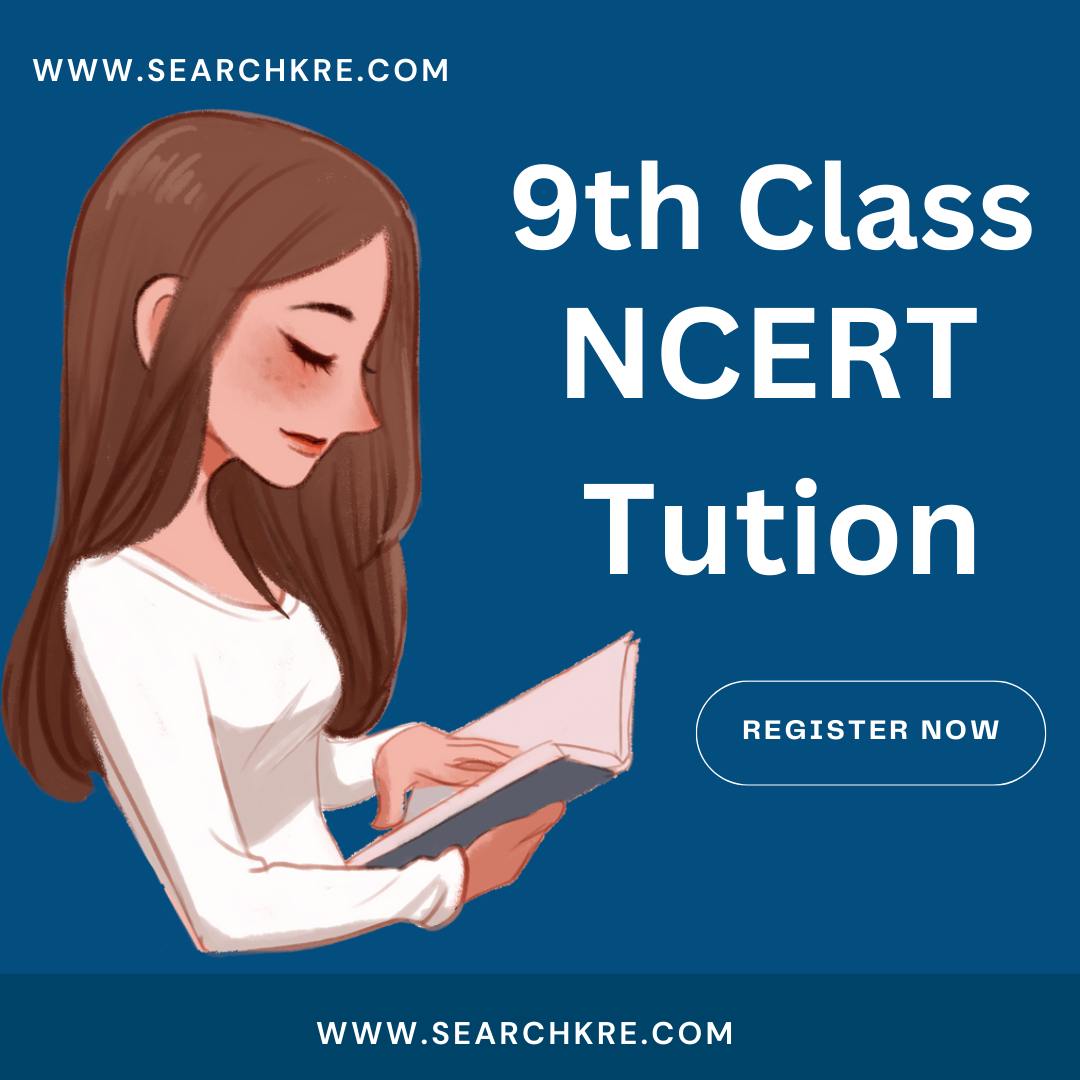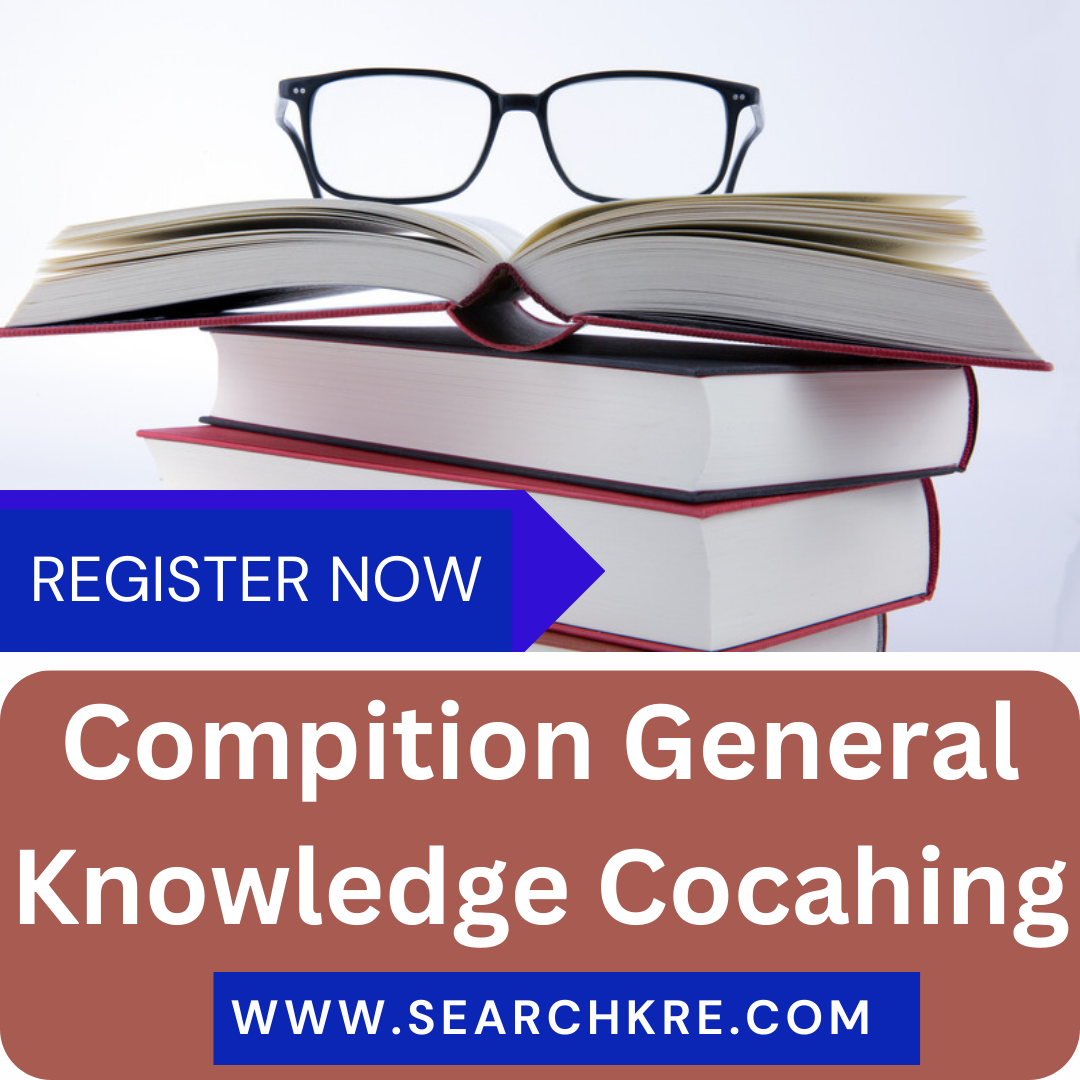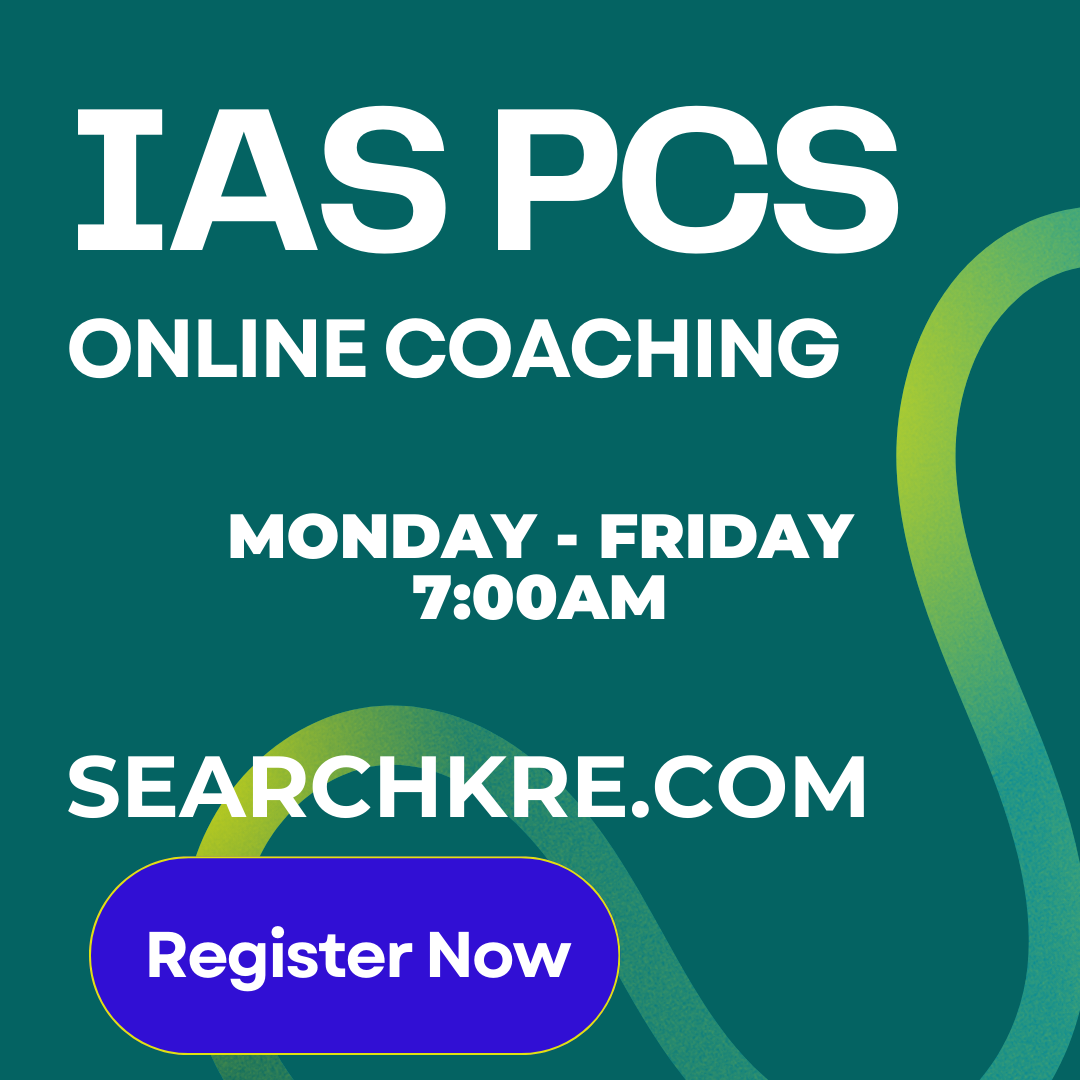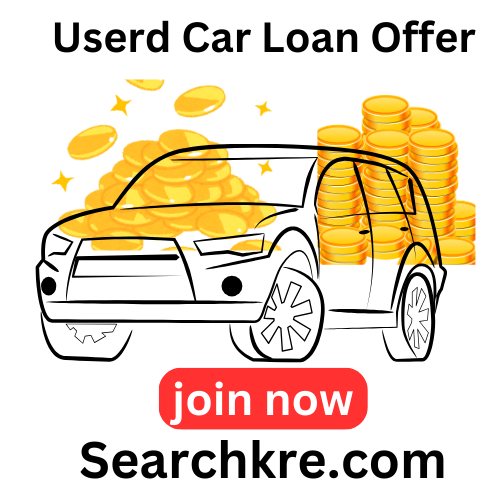.png)
Kundawai
jp Singh
2025-05-22 17:59:51
searchkre.com@gmail.com /
8392828781
कुंदवई
कुंदवई (लगभग 945-1000 ई.)
कुंदवई (लगभग 945-1000 ई.) चोल वंश की एक प्रमुख राजकुमारी थीं, जो सुंदर चोल (परांतक द्वितीय) और उनकी पत्नी वनवनमादेवी की पुत्री थीं। वे आदित्य करिकाल और राजराज चोल प्रथम की बहन थीं। कुंदवई चोल इतिहास में अपनी बुद्धिमत्ता, राजनीतिक कौशल, और धार्मिक-सांस्कृतिक योगदान के लिए जानी जाती हैं। यद्यपि वे स्वयं शासक नहीं थीं, उनकी भूमिका चोल साम्राज्य की स्थिरता और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण थी। नीचे उनके जीवन, योगदान, और प्रभाव का विस्तृत विवरण दिया गया है:
1. पृष्ठभूमि
कुंदवई सुंदर चोल और वनवनमादेवी की पुत्री थीं। वे अपने भाइयों, आदित्य करिकाल और राजराज चोल, के साथ चोल वंश के स्वर्ण युग के प्रारंभिक चरण में सक्रिय थीं। उनका जन्म लगभग 945 ई. के आसपास माना जाता है, और वे चोल राजवंश की एक प्रभावशाली महिला थीं, जिन्हें “इलैया पिराट्टि” (युवा रानी) की उपाधि प्राप्त थी। कुंदवई का
2. राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिका
चोल साम्राज्य की स्थिरता: कुंदवई ने अपने भाइयों, विशेष रूप से राजराज चोल, के शासनकाल में महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में कार्य किया। आदित्य करिकाल की रहस्यमय हत्या (लगभग 969-971 ई.) के बाद, कुंदवई ने राजराज के सिंहासन पर चढ़ने और साम्राज्य को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चालुक्य-चोल गठबंधन: कुंदवई का विवाह विमलादित्य के साथ (लगभग 990 ई.) ने वेंगी (पूर्वी चालुक्य क्षेत्र) और चोल साम्राज्य के बीच एक मजबूत राजनीतिक और वैवाहिक गठबंधन स्थापित किया। इस गठबंधन ने चोल साम्राज्य को उत्तरी क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने में मदद की। प्रशासनिक प्रभाव: शिलालेखों में कुंदवई को विभिन्न प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने स्थानीय सभाओं (उर और सभा) के साथ सहयोग किया और साम्राज्य के प्रशासन में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया।
3. धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान
शैव भक्ति: कुंदवई एक प्रबल शैव भक्त थीं और उन्होंने शैव धर्म को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके भाई राजराज चोल के समय में निर्मित बृहदीश्वर मंदिर (तंजावुर) को उनके समर्थन और प्रभाव का परिणाम माना जाता है। मंदिर निर्माण और दान: कुंदवई ने कई शिव मंदिरों को दान दिया और उनके जीर्णोद्धार में योगदान दिया। शिलालेखों में उनके द्वारा मंदिरों को दिए गए भूमि और आभूषणों के दान का उल्लेख मिलता है। भक्ति आंदोलन: उन्होंने तमिल शैव भक्ति आंदोलन को समर्थन दिया, विशेष रूप से नायनार संतों की रचनाओं, जैसे तेवरम, को प्रोत्साहन दिया। उनके प्रयासों ने तमिल साहित्य और धार्मिक परंपराओं को समृद्ध किया। सांस्कृतिक संरक्षण: कुंदवई ने तमिल कला, नृत्य, और संगीत को प्रोत्साहित किया। उनके समय में चोल साम्राज्य सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा, जिसका श्रेय उनकी सक्रियता को भी जाता है।
4. व्यक्तिगत जीवन और परिवार
विवाह: कुंदवई का विवाह पूर्वी चालुक्य राजकुमार विमलादित्य से हुआ, और उनके पुत्र राजराज नरेंद्र बाद में वेंगी के शासक बने। इस वैवाहिक गठबंधन ने चोल-चालुक्य संबंधों को मजबूत किया, जो बाद में राजेंद्र चोल के समय में और गहरा हुआ।
परिवार में भूमिका: कुंदवई अपने भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच एकजुटता बनाए रखने में महत्वपूर्ण थीं। उनकी बुद्धिमत्ता और कूटनीतिक कौशल ने चोल दरबार को स्थिरता प्रदान की।
बंधित शख्सियतें: उनकी भाभी सेमबियन मादेवी (गंडरादित्य की पत्नी) भी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय थीं, और दोनों ने
5. महत्व और प्रभाव
राजनीतिक स्थिरता: कुंदवई ने आदित्य करिकाल की हत्या के बाद चोल साम्राज्य में संभावित अस्थिरता को रोकने में मदद की। उनकी सलाह और प्रभाव ने राजराज चोल को एक मजबूत शासक बनने में सहायता प्रदान की।
सांस्कृतिक विरासत: कुंदवई की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों ने चोल साम्राज्य को तमिल संस्कृति का केंद्र बनाया। उनके प्रयासों ने बृहदीश्वर मंदिर जैसे स्मारकों के निर्माण को प्रेरित किया।
महिला सशक्तिकरण: कुंदवई चोल इतिहास में एक शक्तिशाली महिला के रूप में उभरीं, जिन्होंने अपने समय में महिलाओं की भूमिका को नया आयाम दिया। उनकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व ने उन्हें तमिल इतिहास में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाया।
6. ऐतिहासिक स्रोत
कुंदवई के बारे में जानकारी मुख्य रूप से तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर शिलालेख, तिरुवलंगाडु ताम्रपत्र, और अन्य समकालीन शिलालेखों से प्राप्त होती है। तमिल साहित्य, जैसे “पेरिय पुराणम,” और ऐतिहासिक ग्रंथों में उनके धार्मिक योगदान और परिवार की भूमिका का उल्लेख मिलता है। उनके विवाह और चालुक्य-चोल गठबंधन का विवरण शिलालेखों और बाद के इतिहास लेखन में दर्ज है।
7. तुलनात्मक विश्लेषण
विजयालय चोल और अन्य पूर्वजों के साथ तुलना: विजयालय, आदित्य प्रथम, और परांतक प्रथम जैसे शासकों ने चोल साम्राज्य की नींव और विस्तार पर ध्यान दिया, जबकि कुंदवई ने साम्राज्य की स्थिरता और सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। आदित्य करिकाल के साथ तुलना: आदित्य करिकाल ने सैन्य विजयों के माध्यम से चोल शक्ति को पुनर्जनन प्रदान किया, जबकि कुंदवई ने कूटनीति और धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से साम्राज्य को मजबूत किया। राजराज चोल के साथ तुलना: राजराज ने चोल साम्राज्य को एक वैश्विक शक्ति बनाया, लेकिन कुंदवई की सलाह और समर्थन ने उनके शासन को स्थिर और प्रभावी बनाया। सेमबियन मादेवी के साथ तुलना: सेमबियन मादेवी और कुंदवई दोनों ने शैव धर्म और मंदिर निर्माण को बढ़ावा दिया, लेकिन कुंदवई की राजनीतिक भूमिका अधिक व्यापक थी।
8. साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में
कुंदवई तमिल साहित्य और आधुनिक ऐतिहासिक उपन्यासों, जैसे कल्कि कृष्णमूर्ति के “पोन्नियिन सेल्वन,” में एक केंद्रीय पात्र के रूप में चित्रित की गई हैं। इस उपन्यास में उन्हें एक बुद्धिमान, कूटनीतिक, और प्रभावशाली राजकुमारी के रूप में दर्शाया गया है। उनकी छवि तमिल संस्कृति में एक आदर्श महिला शक्ति के रूप में स्थापित हुई है, जो बुद्धि, भक्ति, और नेतृत्व का प्रतीक है।
राजेंद्र चोल प्रथम (लगभग 1014-1044 ई.)
राजेंद्र चोल प्रथम (लगभग 1014-1044 ई.) चोल वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे, जिन्होंने अपने पिता राजराज चोल प्रथम की विरासत को न केवल कायम रखा, बल्कि इसे दक्षिण-पूर्व एशिया तक विस्तारित कर चोल साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया। उन्हें “गंगैकोण्ड चोल” (गंगा का विजेता) की उपाधि प्राप्त थी, जो उनके उत्तरी भारत और गंगा नदी तक के अभियानों को दर्शाती है। राजेंद्र ने सैन्य, नौसैनिक, प्रशासनिक, और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उनके शासनकाल में गंगैकोण्डचोलपुरम की स्थापना और वहां का शिव मंदिर (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) उनकी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। नीचे उनके जीवन, उपलब्धियों, और योगदान का विस्तृत विवरण दिया गया है
1. पृष्ठभूमि
राजेंद्र चोल राजराज चोल प्रथम और उनकी पत्नी लोकमहादेवी के पुत्र थे। वे आदित्य करिकाल और कुंदवई के छोटे भाई थे। उनका मूल नाम मदुरांतकन था, और वे “को-परकेसरीवरमन” के रूप में अपने पिता के सह-शासक रहे, जो चोल परंपरा के अनुसार युवराज की उपाधि थी। राजराज की मृत्यु (1014 ई.) के बाद राजेंद्र ने चोल सिंहासन संभाला। उनके शासनकाल में चोल साम्राज्य पहले से ही एक मजबूत शक्ति था, जिसे उन्होंने और विस्तारित किया।
2. सैन्य अभियान और विजय
राजेंद्र चोल एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे, जिन्होंने चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत से दक्षिण-पूर्व एशिया और उत्तरी भारत तक फैलाया। उनकी प्रमुख सैन्य उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:
श्रीलंका पर पूर्ण नियंत्रण: राजेंद्र ने अपने पिता राजराज द्वारा शुरू किए गए श्रीलंका अभियान को पूरा किया। उन्होंने सिंहली राजा महिंद V को पूरी तरह पराजित किया और श्रीलंका के उत्तरी और मध्य हिस्सों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। पोलोन्नरुवा को चोल प्रशासन का केंद्र बनाया गया, और श्रीलंका चोल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।
दक्षिण-पूर्व एशिया पर नौसैनिक अभियान: राजेंद्र की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि थी श्रीविजय साम्राज्य (वर्तमान इंडोनेशिया, मलेशिया, और सिंगापुर क्षेत्र) पर नौसैनिक अभियान (लगभग 1025 ई.)। उन्होंने श्रीविजय की राजधानी कदरम (केदाह) और अन्य बंदरगाहों पर कब्जा किया। यह अभियान हिंद महासागर में चोल नौसेना की सर्वोच्चता को दर्शाता है और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए था। उन्होंने मलेशिया, थाईलैंड, और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्रों में भी प्रभाव स्थापित किया, जिसने चोल साम्राज्य को एक वैश्विक व्यापारिक शक्ति बनाया
गंगा अभियान (उत्तरी भारत): राजेंद्र ने उत्तरी भारत में एक अभूतपूर्व अभियान चलाया (लगभग 1019-1024 ई.), जिसमें उन्होंने गंगा नदी तक के क्षेत्रों को जीता। इस अभियान में उन्होंने पाल वंश (बंगाल), चालुक्य, और अन्य उत्तरी शासकों को पराजित किया। इस विजय के सम्मान में उन्होंने “गंगैकोण्ड चोल” की उपाधि धारण की और गंगैकोण्डचोलपुरम की स्थापना की, जिसे उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाया। गंगा अभियान ने चोल साम्राज्य को भारतीय उपमहाद्वीप में एक अद्वितीय शक्ति के रूप में स्थापित किया।
पांड्य और चेर पर प्रभुत्व: राजेंद्र ने पांड्य और चेर शासकों को पूरी तरह अपने अधीन कर लिया, जिससे दक्षिण भारत में चोल प्रभुत्व और मजबूत हुआ। उन्होंने केरल और दक्षिणी तमिलनाडु के क्षेत्रों को चोल प्रशासन में एकीकृत किया।
पूर्वी चालुक्य और वेंगी: राजेंद्र ने अपनी बहन कुंदवई और विमलादित्य के पुत्र राजराज नरेंद्र को वेंगी का शासक बनाया, जिससे चोल-चालुक्य गठबंधन और मजबूत हुआ। इस गठबंधन ने चोल साम्राज्य को उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने में मदद की।
राष्ट्रकूट और पश्चिमी चालुक्य युद्ध: राजेंद्र ने पश्चिमी चालुक्य राजा जयसिंह द्वितीय के खिलाफ युद्ध लड़ा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। हालांकि, चालुक्यों के साथ संघर्ष बाद में भी जारी रहा।
3. प्रशासन
राजेंद्र ने अपने पिता राजराज द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे को और उन्नत किया। उन्होंने चोल साम्राज्य को एक अत्यधिक संगठित और केंद्रीकृत राज्य बनाया। भूमि सर्वेक्षण और कर प्रणाली: राजेंद्र ने भूमि सर्वेक्षण को और व्यवस्थित किया, जिससे कर संग्रह और प्रशासनिक दक्षता बढ़ी। शिलालेखों में भूमि माप और कर विवरण दर्ज हैं।
स्थानीय शासन: साम्राज्य को नाडु और कूट्रम जैसी छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया, जिन्हें स्थानीय सभाएँ (उर और सभा) संचालित करती
नौसेना और व्यापार: राजेंद्र ने चोल नौसेना को और मजबूत किया, जिसने हिंद महासागर में व्यापार मार्गों पर नियंत्रण बनाए रखा। नागपट्टिनम, कावेरीपट्टनम, और अन्य बंदरगाह व्यापारिक केंद्र बने। गंगैकोण्डचोलपुरम: राजेंद्र ने अपनी नई राजधानी गंगैकोण्डचोलपुरम की स्थापना की, जो चोल प्रशासन और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना।
4. धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान
राजेंद्र एक प्रबल शैव भक्त थे और उन्होंने शैव धर्म को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में चोल वास्तुकला और कला अपने चरम पर थी।
गंगैकोण्डचोलपुरम मंदिर: राजेंद्र ने गंगैकोण्डचोलपुरम में शिव मंदिर (लगभग 1030 ई.) का निर्माण करवाया, जो बृहदीश्वर मंदिर के समान भव्य है। यह मंदिर उनकी गंगा विजय का प्रतीक था और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
मंदिर संरक्षण: उन्होंने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर, कांचीपुरम, और अन्य क्षेत्रों में मंदिरों को संरक्षण और दान प्रदान किया।
कला और साहित्य: उनके शासनकाल में तमिल साहित्य, नृत्य (जैसे भरतनाट्यम), और संगीत को प्रोत्साहन मिला। गंगैकोण्डचोलपुरम मंदिर की नक्काशी इसकी गवाही देती है।
5. उत्तराधिकार और विरासत
राजेंद्र की मृत्यु के बाद (1044 ई.) उनके पुत्र राजाधिराज चोल ने सिंहासन संभाला। उनके अन्य पुत्रों, जैसे राजेंद्र चोल द्वितीय और वीरराजेंद्र, ने भी बाद में शासन किया। राजेंद्र की सबसे बड़ी विरासत थी चोल साम्राज्य को एक वैश्विक शक्ति बनाना। उनकी गंगा और श्रीविजय विजय ने चोल साम्राज्य को भारतीय इतिहास में अद्वितीय स्थान दिलाया। गंगैकोण्डचोलपुरम और वहां का मंदिर उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक है। उनकी नौसेना और व्यापारिक नीतियों ने हिंद महासागर में भारत की स्थिति को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया।
6. ऐतिहासिक स्रोत
राजेंद्र चोल के बारे में जानकारी गंगैकोण्डचोलपुरम शिलालेख, तंजावुर शिलालेख, तिरुवलंगाडु ताम्रपत्र, और अन्य समकालीन शिलालेखों से प्राप्त होती है। तमिल भक्ति ग्रंथ “पेरिय पुराणम” और अन्य साहित्य में उनके धार्मिक योगदान का उल्लेख मिलता है। श्रीविजय अभियान का विवरण चोल शिलालेखों और दक्षिण-पूर्व एशियाई स्रोतों में दर्ज है।
7. महत्व और प्रभाव
राजेंद्र चोल ने चोल साम्राज्य को भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण-पूर्व एशिया में एक वैश्विक शक्ति बनाया। उनकी श्रीविजय और गंगा अभियान भारतीय इतिहास में अद्वितीय हैं। उनकी नौसेना शक्ति ने हिंद महासागर में व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया, जिसने भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच संबंधों को मजबूत किया। गंगैकोण्डचोलपुरम मंदिर और उनकी प्रशासनिक नीतियाँ चोल साम्राज्य की सांस्कृतिक और शासकीय उपलब्धियों का प्रतीक हैं।
8. तुलनात्मक विश्लेषण
विजयालय चोल के साथ तुलना: विजयालय ने चोल वंश की नींव रखी, जबकि राजेंद्र ने इसे वैश्विक स्तर पर ले गए। आदित्य प्रथम के साथ तुलना: आदित्य ने पल्लव साम्राज्य को समाप्त किया, जबकि राजेंद्र ने श्रीविजय और गंगा अभियानों के माध्यम से चोल साम्राज्य का विस्तार किया। परांतक प्रथम के साथ तुलना: परांतक ने पांड्य और श्रीलंका पर प्रारंभिक विजय प्राप्त की, लेकिन राजेंद्र ने इन क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। राजराज चोल के साथ तुलना: राजराज ने चोल साम्राज्य का आधार तैयार किया, जिसे राजेंद्र ने उत्तरी भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया तक विस्तारित किया। कुंदवई के साथ तुलना: कुंदवई ने राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिरता प्रदान की, जबकि राजेंद्र
राजाधिराज चोल (लगभग 1018-1054 ई.)
राजाधिराज चोल (लगभग 1018-1054 ई.) चोल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे, जो राजेंद्र चोल प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और चोल साम्राज्य की सैन्य शक्ति और प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखा। राजाधिराज अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, विशेष रूप से पश्चिमी चालुक्यों के खिलाफ उनकी लड़ाइयों के लिए। उनका शासनकाल चोल साम्राज्य के स्वर्ण युग का हिस्सा था, हालांकि यह पश्चिमी चालुक्यों के साथ बढ़ते संघर्षों द्वारा चिह्नित था। उनकी मृत्यु कोप्पम की लड़ाई (1054 ई.) में हुई, जिसके बाद उनके छोटे भाई राजेंद्र चोल द्वितीय ने सिंहासन संभाला। नीचे उनके जीवन, उपलब्धियों, और योगदान का विस्तृत विवरण दिया गया है:
1. पृष्ठभूमि
राजाधिराज चोल राजेंद्र चोल प्रथम और उनकी पत्नी (संभवतः त्रिभुवनमादेवी) के पुत्र थे। वे राजराज चोल प्रथम के पौत्र थे, जिन्होंने चोल साम्राज्य को एक वैश्विक शक्ति बनाया था। उन्हें “को-परकेसरीवरमन” की उपाधि प्राप्त थी, जो चोल परंपरा के अनुसार युवराज (सह-शासक) को दी जाती थी। वे अपने पिता राजेंद्र के शासनकाल में सह-शासक के रूप में सक्रिय थे। राजेंद्र चोल की मृत्यु (1044 ई.) के बाद राजाधिराज ने चोल सिंहासन संभाला। उनके शासनकाल में चोल साम्राज्य अपने चरम पर था, जिसमें दक्षिण भारत, श्रीलंका, और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्से शामिल थे।
2. सैन्य अभियान और विजय
राजाधिराज चोल एक कुशल योद्धा थे, जिन्होंने चोल साम्राज्य के क्षेत्रों को बनाए रखने और विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए। उनकी प्रमुख सैन्य उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:
पश्चिमी चालुक्यों के खिलाफ युद्ध: राजाधिराज का शासनकाल पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम (आहवमल्ल) के साथ लगातार संघर्षों द्वारा चिह्नित था। चालुक्य चोल साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्रों, विशेष रूप से वेंगी और कर्नाटक, पर दबाव डाल रहे थे।
कोप्पम की लड़ाई (1054 ई.): यह राजाधिराज की सबसे प्रसिद्ध और अंतिम लड़ाई थी। उन्होंने पश्चिमी चालुक्यों के खिलाफ कोप्पम (वर्तमान कर्नाटक) में युद्ध लड़ा। यद्यपि चोल सेना ने जीत हासिल की, राजाधिराज इस लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई राजेंद्र चोल द्वितीय ने युद्ध का नेतृत्व किया और जीत सुनिश्चित की।
श्रीलंका में नियंत्रण: राजाधिराज ने अपने पिता राजेंद्र द्वारा जीते गए श्रीलंका के क्षेत्रों पर चोल नियंत्रण को बनाए रखा। हालांकि, उनके शासनकाल में श्रीलंका में सिंहली विद्रोह शुरू हुए, जिन्हें दबाने के लिए उन्होंने सैन्य अभियान चलाए। श्रीलंका के पोलोन्नरुवा और अन्य क्षेत्रों में चोल प्रशासन को सुदृढ़ किया गया।
पांड्य और चेर क्षेत्रों पर प्रभुत्व: राजाधिराज ने पांड्य और चेर क्षेत्रों पर चोल प्रभुत्व को बनाए रखा। उन्होंने इन क्षेत्रों में विद्रोहों को दबाया और चोल प्रशासन को मजबूत किया। उनके अभियानों ने दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में चोल प्रभाव को स्थिर रखा।
वेंगी और पूर्वी चालुक्य: राजाधिराज ने वेंगी (पूर्वी चालुक्य क्षेत्र) में चोल प्रभाव को बनाए रखा। उनकी चाची कुंदवई और विमलादित्य के पुत्र राजराज नरेंद्र वेंगी के शासक थे, और राजाधिराज ने इस गठबंधन को मजबूत किया। चालुक्य-चोल संबंधों को संतुलित करने में उनकी कूटनीति महत्वपूर्ण थी।
3. प्रशासन
राजाधिराज ने अपने पिता राजेंद्र और दादा राजराज द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखा और इसे और सुदृढ़ किया। भूमि और कर प्रणाली: उन्होंने भूमि सर्वेक्षण और कर संग्रह की व्यवस्था को और व्यवस्थित किया। शिलालेखों में उनके समय में भूमि दान और कर निर्धारण के विवरण मिलते हैं। स्थानीय शासन: चोल साम्राज्य को नाडु और कूट्रम जैसी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित रखा गया, जिन्हें स्थानीय सभाएँ संचालित करती थीं। नौसेना और व्यापार: राजाधिराज ने चोल नौसेना को सक्रिय रखा, जिसने हिंद महासागर में व्यापार मार्गों पर नियंत्रण बनाए रखा। नागपट्टिनम और अन्य बंदरगाह उनके समय में व्यापारिक केंद्र बने रहे। गंगैकोण्डचोलपुरम: राजाधिराज ने गंगैकोण्डचोलपुरम को चोल राजधानी के रूप में बनाए रखा और वहां के प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों को प्रोत्साहन दिया।
4. धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान
राजाधिराज एक प्रबल शैव भक्त थे और उन्होंने शैव धर्म को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में चोल वास्तुकला और कला का विकास जारी रहा। गंगैकोण्डचोलपुरम मंदिर: उन्होंने अपने पिता द्वारा निर्मित गंगैकोण्डचोलपुरम के शिव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया। इस मंदिर को दान और रखरखाव के लिए उनके द्वारा समर्थन मिला। अन्य मंदिर राजाधिराज ने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर, कांचीपुरम, और अन्य क्षेत्रों में मंदिरों को दान और संरक्षण प्रदान किया। भक्ति आंदोलन उन्होंने तमिल शैव भक्ति आंदोलन को समर्थन दिया, और नायनार संतों की रचनाएँ, जैसे तेवरम, उनके समय में लोकप्रिय रहीं। कला और साहित्य उनके शासनकाल में तमिल साहित्य, नृत्य, और संगीत को प्रोत्साहन मिला। मंदिरों की नक्काशी और शिलालेख उनके सांस्कृतिक योगदान को दर्शाते हैं।
5. उत्तराधिकार और विरासत
राजाधिराज की मृत्यु कोप्पम की लड़ाई (1054 ई.) में हुई, जहां वे युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई राजेंद्र चोल द्वितीय ने सिंहासन संभाला। राजाधिराज की सबसे बड़ी विरासत थी चोल साम्राज्य की सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय प्रभुत्व को बनाए रखना, विशेष रूप से पश्चिमी चालुक्यों के खिलाफ। उनकी मृत्यु के बाद चोल साम्राज्य ने अपनी शक्ति को बनाए रखा, और उनके भाइयों (राजेंद्र चोल द्वितीय और वीरराजेंद्र) ने उनके अभियानों को आगे बढ़ाया। कोप्पम की लड़ाई में उनकी वीरता ने उन्हें “वीरमरणम अडैंदार” (युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाला) की उपाधि दिलाई।
6. ऐतिहासिक स्रोत
राजाधिराज के बारे में जानकारी गंगैकोण्डचोलपुरम शिलालेख, तंजावुर शिलालेख, और अन्य समकालीन शिलालेखों से प्राप्त होती है। तमिल भक्ति ग्रंथ “पेरिय पुराणम” और अन्य साहित्य में उनके धार्मिक योगदान का उल्लेख मिलता है। कोप्पम की लड़ाई और उनके सैन्य अभियानों का विवरण चोल और चालुक्य शिलालेखों में दर्ज है।
7. महत्व और प्रभाव
राजाधिराज ने चोल साम्राज्य को अपने पिता राजेंद्र के समय की ऊंचाइयों पर बनाए रखा। उनकी पश्चिमी चालुक्यों के खिलाफ जीत ने चोल प्रभुत्व को उत्तरी सीमाओं पर मजबूत किया। कोप्पम की लड़ाई में उनकी वीरता और बलिदान ने चोल सैन्य परंपराओं को और गौरव प्रदान किया। उनकी प्रशासनिक और धार्मिक नीतियों ने चोल साम्राज्य की सांस्कृतिक और शासकीय विरासत को समृद्ध किया।
विजयालय चोल के साथ तुलना: विजयालय ने चोल वंश की नींव रखी, जबकि राजाधिराज ने इसे अपने चरम पर बनाए रखा। आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम के साथ तुलना: इन शासकों ने चोल साम्राज्य का प्रारंभिक विस्तार किया, जबकि राजाधिराज ने इसे स्थिर और सुरक्षित रखा। राजराज चोल और राजेंद्र चोल के साथ तुलना: राजराज और राजेंद्र ने चोल साम्राज्य को वैश्विक शक्ति बनाया, जबकि राजाधिराज ने इस शक्ति को चालुक्य चुनौतियों के बावजूद बनाए रखा। कुंदवई के साथ तुलना: कुंदवई ने राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिरता प्रदान की, जबकि राजाधिराज ने सैन्य शक्ति पर ध्यान दिया।
राजेंद्र चोल द्वितीय (1052-1064 ई.)
राजेंद्र चोल द्वितीय (1052-1064 ई.) के शासनकाल और योगदान को विस्तार से समझने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। यह जानकारी चोल वंश के इतिहास, उनकी सैन्य उपलब्धियों, प्रशासनिक नीतियों, सांस्कृतिक योगदान और उनके शासन के महत्व को विस्तार से बताती है।
1. पृष्ठभूमि और उत्तराधिकार
वंश और परिवार: राजेंद्र चोल द्वितीय, चोल वंश के महान शासक राजराज प्रथम के पुत्र और राजेंद्र प्रथम के छोटे भाई थे। उनके भाई राजाधिराज प्रथम (1044-1054 ई.) की कोप्पम के युद्ध में मृत्यु के बाद राजेंद्र चोल द्वितीय ने सिंहासन संभाला। यह युद्ध चालुक्यों के खिलाफ लड़ा गया था, और राजेंद्र ने युद्धक्षेत्र में ही राजा के रूप में अभिषेक किया, जो उनकी साहसिकता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है।
शासनकाल: उनका शासन 1052 से 1064 ईस्वी तक रहा। इस दौरान उन्होंने चोल साम्राज्य की विशालता और शक्ति को बनाए रखने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया।
2. सैन्य उपलब्धियाँ
राजेंद्र चोल द्वितीय का शासनकाल चालुक्यों और अन्य पड़ोसी शक्तियों के साथ युद्धों के लिए प्रसिद्ध रहा। उनकी सैन्य रणनीतियाँ और नेतृत्व ने चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत में सर्वोच्च बनाए रखा। प्रमुख सैन्य अभियान निम्नलिखित हैं:
कोप्पम का युद्ध (1054 ई.): यह युद्ध पश्चिमी चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के खिलाफ लड़ा गया। इस युद्ध में राजाधिराज प्रथम की मृत्यु हो गई, लेकिन राजेंद्र चोल द्वितीय ने नेतृत्व संभालकर चालुक्यों को पराजित किया। इस जीत ने चोल साम्राज्य की सैन्य श्रेष्ठता को पुनः स्थापित किया। इस युद्ध में चालुक्य राजधानी को लूटा गया, और चोल सेना ने कई युद्ध हाथियों और खजानों को जब्त किया।
श्रीलंका और अन्य क्षेत्रों में अभियान: राजेंद्र चोल द्वितीय ने श्रीलंका में चोल प्रभुत्व को पुनर्जनन किया। उनके पिता राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को जीता था, लेकिन वहाँ विद्रोह होने लगे थे। राजेंद्र चोल द्वितीय ने इन विद्रोहों को दबाया और चोल साम्राज्य का नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों, जैसे पांड्य और चेर राज्यों, पर भी अपनी सैन्य शक्ति का प्रभाव बनाए रखा।
नौसैनिक शक्ति: चोल वंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। राजेंद्र चोल द्वितीय ने अपने पिता राजेंद्र प्रथम की तरह नौसेना को मजबूत रखा, जिससे समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय प्रभुत्व को बढ़ावा मिला।
3. प्रशासनिक नीतियाँ
प्रशासनिक ढांचा: राजेंद्र चोल द्वितीय ने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ किया। चोल साम्राज्य में ग्राम सभाएँ (स्थानीय स्वशासन) और केंद्रीकृत प्रशासन का मिश्रण था। उन्होंने स्थानीय स्तर पर शासन को प्रभावी बनाए रखने के लिए ग्राम सभाओं को स्वायत्तता प्रदान की।
कर व्यवस्था: चोल शासकों की तरह, राजेंद्र चोल द्वितीय ने कर संग्रह और भूमि प्रबंधन में सुधार किए। उनकी नीतियों ने साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि को बनाए रखा। न्याय व्यवस्था: चोल प्रशासन में न्याय व्यवस्था संगठित थी। राजेंद्र चोल द्वितीय ने अपने शासनकाल में इसे और अधिक प्रभावी बनाया, जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रही।
4. सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान
मंदिर निर्माण और संरक्षण: चोल वंश अपनी मंदिर निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध था। यद्यपि राजेंद्र चोल द्वितीय के समय में कोई बड़ा मंदिर निर्माण कार्य विशेष रूप से उनके नाम से नहीं जुड़ा, उन्होंने अपने पिता राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के रखरखाव और संरक्षण में योगदान दिया।
कला और साहित्य: उनके शासनकाल में तमिल साहित्य और कला को प्रोत्साहन मिला। चोल दरबार में विद्वानों और कवियों को संरक्षण दिया जाता था। धर्म और समाज: राजेंद्र चोल द्वितीय ने शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं को समर्थन दिया, जिससे धार्मिक सामंजस्य बना रहा।
5. आर्थिक समृद्धि और व्यापार
समुद्री व्यापार: चोल साम्राज्य का समुद्री व्यापार दक्षिण-पूर्व एशिया, चीन और मध्य पूर्व तक फैला हुआ था। राजेंद्र चोल द्वितीय ने इस व्यापार नेटवर्क को बनाए रखा, जिससे साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि बढ़ी। बंदरगाह: चोल साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाह, जैसे नागपट्टिनम, व्यापार का केंद्र थे। राजेंद्र चोल द्वितीय ने इन बंदरगाहों के प्रबंधन और सुरक्षा को सुनिश्चित किया।
6. चुनौतियाँ
चालुक्य युद्ध: चालुक्यों के साथ निरंतर युद्धों ने चोल साम्राज्य की संसाधनों पर दबाव डाला। हालांकि राजेंद्र चोल द्वितीय ने कई युद्धों में जीत हासिल की, लेकिन ये युद्ध साम्राज्य के लिए चुनौतीपूर्ण रहे। आंतरिक विद्रोह: श्रीलंका और अन्य क्षेत्रों में समय-समय पर होने वाले विद्रोहों को दबाने में काफी संसाधनों का उपयोग हुआ।
7. उत्तराधिकार और मृत्यु
राजेंद्र चोल द्वितीय की मृत्यु 1064 ईस्वी में हुई। उनके बाद उनके छोटे भाई वीर राजेंद्र (1063-1070 ई.) ने सिंहासन संभाला। वीर राजेंद्र ने भी चालुक्यों के खिलाफ युद्ध जारी रखे और चोल साम्राज्य की शक्ति को बनाए रखा।
8. ऐतिहासिक महत्व
राजेंद्र चोल द्वितीय का शासनकाल चोल साम्राज्य के स्वर्ण युग का हिस्सा था। उन्होंने अपने भाई और पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया और साम्राज्य की एकता और शक्ति को बनाए रखा। उनकी सैन्य और प्रशासनिक उपलब्धियाँ चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति बनाए रखने में महत्वपूर्ण थीं। उनके शासनकाल में चोल साम्राज्य ने सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी अपनी पहचान बनाए रखी।
9. उपाधियाँ और स्मृति
राजेंद्र चोल द्वितीय ने कई उपाधियाँ धारण कीं, जो उनकी सैन्य विजयों और शासन की महिमा को दर्शाती थीं। उनके शासनकाल के शिलालेखों में उनकी उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कई शिलालेखों में उनके शासनकाल की जानकारी संरक्षित है।
वीर राजेंद्र (1063-1070 ई.)
वीर राजेंद्र (1063-1070 ई.) चोल वंश का एक प्रमुख शासक था, जो राजेंद्र चोल द्वितीय का छोटा भाई और उत्तराधिकारी था। वह अपने सैन्य अभियानों, विशेष रूप से चालुक्यों के खिलाफ युद्धों, और चोल साम्राज्य की शक्ति को बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध है। उनके शासनकाल में चोल साम्राज्य ने दक्षिण भारत में अपनी सांस्कृतिक, सैन्य और व्यापारिक श्रेष्ठता को कायम रखा। नीचे उनके जीवन, शासनकाल और योगदान को विस्तार से बताया गया है।
1. पृष्ठभूमि और उत्तराधिकार
वंश: वीर राजेंद्र, चोल वंश के महान शासक राजराज प्रथम का पुत्र और राजेंद्र प्रथम का छोटा भाई था। उनके बड़े भाई राजाधिराज प्रथम (1044-1054 ई.) और राजेंद्र चोल द्वितीय (1052-1064 ई.) के बाद उन्होंने चोल सिंहासन संभाला।
उत्तराधिकार: राजेंद्र चोल द्वितीय की मृत्यु के बाद, वीर राजेंद्र 1063 ईस्वी में चोल साम्राज्य के शासक बने। उनका शासनकाल लगभग 1063 से 1070 ईस्वी तक रहा।
परिस्थितियाँ: वीर राजेंद्र का शासनकाल उस समय शुरू हुआ जब चोल साम्राज्य चालुक्यों के साथ निरंतर युद्धों में उलझा था। उन्होंने साम्राज्य को स्थिर करने और अपनी सैन्य शक्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2. सैन्य उपलब्धियाँ
वीर राजेंद्र का शासनकाल सैन्य अभियानों के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनकी प्रमुख सैन्य उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:
चालुक्यों के खिलाफ युद्ध: वीर राजेंद्र ने पश्चिमी चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम और बाद में सोमेश्वर द्वितीय के खिलाफ कई युद्ध लड़े। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कुडल संगमम का युद्ध (लगभग 1066 ई.) था, जिसमें उन्होंने चालुक्यों को निर्णायक रूप से पराजित किया। इस युद्ध में चोल सेना ने चालुक्य राजधानी को लूटा और कई युद्ध हाथियों और खजानों को जब्त किया। इस विजय ने चोल साम्राज्य की सैन्य श्रेष्ठता को पुनः स्थापित किया। वीर राजेंद्र ने चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को पराजित करने के बाद उनकी राजधानी वेंगी पर भी नियंत्रण स्थापित किया।
श्रीलंका पर नियंत्रण: वीर राजेंद्र ने श्रीलंका में चोल प्रभुत्व को पुनर्जनन किया। उनके पिता राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को जीता था, लेकिन वहाँ समय-समय पर विद्रोह होते रहते थे। वीर राजेंद्र ने इन विद्रोहों को दबाया और श्रीलंका पर चोल नियंत्रण को मजबूत किया। उन्होंने श्रीलंका के सिंहली शासकों को पराजित किया और चोल साम्राज्य की समुद्री शक्ति का प्रदर्शन किया।
पांड्य और चेर राज्यों पर प्रभाव: वीर राजेंद्र ने दक्षिण भारत के पांड्य और चेर राज्यों पर चोल प्रभुत्व बनाए रखा। उन्होंने इन क्षेत्रों में विद्रोहों को दबाया और चोल साम्राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित किया।
3. प्रशासनिक नीतियाँ
केंद्रीकृत प्रशासन: वीर राजेंद्र ने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत किया। चोल साम्राज्य में केंद्रीकृत शासन और स्थानीय स्वशासन (ग्राम सभाओं) का संतुलन था। उन्होंने ग्राम सभाओं को स्वायत्तता प्रदान की, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रशासन प्रभावी रहा। कर प्रणाली: उनकी नीतियों ने साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि को बनाए रखा। भूमि कर और व्यापार कर के माध्यम से चोल साम्राज्य की आय बढ़ी। न्याय व्यवस्था: वीर राजेंद्र ने चोल प्रशासन की न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ किया। उनके शासनकाल में सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई उपाय किए गए।
4. सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान
मंदिर निर्माण और संरक्षण: चोल वंश अपनी मंदिर निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध था। यद्यपि वीर राजेंद्र के नाम से कोई विशाल मंदिर निर्माण कार्य विशेष रूप से दर्ज नहीं है, उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित मंदिरों, जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, के रखरखाव और संरक्षण में योगदान दिया। कला और साहित्य: उनके शासनकाल में तमिल साहित्य और कला को प्रोत्साहन मिला। चोल दरबार में विद्वानों, कवियों और कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया गया। धार्मिक सहिष्णुता: वीर राजेंद्र ने शैव और वैष्णव परंपराओं को समान रूप से समर्थन दिया, जिससे धार्मिक सामंजस्य बना रहा। उनके शासनकाल में कई धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों को बढ़ावा दिया गया।
5. आर्थिक समृद्धि और व्यापार
समुद्री व्यापार: वीर राजेंद्र के शासनकाल में चोल साम्राज्य का समुद्री व्यापार दक्षिण-पूर्व एशिया (श्रीविजय साम्राज्य), चीन, और मध्य पूर्व तक फैला हुआ था। उन्होंने इस व्यापार नेटवर्क को बनाए रखा और इसे और विस्तार देने का प्रयास किया। बंदरगाह: चोल साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाह, जैसे नागपट्टिनम और कावेरीपट्टिनम, व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे। वीर राजेंद्र ने इन बंदरगाहों की सुरक्षा और प्रबंधन को सुनिश्चित किया।
6. चुनौतियाँ
चालुक्य युद्ध: चालुक्यों के साथ निरंतर युद्धों ने चोल साम्राज्य के संसाधनों पर दबाव डाला। हालांकि वीर राजेंद्र ने कई युद्धों में जीत हासिल की, लेकिन ये युद्ध साम्राज्य के लिए चुनौतीपूर्ण रहे। आंतरिक और बाहरी विद्रोह: श्रीलंका और अन्य अधीनस्थ क्षेत्रों में समय-समय पर होने वाले विद्रोहों को दबाने में काफी संसाधनों का उपयोग हुआ।
7. उत्तराधिकार और मृत्यु
वीर राजेंद्र की मृत्यु 1070 ईस्वी में हुई। उनके बाद उनके पुत्र अतिराजेंद्र चोल ने सिंहासन संभाला, लेकिन उनका शासनकाल बहुत संक्षिप्त और अस्थिर रहा। अतिराजेंद्र की मृत्यु के बाद चोल वंश में उत्तराधिकार का संकट पैदा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कुलोत्तुंग चोल प्रथम (1070-1122 ई.) ने सिंहासन संभाला। कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने चोल साम्राज्य को और अधिक समृद्ध किया।
8. ऐतिहासिक महत्व
वीर राजेंद्र का शासनकाल चोल साम्राज्य के स्वर्ण युग का हिस्सा था। उन्होंने अपने भाइयों राजाधिराज प्रथम और राजेंद्र चोल द्वितीय की नीतियों को आगे बढ़ाया और साम्राज्य की एकता और शक्ति को बनाए रखा। उनकी सैन्य विजयों, विशेष रूप से चालुक्यों के खिलाफ, ने चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनके शासनकाल में चोल साम्राज्य ने सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अपनी पहचान बनाए रखी, जो तमिल संस्कृति और कला के लिए एक महत्वपूर्ण काल था।
वीर राजेंद्र ने कई उपाधियाँ धारण कीं, जैसे
9. उपाधियाँ और स्मृति
Conclusion
Thanks For Read
jp Singh
searchkre.com@gmail.com
8392828781
 Gst Registration
Gst Registration
 DSC Registration
DSC Registration
 Pancard Registration
Pancard Registration
 Company Registration
Company Registration
 Fssai Registration
Fssai Registration
 TradeMark Registration
TradeMark Registration
 MSME Registration
MSME Registration
 Passport Registration
Passport Registration
 Income Tax Return
Income Tax Return
 LLP Company Registration
LLP Company Registration
 Marriage And Court Marriage Registration
Marriage And Court Marriage Registration
 PVT LTD Company Registration
PVT LTD Company Registration
 GST Filing Services
GST Filing Services
 Coaching Insititute Registration
Coaching Insititute Registration
 GYM Registration
GYM Registration
 NGO Registration
NGO Registration
 Political Party Registration
Political Party Registration
 Society Registration
Society Registration
 Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
 Make Website on EMI
Make Website on EMI



























































































 9th Class Scholarship Competition Test
9th Class Scholarship Competition Test
 10th Class Scholarship Competition Test
10th Class Scholarship Competition Test
 11th Class Scholarship Competition Test
11th Class Scholarship Competition Test
 12th Class Scholarship Competition Test
12th Class Scholarship Competition Test
 Graduation Scholarship Competition Test
Graduation Scholarship Competition Test
 Post Graduation Scholarship Competition Test
Post Graduation Scholarship Competition Test
 Diploma Scholarship Competition Test
Diploma Scholarship Competition Test
 Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 JEE Coaching Scholarship Competition Test
JEE Coaching Scholarship Competition Test
 NEET Coaching Scholarship Competition Test
NEET Coaching Scholarship Competition Test
 Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test















































.png)