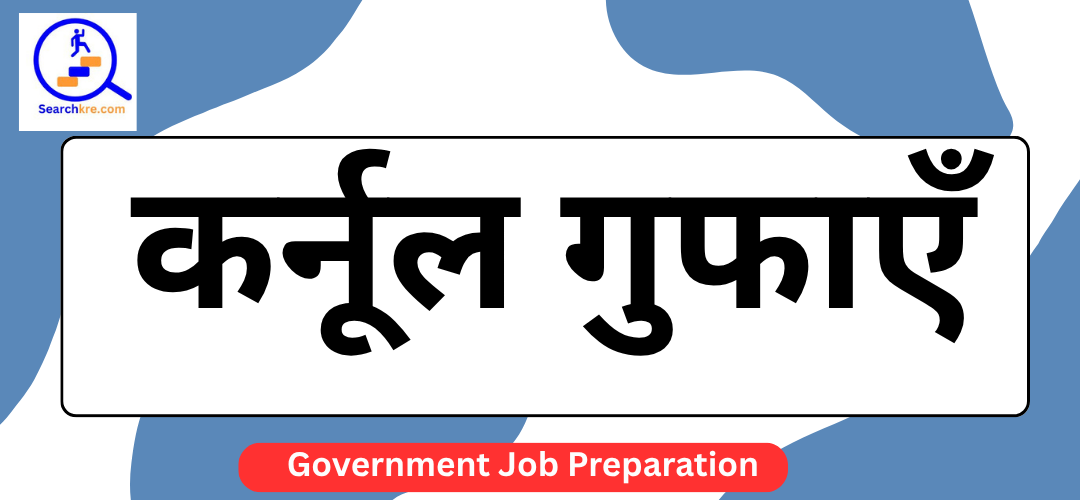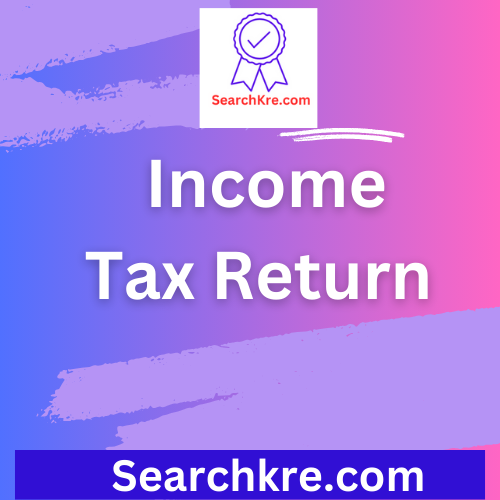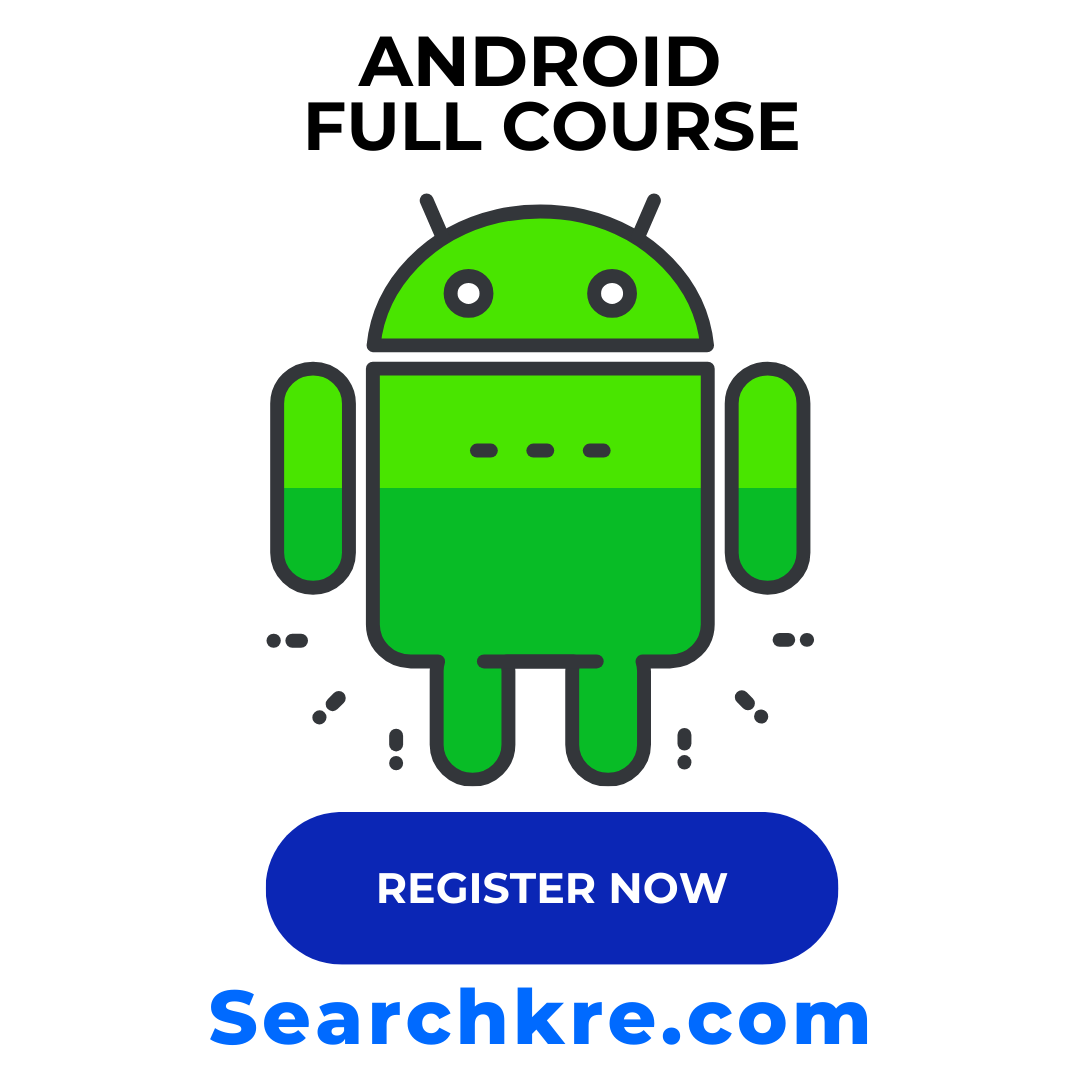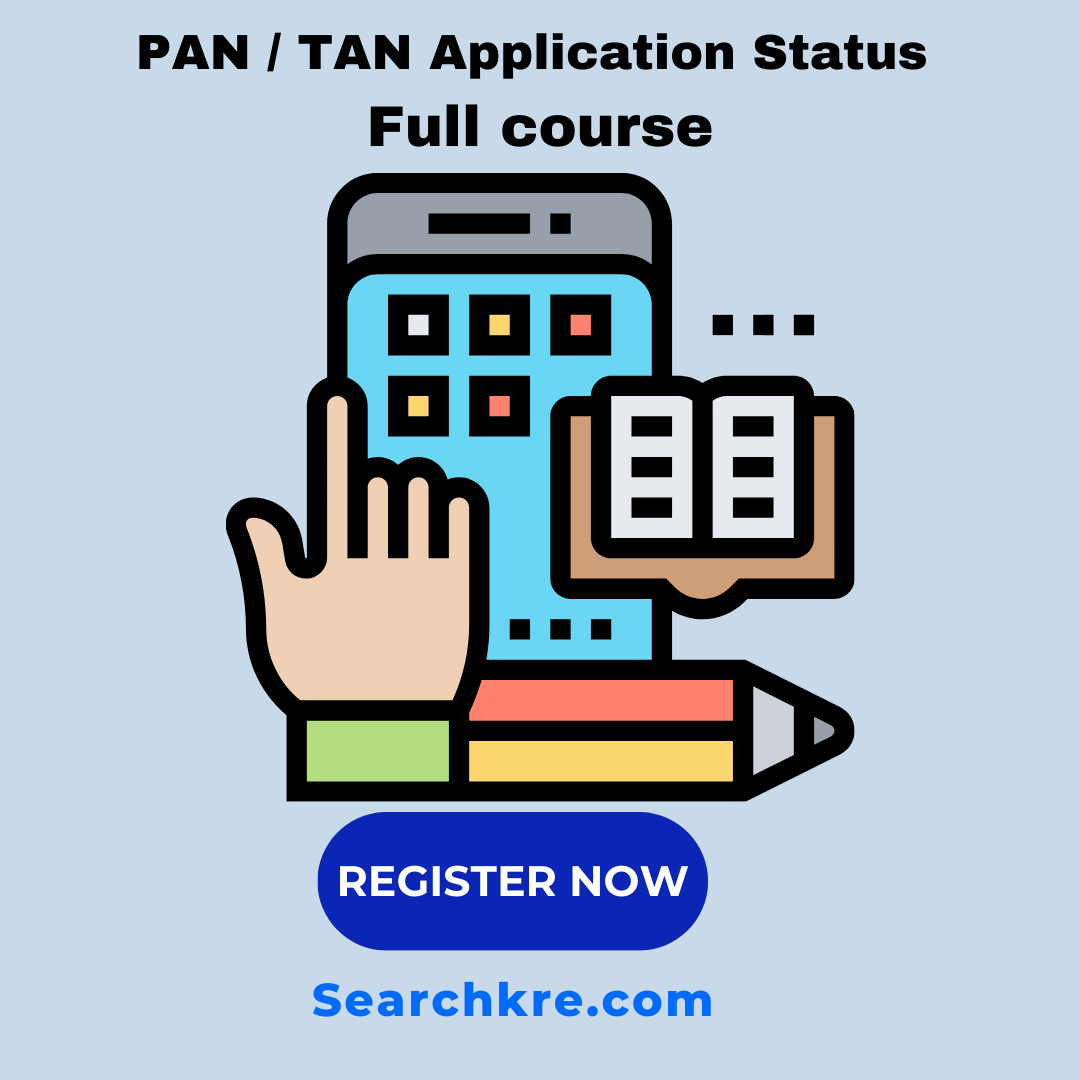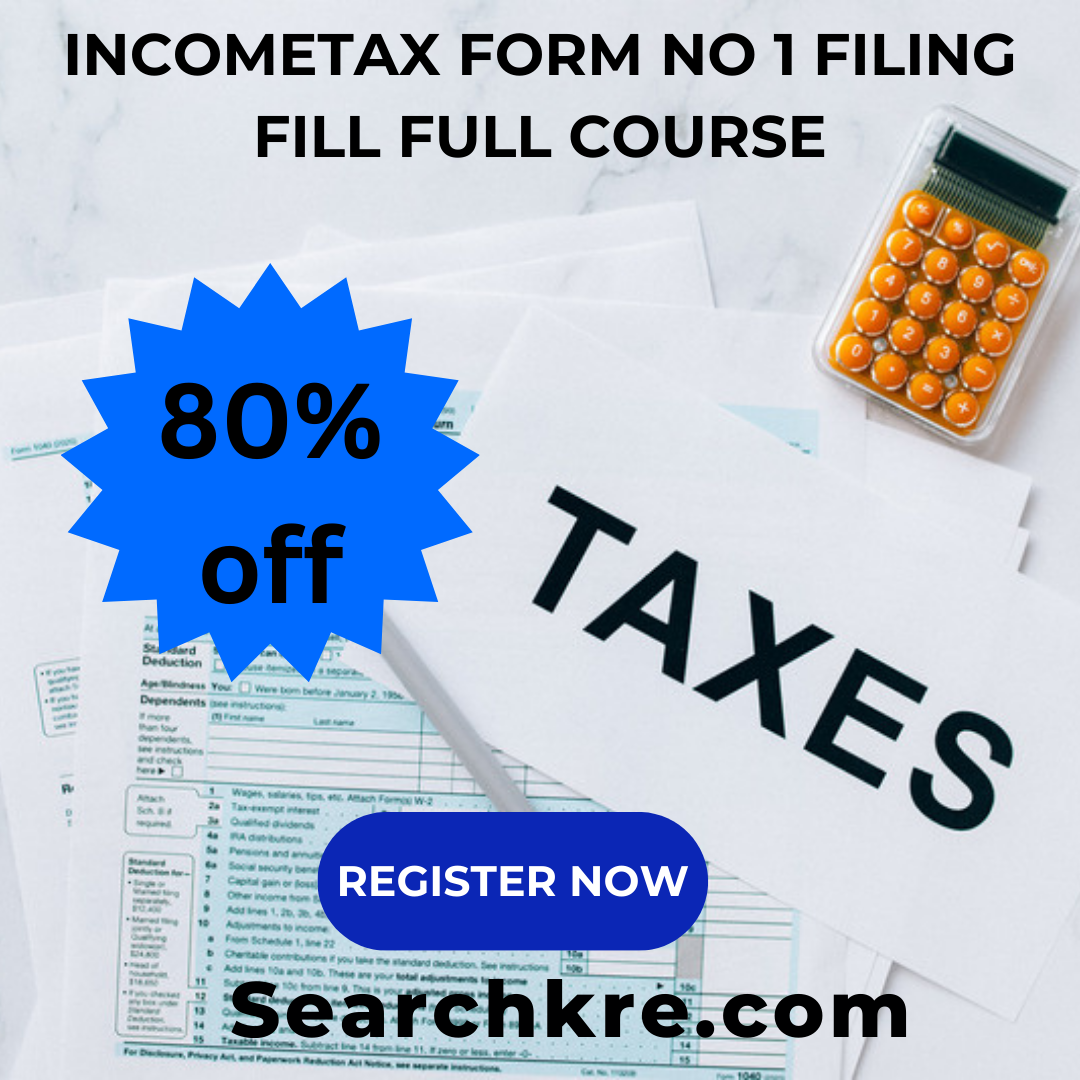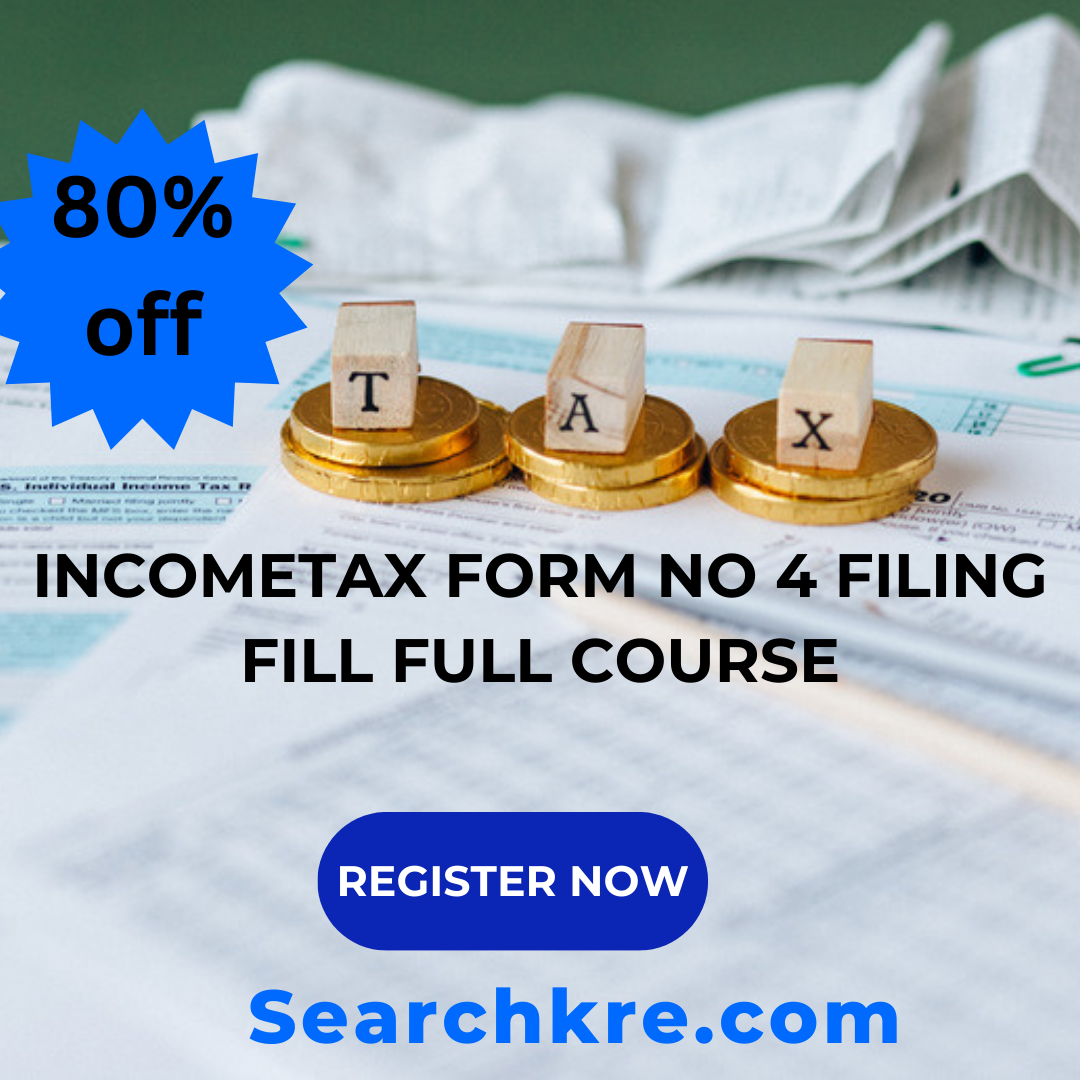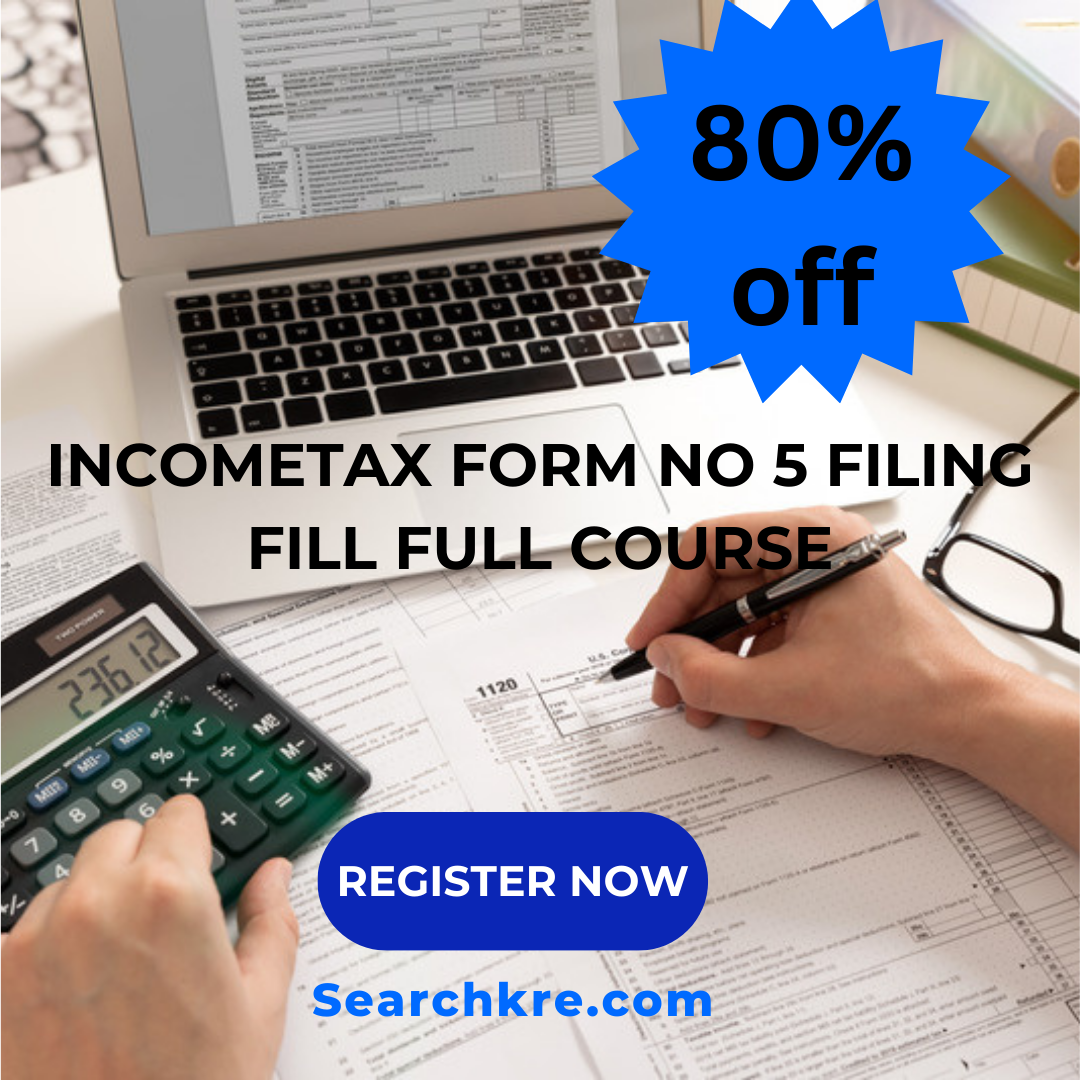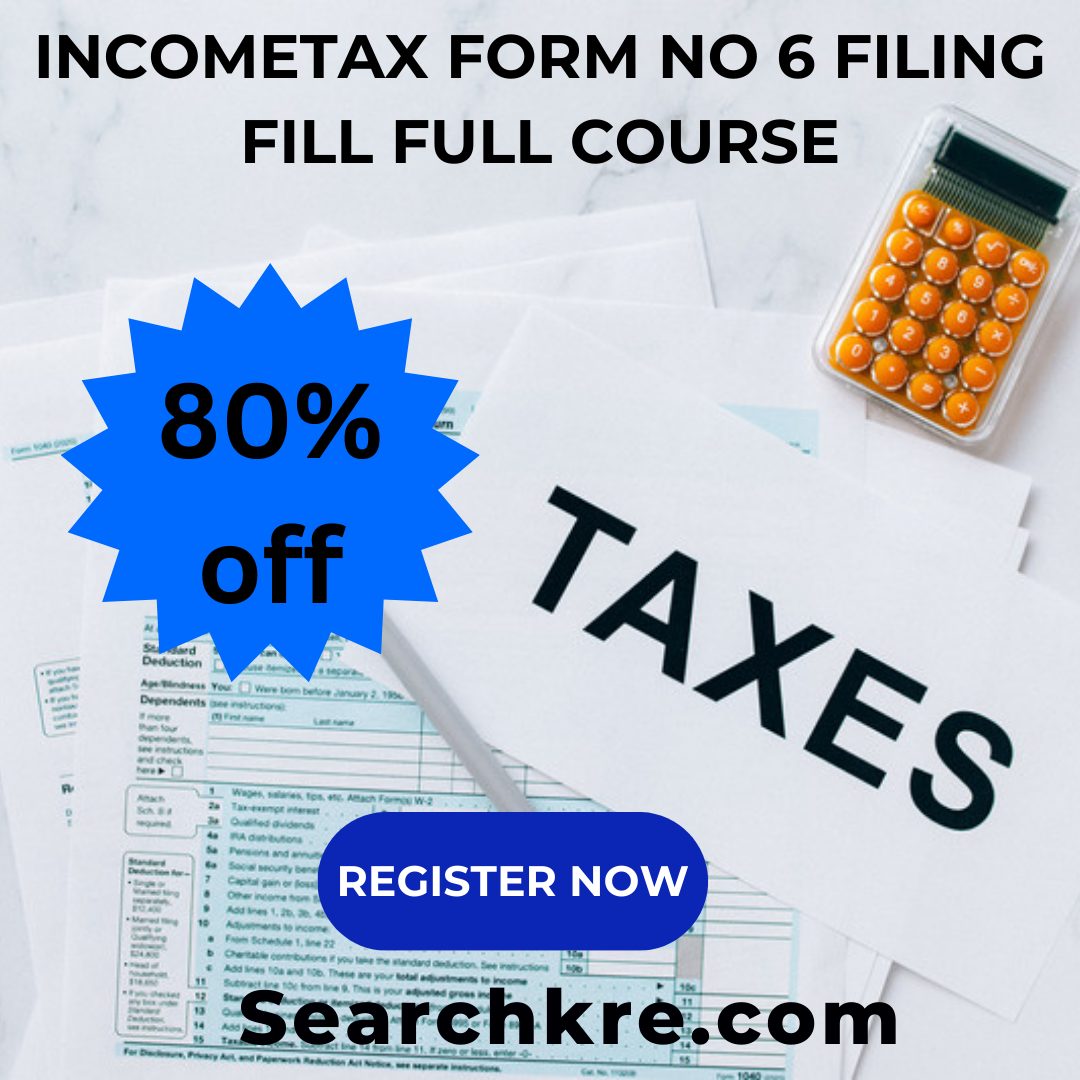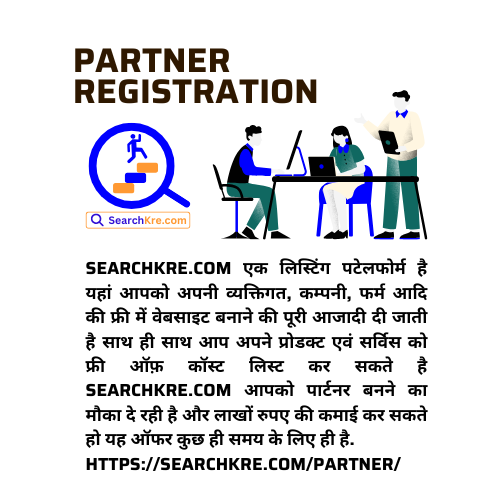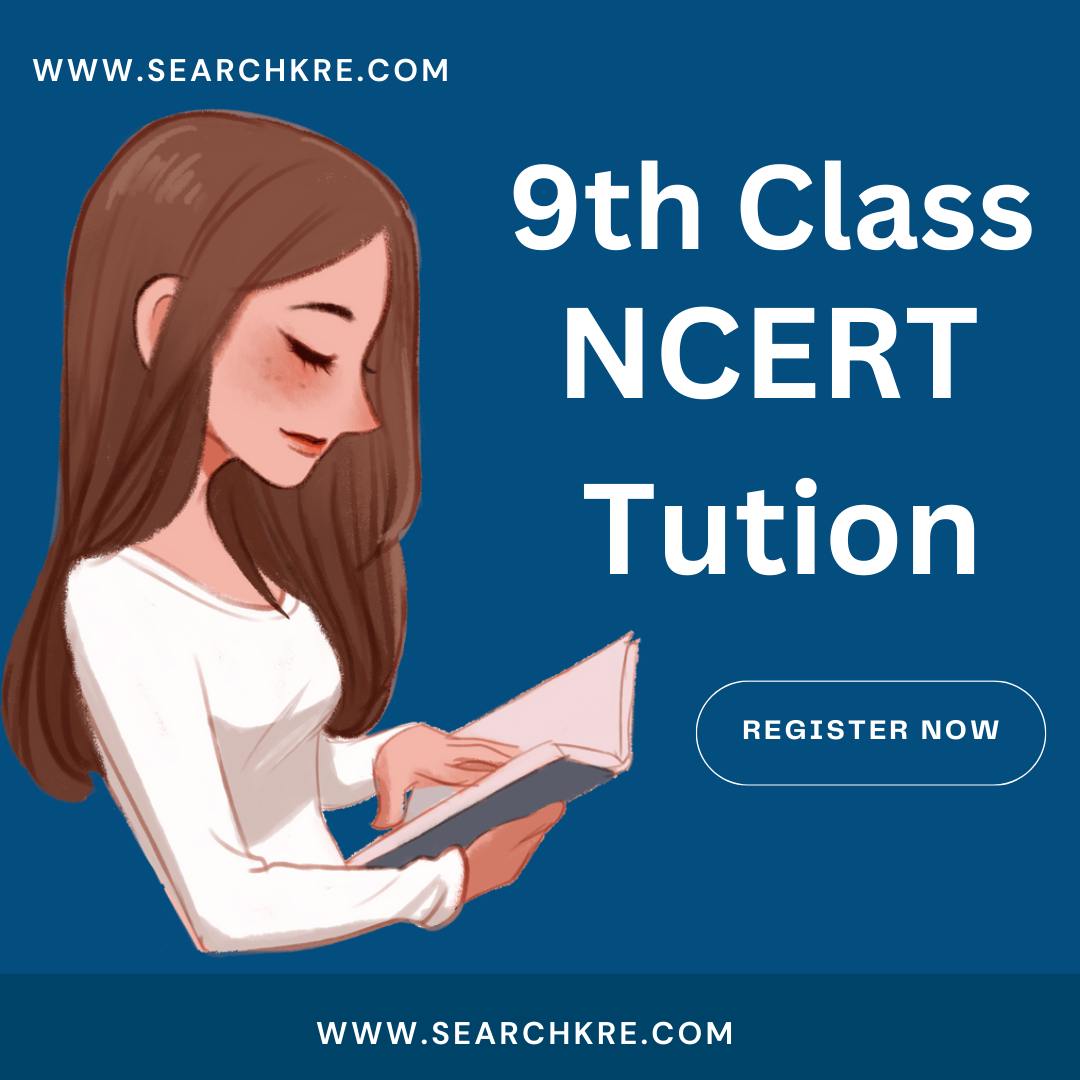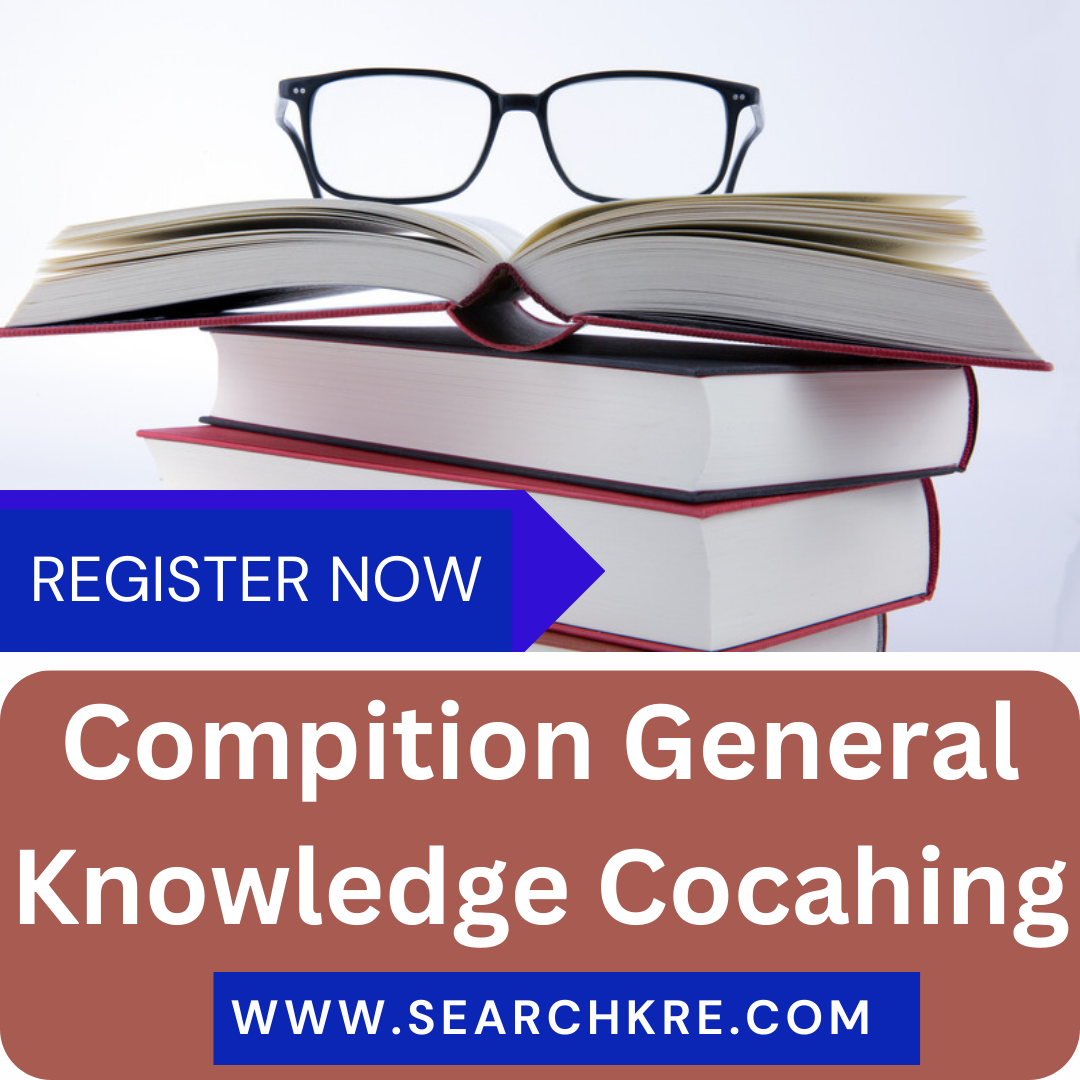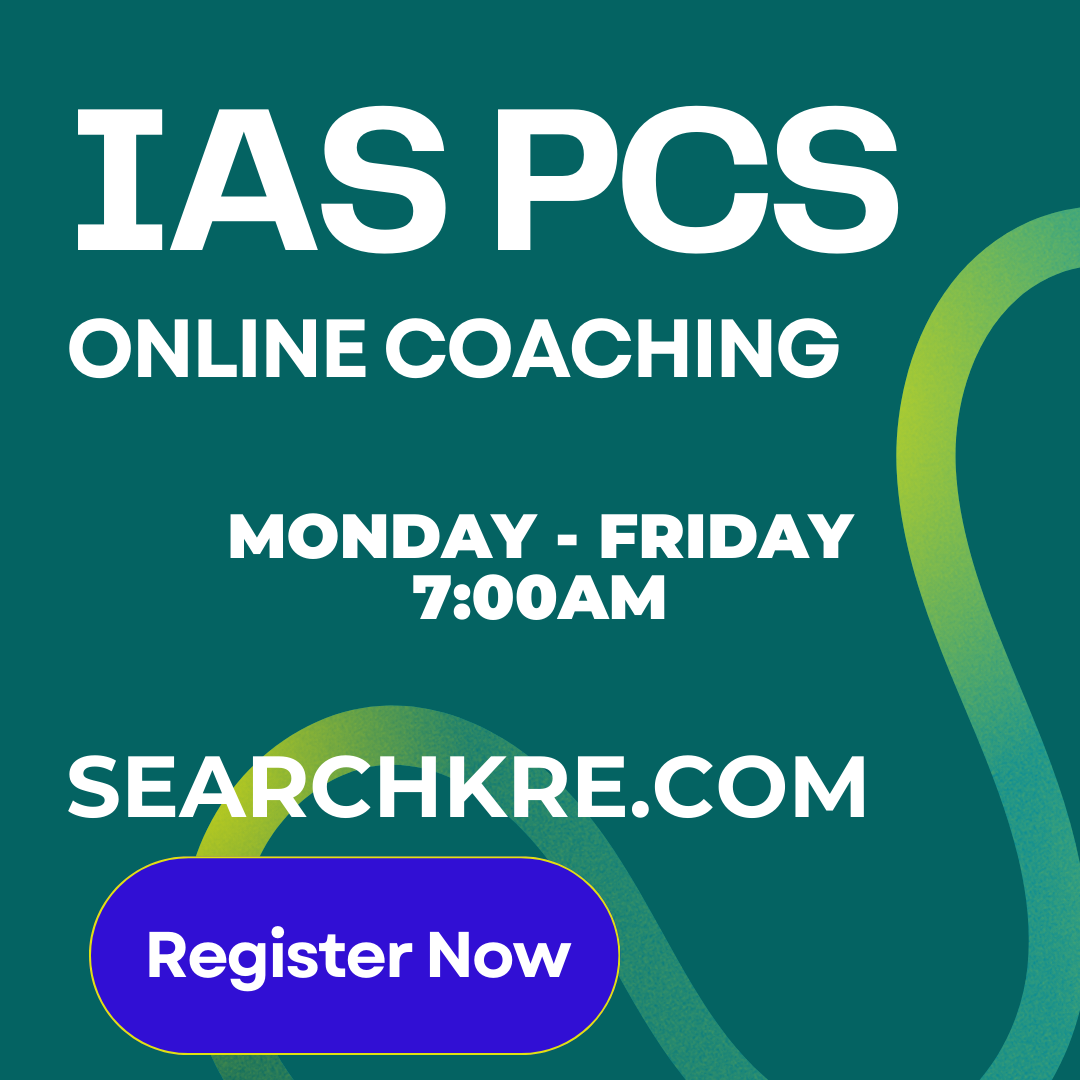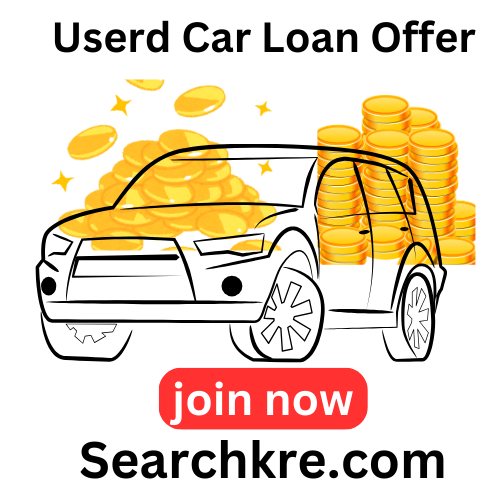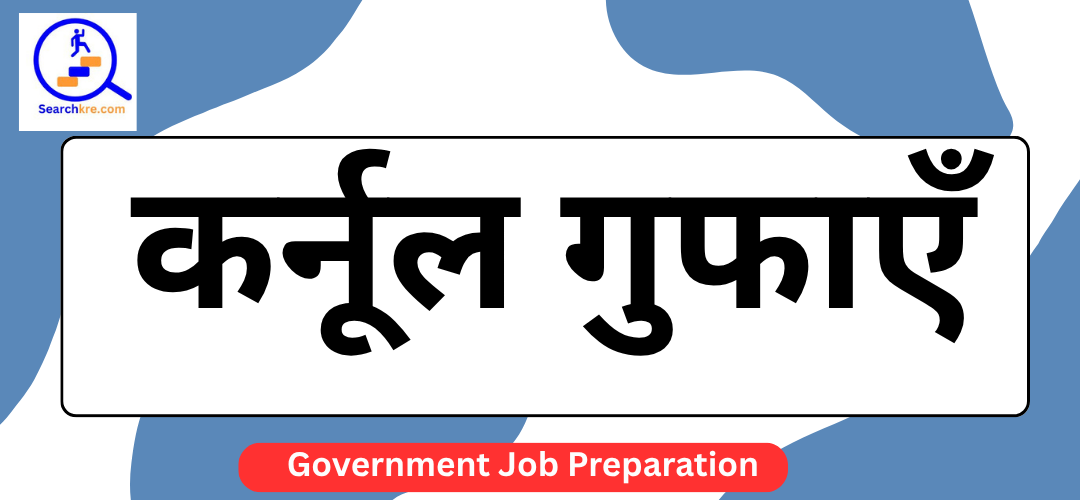
Kurnool Caves
jp Singh
2025-05-20 12:19:59
searchkre.com@gmail.com /
8392828781
कर्नूल गुफाएँ
कर्नूल गुफाएँ (Kurnool Caves)
कर्नूल गुफाएँ (Kurnool Caves), विशेष रूप से बेलम गुफाएँ (Belum Caves), आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित भारत की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण पुरापाषाण युगीन गुफाओं में से एक हैं। ये गुफाएँ अपने भूवैज्ञानिक महत्व, प्राकृतिक सुंदरता, और पुरातात्विक अवशेषों के लिए प्रसिद्ध हैं। कर्नूल क्षेत्र में अन्य गुफाएँ, जैसे यागंती गुफाएँ, और पुरापाषाण युग की शैल चित्रकला (Rock Paintings) भी इस क्षेत्र को प्रागैतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती हैं। नीचे कर्नूल गुफाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है, जिसमें बेलम गुफाएँ मुख्य रूप से शामिल हैं, साथ ही अन्य संबंधित गुफाओं और पुरातात्विक साक्ष्यों का उल्लेख है।
कर्नूल गुफाओं की पृष्ठभूमि
स्थान: बेलम गुफाएँ: कर्नूल जिले के बेलम गाँव में, कर्नूल शहर से लगभग 110 किमी और कोलिमिगुंडला से 15 किमी दूर। यागंती गुफाएँ: कर्नूल जिले के यागंती गाँव में, कर्नूल शहर से लगभग 70 किमी दूर। अन्य स्थल: कर्नूल जिले के केटावरम, जुरेरू वैली, कतावाणी कुंता, और योगंती में शैल चित्रकला और पुरातात्विक अवशेष।
काल: पुरापाषाण युग (Paleolithic Era): लगभग 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। मध्यपाषाण युग (Mesolithic Era): लगभग 10,000 से 5,000 वर्ष पूर्व। बेलम गुफाओं में बौद्ध और जैन भिक्षुओं के अवशेष 4500 वर्ष पुराने (बौद्ध-पूर्व युग) हैं।
खोज: बेलम गुफाएँ: 1884 में ब्रिटिश भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा खोजी गईं। 1982-1984 में जर्मन भूवैज्ञानिक एच. डैनियल गेबौएर ने इसका विस्तृत सर्वेक्षण किया। 1988 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया।
शैल चित्रकला: केटावरम, जुरेरू वैली, और अन्य स्थलों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और अन्य पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई।
पर्यावरण: कर्नूल जिला तुंगभद्रा, हुंड्री, और नीवा नदियों के किनारे बसा है, जो प्राचीन मानव के लिए जल और भोजन का स्रोत प्रदान करती थीं। बेलम गुफाएँ चूना पत्थर (Limestone) से बनी हैं, जो लाखों वर्षों में भूजल और नदी प्रवाह से निर्मित हुईं। क्षेत्र में घने जंगल, पहाड़ियाँ, और जैव-विविधता थी, जो शिकार-संग्रह के लिए उपयुक्त थी।
महत्व: बेलम गुफाएँ भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी गुफाएँ हैं (मेघालय की क्रेम लियत प्राह गुफाएँ सबसे लंबी हैं), जिनकी लंबाई 3.2 किमी है। ये गुफाएँ पुरापाषाण युगीन मानव की उपस्थिति, बौद्ध-जैन संस्कृति, और भूवैज्ञानिक संरचनाओं (स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट) के लिए प्रसिद्ध हैं। कर्नूल क्षेत्र की शैल चित्रकला प्राचीन मानव की कला और जीवनशैली को दर्शाती है।
कर्नूल गुफाओं की विशेषताएं
कर्नूल गुफाएँ, विशेष रूप से बेलम गुफाएँ, अपनी भूवैज्ञानिक, पुरातात्विक, और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। इनके साथ-साथ यागंती गुफाएँ और शैल चित्रकला भी महत्वपूर्ण हैं।
1. बेलम गुफाएँ
भूवैज्ञानिक संरचना: बेलम गुफाएँ चूना पत्थर से बनी हैं, जो लाखों वर्षों में भूजल और नदी प्रवाह से निर्मित हुईं। स्पेलोटेम संरचनाएँ (Speleothems): गुफाओं में स्टैलेक्टाइट (छत से लटकने वाली संरचनाएँ) और स्टैलेग्माइट (जमीन से उभरने वाली संरचनाएँ) की जटिल संरचनाएँ हैं। गुफा की लंबाई 3.2 किमी है, जिसमें लंबे रास्ते, संकीर्ण मार्ग, और चौड़े कक्ष (जैसे मेडिटेशन हॉल, बरगद का पेड़ हॉल, मंडपम) हैं। गुफा में प्राकृतिक जल स्रोत और भूमिगत नदी मार्ग हैं, जो पर्यटकों के लिए आकर्षक हैं।
पुरातात्विक महत्व: गुफाओं में 4500 वर्ष पुराने पात्र मिले हैं, जो बौद्ध और जैन भिक्षुओं की उपस्थिति को दर्शाते हैं। प्राचीन काल में ये गुफाएँ बौद्ध और जैन भिक्षुओं द्वारा ध्यान और निवास के लिए उपयोग की जाती थीं। पुरापाषाण युग के उपकरण और अवशेष गुफाओं के आसपास मिले हैं, जो मानव की प्रारंभिक उपस्थिति को दर्शाते हैं।
पर्यटक आकर्षण: गुफा में रोशनी और वेंटिलेशन की व्यवस्था की गई है, जिससे पर्यटक सुरक्षित रूप से घूम सकते हैं।
प्रमुख क्षेत्र: पातालगंगा (सबसे गहरा बिंदु, 150 फीट नीचे), संगीत हॉल (ध्वनि प्रभाव के लिए), और मेडिटेशन हॉल।
प्रवेश शुल्क: ₹65 (वयस्क), समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे।
सांस्कृतिक महत्व: बेलम गुफाएँ प्रकृति और मानव इतिहास के मिश्रण का प्रतीक हैं। इनका उपयोग धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए होता था। गुफाओं का नाम स्थानीय तेलुगु शब्द बेलम गुहलू (Belum Guhalu) से लिया गया है।
2. यागंती गुफाएँ
स्थान और संरचना: यागंती गुफाएँ यागंती उमा महेश्वर मंदिर (भगवान शिव को समर्पित) के पास पहाड़ियों में स्थित हैं। ये गुफाएँ प्राकृतिक चूना पत्थर से बनी हैं और छोटी लेकिन धार्मिक महत्व की हैं। प्रमुख गुफाएँ: वेंकटेश्वर गुफा, रोकल्ला गुफा, और शंकर गुफा, जो मंदिर के पास हैं।
धार्मिक महत्व: गुफाएँ यागंती मंदिर के साथ जुड़ी हैं, जहाँ नंदी की मूर्ति हर साल आकार में बढ़ती मानी जाती है। इन गुफाओं का उपयोग प्राचीन काल में साधु-संतों द्वारा ध्यान और तपस्या के लिए किया जाता था।
पुरातात्विक साक्ष्य: गुफाओं के आसपास पुरापाषाण युग के कुछ अवशेष और चित्र मिले हैं, जो मानव गतिविधियों को दर्शाते हैं।
पर्यटक आकर्षण: गुफाएँ मंदिर के दर्शन के साथ-साथ रोमांचक अनुभव प्रदान करती हैं। आसपास का शांत वातावरण और प्राकृतिक झरना (पोटुलुरी वीरब्रह्मेंद्र स्वामी द्वारा खोजा गया) पर्यटकों को आकर्षित करता है।
3. शैल चित्रकला (Rock Paintings)
स्थान: कर्नूल जिले के केटावरम, जुरेरू वैली, कतावाणी कुंता, और योगंती में शैल चित्रकला मिली है। ये चित्र गुफाओं और चट्टानों की दीवारों पर हैं।
काल: 35,000 से 40,000 वर्ष पुरानी, जो पुरापाषाण और मध्यपाषाण युग से संबंधित हैं।
विशेषताएँ: चित्रों में जंगली जानवर (हिरण, सुअर, भैंस), मानव आकृतियाँ, शिकार दृश्य, और ज्यामितीय चिह्न शामिल हैं। लाल, पीले, और सफेद रंगों का उपयोग, जो प्राकृतिक खनिजों (जैसे आयरन ऑक्साइड) से बनाए गए थे।
महत्व: ये चित्र प्राचीन मानव की कला, जीवनशैली, और पर्यावरण को दर्शाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भीमबेटका (मध्य प्रदेश) के बाद कर्नूल की शैल चित्रकला सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है।
4. जीवनशैली और आर्थिक गतिविधियाँ
शिकार-संग्रह: कर्नूल गुफाओं के आसपास के मानव शिकारी-संग्रहकर्ता थे। वे जंगली जानवरों (हिरण, सुअर) का शिकार और जंगली फल, जड़ें, और बीज इकट्ठा करते थे। तुंगभद्रा और हुंड्री नदियाँ मछली पकड़ने और जल स्रोत प्रदान करती थीं।
खानाबदोश जीवन: मानव छोटे समूहों (10-30 लोग) में रहता था और गुफाओं को अस्थायी आश्रय के रूप में उपयोग करता था। गुफाएँ प्राकृतिक आपदाओं (बारिश, जंगली जानवर) से सुरक्षा प्रदान करती थीं।
पर्यावरणीय अनुकूलन: कर्नूल का क्षेत्र उपजाऊ मैदानों, जंगलों, और पहाड़ियों से समृद्ध था, जो शिकार और भोजन संग्रह के लिए उपयुक्त था। चूना पत्थर और क्वार्टजाइट पत्थरों की उपलब्धता ने उपकरण निर्माण को बढ़ावा दिया।
प्रारंभिक तकनीक: पुरापाषाण युग में मानव चॉपर, स्क्रेपर, और फ्लेक उपकरण बनाता था।
अग्नि का उपयोग संभवतः शुरू हो चुका था, लेकिन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण सीमित हैं। बर्तन निर्माण, कृषि, और पशुपालन का ज्ञान नहीं था।
5. सामाजिक और धार्मिक संगठन
सामाजिक संरचना: छोटे कबीले-आधारित समूह, जिनमें सहयोग और श्रम विभाजन प्रचलित था। नेतृत्व उम्र, अनुभव, या शारीरिक शक्ति पर आधारित था।
लिंग आधारित भूमिकाएँ: पुरुष शिकार करते थे, जबकि महिलाएँ भोजन संग्रह और बच्चों की देखभाल करती थीं।
धार्मिक विश्वास: पुरापाषाण युग में धार्मिक प्रथाओं के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं, लेकिन प्रकृति पूजा (नदियाँ, पेड़, जानवर) संभव थी। बौद्ध और जैन भिक्षुओं ने बाद में बेलम गुफाओं को ध्यान और तपस्या के लिए उपयोग किया। यागंती गुफाएँ शिव भक्ति और आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ी थीं।
मृतक संस्कार: दफन प्रथाओं के प्रमाण नहीं मिले हैं, जो इस काल की साधारण जीवनशैली को दर्शाता है।
6. पुरातात्विक अवशेष
मानव अवशेष: कर्नूल गुफाओं से मानव कंकाल या जीवाश्म नहीं मिले हैं, लेकिन उपकरण और शैल चित्र मानव उपस्थिति को दर्शाते हैं।
पशु अवशेष: गुफाओं के आसपास हिरण, सुअर, और अन्य जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जो शिकार को दर्शाती हैं।
पाषाण उपकरण: चॉपर, स्क्रेपर, और फ्लेक उपकरण, जो पुरापाषाण युग की मद्रासियन संस्कृति से संबंधित हैं।
बौद्ध-जैन अवशेष: बेलम गुफाओं में 4500 वर्ष पुराने मिट्टी के पात्र, जो बौद्ध और जैन भिक्षुओं से संबंधित हैं।
शैल चित्रकला: केटावरम और जुरेरू वैली में 35,000-40,000 वर्ष पुरानी चित्रकला, जो मानव और जानवरों की आकृतियाँ दर्शाती है।
7. सांस्कृतिक और तकनीकी महत्व
पुरापाषाण युग: कर्नूल गुफाएँ दक्षिण भारत की मद्रासियन संस्कृति का हिस्सा हैं, जो अशूलियन परंपरा (हैंड-एक्स और क्लीवर) से भिन्न है लेकिन चॉपर-स्क्रेपर उपकरणों पर आधारित है। शैल चित्रकला प्राचीन मानव की कला और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाती है।
बौद्ध-जैन संस्कृति: बेलम गुफाएँ बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए ध्यान स्थल थीं, जो दक्षिण भारत में इन धर्मों के प्रसार को दर्शाती हैं।
भूवैज्ञानिक महत्व: बेलम गुफाओं की स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट संरचनाएँ लाखों वर्षों की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को दर्शाती हैं।
वैश्विक संदर्भ: कर्नूल की शैल चित्रकला को मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं और यूरोप की लास्को गुफाओं से तुलना की जाती है, जो वैश्विक पुरापाषाण कला का हिस्सा हैं।
बेलम गुफाएँ अन्य चूना पत्थर गुफाओं (जैसे मलेशिया की निआह गुफाएँ) से भूवैज्ञानिक समानता रखती हैं।
कर्नूल गुफाओं के प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य
3.2 किमी लंबी चूना पत्थर गुफाएँ, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट संरचनाएँ।
4500 वर्ष पुराने बौद्ध-जैन पात्र।
यागंती गुफाएँ: वेंकटेश्वर, रोकल्ला, और शंकर गुफाएँ, जो मंदिर और आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ी हैं।
शैल चित्रकला: केटावरम, जुरेरू वैली, और योगंती में 35,000-40,000 वर्ष पुरानी चित्रकला।
पाषाण उपकरण: चॉपर, स्क्रेपर, और फ्लेक उपकरण, जो पुरापाषाण युग की गतिविधियों को दर्शाते हैं।
पशु अवशेष: हिरण, सुअर, और अन्य जानवरों की हड्डियाँ, जो शिकार को दर्शाती हैं।
कर्नूल गुफाओं का महत्व
मानव विकास का साक्ष्य: कर्नूल गुफाएँ और शैल चित्रकला दक्षिण भारत में पुरापाषाण युगीन मानव की उपस्थिति और कला को दर्शाती हैं। ये स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में मानव विकास और सांस्कृतिक प्रगति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
भूवैज्ञानिक महत्व: बेलम गुफाएँ चूना पत्थर संरचनाओं और स्पेलोटेम गठन के अध्ययन के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला हैं।
धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व: बेलम गुफाएँ बौद्ध और जैन भिक्षुओं के ध्यान स्थल के रूप में, जबकि यागंती गुफाएँ शिव भक्ति के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण हैं।
पर्यटकीय महत्व: बेलम गुफाएँ भारत की सबसे लोकप्रिय गुफाओं में से एक हैं, जो पर्यटकों को रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करती हैं। यागंती गुफाएँ और मंदिर धार्मिक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
वैश्विक महत्व: कर्नूल की शैल चित्रकला और गुफाएँ वैश्विक पुरापाषाण कला और भूवैज्ञानिक संरचनाओं के साथ तुलनीय हैं, जो भारत की प्राचीन विरासत को विश्व पटल पर लाती हैं।
कर्नूल गुफाओं की चुनौतियाँ
संरक्षण: प्राकृतिक क्षरण, नमी, और मानव गतिविधियाँ (पर्यटन, खनन) गुफाओं और शैल चित्रकला को नुकसान पहुँचा रही हैं। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट संरचनाएँ पर्यटकों के स्पर्श से प्रभावित हो रही हैं।
सीमित मानव अवशेष: कर्नूल गुफाओं से मानव कंकाल या जीवाश्म नहीं मिले हैं, जिससे सामाजिक और धार्मिक जीवन का अध्ययन कठिन है।
अनुसंधान की कमी: बेलम गुफाओं को छोड़कर, अन्य गुफाओं (जैसे यागंती) और शैल चित्रकला पर व्यापक अनुसंधान की आवश्यकता है।
जागरूकता: कर्नूल गुफाओं और शैल चित्रकला के महत्व को स्थानीय और वैश्विक स्तर पर और प्रचारित करने की आवश्यकता है।
Conclusion
Thanks For Read
jp Singh
searchkre.com@gmail.com
8392828781
 Gst Registration
Gst Registration
 DSC Registration
DSC Registration
 Pancard Registration
Pancard Registration
 Company Registration
Company Registration
 Fssai Registration
Fssai Registration
 TradeMark Registration
TradeMark Registration
 MSME Registration
MSME Registration
 Passport Registration
Passport Registration
 Income Tax Return
Income Tax Return
 LLP Company Registration
LLP Company Registration
 Marriage And Court Marriage Registration
Marriage And Court Marriage Registration
 PVT LTD Company Registration
PVT LTD Company Registration
 GST Filing Services
GST Filing Services
 Coaching Insititute Registration
Coaching Insititute Registration
 GYM Registration
GYM Registration
 NGO Registration
NGO Registration
 Political Party Registration
Political Party Registration
 Society Registration
Society Registration
 Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
 Make Website on EMI
Make Website on EMI



























































































 9th Class Scholarship Competition Test
9th Class Scholarship Competition Test
 10th Class Scholarship Competition Test
10th Class Scholarship Competition Test
 11th Class Scholarship Competition Test
11th Class Scholarship Competition Test
 12th Class Scholarship Competition Test
12th Class Scholarship Competition Test
 Graduation Scholarship Competition Test
Graduation Scholarship Competition Test
 Post Graduation Scholarship Competition Test
Post Graduation Scholarship Competition Test
 Diploma Scholarship Competition Test
Diploma Scholarship Competition Test
 Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 JEE Coaching Scholarship Competition Test
JEE Coaching Scholarship Competition Test
 NEET Coaching Scholarship Competition Test
NEET Coaching Scholarship Competition Test
 Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test