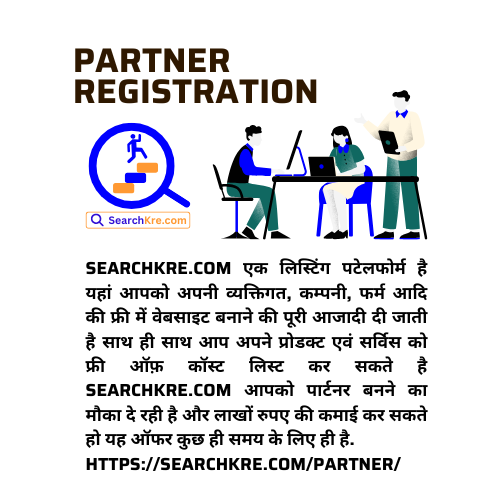Glasgow Climate Conference ग्लास्गो जलवायु सम्मेलन (COP26)
jp Singh
2025-05-03 00:00:00
searchkre.com@gmail.com /
8392828781
Glasgow Climate Conference ग्लास्गो जलवायु सम्मेलन (COP26)
जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट बन चुका है, जो पृथ्वी पर जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। बढ़ते तापमान, बर्फ की बर्फबारी का घटना, समुद्र स्तर में वृद्धि, और जलवायु आपदाएँ जैसे तूफान और बाढ़ इसके मुख्य संकेतक हैं। यह संकट पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। इस संकट से निपटने के लिए विभिन्न देशों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना शुरू किया। इस दिशा में COP26 सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जो 31 अक्टूबर से 12 नवम्बर 2021 तक
1. ग्लास्गो जलवायु सम्मेलन का इतिहास और उद्देश्य
COP (Conference of the Parties) की शुरुआत 1992 में रियो डि जिनेरो में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन का आयोजन किया था। यह सम्मेलन पेरिस समझौते (Paris Agreement) के बाद दुनिया भर के देशों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, जहाँ देशों ने अपनी जलवायु नीतियों को फिर से परखा और भविष्य की रणनीतियों पर विचार किया।
COP26 का आयोजन 2021 में ग्लास्गो में किया गया, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए वैश्विक संकल्पों की घोषणा करना और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाना।
2. ग्लास्गो सम्मेलन में प्रमुख बिंदु
ग्लास्गो सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ और समझौते हुए, जिनसे जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रयासों को गति मिली:
कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य:
सम्मेलन में देशों ने यह संकल्प लिया कि वे 2050 तक नेट ज़ीरो (Net Zero) उत्सर्जन की दिशा में कदम उठाएँगे। इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए जितना कार्बन उत्सर्जित होगा, उतना ही कार्बन अवशोषित करने के उपाय किए जाएंगे।
पेरिस समझौते का पालन:
COP26 में पेरिस समझौते के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना था।
ग्लास्गो जलवायु घोषणाएँ:
इस सम्मेलन में कई देशों ने अपने उत्सर्जन घटाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की। इसमें मुख्य रूप से चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, और भारत जैसे देशों के प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण पहल की।
जलवायु वित्त:
ग्लास्गो में जलवायु वित्त पर भी चर्चा की गई, जिसमें विकसित देशों से विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता देने की प्रतिबद्धता दिखाई गई। यह मुद्दा जलवायु न्याय के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय कर सकें।
3. ग्लास्गो सम्मेलन में भारत की भूमिका
भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, ने ग्लास्गो सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को और मजबूत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पाँच प्रमुख जलवायु प्रतिबद्धताओं की घोषणा की, जिनमें शामिल हैं:
नेट ज़ीरो 2070 तक:
भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन की दिशा में काम करने का वादा किया।
50% ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय:
भारत ने 2030 तक अपनी ऊर्जा का 50% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया।
ऊर्जा दक्षता में वृद्धि:
ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और ऊर्जा उत्सर्जन को कम करने के लिए नई नीतियाँ लागू करने की बात कही।
भारत की भूमिका अन्य विकासशील देशों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आई, जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं, लेकिन उनके पास पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक संसाधन नहीं हैं
4. विकसित और विकासशील देशों की भूमिका
ग्लास्गो सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। जहां विकसित देशों ने अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की, वहीं विकासशील देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहयोग की मांग की।
विकसित देशों का दायित्व था कि वे विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें। इसमें जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, और अन्य सहयोगों की जरूरत थी।
5. COP26 के परिणाम और प्रभाव
ग्लास्गो सम्मेलन ने कई सकारात्मक परिणाम दिए, जिनमें प्रमुख हैं:
कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए ठोस कदम:
देशों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं और रणनीतियों पर काम करने की सहमति दी।
पेरिस समझौते का पालन:
देशों ने पेरिस समझौते के तहत अपने लक्ष्यों को फिर से परिभाषित किया और उन्हें साकार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया।
जलवायु वित्त का वादा:
विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त सहायता में वृद्धि का वादा किया।
6. भारत और अन्य देशों के लिए चुनौतियाँ
भारत और अन्य विकासशील देशों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा
वित्तीय सहायता की कमी:
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी, जो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो सकी।
ऊर्जा संक्रमण:
कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता थी।
7. भविष्य की दिशा और समाधान
ग्लास्गो सम्मेलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर काम करना होगा। कुछ सुझाव इस प्रकार हो सकते हैं:
जलवायु शिक्षा और जागरूकता:
जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को शिक्षित करना और उन्हें जागरूक करना जरूरी है।
नई प्रौद्योगिकियों का विकास:
नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड्स, और कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का विकास महत्वपूर्ण होगा।
सतत विकास की नीतियाँ:
देशों को अपनी विकास नीतियों में सतत विकास को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि पर्यावरण पर कम दबाव पड़े।
9. COP26 के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दे और उनके वैश्विक प्रभाव
ग्लास्गो सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनका वैश्विक प्रभाव हो सकता है। इनमें से कुछ प्रमुख मुद्दे और उनके संभावित प्रभाव निम्नलिखित हैं:
9. कार्बन बाजार और उत्सर्जन व्यापार
एक मुख्य मुद्दा जो COP26 में उठा, वह था कार्बन बाजार। यह बाजार देशों और कंपनियों को अपने कार्बन उत्सर्जन को अन्य देशों या संगठनों से खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। इस व्यापार के माध्यम से, देशों को अपनी उत्सर्जन सीमा तक पहुँचने में मदद मिल सकती है। हालांकि, यह भी सवाल उठता है कि क्या इससे वास्तव में उत्सर्जन में कमी आएगी, या यह केवल एक व्यापारिक उपकरण बनकर रह जाएगा।
10. नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन
COP26 में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने पर चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सौर, पवन, और जल ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग आवश्यक है। देशों ने यह वादा किया कि वे 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अपना योगदान बढ़ाएँगे।
हालांकि, कई विकासशील देशों के लिए यह बड़ी चुनौती है क्योंकि उनके पास इन स्रोतों को विकसित करने के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान नहीं हैं। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता है।
11. जलवायु न्याय (Climate Justice)
COP26 में जलवायु न्याय एक महत्वपूर्ण विषय था। विकासशील देशों और छोटे द्वीपीय देशों ने यह आवाज उठाई कि उनके देशों को जलवायु परिवर्तन के सबसे अधिक नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ता है, जबकि उनका कार्बन उत्सर्जन बहुत कम है। इस प्रकार, उन्होंने यह मांग की कि विकसित देश, जो मुख्य रूप से कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं,
उन्हें जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की मदद करनी चाहिए। यह "सहयोगात्मक न्याय" का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जलवायु परिवर्तन के समाधान में न्यायपूर्ण वितरण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
12. जलवायु संकट के कारण होने वाली आर्थिक असमानताएँ
जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण को ही नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक ढाँचे को भी प्रभावित करता है। COP26 में यह माना गया कि जलवायु संकट से उत्पन्न होने वाली आर्थिक असमानताएँ और सामाजिक असुरक्षा विश्व स्तर पर बढ़ सकती हैं। उदाहरण के लिए, समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण छोटे द्वीप देशों को अपने घरों और संसाधनों से हाथ धोना पड़ सकता है, जिससे उनकी अ
इसके अलावा, कृषि क्षेत्रों में आए बदलाव और जलवायु आपदाओं के कारण विकासशील देशों में बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि हो सकती है। इसलिए, विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए जलवायु संकट से निपटने के लिए वित्तीय और प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करना आवश्यक है।
13. वन संरक्षण और पुनर्वनीकरण
COP26 में वनों के संरक्षण और पुनर्वनीकरण को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में पेश किया गया। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इससे पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कई देशों ने वादा किया कि वे अपने जंगलों के संरक्षण के लिए कदम उठाएँगे औ
14. हरित वित्त (Green Finance)
एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा था हरित वित्त या ग्रीन फाइनेंस। ग्रीन फाइनेंस का उद्देश्य पर्यावरणीय परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देना है, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु-समर्थक कृषि, और जलवायु परिवर्तन से बचाव के उपाय। COP26 में इस पर जोर दिया गया कि वित्तीय संस्थाओं और सरकारों को ग्रीन फाइनेंस के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि कंपनियाँ और देशों को पर्यावरणीय कार्यों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिले।
15. COP26 के प्रभाव और आलोचनाएँ
जैसा कि हर बड़े सम्मेलन में होता है, COP26 के परिणामों के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण हैं। सम्मेलन के दौरान हुए कई समझौतों और घोषणाओं ने उम्मीद की किरण जगाई, लेकिन कुछ आलोचनाएँ भी उठी हैं:
16. उत्सर्जन में वास्तविक कमी का अभाव
COP26 में वैश्विक नेताओं ने कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए कई प्रतिबद्धताएँ कीं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इन वादों का वास्तविक प्रभाव बहुत कम हो सकता है। कुछ देशों ने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं। उदाहरण के लिए, नेट ज़ीरो तक पहुंचने के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाले तकनीकों में निवेश और कार्बन कैप्चर योजनाओं पर काम करने की आवश्यकता है, लेकिन कई देशों ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए।
17. विकासशील देशों की चिंताएँ
विकसित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय मदद देने की बात की गई, लेकिन कई विकासशील देशों का कहना है कि ये वादे वास्तविकता से दूर हैं। इन देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न केवल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें उच्चतम स्तर की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की भी आवश्यकता है, जो बहुत हद तक विकसित देशों पर निर्भर करता है।
18. वित्तीय सहायता के लिए ठोस कदमों का अभाव
विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त के लिए 100 बिलियन डॉलर की सहायता का वादा किया गया था, लेकिन इसकी वास्तविकता पर कई सवाल खड़े हैं। कई विकासशील देशों का कहना है कि उन्हें वास्तविक समय पर सहायता नहीं मिल पा रही है, और यदि यह वादा पूरा नहीं हुआ तो ये देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में असमर्थ रह सकते हैं।
19. भारत का भविष्य: COP26 के बाद की भूमिका
भारत की भूमिका COP26 में बहुत महत्वपूर्ण रही, और यह सम्मेलन भारत के लिए एक अवसर भी था। भारत, जो पहले ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई योजनाएँ बना चुका है, अब COP26 में अपनी प्रतिबद्धताओं को और मजबूत कर सकता है। भारत के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों ही हैं:
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश:
भारत ने यह वादा किया है कि वह 2030 तक अपनी ऊर्जा का 50% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करेगा। इसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता है, और भारत को अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए इस दिशा में सक्रिय कदम उठाने होंगे।
जलवायु वित्त और तकनीकी सहयोग:
भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए। भारत को जलवायु वित्त की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझने और इसे लागू करने की आवश्यकता होगी।
Conclusion
ग्लास्गो जलवायु सम्मेलन (COP26) एक वैश्विक मंच था जहाँ देशों ने जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की और भविष्य के लिए साझा समाधान पर चर्चा की। हालांकि, कई सकारात्मक कदम उठाए गए, लेकिन इसका कार्यान्वयन और वास्तविक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे।
जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए वैश्विक सहयोग और व्यक्तिगत देशों की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना बेहद महत्वपूर्ण होगा। COP26 ने यह संदेश दिया कि यदि हम जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने में असफल रहते हैं, तो इसके परिणाम पृथ्वी पर जीवन के लिए विनाशकारी हो सकते हैं।
Thanks For Read
jp Singh
searchkre.com@gmail.com
8392828781
 Gst Registration
Gst Registration
 DSC Registration
DSC Registration
 Pancard Registration
Pancard Registration
 Company Registration
Company Registration
 Fssai Registration
Fssai Registration
 TradeMark Registration
TradeMark Registration
 MSME Registration
MSME Registration
 Passport Registration
Passport Registration
 Income Tax Return
Income Tax Return
 LLP Company Registration
LLP Company Registration
 Marriage And Court Marriage Registration
Marriage And Court Marriage Registration
 PVT LTD Company Registration
PVT LTD Company Registration
 GST Filing Services
GST Filing Services
 Coaching Insititute Registration
Coaching Insititute Registration
 GYM Registration
GYM Registration
 NGO Registration
NGO Registration
 Political Party Registration
Political Party Registration
 Society Registration
Society Registration
 Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
 Make Website on EMI
Make Website on EMI


























































































 9th Class Scholarship Competition Test
9th Class Scholarship Competition Test
 10th Class Scholarship Competition Test
10th Class Scholarship Competition Test
 11th Class Scholarship Competition Test
11th Class Scholarship Competition Test
 12th Class Scholarship Competition Test
12th Class Scholarship Competition Test
 Graduation Scholarship Competition Test
Graduation Scholarship Competition Test
 Post Graduation Scholarship Competition Test
Post Graduation Scholarship Competition Test
 Diploma Scholarship Competition Test
Diploma Scholarship Competition Test
 Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 JEE Coaching Scholarship Competition Test
JEE Coaching Scholarship Competition Test
 NEET Coaching Scholarship Competition Test
NEET Coaching Scholarship Competition Test
 Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test