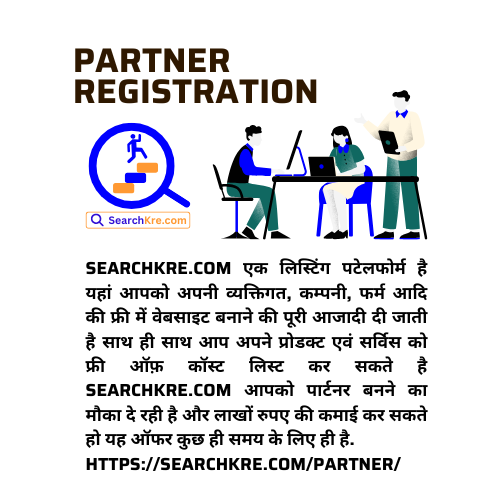Folk songs of Uttarakhand - उत्तराखंड के लोकगीत
jp Singh
2025-05-02 00:00:00
searchkre.com@gmail.com /
8392828781
Folk songs of Uttarakhand - उत्तराखंड के लोकगीत
उत्तराखंड के लोकगीत राज्य की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो यहां की लोकजीवन, परंपराएं, रीति-रिवाज़, प्रकृति और सामाजिक संरचना को प्रतिबिंबित करते हैं। उत्तराखंड के लोकगीतों में पर्वतीय जीवन की कठिनाइयों, प्रकृति की सुंदरता, प्रेम, भक्ति, वीरता और सामाजिक उत्सवों की झलक मिलती है।
1. उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीतों के प्रकार:
1. जागर गीत
यह गीत देवी-देवताओं को जागृत करने के लिए गाए जाते हैं। यह एक तरह का धार्मिक अनुष्ठान होता है जिसमें गायन के माध्यम से लोकदेवताओं को बुलाया जाता है। इनमें पौराणिक कथाओं और लोककथाओं को गाया जाता है।
2. थड्या गीत (थड़िया)
यह गीत सामूहिक नृत्य के साथ गाए जाते हैं। त्योहारों और मेलों में महिलाओं द्वारा समूह में गाए जाते हैं। इनमें खुशी, प्रेम और जीवन के उत्सवों का वर्णन होता है।
3. छपेली गीत
यह युवक-युवतियों द्वारा सामूहिक नृत्य करते हुए गाए जाते हैं। छपेली गीतों में हास्य, प्रेम और सामाजिक व्यवहार की झलक होती है। यह गीत आमतौर पर वसंत ऋतु में लोकप्रिय होते हैं।
4. न्यौली गीत
यह एक प्रकार का विरह गीत होता है जिसमें महिला अपने प्रवासी पति या प्रेमी के लिए पीड़ा व्यक्त करती है। उत्तराखंड की प्रवासी संस्कृति के कारण यह गीत बहुत संवेदनशील और लोकप्रिय हैं।
5. मांगल गीत
ये गीत शादी-विवाह और शुभ कार्यों में गाए जाते हैं। वर-वधू, परिवार और देवी-देवताओं की स्तुति की जाती है।
6. वीर रस के गीत
युद्ध, बलिदान और वीरता को दर्शाते हैं। स्थानीय नायकों और योद्धाओं जैसे गब्बर सिंह नेगी, तिलक राम के बलिदान की गाथाएँ इनमें शामिल हैं।
बिरहा गीत:
यह गीत खासतौर पर विरह या दूर देश में बसे प्रियजनों के लिए गाए जाते हैं। इन गीतों में उनकी याद, प्रेम और मिलने की चाहत व्यक्त की जाती है।
2.उत्तराखंड के लोकगीतों की ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि
उत्तराखंड का जीवन सदियों से कठिन पर्वतीय परिस्थितियों और सीमित संसाधनों में ढला हुआ रहा है। ऐसे में लोकगीत लोगों के भावनात्मक और मानसिक संबल का माध्यम बने। ये गीत न केवल मनोरंजन करते थे, बल्कि सामूहिक एकता, श्रम, प्रेम, आध्यात्म और जीवन संघर्ष की कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते थे।
कृषि और पर्व आधारित गीत:
फसल बोने, कटाई, बुआई, या पर्व जैसे हरेला, भिताुला, बिस्सू, घुघुतिया आदि के समय विशेष गीत गाए जाते हैं।
प्रवासन और विरह के गीत:
चूंकि उत्तराखंड में आजीविका की तलाश में पुरुष अक्सर बाहर चले जाते हैं, इसलिए महिलाओं द्वारा गाए गए विरह गीत जैसे न्योली या बिरहा गीत भावनात्मक रूप से अत्यंत मार्मिक होते हैं।
3. लोकगायकों की भूमिका
उत्तराखंड के कई प्रसिद्ध लोकगायक और गायिकाओं ने इन गीतों को मंच, रिकॉर्डिंग और डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से नई पहचान दी है:
गोपाल बाबू गोस्वामी: कुमाऊँ क्षेत्र के अमर लोकगायक जिनके गीत आज भी लोकप्रिय हैं।
प्रीतम भरतवाण: हुड़का वादन और जागर पर आधारित गीतों के लिए प्रसिद्ध।
नरेन्द्र सिंह नेगी: गढ़वाली लोकसंगीत के सर्वाधिक प्रभावशाली गायक और रचनाकार।
जगदीश चंद्र रतूड़ी: गढ़वाल के पारंपरिक गीतों को आधुनिक मंच पर लाने वाले प्रमुख कलाकार।
4. उत्तराखंड के लोकगीतों की विशेषताएँ
1. स्वर और लय की सादगी: भावों को सीधे छू लेने वाले सुर और लोक रागों पर आधारित गायन शैली।
2. प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन: गीतों में हिमालय, नदियाँ, फूलों की घाटियाँ और वनों का अत्यंत सुंदर चित्रण।
3. स्त्री केंद्रित दृष्टिकोण: स्त्रियों की भावनाओं, संघर्षों और जीवन को प्रमुखता से व्यक्त किया गया है।
4. सामूहिकता की भावना: इन गीतों में सामाजिक एकता, मेल-जोल और सहयोग की भावना झलकती है।
प्रकृति से जुड़ाव: उत्तराखंड के लोकगीतों में हिमालय, नदियाँ, फूल, जंगल और मौसम की प्रमुख भूमिका होती है।
संगीत वाद्य: हुड़का, ढोल, दमाऊ, रणसिंघा, बीन जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है।
5. समकालीन परिप्रेक्ष्य में लोकगीत
आज लोकगीत केवल गांवों तक सीमित नहीं रहे। सोशल मीडिया, यूट्यूब और अन्य डिजिटल माध्यमों ने इन्हें वैश्विक दर्शकों तक पहुंचा दिया है। अब इन्हें फ़्यूज़न संगीत, रॉक बैंड्स, और फिल्मों में भी शामिल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए: "बेडू पाको बारामासा" उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध गीत है जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया गया है।
आज के दौर में उत्तराखंड के लोकगीतों को नए संगीत संयोजन और मंचों के माध्यम से लोकप्रियता मिल रही है। लोकगायक जैसे मांगल सिंह, गोपाल बाबू गोस्वामी, प्रीतम भरतवाण और जगदीश चंद्र रतूड़ी ने लोकगीतों को नई पहचान दी है। यहाँ उत्तराखंड के लोकगीतों पर और विस्तार से जानकारी दी जा रही है, जिससे इनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता को गहराई से समझा जा सके:
6. संरक्षण की आवश्यकता
लोकगीत उत्तराखंड की धरोहर हैं लेकिन शहरीकरण, पॉप संस्कृति और भाषाई संकट के कारण इनका अस्तित्व खतरे में है। इसलिए:
लोकगायकों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। विद्यालयों और महाविद्यालयों में लोकसंगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए। सरकारी एवं निजी संस्थानों द्वारा संरक्षण योजनाएँ बननी चाहिए। यहाँ उत्तराखंड के लोकगीतों पर और भी विस्तार से जानकारी दी जा रही है, जिसमें उनके सामाजिक सरोकार, सांस्कृतिक महत्व, भाषाई विविधता और आधुनिक प्रयोग को समाहित किया गया है
7.भाषाई विविधता और लोकगीत
उत्तराखंड तीन प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित है - गढ़वाल, कुमाऊँ, और जौनसार-बावर। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट भाषा और बोली है, और लोकगीत इन्हीं भाषाई परंपराओं में रचे गए हैं:- गढ़वाली लोकगीत: सरल, भावनात्मक और गूढ़ प्रतीकों से भरपूर। कुमाऊँनी लोकगीत: सौम्यता और भक्ति रस में डूबे गीत। जौनसारी गीत: उत्सवधर्मी, मस्त शैली में गाए जाने वाले गीत।
उदाहरण:
गढ़वाली में: “नंदा तेरी जय हो” (नंदा देवी की आराधना)
कुमाऊँनी में: “घुघुति ना बासा…” (घुघुतिया पर्व पर)
जौनसारी में: “झुमेलु ओ म्यरु झुमेलु…” (लोकनृत्य गीत)
8. लोकगीतों में सामाजिक विषयों की अभिव्यक्ति
उत्तराखंड के लोकगीत केवल मनोरंजन या भक्ति तक सीमित नहीं हैं। ये समाज के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाते हैं:
1. प्रवासन (Migration):
गीतों में घर से दूर गए प्रियजनों की याद, अकेलापन और प्रतीक्षा की पीड़ा। उदाहरण: "ओ मेरो पिया घर कभ जालु?"
2. नारी चेतना:
स्त्री की पीड़ा, परित्याग, सास-बहू संबंध और मातृत्व के भाव। उदाहरण: "ब्याह की रात मेरी आँखों में आँसू थे…"
3. प्राकृतिक आपदाएँ और पीड़ा:
भूकंप, बादल फटने जैसी घटनाओं पर भी समय-समय पर गीत रचे गए हैं।
4. पर्यावरण जागरूकता:
हरेला जैसे पर्वों पर गाए जाने वाले गीत पर्यावरण के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं।
9.उत्तराखंड के कुछ अमर लोकगीत
1. बेडू पाको बारामासा
उत्तराखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत। "बेडू" (एक फल) और "पाको" (पकना) के माध्यम से प्रकृति और प्रेम का प्रतीकात्मक चित्रण।
2. ओ लालड़ी…
प्रियतम से बिछड़ने की वेदना। पहाड़ी युवतियों की भावना का प्रतीक।
3. घुघुति ना बासा…
बच्चों द्वारा गाया जाने वाला पारंपरिक गीत, जो उत्तराखंड की मातृसत्तात्मक भावनाओं को दर्शाता है।
10.आधुनिक प्रयोग और लोकगीतों का भविष्य
आज उत्तराखंड के लोकगीत कई माध्यमों से एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं:
लोक-रॉक और फ्यूज़न संगीत:
जैसे Masakali Band, Pandavaas, PAHADIA जैसे युवा बैंड लोकगीतों को नए अंदाज़ में प्रस्तुत कर रहे हैं।
फिल्म और डॉक्यूमेंट्री:
कई पहाड़ी फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज़ में पारंपरिक लोकगीतों का प्रयोग किया गया है।
यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म:
लोकगायक अब सीधे श्रोताओं से जुड़ पा रहे हैं। नए गायकों ने पारंपरिक गीतों को आधुनिक वाद्ययंत्रों और सिनेमाई अंदाज़ में पेश किया है।
11. लोकगीतों का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ
उत्तराखंड के लोकगीत न केवल मनोरंजन का माध्यम हैं, बल्कि वे सामाजिक संदेश, धार्मिक विश्वासों और संस्कृति की रीढ़ के रूप में भी कार्य करते हैं। ये गीत एक तरह से उस समाज की जीवनशैली, परंपराओं और समाजिक जटिलताओं का आईना होते हैं।
1. धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनाएँ
उत्तराखंड का अधिकांश क्षेत्र धार्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध है। यहां के लोकगीत अक्सर धार्मिक आदर्शों, मान्यताओं और त्योहारों से जुड़े होते हैं। नंदा देवी, कालिया देवी, गंगा, और कैलाश जैसे देवता इन गीतों के केंद्र में होते हैं।
जागर गीत:
उत्तराखंड में देवी-देवताओं को जागृत करने के लिए विशेष रूप से जागर गीत गाए जाते हैं। ये गीत एक प्रकार की प्रार्थना होती है, जिसमें देवता की महिमा का गान किया जाता है। इन्हें आमतौर पर पूजा-अर्चना के दौरान गाया जाता है।
सप्तशती गीत:
यह गीत खासतौर पर नवदुर्गा की पूजा के समय गाए जाते हैं। इन गीतों में देवी की शक्तियों और उनके आशीर्वाद की कामना की जाती है।
2. सामाजिक समरसता और लोकगीत
लोकगीतों में सामूहिकता और समाज में एकता का संदेश भी छिपा होता है। जब कोई बड़ा सामूहिक कार्य जैसे कृषि, निर्माण या मेलों के आयोजन होते हैं, तो लोग एक साथ मिलकर गीत गाते हैं। यह न केवल मेहनत को सरल बनाता है, बल्कि सामाजिक एकता को भी सुदृढ़ करता है।
श्रम गीत:
खेती के समय, लकड़ी काटते समय, या अन्य शारीरिक श्रम के दौरान गाए गए गीत काम को हल्का और आसान बना देते थे। इस प्रकार के गीतों में काम की गति, मेहनत और मेहनत से जुड़े अनुभवों को साझा किया जाता था।
समाज सुधार के गीत:
कुछ लोकगीत समाज में समानता, सामाजिक न्याय, और नारी के अधिकार जैसे मुद्दों को उठाते हैं। विशेषकर, महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता पर आधारित गीत समाज के पुरुष प्रधान दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं।
12. लोकगीतों में इतिहास और वीरता का महत्व
उत्तराखंड का इतिहास वीरों, संघर्षों और लड़ाइयों से भरा हुआ है। लोकगीतों में वीरता और बलिदान की कहानियाँ शामिल होती हैं। कई लोकगीत उत्तराखंड के स्थानीय नायकों और संघर्षों की याद दिलाते हैं।
वीरगाथाएँ:
गब्बर सिंह नेगी, भीम सिंह रावत जैसे लोक नायक और उनके युद्धों की गाथाएँ लोकगीतों में गाई जाती हैं। इन गीतों में युद्ध, संघर्ष, बलिदान और साहस के तत्व होते हैं। उदाहरण के लिए, गब्बर सिंह नेगी की वीरता को दर्शाने वाला गीत बहुत प्रसिद्ध है।
लोक युद्ध गीत:
यह गीत किसी विशेष युद्ध, संघर्ष या सामाजिक क्रांति के बारे में होते हैं। इन गीतों में नायक के संघर्ष, उसके परिवार के दर्द और युद्ध के परिणामों का चित्रण होता है।
13. उत्तराखंड के लोकगीत और नृत्य
उत्तराखंड के लोकगीतों का गहन संबंध नृत्य से भी है। अधिकांश लोकगीतों में एक विशेष नृत्य शैली जुड़ी होती है, जो गीत के भावनात्मक प्रभाव को और बढ़ा देती है। विभिन्न लोक नृत्य जैसे छपेली, कुमाऊंनी रास, ठाडी, घुडिया, झुमेलू इन गीतों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं।
1. झुमेलू और छपेली नृत्य
झुमेलू:
यह एक प्रकार का समूह नृत्य है जो विशेष रूप से वसंत और फसल कटाई के समय गाया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएँ एक साथ मिलकर नृत्य करते हैं और लोकगीतों के साथ सामूहिक आनंद का अनुभव करते हैं। झुमेलू नृत्य आमतौर पर प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य और फसल के अच्छे होने की कामना से जुड़ा होता है।
छपेली नृत्य:
यह नृत्य विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय है। इसमें महिलाएँ एक साथ मिलकर नृत्य करती हैं, और गीतों के साथ उसकी ताल और लय में नृत्य की विशेषताएँ शामिल होती हैं। यह नृत्य समृद्धि, प्यार और समर्पण का प्रतीक होता है।
14.लोकगीत और लोककला का भविष्य
आजकल, आधुनिक मीडिया और तकनीकी प्लेटफॉर्म्स पर उत्तराखंड के लोकगीतों की पुनः जागृति हो रही है। युवा पीढ़ी अब इन लोकगीतों को न केवल सुन रही है, बल्कि उसे अपनी आवाज और संगीत में भी पेश कर रही है।
डिजिटल युग में लोकगीत:
यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर उत्तराखंड के लोकगीत अब नए रंग रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। लोकगायक अब अपने गीतों को फ़्यूज़न संगीत और नए वाद्ययंत्रों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे लोकगीतों की लोकप्रियता को एक नया मोड़ मिला है।
झुमेलू:
कुछ हिंदी फिल्मों और वेब-सीरीज़ में उत्तराखंड के लोकगीतों का प्रयोग किया गया है, जिससे उनकी पहुंच और लोकप्रियता बढ़ी है।
Conclusion
उत्तराखंड के लोकगीतों में वह सब कुछ है जो किसी समाज की संस्कृति, इतिहास, और आध्यात्मिकता को समझने के लिए जरूरी होता है। इन गीतों की भावनात्मक गहराई, सामाजिक संदेश, और सांस्कृतिक प्रतीक भारतीय लोककला की धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। उनका संरक्षण, प्रसार और समकालीन संदर्भ में पुनः प्रयोग करना जरूरी है ताकि भविष्य की पीढ़ियाँ इस धरोहर से जुड़ी रहें।
Thanks For Read
jp Singh
searchkre.com@gmail.com
8392828781
 Gst Registration
Gst Registration
 DSC Registration
DSC Registration
 Pancard Registration
Pancard Registration
 Company Registration
Company Registration
 Fssai Registration
Fssai Registration
 TradeMark Registration
TradeMark Registration
 MSME Registration
MSME Registration
 Passport Registration
Passport Registration
 Income Tax Return
Income Tax Return
 LLP Company Registration
LLP Company Registration
 Marriage And Court Marriage Registration
Marriage And Court Marriage Registration
 PVT LTD Company Registration
PVT LTD Company Registration
 GST Filing Services
GST Filing Services
 Coaching Insititute Registration
Coaching Insititute Registration
 GYM Registration
GYM Registration
 NGO Registration
NGO Registration
 Political Party Registration
Political Party Registration
 Society Registration
Society Registration
 Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
 Make Website on EMI
Make Website on EMI


























































































 9th Class Scholarship Competition Test
9th Class Scholarship Competition Test
 10th Class Scholarship Competition Test
10th Class Scholarship Competition Test
 11th Class Scholarship Competition Test
11th Class Scholarship Competition Test
 12th Class Scholarship Competition Test
12th Class Scholarship Competition Test
 Graduation Scholarship Competition Test
Graduation Scholarship Competition Test
 Post Graduation Scholarship Competition Test
Post Graduation Scholarship Competition Test
 Diploma Scholarship Competition Test
Diploma Scholarship Competition Test
 Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 JEE Coaching Scholarship Competition Test
JEE Coaching Scholarship Competition Test
 NEET Coaching Scholarship Competition Test
NEET Coaching Scholarship Competition Test
 Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test