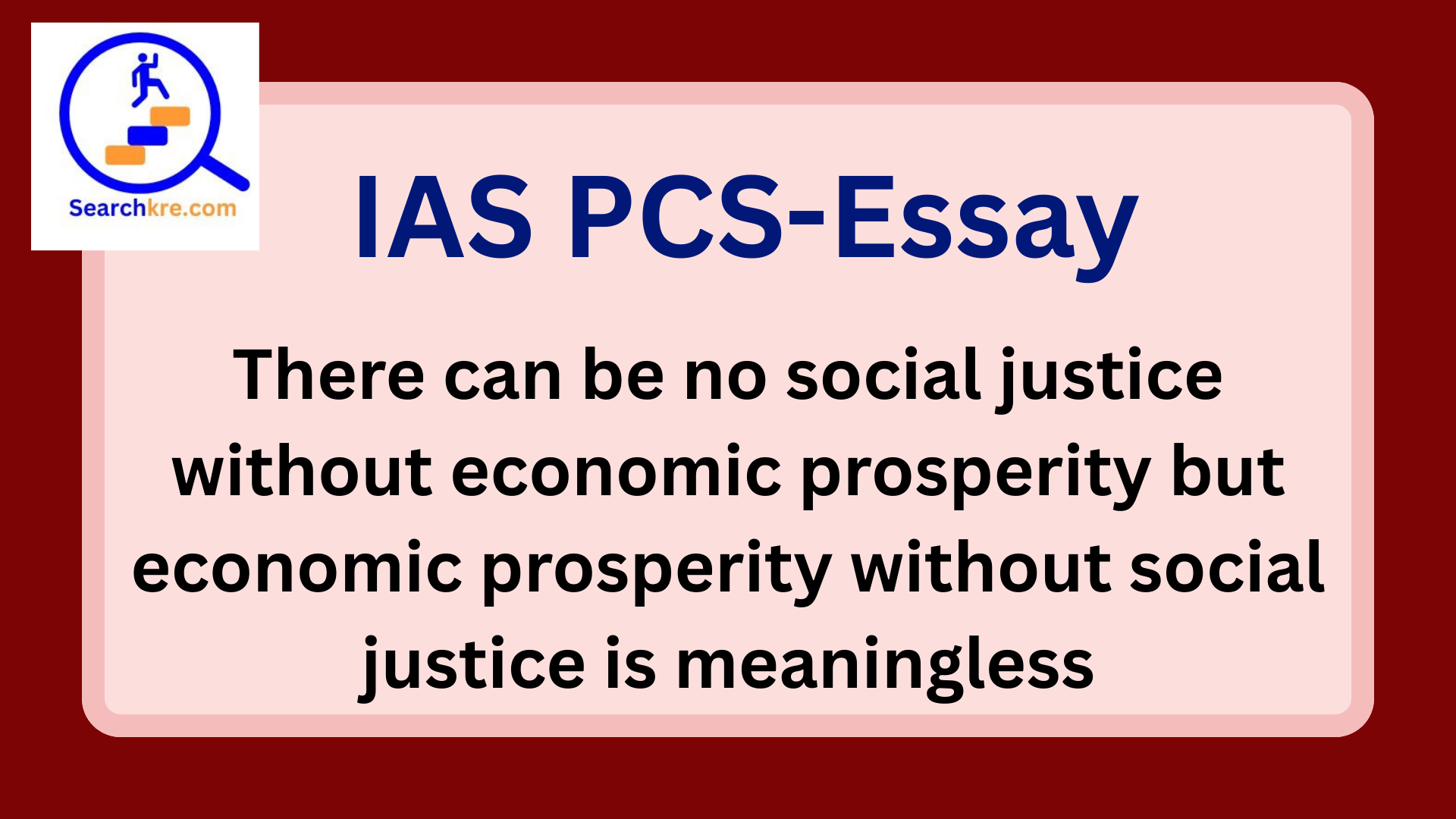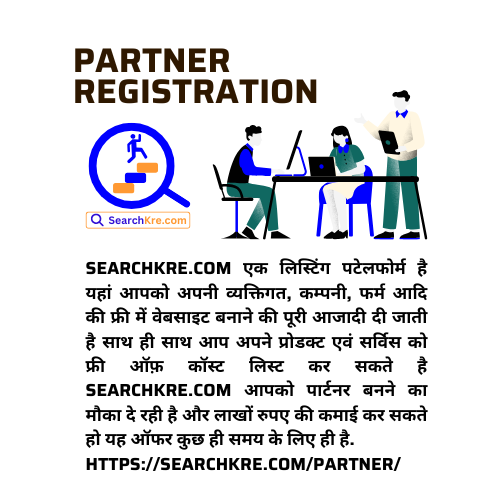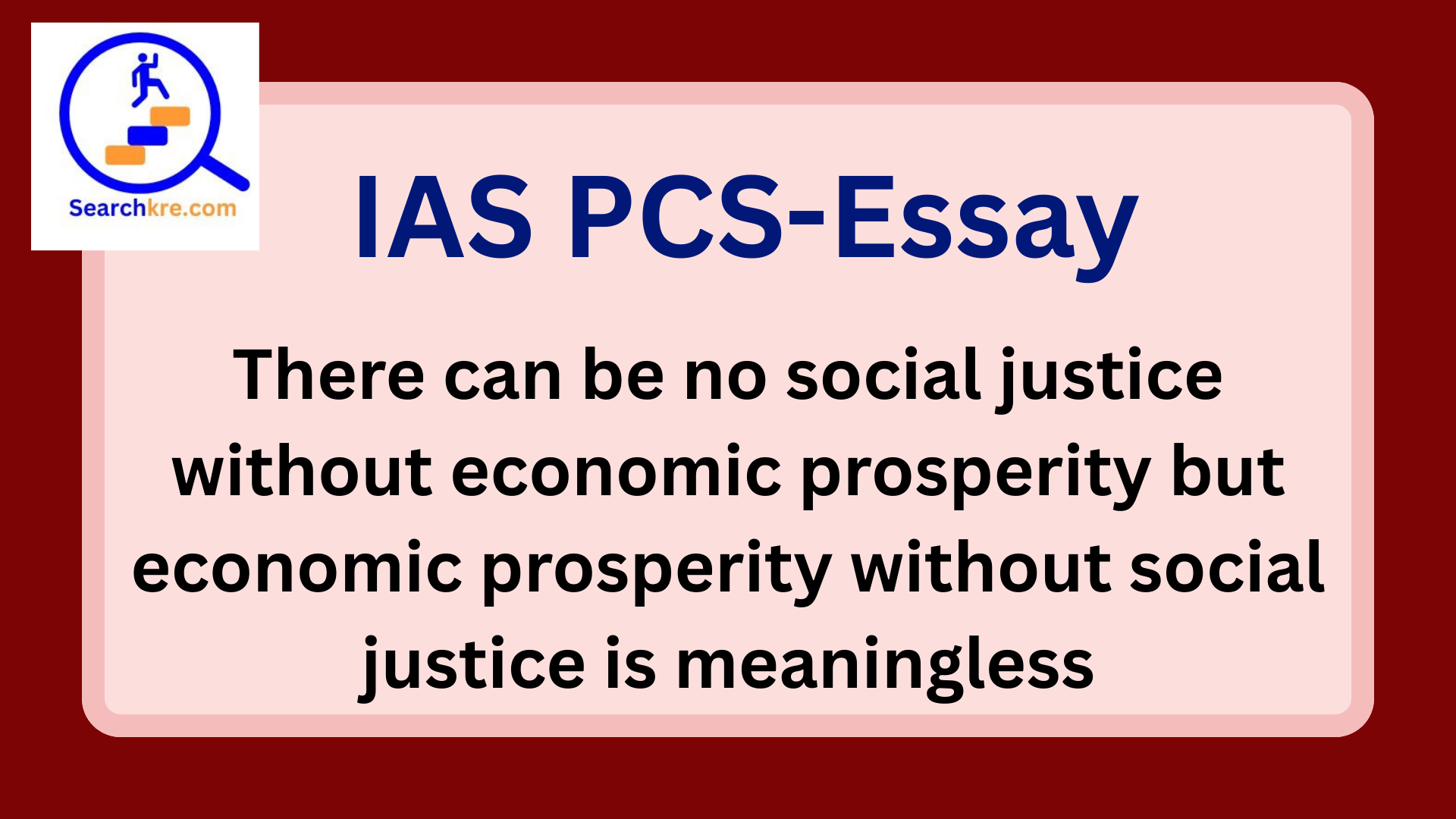
jp Singh
2025-05-02 00:00:00
searchkre.com@gmail.com /
8392828781
आर्थिक समृद्धि के बिना कोई सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है लेकिन सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि निरर्थक है
आर्थिक समृद्धि के बिना कोई सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है लेकिन सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि निरर्थक है
भूमिका
"आर्थिक समृद्धि के बिना कोई सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है लेकिन सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि निरर्थक है" — यह वक्तव्य आधुनिक सामाजिक-आर्थिक विमर्श के दो प्रमुख स्तंभों के परस्पर संबंध को उजागर करता है। यह कथन हमें उस द्वंद्व की ओर ले जाता है जहाँ एक ओर आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाती है, तो दूसरी ओर सामाजिक न्याय को एक नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी माना जाता है। यह द्वंद्व केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि व्यावहारिक नीतियों, योजनाओं और संसाधन आवंटन में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।
भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ जाति, लिंग, वर्ग, धर्म और क्षेत्रीय असमानताएँ गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, वहाँ यह बहस और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक समाजवादी मॉडल अपनाया, जिसमें आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय को भी उतना ही महत्व दिया गया। संविधान के नीति निदेशक तत्वों में सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। लेकिन समय के साथ, वैश्वीकरण और बाजारीकरण की लहर में सामाजिक न्याय के कई मुद्दे पीछे छूटते गए।
आज भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है—ऊँची इमारतें, बढ़ती GDP, विदेशी निवेश, तकनीकी नवाचार; लेकिन दूसरी ओर झुग्गियों में रहने वाले करोड़ों लोग, कुपोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा और जातिगत भेदभाव से ग्रस्त समाज भी इसका ही हिस्सा हैं। सवाल यह है कि क्या यह विकास सभी के लिए समान अवसर पैदा कर रहा है? क्या यह समृद्धि वंचित वर्गों तक पहुँच पा रही है?
इसी संदर्भ में यह कथन हमें सोचने पर विवश करता है कि यदि केवल आर्थिक समृद्धि को लक्ष्य बनाया जाए और सामाजिक न्याय की उपेक्षा की जाए, तो वह समृद्धि केवल कुछ वर्गों तक सीमित रह जाती है। दूसरी ओर, यदि हम केवल सामाजिक न्याय की बात करें लेकिन आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता न हो, तो न्याय सिर्फ एक आदर्श बनकर रह जाएगा, वास्तविकता में नहीं उतर पाएगा।
वर्तमान में चल रहे कई सामाजिक आंदोलन, जैसे जाति आधारित जनगणना की माँग, महिला आरक्षण का संघर्ष, किसानों की आय सुरक्षा, और शिक्षा में समावेशन जैसे मुद्दे इस बात को रेखांकित करते हैं कि सामाजिक न्याय की माँगें केवल नैतिकता नहीं, बल्कि व्यावहारिक आवश्यकता भी बन चुकी हैं। दूसरी ओर, सरकारें आर्थिक समृद्धि के लिए बड़े निवेश, आधारभूत संरचना विकास, स्टार्टअप्स और विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार को प्राथमिकता दे रही हैं, जो अपने आप में आवश्यक है, लेकिन यदि यह समावेशी नहीं है,
2. आर्थिक समृद्धि का स्वरूप और अर्थ
आर्थिक समृद्धि किसी भी राष्ट्र के विकास का मूल आधार मानी जाती है। यह वह स्थिति है जब कोई देश न केवल अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहा हो, बल्कि उन्हें बेहतर जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उपभोग के अवसर भी प्रदान कर रहा हो। परंतु आर्थिक समृद्धि केवल बढ़ती हुई GDP या निवेश तक सीमित नहीं है; इसका प्रभाव व्यापक सामाजिक ढांचे पर पड़ता है और यह सामाजिक न्याय की दिशा में भी निर्णायक भूमिका निभाता है।
आर्थिक समृद्धि की परिभाषा और मापदंड
आर्थिक समृद्धि को आमतौर पर राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, GDP वृद्धि दर, औद्योगिक उत्पादन, सेवा क्षेत्र का विस्तार, निर्यात में वृद्धि, और निवेश में इजाफा जैसे आर्थिक संकेतकों के आधार पर मापा जाता है। परंतु ये मात्र आंकड़े नहीं होते; ये इस बात का संकेत देते हैं कि कोई देश कितनी क्षमता रखता है अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन देने की।
उदाहरण: भारत की GDP 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद तीव्र गति से बढ़ी। सेवा क्षेत्र, IT, और वित्तीय बाजारों ने अर्थव्यवस्था को वैश्विक मानचित्र पर प्रतिस्पर्धी बनाया। भारत आज विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या यह आर्थिक समृद्धि सभी तबकों तक पहुँची है? यह एक विचारणीय प्रश्न है।
आर्थिक समृद्धि के स्रोत
उद्योग और विनिर्माण:
रोजगार सृजन और निर्यात में वृद्धि के लिए उद्योग एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे—मेक इन इंडिया, PLI स्कीम। - सेवा क्षेत्र: IT, बैंकिंग, पर्यटन और टेलीकॉम जैसे क्षेत्र आर्थिक समृद्धि के मजबूत स्तंभ बन चुके हैं।
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था:
हालाँकि कृषि की हिस्सेदारी GDP में घटी है, परंतु यह आज भी 50% से अधिक आबादी को रोजगार देती है। कृषि क्षेत्र की समृद्धि, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए, सामाजिक न्याय की आधारशिला है।
विदेशी निवेश:
FDI और FII के माध्यम से आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ती है जिससे आधारभूत संरचना और स्टार्टअप्स को बल मिलता है।
उद्यमिता और स्टार्टअप:
युवा भारत की ऊर्जा को स्वरोजगार और नवाचार में लगाना देश की समृद्धि के नए रास्ते खोल रहा है।
आर्थिक समृद्धि के लाभ
रोजगार के अवसरों में वृद्धि:
जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियाँ पैदा होती हैं। सरकारी राजस्व में वृद्धि: जिससे कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक खर्च किया जा सकता है।
उपभोक्ता सुविधाओं में सुधार:
स्वास्थ्य सेवाएँ, परिवहन, शिक्षा, डिजिटल तकनीक में नवाचार।
वैश्विक प्रभाव:
आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र की विदेश नीति, रणनीतिक स्थिति और वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।
भारत में आर्थिक समृद्धि की दशा
1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत ने निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। इससे देश में निवेश आया, उद्यमिता बढ़ी, और नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। 2000 के बाद IT और सेवा क्षेत्र ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई।
आर्थिक समृद्धि की सीमाएँ
आर्थिक समृद्धि अपने आप में संपूर्ण नहीं है, विशेषतः जब उसका वितरण असमान हो:
केवल GDP बढ़ना पर्याप्त नहीं जब तक उसकी लाभांश सभी को समान रूप से न मिले।, अक्सर समृद्धि का केंद्रीकरण शहरी क्षेत्रों, कॉर्पोरेट समूहों या उच्च वर्गों तक सीमित रहता है।, ग्रामीण भारत, आदिवासी समुदाय, दलित, महिलाएँ, और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अक्सर इस समृद्धि से वंचित रह जाते हैं।
वर्तमान उदाहरण:
भारत में सबसे धनी 1% लोगों के पास देश की 40% से अधिक संपत्ति है, जबकि निचले 50% के पास मात्र 13%। यह आर्थिक असमानता सामाजिक न्याय के लिए चुनौती बनती है।
3. सामाजिक न्याय की अवधारणा
सामाजिक न्याय वह मूल्य है जो एक समाज को समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की ओर अग्रसर करता है। यह केवल एक नैतिक आदर्श नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक सिद्धांत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर, अधिकार और संसाधनों तक पहुँच प्राप्त हो। भारत जैसे सामाजिक रूप से विभाजित देश में सामाजिक न्याय न केवल आवश्यक है, बल्कि यह संवैधानिक रूप से भी अनिवार्य बना दिया गया है।
सामाजिक न्याय की परिभाषा और मूल भावना
सामाजिक न्याय का सीधा संबंध इस बात से है कि क्या समाज में सभी वर्गों को-चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या क्षेत्र से हों—एक समान अवसर मिल रहा है या नहीं। सामाजिक न्याय यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जन्म-आधारित स्थिति के कारण अवसरों से वंचित न रह जाए। यह एक ऐसा समाज बनाने की प्रक्रिया है जहाँ कोई भी व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भेदभाव या वंचना का शिकार न हो डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था इस पर आधारित भारत का भविष्य देखा
भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय
भारतीय संविधान ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को अपने मूलभूत ढाँचे का हिस्सा बनाया है:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और कानून के संरक्षण का अधिकार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16: रोजगार के मामलों में समान अवसर
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39: नीति निदेशक तत्व – समान वेतन, बच्चों और महिलाओं का संरक्षण, जीवनयापन के लिए पर्याप्त साधन
इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था, विशेष योजनाएँ और कानूनी संरक्षण सामाजिक न्याय की दिशा में उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदम हैं।
सामाजिक न्याय के प्रमुख आयाम
जातीय न्याय:
भारत में जाति व्यवस्था एक ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय रही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को बराबरी के अवसर प्रदान करना सामाजिक न्याय का मूल लक्ष्य है।
लैंगिक न्याय:
महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान भागीदारी देना सामाजिक न्याय की अनिवार्यता है।
आर्थिक न्याय:
आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और न्यूनतम आय सुनिश्चित करना।
शैक्षणिक न्याय:
सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच देना, ताकि अवसरों की समानता संभव हो सके।
सांस्कृतिक न्याय:
विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और धार्मिक समूहों को सम्मान और संरक्षण देना।
सामाजिक न्याय का वर्तमान परिप्रेक्ष्य
आज भी सामाजिक न्याय की आवश्यकता बनी हुई है क्योंकि असमानता के विभिन्न रूप समाज में अब भी विद्यमान हैं:
जातिगत भेदभाव:
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अस्पृश्यता के नए रूप दिखाई देते हैं।
लैंगिक असमानता:
रूप दिखाई देते हैं। - लैंगिक असमानता: महिलाओं को वेतन, पदोन्नति, और सुरक्षा में बराबरी नहीं मिलती। - आर्थिक विषमता: गरीब और अमीर के बीच खाई लगातार बढ़ रही है।
शैक्षणिक असमानता:
निजी और सरकारी स्कूलों के बीच की गुणवत्ता में बड़ा अंतर है। - डिजिटल डिवाइड: तकनीक आधारित विकास से वंचित समुदाय पीछे छूटते जा रहे हैं।
सामाजिक न्याय की चुनौतियाँ
संसाधनों की सीमितता:
गरीबों के लिए योजनाएँ बनाने के बावजूद उनका क्रियान्वयन सीमित रहता है।
राजनीतिक लाभ के लिए न्याय का उपयोग:
कभी-कभी आरक्षण जैसी नीतियाँ वोट बैंक के लिए उपयोग की जाती हैं।
समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ:
मानसिकता में बदलाव न आने के कारण कानूनों का प्रभाव सीमित हो जाता है।
न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता:
वंचित वर्गों को न्यायिक प्रणाली तक पहुँचने में कठिनाई होती है।
सामाजिक न्याय के लिए चल रही पहलकदमी
न्यायिक सक्रियता:
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर सामाजिक न्याय को संरक्षित किया है (उदाहरण: मंडल आयोग केस, सबरीमाला, ट्रिपल तलाक निर्णय)।
नीतिगत प्रयास:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, POSH कानून (महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न रोकथाम), अत्याचार निवारण अधिनियम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत—ये योजनाएँ आर्थिक और सामाजिक समावेशन की दिशा में हैं।
4. आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय क्यों असंभव है
सामाजिक न्याय की अवधारणा तब तक केवल एक आदर्श बनी रहती है जब तक उसके पीछे आर्थिक संसाधनों का मजबूत आधार न हो। यदि सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है, तो वह न तो समान अवसरों की व्यवस्था कर सकती है, न ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, और रोजगार की गारंटी दे सकती है। अतः सामाजिक न्याय की वास्तविक स्थापना आर्थिक समृद्धि के बिना संभव नहीं है।
1. सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक संसाधन आवश्यक क्यों हैं?
सामाजिक न्याय केवल संविधान में दर्ज अधिकारों और न्यायिक निर्णयों से साकार नहीं होता। इसे जमीन पर उतारने के लिए सार्वजनिक खर्च, कल्याणकारी योजनाएँ, बुनियादी ढाँचे का विकास, और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है। ये सभी तभी संभव हैं जब सरकार और समाज के पास आवश्यक संसाधन हों।
उदाहरण के लिए:-
अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए छात्रवृत्तियाँ, विशेष विद्यालय और कोचिंग सेंटर चलाने के लिए आर्थिक व्यय की आवश्यकता होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के लिए साइकिल वितरण, छात्रावास और मिड-डे मील जैसी योजनाएँ तभी सफल होती हैं जब सरकार के पास बजट हो।
2. आर्थिक समृद्धि और कल्याणकारी योजनाओं का संबंध
(क) शिक्षा का अधिकार – RTE (Right to Education) अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को स्कूल, शिक्षक, भवन, भोजन, पुस्तकों, और ड्रेस की व्यवस्था करनी होती है। ये सब व्यय-भार आर्थिक संसाधनों पर निर्भर है।
(ख) स्वास्थ्य सेवाएँ – आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाएँ सामाजिक न्याय की ओर बड़े कदम हैं, परंतु इनका संचालन और विस्तार आर्थिक समृद्धि पर आधारित है।
(ग) रोजगार गारंटी – मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए सालाना हजारों करोड़ का बजट चाहिए होता है। आर्थिक विकास के बिना यह दीर्घकालिक नहीं रह सकता।
3. सामाजिक असमानता दूर करने के लिए निवेश आवश्यक है
यदि हम जातिगत, लैंगिक या क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करना चाहते हैं, तो हमें वंचित समूहों को उन्नति के लिए विशेष सहायता देनी होगी। यह सहायता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा के रूप में दी जाती है, जिसके लिए लगातार निवेश की आवश्यकता होती है।
उदाहरण:
एक दलित छात्र को IIT में पढ़ाई के लिए शिक्षा लोन, छात्रवृत्ति, और हॉस्टल की जरूरत होती है। यह सब आर्थिक सहायता के बिना संभव नहीं।, किसी आदिवासी महिला को मातृत्व स्वास्थ्य सेवा, पोषण, और उद्यमिता के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
4. ऐतिहासिक उदाहरण – समृद्धि से सामाजिक सुधार
(क) केरल मॉडल – केरल ने उच्च साक्षरता, महिला स्वास्थ्य, और सामाजिक समावेशन में बड़ी सफलता इसलिए पाई क्योंकि उसने आर्थिक विकास को शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ जोड़ा।
(ख) नॉर्डिक देश (स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क) – इन देशों में उच्च कर संग्रहण और आर्थिक समृद्धि के कारण सार्वभौमिक स्वास्थ्य, मुफ्त शिक्षा, और सामाजिक सुरक्षा जैसे सामाजिक न्याय के मजबूत तंत्र बनाए गए
(ग) भारत में हरियाणा और पंजाब – जहाँ हरित क्रांति से आर्थिक समृद्धि आई, वहाँ शिक्षा, खेल और बुनियादी ढाँचे में निवेश हुआ, जिससे सामाजिक विकास को बल मिला।
5. जब आर्थिक संसाधनों की कमी हो तो क्या होता है?
कमजोर कल्याणकारी योजनाएँ – योजनाएँ केवल कागजों पर रह जाती हैं।
अधूरी न्याय प्रक्रिया – गरीब लोग न्याय पाने में वर्षों खर्च कर देते हैं।
असमान अवसर – वंचित समुदाय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं।
नक्सलवाद और असंतोष – जब न्याय नहीं मिलता, तो कुछ समूह हिंसक प्रतिरोध की ओर बढ़ते हैं
उदाहरण:
झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन ने नक्सलवाद को जन्म दिया। यदि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जनघनत्व वाले राज्यों में शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश नहीं बढ़ेगा, तो वहाँ सामाजिक न्याय की कल्पना केवल भाषणों तक सीमित रह जाएगी।
आज के युग में डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट सुविधा, ऑनलाइन शिक्षा और ई-गवर्नेंस भी सामाजिक समावेशन के लिए आवश्यक हैं। इन सभी क्षेत्रों में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। उदाहरण:- डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का कार्य, आर्थिक समृद्धि के अभाव में अधूरा रह जाता। ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन प्रणाली, महिला हेल्पलाइन, या कोविड वैक्सीनेशन जैसे कार्यक्रम तभी सफल हो सकते हैं जब डिजिटल ढाँचा मजबूत हो।
5. सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि क्यों निरर्थक है
यदि एक राष्ट्र आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाए, परंतु उसकी समृद्धि कुछ वर्गों, समुदायों या क्षेत्रों तक सीमित रह जाए, तो वह समृद्धि न तो स्थायी होती है, न ही नैतिक। एक ऐसे समाज में जहाँ सामाजिक न्याय की अनुपस्थिति हो, वहाँ आर्थिक विकास केवल असमानता, असंतोष और संघर्ष को जन्म देता है। अतः यह कहना अत्यंत सार्थक है कि "सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि निरर्थक है"।
असमान समृद्धि की वास्तविकता
भारत सहित विश्व के कई देशों में देखा गया है कि आर्थिक विकास के आँकड़े तो ऊँचे होते हैं, परंतु गरीब, वंचित, महिलाएँ, दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग उससे लाभान्वित नहीं होते। यह "Growth without equity" की स्थिति होती है। उदाहरण:- भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी है, परंतु ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 100 से नीचे है। देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, परंतु मजदूर वर्ग न्यूनतम वेतन के लिए संघर्ष कर रहा है। मेट्रो शहरों में चमक-दमक के बावजूद स्लम क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएँ
सामाजिक न्याय के बिना समृद्धि का परिणाम – सामाजिक विघटन
जब आर्थिक विकास समाज के सभी वर्गों तक न पहुँचे, तो वह विभाजन को जन्म देता है:
न्याय की कमी → आक्रोश और विद्रोह
अवसरों की असमानता → प्रतिभा का दमन
मानव संसाधन का दुरुपयोग → उत्पादकता में कमी
नतीजा – समाज में वैमनस्य, शोषण, और अस्थिरता बढ़ती है, जो आर्थिक समृद्धि को खोखला बना देती है।
कॉरपोरेट विकास बनाम आमजन की स्थिति
जब सरकार केवल कॉरपोरेट क्षेत्र को बढ़ावा देती है और आम जनता की अनदेखी करती है, तो आर्थिक असमानता बढ़ती है। विकास का लाभ तब चंद बड़े उद्योगपतियों तक सीमित रह जाता है। उदाहरण:- सरकार द्वारा बड़े कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की जाती है, लेकिन श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा में कटौती हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए आदिवासी भूमि का अधिग्रहण होता है, पर पुनर्वास और मुआवज़ा नहीं दिया जाता। यह विकास न केवल असंतुलित है, बल्कि सामाजिक असंतोष को जन्म देता है।
सामाजिक न्याय – समावेशी विकास की नींव
यदि सामाजिक न्याय न हो, तो समृद्धि का कोई अर्थ नहीं क्योंकि- शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों में असमानता बनी रहती है। समाज का एक बड़ा वर्ग गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर नहीं निकल पाता। लोकतंत्र खोखला हो जाता है क्योंकि वंचित वर्गों की भागीदारी सीमित हो जाती है। Inclusive Growth का अर्थ ही यह है कि सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों को अपनाते हुए आर्थिक समृद्धि को सबके लिए सुलभ बनाया जाए।
ऐतिहासिक और वैश्विक दृष्टिकोण
(क) दक्षिण अफ्रीका – अपार्थेड युग में वहाँ पर आर्थिक समृद्धि तो थी, पर वह केवल गोरों तक सीमित थी। नस्लभेद के कारण सामाजिक अन्याय था, जिससे अंततः पूरे देश को राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन के दौर से गुजरना पड़ा।
(ख) ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति – प्रारंभ में आर्थिक विकास हुआ, पर मजदूरों का शोषण, बाल श्रम, और अमानवीय परिस्थितियाँ सामाजिक न्याय के अभाव को दर्शाती हैं। बाद में ट्रेड यूनियनों और सामाजिक सुधारों ने ही विकास को स्थिर और न्यायसंगत बनाया।
(ग) भारत में आर्थिक उदारीकरण (1991 के बाद) – देश में समृद्धि तो आई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े राज्यों और वंचित समुदायों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला, जिससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी।
सामाजिक न्याय से ही टिकाऊ समृद्धि संभव
मानव पूँजी का विकास – जब सभी वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण मिलेगा, तभी वे अर्थव्यवस्था में सक्रिय और उत्पादक भूमिका निभा सकेंगे।
सामाजिक स्थिरता – जब हर व्यक्ति को लगे कि उसके साथ न्याय हो रहा है, तो समाज में शांति और सहयोग का वातावरण बनता है।
लोकतांत्रिक भागीदारी – वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होती है, जिससे नीतियाँ अधिक समावेशी बनती हैं।
सामाजिक न्याय के बिना समृद्धि के खतरे
नक्सलवाद और अलगाववाद – छत्तीसगढ़, झारखंड, कश्मीर जैसे क्षेत्रों में विकास के बावजूद न्याय की अनुपस्थिति ने विद्रोह को जन्म दिया। शहरी अशांति – स्लम क्षेत्रों में युवा बेरोजगारी और असमानता के कारण अपराध और असंतोष में लिप्त होते हैं। राजनीतिक अस्थिरता – जब बड़े वर्ग उपेक्षित महसूस करते हैं, तो जनांदोलन और अविश्वास फैलता है।
महापुरुषों के विचार
डॉ. अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा, “राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित न किया जाए।”
जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित आर्थिक नियोजन की बात करते हुए कहा था कि विकास तभी सार्थक है जब वह आमजन के जीवन को बेहतर बनाए।
महात्मा गांधी ने कहा था, “असली भारत गाँवों में बसता है। जब तक अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक विकास अधूरा है।
भारत के संदर्भ में समावेशी विकास के प्रयास और चुनौतियाँ
भारत एक विविधतापूर्ण, बहु-जातीय, बहु-धार्मिक और बहुभाषी राष्ट्र है। यहाँ समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि का सपना अधूरा ही रहेगा। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अनेक प्रयास किए हैं जिससे कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। फिर भी कई चुनौतियाँ आज भी मौजूद हैं, जो इस समावेशन की राह में बाधा बनती हैं।
समावेशी विकास के लिए भारत द्वारा किए गए प्रमुख प्रयास (क) पंचवर्षीय योजनाएँ और समाजवाद आधारित नीति: स्वतंत्रता के बाद भारत ने नियोजित विकास मॉडल अपनाया जिसमें सामाजिक न्याय प्राथमिक उद्देश्य था। भूमि सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, रोजगार सृजन, गरीबों के लिए अनाज वितरण – ये सब योजनाएँ आर्थिक समृद्धि को न्यायसंगत बनाने की दिशा में थे। (ख) आरक्षण नीति:अनुसूचित जातियों, जनजातियों, और पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण दिया गया।
(ग) गरीबी उन्मूलन योजनाएँ:- इंदिरा आवास योजना, मनरेगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन – इन सभी योजनाओं का उद्देश्य वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ना रहा। (घ) समावेशी वित्तीय प्रणाली:- जन-धन योजना, आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और UPI जैसे उपायों से वित्तीय सेवाओं की पहुँच गरीब और ग्रामीण जनता तक पहुँची। (ङ) शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पहल: - सरव शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ
Conclusion
“आर्थिक समृद्धि के बिना कोई सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है लेकिन सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि निरर्थक है” — यह कथन भारत जैसे देश में एक गहन और प्रासंगिक सत्य को उजागर करता है। सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि, दोनों न तो एक-दूसरे के विकल्प हैं और न ही अलग-अलग रास्ते हैं, बल्कि ये एक ही समग्र विकास यात्रा के दो पहिये हैं। यदि एक भी पहिया बाधित होता है, तो राष्ट्र की विकास गाड़ी रुक जाती है या असंतुलित हो जाती है।
Thanks For Read
jp Singh
searchkre.com@gmail.com
8392828781
 Gst Registration
Gst Registration
 DSC Registration
DSC Registration
 Pancard Registration
Pancard Registration
 Company Registration
Company Registration
 Fssai Registration
Fssai Registration
 TradeMark Registration
TradeMark Registration
 MSME Registration
MSME Registration
 Passport Registration
Passport Registration
 Income Tax Return
Income Tax Return
 LLP Company Registration
LLP Company Registration
 Marriage And Court Marriage Registration
Marriage And Court Marriage Registration
 PVT LTD Company Registration
PVT LTD Company Registration
 GST Filing Services
GST Filing Services
 Coaching Insititute Registration
Coaching Insititute Registration
 GYM Registration
GYM Registration
 NGO Registration
NGO Registration
 Political Party Registration
Political Party Registration
 Society Registration
Society Registration
 Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
 Make Website on EMI
Make Website on EMI


























































































 9th Class Scholarship Competition Test
9th Class Scholarship Competition Test
 10th Class Scholarship Competition Test
10th Class Scholarship Competition Test
 11th Class Scholarship Competition Test
11th Class Scholarship Competition Test
 12th Class Scholarship Competition Test
12th Class Scholarship Competition Test
 Graduation Scholarship Competition Test
Graduation Scholarship Competition Test
 Post Graduation Scholarship Competition Test
Post Graduation Scholarship Competition Test
 Diploma Scholarship Competition Test
Diploma Scholarship Competition Test
 Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 JEE Coaching Scholarship Competition Test
JEE Coaching Scholarship Competition Test
 NEET Coaching Scholarship Competition Test
NEET Coaching Scholarship Competition Test
 Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test