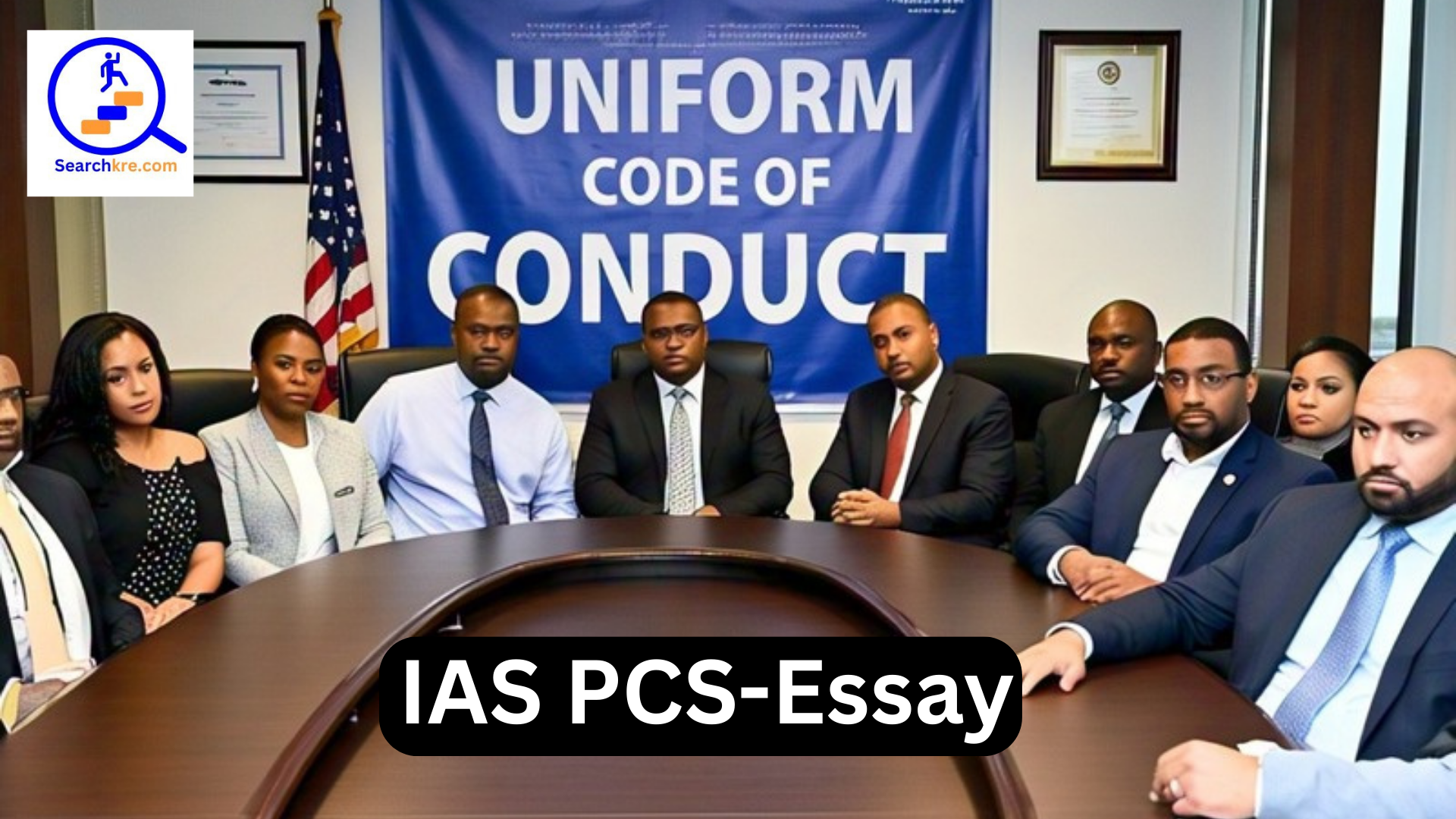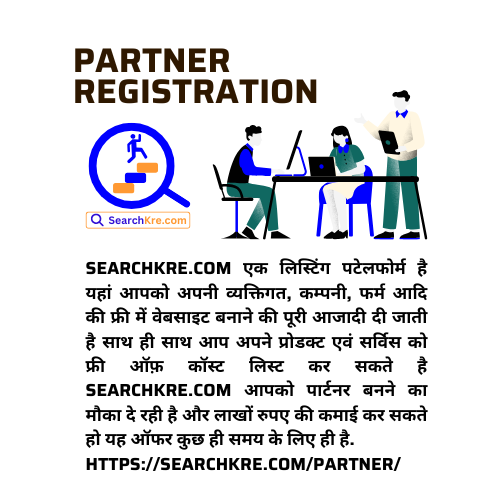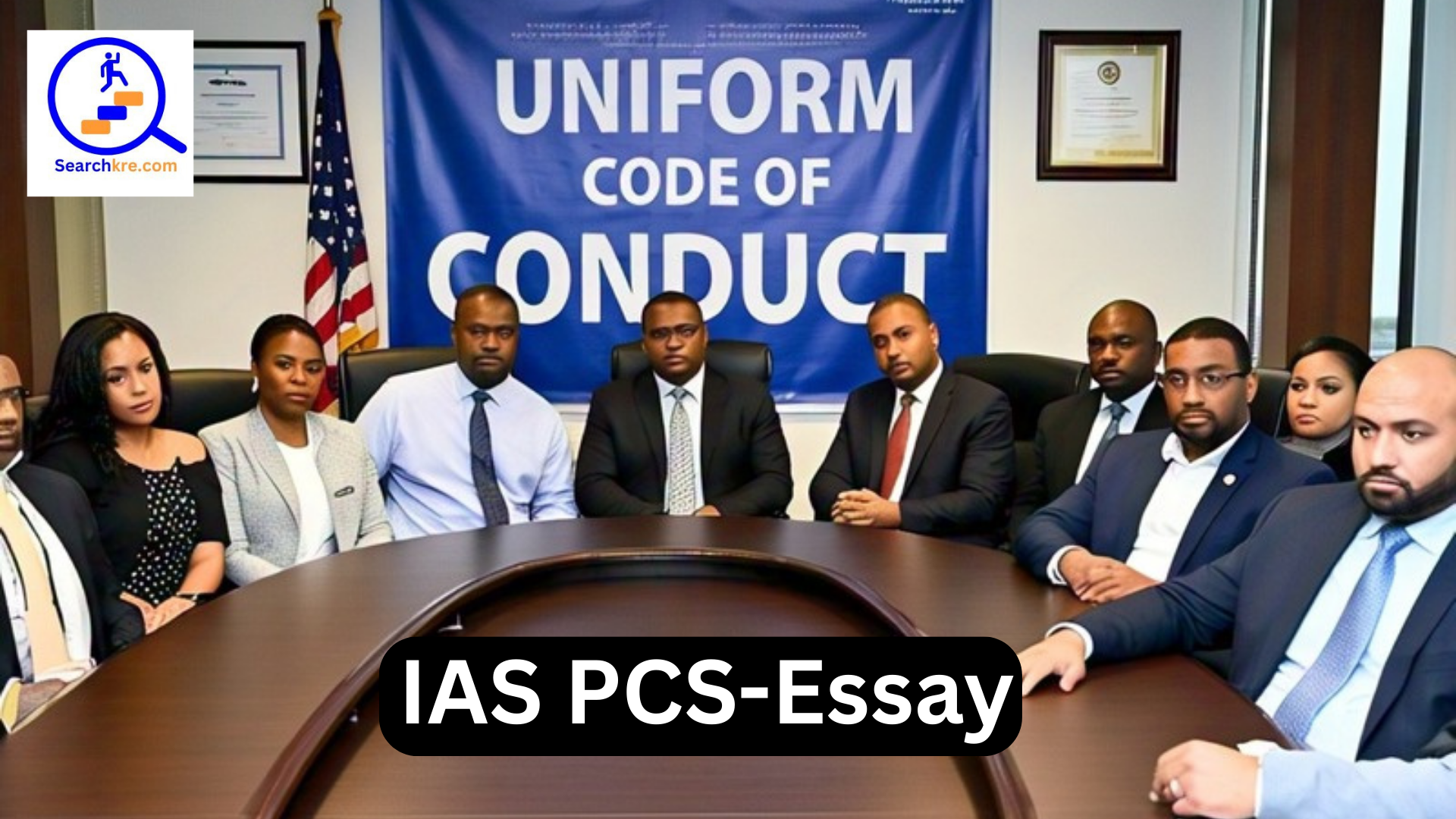
Uniform code of conduct समान आचार संहिता
jp Singh
2025-05-08 14:47:09
searchkre.com@gmail.com /
8392828781
Uniform code of conduct समान आचार संहिता
भारत विविधताओं का देश है — भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक और जातीय दृष्टि से अत्यंत विविध। इन विविधताओं के बावजूद भारत एक गणराज्य के रूप में संगठित है। भारतीय संविधान में नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है, परंतु जब बात नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों की आती है — जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि — तो धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं। इसी असमानता को समाप्त करने तथा नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू करने हेतु "समान आचार संहिता" (Uniform Civil Code- UCC) की अवधारणा प्रस्तुत की गई।
समान आचार संहिता क्या है?
समान आचार संहिता वह कानूनी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू होंगे, चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग या पंथ कुछ भी हो। यह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे निजी विषयों को एक समान दायरे में लाता है, जिससे सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार और दायित्व प्राप्त हों।
इतिहास और पृष्ठभूमि
समान आचार संहिता की अवधारणा कोई नई नहीं है। ब्रिटिश काल में ही इस विषय पर चर्चा आरंभ हो गई थी। 1835 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कानून प्रणाली पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें सुझाव दिया गया था कि आपराधिक कानून तो सबके लिए समान हो सकता है लेकिन निजी कानून धर्म के अनुसार अलग-अलग रहेंगे।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेक विचारकों जैसे महात्मा गांधी, नेहरू और अंबेडकर ने समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपनी राय रखी। संविधान सभा में इस विषय पर व्यापक बहस हुई। डॉ. अंबेडकर ने समान आचार संहिता को आधुनिक भारत के निर्माण के लिए आवश्यक बताया, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण यह अनुच्छेद 44 के रूप में केवल नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्थान पा सका, न कि मौलिक अधिकार के रूप में।
संवैधानिक संदर्भ
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है: “राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।” यह अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, अर्थात इसे लागू करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, परंतु इस पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
वर्तमान कानून व्यवस्था
वर्तमान में भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून हैं
हिंदू कानून: विवाह, उत्तराधिकार आदि के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 आदि लागू होते हैं।
मुस्लिम कानून: शरीयत अधिनियम, 1937 के अंतर्गत मुस्लिम नागरिकों पर शरीयत आधारित कानून लागू होते हैं।
ईसाई कानून: ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 लागू होता है।
पारसी कानून: पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 के अंतर्गत आता है।
समान आचार संहिता के पक्ष में तर्क
1. समानता का सिद्धांत: यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) को मजबूत करता है।
2. लैंगिक न्याय: विभिन्न धार्मिक कानूनों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिए जाते। समान आचार संहिता से यह असमानता दूर हो सकती है।
3. राष्ट्रीय एकता और अखंडता: एक समान नागरिक संहिता से सभी नागरिकों के बीच एकता की भावना विकसित होती है।
4. कानूनी जटिलताओं में कमी: विविध कानूनों के कारण न्याय व्यवस्था में जटिलता आती है, जो एक संहिता से कम हो सकती है।
5. सामाजिक सुधार: यह सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का एक प्रभावी साधन बन सकता है।
विरोध के तर्क
1. धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन: अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। विरोधियों का कहना है कि समान आचार संहिता इस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है।
2. अल्पसंख्यकों की असुरक्षा: कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक इसे अपनी पहचान पर खतरे के रूप में देखते हैं।
3. एकरूपता थोपने का प्रयास: आलोचकों का मानना है कि यह विविधताओं को मिटाकर एक खास बहुसंख्यक समुदाय की प्रणाली को सब पर लागू करने का प्रयास है।
4. धार्मिक भावनाओं को ठेस: निजी मामलों में हस्तक्षेप धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकता है, जिससे सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है।
विभिन्न आयोगों की सिफारिशें
विधान आयोग (Law Commission) 2018 ने कहा था कि "समानता का अर्थ एकरूपता नहीं होता" और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में समान आचार संहिता आवश्यक नहीं है, बल्कि प्रत्येक समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों में सुधार होना चाहिए। हाल ही में 22वें विधान आयोग ने पुनः इस विषय पर जनता से राय मांगी है और एक नई रिपोर्ट की तैयारी कर रहा है।
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
समान आचार संहिता एक अत्यंत संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। कुछ राजनीतिक दल इसका समर्थन करते हैं, यह मानते हुए कि यह सामाजिक सुधार के लिए अनिवार्य है। वहीं कुछ दल इसे धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के विरुद्ध मानते हैं।
गोवा मॉडल
गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ "यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड" लागू है। पुर्तगाली उपनिवेशकाल से ही वहाँ एक समान नागरिक संहिता लागू है जो सभी धर्मों के नागरिकों पर एकसमान लागू होती है। गोवा मॉडल को एक आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु इसकी भी सीमाएँ हैं।
न्यायपालिका की भूमिका
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर समान आचार संहिता के पक्ष में राय दी है:
शाहबानो केस (1985): न्यायालय ने मुस्लिम महिला को भरण-पोषण का अधिकार दिया और सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने की सिफारिश की।
सुष्मिता घोष केस, शायरा बानो केस (तीन तलाक) आदि में न्यायालय ने समान कानून की आवश्यकता को दोहराया।
भविष्य की दिशा
भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में समान आचार संहिता लागू करना आसान नहीं है। इसके लिए आवश्यक है:
1. सर्वसम्मति का निर्माण: इसे लागू करने से पहले सभी समुदायों से संवाद कर सहमति बनाई जाए।
2. चरणबद्ध क्रियान्वयन: एक साथ संपूर्ण संहिता लागू करने के बजाय, विभिन्न चरणों में सुधार किया जाए।
3. संतुलित विधायी प्रक्रिया: ऐसा कानून बनाया जाए जो सभी धर्मों की भावनाओं और संवेदनशीलताओं का सम्मान करे।
4. लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना: महिला अधिकारों की रक्षा करते हुए न्यायसंगत और व्यावहारिक व्यवस्था लागू की जाए।
धर्मनिरपेक्षता और समान आचार संहिता
भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को आधारभूत मूल्य के रूप में स्थापित करता है। इसका आशय यह है कि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। इसी के अनुरूप राज्य को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो सभी नागरिकों को समान रूप से प्रभावित करें, न कि किसी विशेष धर्म के मानदंडों के आधार पर। धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य केवल पूजा-पद्धतियों की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि इस बात की गारंटी भी है कि राज्य के कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान होंगे। जब तक नागरिकों के लिए अलग-अलग धर्म आधारित कानून लागू रहते हैं, तब तक पूर्ण धर्मनिरपेक्षता अधूरी मानी जाती है।
महिला अधिकार और समान आचार संहिता
भारत में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से दोयम रही है, विशेषकर विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के मामलों में। कई धार्मिक कानून महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष अधिकार नहीं देते। उदाहरण के लिए: मुस्लिम कानून में एक पुरुष एकतरफा तीन तलाक देकर विवाह समाप्त कर सकता था (हालांकि अब यह अवैध हो गया है)। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में भी पहले महिलाओं के साथ भेदभाव था, जिसे बाद में संशोधित किया गया।
सांस्कृतिक विविधता और उसका सम्मान
समान आचार संहिता लागू करने की सबसे बड़ी चुनौती भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता है। हर समुदाय के पास अपनी परंपराएं, विवाह की विधियाँ, रीति-रिवाज और जीवनशैली होती है। यह जरूरी है कि समान आचार संहिता बनाते समय इन विविधताओं का सम्मान किया जाए और इसे जबरन थोपा न जाए। इसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो "सामंजस्य" पर आधारित हो, न कि "आदेश" पर।
अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
दुनिया के अधिकांश लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देशों में समान नागरिक कानून लागू हैं। उदाहरण के लिए: फ्रांस और अमेरिका में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों न हों। तुर्की ने अपने धर्म आधारित कानूनों को खत्म कर एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लागू की थी। भारत जैसे देश में भी, जहाँ संविधान लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की नींव पर खड़ा है, समान नागरिक संहिता लागू करना कोई असंभव कार्य नहीं है।
मीडिया और जनभावनाएँ
मीडिया की भूमिका इस बहस में दोहरी रही है। एक ओर, कुछ मीडिया समूह समान आचार संहिता को महिला अधिकारों, आधुनिकता और समानता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं; वहीं दूसरी ओर, कुछ इसे धार्मिक हस्तक्षेप और राजनीतिक हथियार के रूप में चित्रित करते हैं। जनता की राय भी विभाजित रही है। कुछ लोग इसे समय की माँग मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात के रूप में देखते हैं। इसलिए इस विषय में "लोक शिक्षा" और "संवाद" की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
न्यायपालिका के कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय
1. सरला मुद्गल बनाम भारत सरकार (1995): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान आचार संहिता की अनुपस्थिति सामाजिक भेदभाव और धार्मिक अवसरवाद को जन्म देती है।
2. शायरा बानो बनाम भारत सरकार (2017): तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करते हुए कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की ओर स्पष्ट संकेत दिए।
3. जोसेफ शाइन केस (2018): व्यभिचार (adultery) को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए कोर्ट ने व्यक्तिगत अधिकारों की स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना।
इन सभी निर्णयों में न्यायपालिका ने समानता, स्वतंत्रता और धार्मिक सुधारों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।
Conclusion
समान आचार संहिता केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारत के संवैधानिक भविष्य और सामाजिक संरचना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह नागरिकों की समानता, लैंगिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता जैसे उच्च आदर्शों से जुड़ा हुआ है।
Thanks For Read
jp Singh
searchkre.com@gmail.com
8392828781
 Gst Registration
Gst Registration
 DSC Registration
DSC Registration
 Pancard Registration
Pancard Registration
 Company Registration
Company Registration
 Fssai Registration
Fssai Registration
 TradeMark Registration
TradeMark Registration
 MSME Registration
MSME Registration
 Passport Registration
Passport Registration
 Income Tax Return
Income Tax Return
 LLP Company Registration
LLP Company Registration
 Marriage And Court Marriage Registration
Marriage And Court Marriage Registration
 PVT LTD Company Registration
PVT LTD Company Registration
 GST Filing Services
GST Filing Services
 Coaching Insititute Registration
Coaching Insititute Registration
 GYM Registration
GYM Registration
 NGO Registration
NGO Registration
 Political Party Registration
Political Party Registration
 Society Registration
Society Registration
 Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
 Make Website on EMI
Make Website on EMI


























































































 9th Class Scholarship Competition Test
9th Class Scholarship Competition Test
 10th Class Scholarship Competition Test
10th Class Scholarship Competition Test
 11th Class Scholarship Competition Test
11th Class Scholarship Competition Test
 12th Class Scholarship Competition Test
12th Class Scholarship Competition Test
 Graduation Scholarship Competition Test
Graduation Scholarship Competition Test
 Post Graduation Scholarship Competition Test
Post Graduation Scholarship Competition Test
 Diploma Scholarship Competition Test
Diploma Scholarship Competition Test
 Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 JEE Coaching Scholarship Competition Test
JEE Coaching Scholarship Competition Test
 NEET Coaching Scholarship Competition Test
NEET Coaching Scholarship Competition Test
 Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test