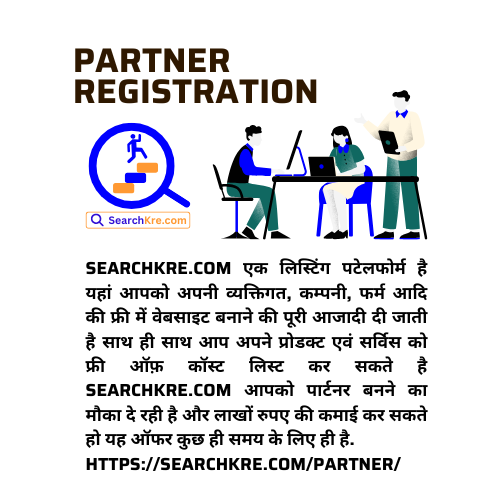भारत-पाकिस्तान संबंध: आज India-Pakistan Relations Today
jp Singh
2025-05-07 00:00:00
searchkre.com@gmail.com /
8392828781
भारत-पाकिस्तान संबंध: आज India-Pakistan Relations Today
भारत और पाकिस्तान का रिश्ता एक ऐसा विषय है जो केवल भौगोलिक सीमाओं या राजनीतिक नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति, धर्म, भावनाओं और संघर्षों का जटिल मिश्रण है। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली और पाकिस्तान का जन्म हुआ, तब से ही दोनों देशों के संबंधों में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। यह विभाजन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मानवीय त्रासदी भी थी जिसने लाखों लोगों को विस्थापित किया और सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया। विभाजन की यह त्रासदी दोनों देशों के सामूहिक अवचेतन में गहरे बैठी हुई है और आज तक उनकी आपसी सोच और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। दोनों देशों की जनता के बीच भावनाओं का समंदर है — कहीं घृणा, कहीं दया, कहीं उम्मीद, तो कहीं विरोध। भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते न केवल दो सरकारों के संबंधों का प्रतीक हैं, बल्कि यह दो समाजों की परस्पर धारणाओं और पूर्वाग्रहों का भी दर्पण हैं।
पिछले सात दशकों में दोनों देशों ने एक-दूसरे के साथ कई युद्ध लड़े, अनेक बार शांति वार्ताएं कीं, और अनेक बार एक-दूसरे के नागरिकों को सांस्कृतिक, खेल और व्यापार के माध्यम से करीब लाने का प्रयास भी किया। इन सब प्रयासों के बावजूद, आज भी भारत-पाकिस्तान संबंध सामान्य नहीं कहे जा सकते। सीमाओं पर तनाव, आतंकवाद, कूटनीतिक संघर्ष और आपसी अविश्वास आज भी दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करते हैं। 21वीं सदी में वैश्वीकरण और तकनीकी विकास ने दुनिया को करीब ला दिया है, लेकिन भारत-पाकिस्तान संबंध आज भी पुराने विवादों में उलझे हुए हैं। जहां एक ओर दोनों देशों के बीच संवाद की आवश्यकता महसूस की जाती है, वहीं दूसरी ओर आतंकवाद जैसे मुद्दों पर कोई भी नरमी स्वीकार्य नहीं है। इस स्थिति में सवाल उठता है — क्या भारत और पाकिस्तान कभी स्थायी शांति और सहयोग की ओर बढ़ सकते हैं? भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति-संपन्न देश हैं और उनके बीच किसी भी प्रकार का युद्ध या टकराव न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरे विश्व की शांति के लिए खतरा हो सकता है। अतः इस संबंध का अध्ययन केवल अकादमिक जिज्ञासा नहीं है
स्वतंत्रता के बाद के संबंध (1947–1971)
भारत-पाकिस्तान विभाजन और कश्मीर विवाद की शुरुआत
1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों के रूप में अस्तित्व में आए, तब ही उनके संबंधों में जटिलता का बीज बोया जा चुका था। विभाजन एक अत्यंत दर्दनाक प्रक्रिया थी जिसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों को विस्थापित होना पड़ा। धर्म के आधार पर विभाजन होने के बावजूद कई ऐसे क्षेत्र थे, जिनका राजनीतिक भविष्य अस्पष्ट था। इन्हीं में से एक था जम्मू और कश्मीर।
जम्मू और कश्मीर एक रियासत थी जिसका शासक हिंदू (महाराजा हरि सिंह) था, जबकि जनसंख्या बहुलता में मुस्लिम थी। महाराजा ने आरंभ में स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, लेकिन जब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, तब महाराजा ने भारत से सैन्य सहायता मांगी। बदले में उन्होंने भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार कश्मीर भारत का हिस्सा बना और यहीं से भारत-पाक संबंधों में पहला बड़ा संघर्ष शुरू हुआ।
प्रथम भारत-पाक युद्ध (1947–48)
कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच पहला युद्ध 1947 में हुआ। भारतीय सेना ने बड़ी कुशलता से कश्मीर के अधिकांश हिस्से को बचा लिया, लेकिन पाकिस्तान-समर्थित हमलावरों ने कश्मीर के एक तिहाई हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे आज 'पाक-अधिकृत कश्मीर' (POK) कहा जाता है। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा और 1949 में युद्धविराम हुआ। इसके बाद एक 'सीज़फायर लाइन' बनाई गई, जो आज 'लाइन ऑफ कंट्रोल' (LOC) के नाम से जानी जाती है।
दूसरा भारत-पाक युद्ध (1965)
1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ करवाई, जिसका उद्देश्य कश्मीर की जनता को भारत के खिलाफ भड़काना था। परन्तु इस योजना में असफलता मिली और भारत ने पाकिस्तान पर पूर्ण सैन्य हमला किया। यह युद्ध दोनों देशों के बीच दूसरे व्यापक संघर्ष के रूप में दर्ज हुआ। युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। इस युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र और रूस की मध्यस्थता से हुआ और दोनों देशों ने 1966 में ताशकंद समझौता किया। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु इसी समझौते के बाद ताशकंद में ही रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई, जिससे भारत में आंतरिक हलचल और असंतोष भी पैदा हुआ।
तीसरा भारत-पाक युद्ध (1971) और बांग्लादेश का निर्माण
1971 का भारत-पाक युद्ध इन संबंधों का सबसे निर्णायक मोड़ था। इसका मूल कारण था पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में राजनीतिक असंतोष और मानवाधिकारों का उल्लंघन। पूर्वी पाकिस्तान में जनता ने शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को चुनावों में बहुमत दिया था, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान की सरकार ने सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया। इसके विरोध में पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह हुआ और पाकिस्तानी सेना ने नागरिकों पर अत्याचार शुरू कर दिए।
इस क्रूरता से लाखों शरणार्थी भारत की सीमाओं में आ गए। भारत के लिए यह न केवल मानवीय संकट था, बल्कि सुरक्षा का भी प्रश्न बन गया। अंततः भारत ने 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में भारत ने निर्णायक विजय प्राप्त की और केवल 13 दिनों में पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में आत्मसमर्पण कर दिया। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में आए और एक नया देश — बांग्लादेश — अस्तित्व में आया। इस युद्ध के बाद भारत-पाक संबंधों में असमानता स्पष्ट रूप से सामने आई। भारत ने अपने सैन्य और रणनीतिक कौशल से एक नए राष्ट्र का निर्माण करवाया, जबकि पाकिस्तान को एक बड़ी राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक हार का सामना करना पड़ा।
शिमला समझौता (1972)
1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि दोनों देश अपने विवादों को केवल द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करेंगे। यह समझौता द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार किया गया। यह भी तय हुआ कि युद्धबंदी रेखा को 'लाइन ऑफ कंट्रोल' (LOC) का नाम दिया जाएगा और भविष्य में इस सीमा का सम्मान किया जाएगा। हालांकि, शिमला समझौते से आशा की किरण जागी, लेकिन विश्वास की कमी और परस्पर संदेह ने इन आशाओं को समय के साथ कमजोर कर दिया।
1990 के दशक में भारत-पाकिस्तान संबंध
दशक की शुरुआत: तनाव और उथल-पुथल
1990 का दशक भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कई दृष्टियों से परिवर्तनकारी रहा। इस समय के दौरान वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण घटनाएँ हो रही थीं — सोवियत संघ का विघटन, वैश्वीकरण की शुरुआत, और दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक संघर्षों का उदय। भारत ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया, वहीं पाकिस्तान सैन्य और नागरिक शासन के बीच संघर्ष से जूझता रहा। इस दौरान कश्मीर में उग्रवाद ने भी ज़ोर पकड़ा, जिसने दोनों देशों के संबंधों को और अधिक जटिल बना दिया।
कश्मीर में उग्रवाद और पाकिस्तान की भूमिका
1990 के दशक की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद ने तेजी से जोर पकड़ा। इस उग्रवाद को भारत ने सीमापार से प्रायोजित आतंकवाद के रूप में देखा, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका होने के आरोप लगे। भारत ने बार-बार यह दावा किया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रशिक्षण, शस्त्र और आर्थिक सहायता दे रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया और इसे 'कश्मीरी जनता की स्वतंत्रता की लड़ाई' बताया। यह मुद्दा भारत-पाक संबंधों में मुख्य बाधा बना रहा और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कई बार बाधित हुई।
परमाणु परीक्षण और क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन
1998 में भारत ने पोखरण में पाँच परमाणु परीक्षण किए, जिनके बाद पाकिस्तान ने भी चगाई में अपने परमाणु परीक्षण किए। इस प्रकार दोनों देश अब "घोषित परमाणु शक्ति" बन गए। इन परीक्षणों ने पूरे विश्व को चौंका दिया और अमेरिका सहित कई देशों ने दोनों पर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन यह घटनाक्रम भारत-पाक संबंधों की दिशा में एक नया अध्याय बन गया। हालांकि इन परीक्षणों ने दोनों देशों के बीच शक्ति-संतुलन स्थापित किया, लेकिन इसके साथ ही युद्ध की संभावना और भय भी बढ़ गया, क्योंकि अब किसी भी संघर्ष का परिणाम विनाशकारी हो सकता था।
बस सेवा और लाहौर घोषणापत्र: शांति की आशा
1999 की शुरुआत में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 'लाहौर बस यात्रा' की शुरुआत की और बस से लाहौर पहुँचे। उन्होंने वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ लाहौर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों ने आपसी संबंध सुधारने और कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्वक हल करने की प्रतिबद्धता जताई। यह पहल दोनों देशों की जनता के बीच सकारात्मक संदेश लेकर आई और शांति की वास्तविक संभावना नजर आई। लेकिन यह आशा बहुत कम समय तक टिक सकी।
कारगिल युद्ध (1999): विश्वासघात का प्रतीक
लाहौर घोषणापत्र के कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान की सेना ने कारगिल क्षेत्र में भारतीय सीमाओं में घुसपैठ कर दी। यह घुसपैठ मुख्यतः पाकिस्तानी सेना और ISI के द्वारा प्रायोजित थी, जिसमें पाकिस्तानी नियमित सैनिक भी शामिल थे। भारत ने इस घुसपैठ को "आक्रामक युद्ध" माना और कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में भारत ने वीरता और रणनीतिक कुशलता का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विशेषतः अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के हस्तक्षेप के बाद, पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। कारगिल युद्ध को भारत ने पाकिस्तान द्वारा किए गए "विश्वासघात" के रूप में देखा, क्योंकि यह उस समय हुआ जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने शांति समझौता किया था।
21वीं सदी में भारत-पाक संबंधों का नया दौर
21वीं सदी के आरंभिक वर्षों में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक बार फिर से वार्ता और शांति प्रक्रिया की संभावना बनी, लेकिन आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य टकरावों ने इन प्रयासों को बार-बार पटरी से उतार दिया। यह दौर उन घटनाओं से भरा रहा जिन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्तों को कभी उम्मीदों से भर दिया, तो कभी कड़वाहट से भर दिया।
संसद पर हमला (2001): बातचीत पर विराम
13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले ने भारत-पाक संबंधों को एक बार फिर गहरे संकट में डाल दिया। भारत ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों — जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद — को जिम्मेदार ठहराया। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध लगभग समाप्त हो गए और सीमा पर तनाव चरम पर पहुँच गया। भारत ने पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जबकि पाकिस्तान ने आरोपों को नकारते हुए "सबूत" की बात कही। इस घटना ने द्विपक्षीय वार्ता को पूरी तरह रोक दिया।
अग्नि और अमन: शांति की पहलें (2003–2007)
2003 में दोनों देशों ने सीज़फायर समझौते पर सहमति जताई, जिससे LOC पर शांति बनी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे "Composite Dialogue Process" कहा गया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न पहलें की गईं: - दिल्ली–लाहौर बस सेवा का पुनरारंभ - मुज़फ्फराबाद-श्रीनगर बस सेवा की शुरुआत - व्यापार और लोगों के बीच आवाजाही को बढ़ावा - आगरा शिखर वार्ता (2001) — भले ही विफल रही, पर एक कूटनीतिक प्रयास के रूप में महत्त्वपूर्ण रही इन प्रयासों के चलते जनता में यह विश्वास बढ़ा कि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य किया जा सकता है। पर यह स्थायीत्व नहीं रहा।
26/11 मुंबई हमला (2008): एक और बड़ा झटका
26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले ने भारत-पाक संबंधों को फिर से गहरे अंधकार में धकेल दिया। इस हमले में 166 लोग मारे गए और इसका संचालन पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किया गया था। अजमल कसाब नामक आतंकी को भारत ने जीवित पकड़ा, जिसने पाकिस्तान से संपर्कों की पुष्टि की। भारत ने पाकिस्तान से ठोस कार्रवाई और जिम्मेदारों को सज़ा दिलाने की मांग की, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई। भारत ने द्विपक्षीय बातचीत पर फिर विराम लगा दिया। यह हमला आम भारतीय जनमानस में पाकिस्तान के प्रति अत्यधिक आक्रोश का कारण बना और द्विपक्षीय संबंधों में अविश्वास की गहराई और बढ़ गई।
सर्जिकल स्ट्राइक (2016) और उरी हमला
सितंबर 2016 में जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना पर बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 19 जवान शहीद हुए। इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों को माना गया। इसके जवाब में भारत ने पहली बार सीमा पार जाकर "सर्जिकल स्ट्राइक" की, जिसमें LOC पार आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। भारत सरकार ने इसे 'नई रणनीति' का संकेत बताया — जिसमें आतंकवाद का जवाब आतंकवादियों पर सीधे कार्रवाई से दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को नकारा, लेकिन भारत के इस कदम ने देश में भारी समर्थन और वैश्विक ध्यान अर्जित किया।
पुलवामा हमला और बालाकोट एयरस्ट्राइक (2019)
14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 जवान शहीद हुए। जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली। इसके जवाब में भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट में एयरस्ट्राइक की, जिसमें कथित आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने अगले दिन भारत के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला किया और भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ लिया गया। बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने अभिनंदन को लौटाया, जिसे भारत ने "शांति की पहल" नहीं बल्कि दबाव का परिणाम कहा। यह घटनाएँ दर्शाती हैं कि भारत ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है — अब केवल कूटनीतिक विरोध नहीं, बल्कि सैन्य कार्रवाई भी संभावित विकल्पों में है।
पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति का प्रभाव
इस दौर में पाकिस्तान में कई राजनीतिक उथल-पुथल हुईं। वहाँ की सेना का हस्तक्षेप, लोकतंत्र की अस्थिरता और कट्टरपंथी तत्वों का प्रभाव बढ़ता गया। भारत को यह स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा कि पाकिस्तान में वास्तविक सत्ता सेना और ISI के पास है, न कि लोकतांत्रिक सरकार के पास। इस अस्थिरता ने भारत-पाक वार्ता को बार-बार बाधित किया, क्योंकि भारत किसी ऐसे पक्ष से गंभीर बातचीत नहीं करना चाहता था जो अपने निर्णयों में स्वतंत्र न हो।
अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण में परिवर्तन
इन वर्षों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखी। फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा, क्योंकि वह आतंकवाद को रोकने में असफल रहा। भारत ने अमेरिका, फ्रांस, रूस और कई देशों को अपने पक्ष में किया, जिससे पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव बढ़ा। उधर, चीन और पाकिस्तान की निकटता — विशेषतः CPEC परियोजना के माध्यम से — भारत के लिए नई चुनौतियाँ लेकर आई। भारत को अपनी कूटनीति को संतुलित करना पड़ा।
भारत-पाकिस्तान संबंध: आज की स्थिति (2020–2024)
कोविड-19 काल और आपसी संवाद की ठंडी बयार
2020 में वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण पूरे विश्व की राजनीति और कूटनीति में ठहराव आया। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने इस दौरान घरेलू समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। इस काल में द्विपक्षीय संबंधों में कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन सीमाओं पर संघर्ष भी सीमित रहा। यह वह दौर था जब दोनों देशों के बीच 'न तो युद्ध, न ही वार्ता' वाली स्थिति बनी रही। हालांकि भारत ने कोविड संकट के दौरान दक्षिण एशियाई देशों को सहायता प्रदान की, लेकिन पाकिस्तान ने इन प्रयासों का भाग नहीं लिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि आपसी संबंधों में अभी भी अविश्वास बना हुआ है।
सीज़फायर समझौता 2021: अचानक सुकून की लहर
फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान ने अचानक एक संयुक्त बयान जारी कर यह घोषणा की कि दोनों देश लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) पर 2003 के सीज़फायर समझौते का पुनः पूर्ण पालन करेंगे। यह निर्णय सेना के डीजीएमओ (Director General of Military Operations) स्तर पर हुई बातचीत के बाद लिया गया। इस घोषणा को एक सकारात्मक संकेत माना गया, खासकर तब जब इससे पूर्व दोनों देशों के बीच लंबे समय से संवाद ठप पड़ा था। सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं में गिरावट आई, और सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों को राहत मिली। यह घटनाक्रम दोनों देशों की सेना के बीच भरोसे की एक झलक प्रस्तुत करता है। हालांकि यह भी स्पष्ट हो गया कि यह पहल केवल सीमा प्रबंधन तक सीमित है — इससे राजनीतिक या कूटनीतिक स्तर पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकला।
कश्मीर मुद्दे पर स्थिति और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया
अगस्त 2019 में भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जोर-शोर से उठाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने इसे 'अवैध क़ब्ज़ा' करार दिया और संयुक्त राष्ट्र, OIC (इस्लामिक देशों का संगठन) और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाई। हालांकि भारत ने इसे पूरी तरह आंतरिक मामला बताते हुए किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार कर दिया। 2020–2024 के बीच पाकिस्तान लगातार यह मांग करता रहा कि भारत अनुच्छेद 370 को पुनः बहाल करे, तभी कोई संवाद संभव है। भारत ने इस शर्त को पूरी तरह खारिज कर दिया और वार्ता के लिए 'आतंकवाद मुक्त माहौल' की आवश्यकता को दोहराया।
कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध: ठप स्थिति
वर्ष 2019 के बालाकोट हमले और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को घटाकर अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया और द्विपक्षीय व्यापार भी निलंबित कर दिया। इसके बाद से 2024 तक व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते लगभग शून्य स्तर पर बने हुए हैं। भारत ने भी इस स्थिति को 'पाकिस्तान की राजनीतिक पसंद' कहकर स्वीकार कर लिया और किसी भी पुनर्संवाद के लिए आतंकवाद पर कार्रवाई को शर्त रखा। पाकिस्तान ने भारत पर 'संघीय मानसिकता' का आरोप लगाया और कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाए रखने का प्रयास किया। व्यापारिक संबंधों की अनुपस्थिति से दोनों देशों की सीमावर्ती जनता को आर्थिक नुकसान हुआ है, विशेषतः पाकिस्तान के लिए, जो कई वस्तुओं के लिए भारत पर निर्भर रहा करता था।
सीमा पर ड्रोन, आतंकवाद और सुरक्षा चिंताएँ
हाल के वर्षों में भारत-पाक सीमा पर ड्रोन गतिविधियों में तेज़ी आई है। पंजाब और जम्मू क्षेत्रों में हथियारों और नशीले पदार्थों की आपूर्ति के लिए पाकिस्तानी ड्रोन का उपयोग किया गया। भारत ने इन गतिविधियों को सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। साथ ही, सीमापार आतंकवाद के प्रयास अब भी पूरी तरह रुके नहीं हैं। भारत लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान अब भी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों को समर्थन दे रहा है। हालांकि बड़ी आतंकी घटनाओं में गिरावट आई है, लेकिन LOC पर घुसपैठ और मुठभेड़ों की घटनाएँ जारी हैं।
भारत की विदेश नीति: पड़ोसी लेकिन प्राथमिकता नहीं
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान अब उसकी विदेश नीति की प्राथमिकता नहीं है। भारत ने वैश्विक मंचों पर अपनी छवि को उदार, निर्णायक और आधुनिक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने पर ज़ोर दिया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत की संभावना केवल तभी खुलेगी जब वहां आतंकवाद के खिलाफ ठोस और मापनीय कार्रवाई हो। भारत ने हाल के वर्षों में पाकिस्तान को "अलग-थलग करने की नीति" (Isolation Policy) अपनाई है, जो संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 तक विभिन्न मंचों पर दिखी है।
पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और सेना का नियंत्रण
2020–2024 के बीच पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति अस्थिर रही। इमरान खान की सरकार गिरने, और सेना के साथ संघर्षों ने लोकतंत्र को कमजोर किया। पाकिस्तान में सेना अब भी विदेश नीति, विशेषकर भारत नीति, पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। भारत में यह धारणा गहरी हो चुकी है कि पाकिस्तान की अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था, आतंकवाद की स्वीकार्यता और सेना की निर्णायक भूमिका — ये सभी मिलकर किसी भी स्थायी समझौते की राह को बाधित करते हैं।
सामरिक दृष्टिकोण और वैश्विक बदलती प्राथमिकताएँ
भारत अब चीन को अपनी प्रमुख सामरिक चुनौती मानता है, और पाकिस्तान को द्वितीयक खतरे के रूप में देखता है। भारत की रक्षा रणनीति, सीमाई निगरानी और कूटनीतिक संसाधन अब मुख्यतः चीन की ओर केंद्रित हैं। इसका असर यह हुआ है कि पाकिस्तान के प्रति भारत का दृष्टिकोण अब ज्यादा 'प्रतिक्रियात्मक' है — यानी, जब तक पाकिस्तान कोई उत्तेजक कार्रवाई न करे, तब तक भारत का रुख तटस्थ या ठंडा रहता है।
संभावनाएँ और भविष्य की राह
भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध दशकों से टकराव, अविश्वास और संघर्ष की कहानी रहे हैं। लेकिन इस अंधेरे में भी कुछ किरणें ऐसी हैं जो आशा जगाती हैं। यदि दोनों देश संकल्प लें और नीतिगत दूरदर्शिता दिखाएँ, तो यह संबंध शांति, सहयोग और स्थायित्व की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इस खंड में हम इन्हीं संभावनाओं, चुनौतियों और व्यावहारिक सुझावों का विश्लेषण करेंगे।
कूटनीतिक संवाद की पुनर्स्थापना
संवाद किसी भी द्विपक्षीय संबंध का आधार होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संवाद वर्षों से रुका हुआ है। वर्तमान में कोई उच्च स्तरीय वार्ता प्रक्रिया नहीं चल रही है, और न ही दूतावासों में पूर्ण राजनयिक उपस्थिति है।
भविष्य में यदि:
- दोनों देश बिना पूर्व शर्तों के बैठक और वार्ता के लिए तैयार हों, - एक स्थायी वार्ता प्रक्रिया शुरू हो जिसमें हर विषय पर चरणबद्ध रूप से चर्चा हो, - और कुछ नॉन-कॉन्टेक्ट मुद्दों (जैसे पर्यावरण, जलवायु, व्यापार) पर पहल की जाए, तो शांति की ओर पहला कदम बढ़ सकता है।
सीमा प्रबंधन और आतंकवाद पर संयुक्त नीति
भारत की सबसे बड़ी चिंता सीमापार आतंकवाद है। पाकिस्तान यदि गंभीरता से आतंकवाद को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए: - आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को दिखावे की बजाय प्रभावी बनाना, - FATF (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की शर्तों का वास्तविक पालन करना, - और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से आतंकी नेटवर्क पर लगाम कसना, तो भारत के लिए भरोसे का आधार बनेगा। इसके साथ-साथ सीमा सुरक्षा बलों के बीच संपर्क, सूचनाओं का आदान-प्रदान, और ड्रोन गतिविधियों पर समझौता जैसी पहलें आवश्यक हैं।
व्यापार और आर्थिक सहयोग की संभावनाएँ
भारत और पाकिस्तान का व्यापार 2019 के बाद लगभग शून्य हो गया है, जबकि 2012–2014 के बीच यह लगभग 2.5 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया था।
भविष्य के लिए:
- सीमित व्यापार को कृषि, फार्मा, कपड़ा, और चिकित्सा उपकरणों जैसे क्षेत्रों तक सीमित करके पुनः शुरू किया जा सकता है। - करतारपुर कॉरिडोर की तरह आर्थिक "कॉरिडोर" भी विकसित किए जा सकते हैं जो दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ें। व्यापारिक संबंध न केवल आर्थिक लाभ देते हैं, बल्कि संवाद और संपर्क की ज़मीन भी तैयार करते हैं।
जल और पर्यावरणीय सहयोग
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि (1960) एकमात्र ऐसी संधि है जो हर संघर्ष के बावजूद लागू रही है। इस संधि के अंतर्गत सहयोग बढ़ाया जा सकता है: - जलवायु परिवर्तन, बाढ़ नियंत्रण और जल स्रोत प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी हो, - सतलुज–रावी नदी बेसिन जैसे क्षेत्रों में संयुक्त पर्यावरणीय परियोजनाएँ हों। यह न केवल संबंधों को स्थायित्व देगा, बल्कि आम जनता को भी लाभ पहुँचेगा।
जन संवाद और सांस्कृतिक जुड़ाव
राजनीतिक तनावों के बीच आम जनता की भूमिका अक्सर अनदेखी रह जाती है। भारत और पाकिस्तान की जनता के बीच सांस्कृतिक, भाषाई, और पारिवारिक संबंध हैं। इन्हें आधार बनाकर: - छात्र और कलाकारों के लिए विज़ा नियम सरल किए जाएँ, - साहित्य, संगीत, और सिनेमा के माध्यम से संवाद बढ़े, - सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जवाबदेही के साथ सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा मिले। जन संवाद एक मजबूत शांति नींव तैयार कर सकता है।
अफगानिस्तान और क्षेत्रीय संतुलन
2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी ने भारत-पाक समीकरण को भी प्रभावित किया है। पाकिस्तान के लिए यह सामरिक लाभ हो सकता है, लेकिन भारत के लिए सुरक्षा चिंता भी। दोनों देश यदि अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग का मार्ग अपनाएँ तो: - अफगानिस्तान में स्थिरता आ सकती है, - और यह क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक सकारात्मक संकेत होगा। इसके लिए दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन (SAARC) को भी पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।
मीडिया की भूमिका: जिम्मेदारी बनाम उकसावा
दोनों देशों के मीडिया, विशेषकर टीवी चैनलों ने अक्सर राष्ट्रवाद के नाम पर युद्धोन्माद को बढ़ावा दिया है। भविष्य में: - मीडिया संस्थानों को स्व-नियमन की नीति अपनानी चाहिए, - और सरकारों को विश्वसनीय संवाद के लिए स्वतंत्र मीडिया मंच विकसित करने चाहिए। सकारात्मक रिपोर्टिंग और सचेत विमर्श से जनमत को शांति की ओर मोड़ा जा सकता है।
वैश्विक मध्यस्थता की सीमाएँ और संभावनाएँ
भारत सदैव द्विपक्षीय वार्ता का समर्थक रहा है, जबकि पाकिस्तान ने बार-बार संयुक्त राष्ट्र या तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की मांग की है। भविष्य में: - किसी बाहरी हस्तक्षेप की बजाय पारस्परिक स्वीकृति से समाधान तलाशा जाना चाहिए, - लेकिन आर्थिक और आतंकवाद विरोधी संगठनों में साझा भागीदारी से दोनों देशों पर वैश्विक दबाव बनाया जा सकता है।
शिक्षा, विज्ञान और स्वास्थ्य में सहयोग
भविष्य की एक सकारात्मक दिशा यह भी हो सकती है कि: - दोनों देश संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं में भाग लें (जैसे — जलवायु परिवर्तन, वैक्सीन विकास), - शिक्षा क्षेत्र में छात्रवृत्तियाँ दी जाएँ, - और कोविड जैसी महामारी में साझा रणनीति बने। इससे एक नया ‘ट्रस्ट बिल्डिंग मेकैनिज़्म’ तैयार किया जा सकता है।
भारत-पाकिस्तान संबंध — अतीत की छाया से भविष्य की राह तक
भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध एक अत्यंत जटिल और संवेदनशील विषय रहा है, जिसकी जड़ें इतिहास, धर्म, भू-राजनीति और भावनात्मक स्मृतियों में गहराई से पैठी हुई हैं। 1947 में बँटवारे के साथ जो यात्रा आरंभ हुई थी, वह आज भी न तो स्थिर शांति तक पहुँच पाई है और न ही पूर्ण संघर्षविराम तक। यह संबंध न केवल दो देशों के बीच का मामला है, बल्कि दक्षिण एशिया की स्थिरता, विकास और मानवीय समृद्धि से भी सीधे जुड़ा हुआ है।
इस निबंध में हमने भारत-पाकिस्तान संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रमुख युद्ध और संघर्ष, कूटनीतिक पहल, विवादास्पद मुद्दों, हालिया घटनाक्रमों और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया। समग्र दृष्टि से यह स्पष्ट होता है कि दोनों देशों के बीच विश्वास की खाई बहुत गहरी है, जिसे भरने के लिए केवल राजनीतिक घोषणाएँ ही नहीं, बल्कि ठोस नीतिगत कार्रवाई और जन समर्थन की आवश्यकता है।
अतीत: एक टूटा विश्वास और संघर्ष की विरासत
1947 में विभाजन की पीड़ा, लाखों लोगों की जानें, और संपत्ति का विनाश — यह सब भारत और पाकिस्तान के सामूहिक अवचेतन में आज भी जीवित है। इसके बाद के युद्धों (1947–48, 1965, 1971, 1999) ने इस घाव को और गहरा किया। कश्मीर जैसे मुद्दे ने दोनों देशों के राजनीतिक विमर्श को आक्रामक और सुरक्षा-केंद्रित बनाए रखा। इतिहास ने यह सिद्ध किया है कि बल, प्रतिशोध और टकराव से केवल क्षति ही होती है। शांति प्रयास, जैसे 2003 का सीज़फायर, 2008 का साझा आर्थिक संवाद, और 2021 में LOC शांति बहाली — यह दर्शाते हैं कि जब इच्छा होती है, तो स्थिरता संभव है। लेकिन यह प्रयास टिकाऊ तभी बन सकते हैं जब वे सैद्धांतिक नहीं, व्यावहारिक और जनोन्मुखी हों।
वर्तमान: जमी हुई बर्फ, पर भीतर बहता जल
आज की स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद लगभग ठप है, राजनयिक संबंध न्यूनतम हैं, और व्यापार बंद है। कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों की स्थिति सख्त बनी हुई है — भारत इसे आंतरिक मामला मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास करता है। भारत अब पाकिस्तान को प्राथमिकता नहीं देता, उसकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु चीन, अमेरिका, और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र हो गया है। वहीं पाकिस्तान आंतरिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, और सेना-राजनीति के टकरावों से जूझ रहा है। फिर भी, सीमाओं पर गोलीबारी में कमी, आतंकवाद के मामलों में कुछ हद तक गिरावट, और करतारपुर जैसे सांस्कृतिक पुल यह संकेत देते हैं कि संवाद के द्वार पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं।
भविष्य: विकल्पों की तलाश और शांति की रणनीति
भविष्य के लिए भारत-पाकिस्तान संबंधों को सकारात्मक दिशा में ले जाने हेतु निम्नलिखित बिंदु अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं:
(क) परस्पर सम्मान और समानता का आधार:
कोई भी वार्ता तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक दोनों पक्ष समान अधिकार और सम्मान के साथ बैठें। भारत का 'बड़े भाई' वाला रवैया और पाकिस्तान का 'पीड़ित मानसिकता' वाला दृष्टिकोण — दोनों को ही बदलना होगा।
(ख) आतंकवाद पर निर्णायक रुख:
पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि आतंकवाद सिर्फ भारत का नहीं, उसका भी शत्रु है। आतंकवादी गुटों के विरुद्ध निष्क्रियता, केवल भारत नहीं, बल्कि वैश्विक समुदाय को भी अस्वीकार्य है।
(ग) जन स्तर पर संपर्क और संवाद:
छात्र, कलाकार, लेखकों, मीडिया, और सामाजिक संगठनों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना दोनों देशों के भविष्य के नागरिकों के बीच विश्वास निर्माण की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है।
(घ) क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक साझेदारी:
SAARC जैसे मंचों को सक्रिय कर, आपसी व्यापार को सीमित लेकिन रणनीतिक स्तर पर पुनः प्रारंभ कर, दोनों देश एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं।
(ङ) मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका:
मीडिया का राष्ट्रवाद और सनसनी फैलाने का चलन, दोनों देशों में जनमानस को उकसाता है। संयमित, सत्यपरक और संवादोन्मुख मीडिया ही एक नए सामाजिक मानस का निर्माण कर सकता है।
क्या शांति संभव है?
यह प्रश्न बार-बार उठता है — क्या भारत और पाकिस्तान कभी सच्चे मित्र बन सकते हैं? इसका उत्तर सरल नहीं, पर असंभव भी नहीं है।
विश्व राजनीति में कई उदाहरण हैं जहाँ दशकों तक संघर्ष करने वाले देश अंततः संवाद और सहयोग की ओर बढ़े हैं — फ्रांस और जर्मनी, अमेरिका और वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी राष्ट्र। यह दिखाता है कि अगर राजनीतिक नेतृत्व दूरदर्शिता और साहस दिखाए, तो असंभव को संभव बनाया जा सकता है। शांति कोई आदर्श नहीं — आवश्यकता है। युद्ध अब किसी का समाधान नहीं है, विशेषतः जब दोनों देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं। विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, और जलवायु जैसे मुद्दे कहीं अधिक जरूरी हैं।
भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के लिए:
- स्मृतियों को भुलाना नहीं, बल्कि समझदारी से पुनर्परिभाषित करना होगा,
- टकराव की भाषा को त्याग कर सहयोग की शब्दावली अपनानी होगी,
- और शक्ति प्रदर्शन की राजनीति से निकलकर जनकल्याण की कूटनीति को अपनाना होगा।
भारत-पाक संबंध एक ऐसी परीक्षा है जिसमें दोनों देश पास या फेल नहीं — साथ में ही सफल या असफल हो सकते हैं।
“यदि युद्ध के शोर में हम संवाद की आवाज़ न खो दें — तो एक दिन जरूर वह दिन आएगा जब वाघा बॉर्डर केवल सलामी की जगह नहीं, साझेदारी का प्रतीक बनेगा।”
Conclusion
1947 से 1971 तक भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की दिशा को मुख्यतः युद्ध, संघर्ष और अविश्वास ने परिभाषित किया। कश्मीर विवाद ने प्रारंभिक वर्षों में ही दोनों देशों के बीच गहरी खाई बना दी, जिसे बार-बार हुए युद्धों और राजनीतिक अस्थिरता ने और गहरा कर दिया। हालांकि शिमला समझौता एक सकारात्मक पहल थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि केवल समझौतों से शांति नहीं आती, जब तक दोनों पक्षों में वास्तविक राजनीतिक इच्छाशक्ति, परस्पर सम्मान और विश्वास न हो। 1990 का दशक भारत-पाक संबंधों के लिए एक ऐसा कालखंड रहा जिसमें शांति और संघर्ष दोनों के प्रयास देखने को मिले। एक ओर जहां कश्मीर में उग्रवाद, सीमा पार आतंकवाद और कारगिल जैसे घटनाक्रमों ने संबंधों को विषाक्त किया, वहीं दूसरी ओर लाहौर यात्रा जैसी पहलें शांति की संभावना
यह युग यह दर्शाता है कि जब तक पाकिस्तान अपनी नीति में कट्टरपंथ और आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक स्थायी शांति की संभावनाएँ क्षीण बनी रहेंगी। शांति की कोई भी संभावना तब तक नहीं उभर सकती जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का परित्याग नहीं करता और दोनों देशों में परस्पर सम्मान एवं व्यावहारिक संवाद की भावना विकसित नहीं होती। शांति कोई आदर्शवादी स्वप्न नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता है — और इसकी पहली ईंट संवाद और विश्वास से रखी जा सकती है। “यदि युद्ध के शोर में हम संवाद की आवाज़ न खो दें — तो एक दिन जरूर वह दिन आएगा जब वाघा बॉर्डर केवल सलामी की जगह नहीं, साझेदारी का प्रतीक बनेगा।”
Thanks For Read
jp Singh
searchkre.com@gmail.com
8392828781
 Gst Registration
Gst Registration
 DSC Registration
DSC Registration
 Pancard Registration
Pancard Registration
 Company Registration
Company Registration
 Fssai Registration
Fssai Registration
 TradeMark Registration
TradeMark Registration
 MSME Registration
MSME Registration
 Passport Registration
Passport Registration
 Income Tax Return
Income Tax Return
 LLP Company Registration
LLP Company Registration
 Marriage And Court Marriage Registration
Marriage And Court Marriage Registration
 PVT LTD Company Registration
PVT LTD Company Registration
 GST Filing Services
GST Filing Services
 Coaching Insititute Registration
Coaching Insititute Registration
 GYM Registration
GYM Registration
 NGO Registration
NGO Registration
 Political Party Registration
Political Party Registration
 Society Registration
Society Registration
 Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
 Make Website on EMI
Make Website on EMI


























































































 9th Class Scholarship Competition Test
9th Class Scholarship Competition Test
 10th Class Scholarship Competition Test
10th Class Scholarship Competition Test
 11th Class Scholarship Competition Test
11th Class Scholarship Competition Test
 12th Class Scholarship Competition Test
12th Class Scholarship Competition Test
 Graduation Scholarship Competition Test
Graduation Scholarship Competition Test
 Post Graduation Scholarship Competition Test
Post Graduation Scholarship Competition Test
 Diploma Scholarship Competition Test
Diploma Scholarship Competition Test
 Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 JEE Coaching Scholarship Competition Test
JEE Coaching Scholarship Competition Test
 NEET Coaching Scholarship Competition Test
NEET Coaching Scholarship Competition Test
 Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test