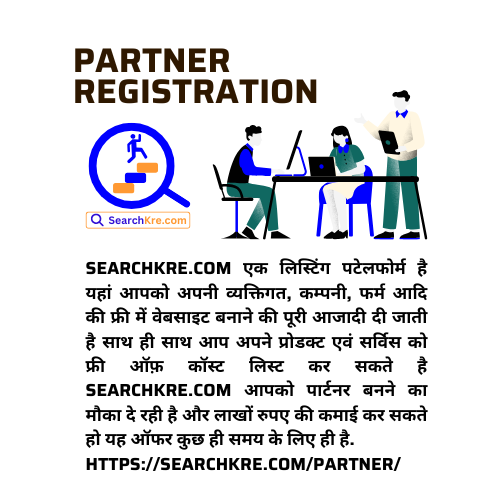"बायोरेमेडिएशन की भूमिका" (Role of Bioremediation)
jp Singh
2025-05-06 00:00:00
searchkre.com@gmail.com /
8392828781
"बायोरेमेडिएशन की भूमिका" (Role of Bioremediation)
आज विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण प्रदूषण की है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, रासायनिक खेती, और जनसंख्या वृद्धि ने जल, मृदा एवं वायु को विषैला बना दिया है। इस संकट से उबरने के लिए बायोरेमेडिएशन एक सशक्त और स्वाभाविक उपाय के रूप में उभर कर सामने आया है। यह ऐसी जैविक प्रक्रिया है, जिसमें जीवाणु, कवक, पौधे या अन्य जैविक घटक प्राकृतिक रूप से प्रदूषकों को निष्क्रिय या नष्ट कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रकृति में अनेक ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, जिनका समाधान केवल आधुनिक तकनीक से ही नहीं, बल्कि प्रकृति-प्रदत्त उपायों से भी संभव है। बायोरेमेडिएशन (Bioremediation) ऐसा ही एक जैविक उपाय है, जो प्रदूषित पर्यावरण को पुनः स्वच्छ और संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह प्रक्रिया सूक्ष्मजीवों, पौधों या उनके एंजाइमों की सहायता से प्रदूषित मिट्टी, जल या वायु से हानिकारक तत्वों को नष्ट करने या उन्हें कम विषैले रूप में बदलने का कार्य करती है।
बायोरेमेडिएशन का शाब्दिक अर्थ और परिभाषा
‘बायोरेमेडिएशन’ दो शब्दों से मिलकर बना है – "बायो" अर्थात "जीव" और "रेमेडिएशन" अर्थात "उपचार"। इसका तात्पर्य हुआ – "जीवों द्वारा उपचार"। वैज्ञानिक रूप में, यह एक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीव या जैविक तत्व पर्यावरणीय प्रदूषकों को हानिरहित पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं।
बायोरेमेडिएशन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
हालांकि यह प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से सदियों से होती आ रही है, परंतु वैज्ञानिक रूप से इसकी पहचान 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई। 1970 के दशक में अमेरिका के अलास्का में तेल रिसाव की घटनाओं के बाद वैज्ञानिकों ने पहली बार व्यवस्थित रूप से बायोरेमेडिएशन का प्रयोग किया। भारत में भी यह प्रक्रिया हाल के दशकों में तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
बायोरेमेडिएशन की कार्यप्रणाली
कुछ सूक्ष्मजीव प्रदूषकों को भोजन के रूप में उपयोग करके उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य कम हानिकारक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। इसके लिए उपयुक्त तापमान, नमी, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
बायोरेमेडिएशन के प्रमुख प्रकार
(i) इन-सीटू (In-situ) इसमें प्रदूषित स्थल को यथावत् रखकर उसी स्थान पर उपचार किया जाता है। उदाहरण: भूजल का जैव उपचार।
(ii) एक्स-सीटू (Ex-situ) इसमें प्रदूषित मृदा या जल को निकालकर प्रयोगशाला या किसी अलग स्थान पर उपचारित किया जाता है। उदाहरण: बायोपाइल, स्लरी फेज बायोरिएक्टर।
(iii) बायोवेंटींग (Bioventing) यह एक इन-सीटू प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन प्रवाहित करके मृदा में उपस्थित जीवाणुओं को सक्रिय किया जाता है।
(iv) बायोस्पार्जिंग (Biosparging) इसमें ऑक्सीजन और पोषक तत्व सीधे भूजल में इंजेक्ट किए जाते हैं।
(v) फाइटोरेमेडिएशन (Phytoremediation) पौधों की सहायता से मिट्टी और जल को स्वच्छ करना।
बायोरेमेडिएशन के घटक
सूक्ष्मजीव (Microorganisms): जैसे Pseudomonas, Bacillus, Rhizobium आदि। पौधे (Plants): जैसे Sunflower, Mustard, Indian Mustard heavy metals को अवशोषित कर सकते हैं। एंजाइम (Enzymes): विशिष्ट रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं।
बायोरेमेडिएशन के अनुप्रयोग
(i) तेल रिसाव की सफाई में समुद्री क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण पारिस्थितिकी पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। Alcanivorax जैसे बैक्टीरिया तेल को विघटित कर सकते हैं।
(ii) औद्योगिक कचरे का निपटान धातुओं, कीटनाशकों, सॉल्वेंट्स आदि को सूक्ष्मजीवों की मदद से निष्क्रिय किया जा सकता है।
(iii) रेडियोधर्मी अपशिष्ट नियंत्रण हालांकि कठिन, परंतु कुछ पौधे और जीव रेडियोधर्मी तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम हैं।
(iv) कृषि क्षेत्र में कीटनाशक अवशेषों को नष्ट करने हेतु उपयोगी।
(v) शहरी कचरा प्रबंधन लैंडफिल क्षेत्रों की जैविक सफाई।
भारत में बायोरेमेडिएशन की स्थिति और प्रयास
(i) सरकारी परियोजनाएँ नमामि गंगे मिशन: गंगा सफाई हेतु बायोरेमेडिएशन तकनीकों का प्रयोग। CPHEEO और CPCB के दिशा-निर्देश: शहरी मलजल शोधन में बायोरेमेडिएशन की सिफारिश।
(ii) प्रमुख संस्थान नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (NEERI) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) IITs और NITs में शोधकार्य
(iii) व्यावसायिक मॉडल बायोफर्टिलाइज़र और बायोकीटनाशकों के रूप में MSMEs द्वारा अपनाया जा रहा है।
प्रमुख केस स्टडी
(i) यमुना शुद्धिकरण (दिल्ली) बायोरेमेडिएशन तकनीक से झीलों और जलधाराओं का उपचार किया गया। (ii) गाज़ीपुर लैंडफिल (दिल्ली) कचरे के पहाड़ को सूक्ष्मजीवों की सहायता से धीरे-धीरे जैविक रूप से विघटित करने का प्रयास। (iii) अलास्का एक्सॉन वाल्डेज़ दुर्घटना इस अंतरराष्ट्रीय उदाहरण ने बायोरेमेडिएशन की क्षमताओं को वैश्विक पहचान दिलाई।
लाभ
कम लागत और ऊर्जा खपत पर्यावरण के अनुकूल स्थायी समाधान स्थानीय संसाधनों पर आधारित रासायनिक विधियों की तुलना में सुरक्षित
सीमाएँ और चुनौतियाँ
जैविक प्रक्रियाएँ धीमी होती हैं कुछ प्रदूषकों पर प्रभाव सीमित आवश्यक पर्यावरणीय शर्तों की उपलब्धता जरूरी जन-जागरूकता और तकनीकी प्रशिक्षण की कमी कुछ सूक्ष्मजीवों का नियंत्रण कठिन
भविष्य की संभावनाएँ
जैव-नवाचार (Bio-innovation): जीन-संशोधित सूक्ष्मजीवों का विकास नैनोटेक्नोलॉजी का समावेश शहरी विकास और स्मार्ट सिटी मिशनों में एकीकरण जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहयोगी तकनीक जैव-आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना
जन-जागरूकता और शिक्षा की भूमिका
विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में समावेश NGO और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण मीडिया के माध्यम से जानकारी का प्रचार-प्रसार
अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बायोरेमेडिएशन
विश्व के विभिन्न देशों में बायोरेमेडिएशन का उपयोग पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए सक्रिय रूप से किया जा रहा है:
संयुक्त राज्य अमेरिका:
अमेरिका की Environmental Protection Agency (EPA) ने कई सुपरफंड साइट्स पर बायोरेमेडिएशन तकनीकों का प्रयोग किया है, जैसे कि न्यू जर्सी और टेक्सास में।
कनाडा:
खनन और तेल क्षेत्र में बायोरेमेडिएशन द्वारा भारी धातुओं और हाइड्रोकार्बनों को हटाने की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।
नीदरलैंड्स और जर्मनी:
शहरी जल निकासी प्रणाली में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग कर जल को स्वच्छ किया जा रहा है।
इससे स्पष्ट है कि यह तकनीक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुकी है।
जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में बायोरेमेडिएशन की भूमिका
बायोरेमेडिएशन सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन से नहीं जुड़ा है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से यह सहायक है: ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करने वाले पौधे: कुछ फाइटोरेमेडिएशन पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में भी सहायक होते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता बहाल करके कार्बन सिंक बनाना: स्वस्थ मिट्टी अधिक कार्बन अवशोषित कर सकती है। ऊर्जा की खपत में कमी: रासायनिक उपचार की अपेक्षा यह तकनीक कम ऊर्जा का उपयोग करती है, जिससे CO₂ उत्सर्जन घटता है।
बायोरेमेडिएशन और सतत विकास लक्ष्य (SDGs)
संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) में बायोरेमेडिएशन का योगदान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है:
SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता): दूषित जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने में सहायता। SDG 13 (जलवायु कार्रवाई): जलवायु के अनुकूल तकनीक का उपयोग। SDG 15 (स्थलीय जीवन): भूमि की गुणवत्ता सुधारकर जैव विविधता की रक्षा। SDG 12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन): जैविक कचरे का सुरक्षित प्रबंधन।
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
(i) रोजगार सृजन: MSME सेक्टर में जैव उर्वरकों, बायो कीटनाशकों और अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। (ii) ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग: ग्राम पंचायतों द्वारा बायोरेमेडिएशन आधारित शौचालय शुद्धिकरण और जल पुनः उपयोग योजनाएँ अपनाई जा रही हैं। (iii) महिला सशक्तिकरण: स्व-सहायता समूहों द्वारा जैव-प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार को बढ़ावा मिला है।
नीति-निर्माण में बायोरेमेडिएशन की आवश्यकता
भारत में अब तक बायोरेमेडिएशन के लिए कोई स्पष्ट और विस्तृत नीति नहीं है, जबकि यह आवश्यकता बन चुकी है। कुछ सुझाव: राष्ट्रीय बायोरेमेडिएशन मिशन की स्थापना MSME नीति में विशेष प्रोत्साहन शहरी नियोजन में इसका समावेश (Urban Planning) प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा अनिवार्य गाइडलाइंस
अनुसंधान की दिशा में भारत का योगदान
भारत में निम्न संस्थान बायोरेमेडिएशन पर शोध कार्य कर रहे हैं:
NEERI (नागपुर) औद्योगिक अपशिष्ट उपचार
TERI (नई दिल्ली) ऊर्जा और पर्यावरणीय समाधान
IIT कानपुर बायो-सेंसर्स और स्मार्ट तकनीक
IISc बेंगलुरु नैनो-बायो टेक्नोलॉजी
तकनीकी नवाचार और भविष्य
बायोरेमेडिएशन के क्षेत्र में निम्नलिखित नवाचार भविष्य को बदल सकते हैं:
जीन-संपादित सूक्ष्मजीव: CRISPR तकनीक द्वारा अत्यधिक प्रभावी जीवों का विकास। नैनो-बायो संवर्धन: नैनोपार्टिकल्स के साथ सूक्ष्मजीवों को सक्रिय करना। AI आधारित निगरानी: प्रदूषक स्तरों की पहचान और स्वचालित उपचार प्रणाली।
आलोचनात्मक दृष्टिकोण
जहाँ बायोरेमेडिएशन में कई लाभ हैं, वहीं आलोचक इसकी निम्न बातों की ओर इशारा करते हैं: अनिश्चितता: प्रदूषकों का पूर्ण विघटन सुनिश्चित नहीं होता। जैव विविधता पर प्रभाव: कभी-कभी बाहरी सूक्ष्मजीव स्थानीय जैव विविधता को प्रभावित कर सकते हैं। लंबा समय: उपचार में महीनों से वर्षों तक का समय लग सकता है।
साहित्य और फिल्म में बायोरेमेडिएशन
हाल के वर्षों में बायोरेमेडिएशन विषय पर कुछ वृत्तचित्र और पुस्तकें भी सामने आई हैं: "Erin Brockovich" (हॉलीवुड फिल्म): प्रदूषित जल पर आधारित कहानी जिसमें जैविक उपचार की मांग उठती है। "Silent Spring" (Rachel Carson): कीटनाशकों के दुष्प्रभाव और प्रकृति में संतुलन पर आधारित।
सामुदायिक भागीदारी और जनसहभागिता
बायोरेमेडिएशन की सफलता में स्थानीय समुदायों की भूमिका महत्वपूर्ण है: ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय जलाशयों की सफाई में भागीदारी। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जैविक खाद तैयार करने में सहयोग। विद्यालयों में बच्चों को बायोरेमेडिएशन आधारित परियोजनाओं से जोड़ना। उदाहरण: केरल में कुछ पंचायतों ने स्थानीय स्कूलों के सहयोग से ‘बायो गार्डेन’ प्रोजेक्ट चलाया जिसमें घरेलू जैव अपशिष्ट से खाद बनाई जाती है और उससे मिट्टी को पुनर्जीवित किया जाता है।
बायोरेमेडिएशन और भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली
भारत में पारंपरिक रूप से कुछ बायोरेमेडिएशन-समरूप प्रथाएं प्रचलित रही हैं: गोबर और गौमूत्र का उपयोग: जल और मृदा शुद्धिकरण में पारंपरिक रूप से प्रयुक्त। नीम, तुलसी और सहजन के पौधों का उपयोग: प्रदूषण नियंत्रण और कीट प्रतिरोधक गुणों के लिए। जल संरक्षण की तकनीकें: जैसे कि बावड़ी, तालाब, जिन्हें जैविक रूप से स्वच्छ रखने की परंपरा रही है। यह स्पष्ट करता है कि आधुनिक बायोरेमेडिएशन तकनीकों की जड़ें हमारी परंपराओं में भी मौजूद रही हैं।
शहरों के लिए एक मॉडल — बायोरेमेडिएशन सिटी प्लान
अगर भारत के बड़े नगरों को पर्यावरणीय संतुलन की ओर ले जाना है, तो ‘बायोरेमेडिएशन-सिटी’ मॉडल अपनाना होगा: हर वार्ड में बायो-स्लरी उपचार केंद्र। शहरी झीलों का बायोरेमेडिएशन द्वारा पुनर्जीवन। निर्माण स्थलों पर जैव अपशिष्ट शोधन की अनिवार्यता। शहरों के लिए "ग्रीन कोड" जिसमें बायोरेमेडिएशन को अनिवार्य किया जाए।
बायोरेमेडिएशन और अंतरविषयी अध्ययन (Interdisciplinary Approach)
इस तकनीक का अध्ययन और प्रयोग विभिन्न विषयों से जुड़कर और प्रभावी बनता है: जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology) रसायन विज्ञान (Chemistry) पर्यावरण इंजीनियरिंग (Environmental Engineering) सामाजिक विज्ञान (Social Sciences) — नीतिगत पक्ष नागरिक प्रशासन (Public Policy) — नीति निर्माण और क्रियान्वयन
विशेष सुझाव: भारत के लिए बायोरेमेडिएशन नीति का खाका
(i) अल्पकालिक सुझाव: सभी नगर पालिकाओं को कम-से-कम एक बायोरेमेडिएशन प्रयोगशाला देना। प्रदूषित नदियों की प्राथमिक सूची बनाकर उपचार योजना तैयार करना। (ii) दीर्घकालिक सुझाव: राष्ट्रीय बायोरेमेडिएशन नीति बनाना। UGC और AICTE द्वारा तकनीकी शिक्षा में बायोरेमेडिएशन पाठ्यक्रम अनिवार्य करना। CSR के तहत कंपनियों द्वारा प्रदूषण वाले क्षेत्रों में बायोरेमेडिएशन अपनाना।
जनसंख्या दबाव और शहरी प्रदूषण में बायोरेमेडिएशन की आवश्यकता
भारत जैसे देश, जहाँ शहरीकरण और जनसंख्या विस्फोट तेजी से बढ़ रहे हैं, वहाँ अपशिष्ट और प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्न उपायों में बायोरेमेडिएशन अनिवार्य है: शौचालयों से निकलने वाले जैव अपशिष्ट का उपचार। झुग्गी बस्तियों में उत्पन्न कचरे का जैविक प्रबंधन। शहरी नालों को बायोरेमेडिएशन आधारित साफ करने की प्रक्रिया।
बायोरेमेडिएशन और 'पर्यावरणीय न्याय' (Environmental Justice)
बायोरेमेडिएशन का उपयोग केवल एक तकनीकी समाधान नहीं है, बल्कि यह पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करने का भी माध्यम बन सकता है: वंचित वर्गों को disproportionate रूप से प्रदूषण झेलना पड़ता है, जैसे कि झुग्गियों, आदिवासी क्षेत्रों या औद्योगिक बेल्टों में रहने वाले लोग। इन क्षेत्रों में बायोरेमेडिएशन आधारित स्वच्छता और जल पुनःशोधन परियोजनाएँ लागू कर समानता और अधिकारों की पुनःस्थापना की जा सकती है। यह तकनीक स्थानीय स्तर पर स्वशासन और पर्यावरणीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।
जल, जंगल, जमीन – त्रिस्तरीय पारिस्थितिकी में बायोरेमेडिएशन की भूमिका
जल: नदियों, झीलों और नालों की बायो-फिल्टरेशन द्वारा सफाई। औद्योगिक अपशिष्ट वाले जल में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग।
जंगल: वनों में फैले प्लास्टिक और कीटनाशकों के अवशेषों को जैविक तकनीकों से विघटित करना। आग से नष्ट हुए क्षेत्रों में मिट्टी पुनर्जीवन के लिए पौधारोपण आधारित बायोरेमेडिएशन।
जमीन: प्रदूषित भूभाग (contaminated lands) जैसे कि डंपिंग ग्राउंड्स को पुनः कृषि योग्य बनाना। भारी धातुओं से दूषित मिट्टी का जैविक उपचार।
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और बायोरेमेडिएशन
भारत की कंपनियाँ CSR अधिनियम 2013 के अंतर्गत बायोरेमेडिएशन को अपनाकर कई सकारात्मक पहल कर सकती हैं: फैक्ट्री साइट्स के आसपास के क्षेत्रों में जैव उपचार प्रणाली। स्थानीय समुदायों के लिए बायो-कचरा प्रबंधन प्रशिक्षण। शहरी झीलों या सार्वजनिक स्थलों की सफाई में भागीदारी। उदाहरण: कुछ आईटी कंपनियाँ अपने परिसर में बायोरेमेडिएशन आधारित वेस्टवॉटर रीसायकलिंग प्लांट्स चला रही हैं।
शिक्षा और जन-जागरूकता में बायोरेमेडिएशन का समावेश
विद्यालय स्तर पर: विज्ञान प्रदर्शनी और कार्यशालाओं में बायोरेमेडिएशन मॉडल को स्थान देना। स्कूली पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय समाधान के रूप में इसकी व्याख्या।
उच्च शिक्षा में: बायोटेक्नोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान और सिविल इंजीनियरिंग में विशेष पाठ्यक्रम। प्रयोगात्मक शिक्षण हेतु विश्वविद्यालयों में बायोरेमेडिएशन लैब की स्थापना।
सामुदायिक स्तर पर: लोक भाषाओं में जागरूकता अभियान। रेडियो/टीवी/OTT जैसे माध्यमों द्वारा बायोरेमेडिएशन पर आधारित कार्यक्रम।
भविष्य की चुनौतियाँ और समाधान
सूक्ष्मजीवों की कार्यक्षमता में अस्थिरता , स्थान विशेष के अनुसार अनुकूलित जीवों का चयन
जलवायु परिवर्तन के कारण जैव प्रक्रियाओं पर असर , ताप-सहिष्णु जीवों का विकास
सामाजिक जागरूकता की कमी , स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण और सफलता कथाएँ
नीति का अभाव , स्पष्ट और पृथक बायोरेमेडिएशन नीति की आवश्यकता
बायोरेमेडिएशन और ‘ग्राम पंचायतों’ की भूमिका
भारत के लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में इस तकनीक को अपनाने से व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है: स्वच्छ भारत मिशन के साथ समन्वय करके गांवों के सीवेज और कचरे का जैव उपचार। गौशालाओं, कम्पोस्ट यार्ड और नालियों की सफाई में इसका उपयोग। जल संचयन योजनाओं में बायोफिल्टर प्लांट की स्थापना। यह "गांव से शहर की ओर" सतत विकास की आधारशिला बन सकता है।
वैश्विक जलवायु नीतियों में भारत का योगदान
भारत यदि बायोरेमेडिएशन को व्यापक स्तर पर अपनाता है, तो यह COP सम्मेलन, पेरिस जलवायु संधि, और SDGs में उसका योगदान और भी स्पष्ट रूप से उभर सकता है। यह कदम भारत को "विकासशील देश" से "पर्यावरणीय अगुआ" देश में बदल सकता है।
Conclusion
बायोरेमेडिएशन न केवल पर्यावरणीय संकटों का समाधान है, बल्कि यह प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करने का मार्ग भी है। यह एक स्वाभाविक, सतत और जनोन्मुखी तकनीक है, जिसे वैज्ञानिक नीति, जनसहभागिता और नवाचार के साथ आगे बढ़ाया जाए तो यह भारत जैसे देश की पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान बन सकती है।
बायोरेमेडिएशन का आशय केवल प्रदूषण हटाना नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के साथ एक ऐसा सहजीवी संबंध स्थापित करना है जिसमें हम उपभोक्ता नहीं, संरक्षक बनते हैं। यह तकनीक एक पर्यावरणीय आंदोलन का आधार बन सकती है — यदि इसमें नीति, विज्ञान, समाज और नैतिकता सभी एक साथ जुड़ें। "जब तक विज्ञान संवेदना से नहीं जुड़ता, तब तक वह केवल प्रयोगशाला की खोज बना रहता है। बायोरेमेडिएशन — विज्ञान और संवेदना का ऐसा ही संगम है।"
Thanks For Read
jp Singh
searchkre.com@gmail.com
8392828781
 Gst Registration
Gst Registration
 DSC Registration
DSC Registration
 Pancard Registration
Pancard Registration
 Company Registration
Company Registration
 Fssai Registration
Fssai Registration
 TradeMark Registration
TradeMark Registration
 MSME Registration
MSME Registration
 Passport Registration
Passport Registration
 Income Tax Return
Income Tax Return
 LLP Company Registration
LLP Company Registration
 Marriage And Court Marriage Registration
Marriage And Court Marriage Registration
 PVT LTD Company Registration
PVT LTD Company Registration
 GST Filing Services
GST Filing Services
 Coaching Insititute Registration
Coaching Insititute Registration
 GYM Registration
GYM Registration
 NGO Registration
NGO Registration
 Political Party Registration
Political Party Registration
 Society Registration
Society Registration
 Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
Advertise ( Digial Marketing Services Booking )
 Make Website on EMI
Make Website on EMI


























































































 9th Class Scholarship Competition Test
9th Class Scholarship Competition Test
 10th Class Scholarship Competition Test
10th Class Scholarship Competition Test
 11th Class Scholarship Competition Test
11th Class Scholarship Competition Test
 12th Class Scholarship Competition Test
12th Class Scholarship Competition Test
 Graduation Scholarship Competition Test
Graduation Scholarship Competition Test
 Post Graduation Scholarship Competition Test
Post Graduation Scholarship Competition Test
 Diploma Scholarship Competition Test
Diploma Scholarship Competition Test
 Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Banking Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UPSC Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 JEE Coaching Scholarship Competition Test
JEE Coaching Scholarship Competition Test
 NEET Coaching Scholarship Competition Test
NEET Coaching Scholarship Competition Test
 Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Army Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Railway Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
UP Police Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
PCSJ Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
APO Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
NDA Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
 Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test
Lower PCS Recruitment Coaching Scholarship Competition Test